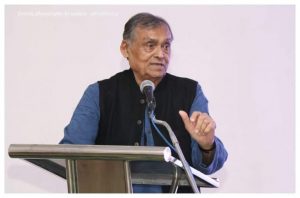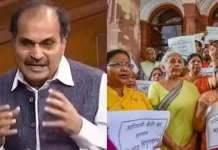— कनक तिवारी —
(कल प्रकाशित लेख का बाकी हिस्सा)
इसके बरक्स मुख्यतः के.एम. मुंशी, अलादि कृष्णास्वामी अय्यर और डाॅ आम्बेडकर ने समझाने की कोशिश की कि समान नागरिक संहिता एक नवोदित, स्वतंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष देश के लिए पूरी तौर पर जरूरी है। अंगरेजों के शासनकाल में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के कई निजी कानूनों में हस्तक्षेप कर सामाजिक व्यवहार के लिए समान सिविल कोड बना ही दिये गए हैं। कई मुस्लिम देशों में भी समान सिविल कोड है। ऐसे देशों में भी है जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। समान संहिता बनने से सबसे अधिक फायदा मुस्लिम महिलाओं को होगा। उन्हें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के प्रचलित कानूनों के कारण हिन्दू तथा ईसाई महिलाओं आदि के बराबर अधिकार भी हासिल नहीं हैं।
आज भी संविधान सभा की मंशा को न्यायिक तौर पर समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकतर सरकार के विधिमंत्री तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डाॅ. अंबेडकर की समझाइश पर निर्भर होता है।
आंबेडकर ने चुटीली भाषा में कहा था कि निजी कानूनों के इलाके में ही समान कोड पर अब तक हमला नहीं किया गया है। उन्होंने ‘हमला‘ शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल किया था। आंबेडकर ने ऐतिहासिक आश्वासन दिया कि समान सिविल कोड बनेगा। तब भी उसे सब लोगों पर जबरिया नहीं लादा जाएगा। उन्होंने भविष्य की संसद से उम्मीद की थी कि वह ऐसे समुदायों के लिए ही समान सिविल कोड बनाएगी जो घोषणा करें कि वह उन पर लागू किया जाए।
जाहिर है, मोदी सरकार आंबेडकर की इस समझाइश को पूरा करने में असमर्थता महसूस करेगी। आंबेडकर के इस सुझाव को अमल में लाने में एक व्यावहारिक दिक्कत भी है। यदि एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा विवाह के पहले या बाद में समान सिविल कोड को मानने या नहीं मानने के संबंध में अलग अलग राय व्यक्त करे, तब क्या होगा?
कई प्रमुख टिप्पणीकारों ने संवैधानिक भाषा की बारीकियों में जाकर इसके असली मकसद को समझने का दावा किया है।
अनुच्छेद नहीं कहता कि राज्य समान नागरिक संहिता बनाएगा। कहता है कि उसे हासिल करने का प्रयास करेगा।
सिविल कोड के विरोधियों को समझाइश देना, विमर्श करना, अनिच्छुक समुदायों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच सहमति का माहौल तैयार करना, संविधान में वर्णित राष्ट्रीय आदर्शों को क्षति पहुंचाये बिना अनुकूलता का वातावरण तैयार करना आदि भी इस लचीली परिभाषा के तहत हैं।
हिन्दुत्व के समर्थकों में लेकिन इन्सानी सम्भावनाओं को दरकिनार कर उत्साह, आग्रह और उन्माद सब कुछ है।
संविधान की समझ का सयानापन ही लोकतंत्र का प्राणतत्त्व होता है।
अगस्त 1972 में ‘मदरलैंड‘ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने कहा था कि, ‘ऐसा नहीं है कि उन्हें समान सिविल कोड के प्रति कोई आपत्ति है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई बात इसीलिए मंजूर नहीं हो सकती कि उसका उल्लेख संविधान में किया गया है।’
रामराज्य परिषद के संस्थापक करपात्री जी ने भी नेहरू के नेतृत्व वाले हिन्दू कोड बिल की मुखालफत करते हुए कहा था कि ‘किसी समुदाय की विवाह आदि प्रथाओं में कानूनी हस्तक्षेप मुनासिब नहीं है। जो हिन्दू धर्मशास्त्रों के लिए तथा मुसलमान कुरान शरीफ के लिए वफादार नहीं हैं, संविधान के प्रति भी वफादार नहीं हो सकते।’
संविधान सभा में यह तो हुआ है कि पहले आम्बेडकर ने मुस्लिम सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें नागरिक संहिता के सवाल को लेकर संदेह और अविश्वास में डूबना नहीं चाहिए। अंगरेजों के जमाने में भी कई नागरिक अधिकारों को, हिन्दू मुसलमान या अन्य धर्म की परवाह किए बिना, सभी के लिए समतल कर दिया गया है। इसके भी अलावा भारत के कुछ इलाकों में, मसलन पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश और मलाबार वगैरह में कई हिन्दू विधियां मुसलमानों पर स्वेच्छा से लागू रही हैं। इसलिए इस मामले में लचीला रुख अपनाने की जरूरत होगी। विस्तार से अपनी समाज-दार्शनिक उपपत्ति गढ़ते आम्बेडकर ने आखिर में एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही थी। उसका आज के घटनाक्रम में निर्णायक महत्त्व होना चाहिए।
आम्बेडकर ने कहा, मैं मुसलमान सदस्यों को आश्वासन देता हूॅं। उन्होंने ‘आश्वासन‘ शब्द का इस्तेमाल किया था। आम्बेडकर ने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह भी सभी नागरिकों पर, क्योंकि वे नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि भविष्य की संसद शुरू में नागरिक संहिता के लिए ऐसा प्रावधान बनाए कि उसका लागू किया जाना पूरी तौर पर स्वैच्छिक होगा। इसके लिए संसद मुनासिब चिंतन कर सकती है।
यह कोई अभिनव प्रयोग नहीं होगा। 1937 में शरिया अधिनियम को लागू करने के वक्त भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी कि जो मुसलमान चाहें उनके लिए ही शरिया कानून लागू किया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी संसद यही कर सकती है ताकि मुस्लिम सांसदों के उस संदेह को दूर किया जा सके कि नागरिक संहिता का कानून उन पर जबरिया लादा जाएगा।
मुस्लिम सदस्यों ने कई संशोधन इसी आशय के पेश किए थे कि उनके समुदाय की मर्जी के बिना नागरिक संहिता लागू नहीं की जाए। यह इतिहास का सच है कि अपने द्वारा दिए गए आश्वासनों के कारण डा. आम्बेडकर के हस्तक्षेप से ही मुस्लिम सदस्यों के संशोधन अस्वीकार कर दिए गए और नागरिक संहिता का मौजूदा ड्राफ्ट अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक कानून बन गया।
’समान नागरिक संहिता’ लागू करने का अनुच्छेद 44 हैरत में है कि यह आधा-अधूरा उल्लेख राज्यसत्ता के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गया है।
संविधान जिन कई वायदों को साधारण बहुमत द्वारा लागू करने के निर्देश देता है उन्हें तक पूरा करने की सरकार की नीयत नहीं है। शायद उसे फुर्सत भी नहीं है। जो वायदा पेट से नहीं, जेहन और परम्परा से उत्पन्न होकर उल्लेखित है, उसे लागू करने के लिए धरती आसमान एक किए जा रहे हैं।
दो तिहाई बहुमत के बावजूद ’समान नागरिक संहिता’ के मसले को आधा प्रकट, आधा गुप्त एजेंडा पर रखने के बाद अब प्रकट किया जा रहा है।
प्रावधान को संविधान निर्माताओं का महत्त्वपूर्ण स्वप्न प्रचारित किया जा रहा है। देश को जानना जरूरी है कि संविधान की अल्पसंख्यक सलाहकार उपसमिति ने भी यह सिफारिश की थी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा अल्पसंख्यकों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। उपसमिति में अन्य लोगों के अलावा डाॅ. आम्बेडकर और श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी थे।
आम्बेडकर के अनुयायी तो अपने पूर्वज के वचनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं लेकिन डाॅ श्यामाप्रसाद मुखर्जी की अपने उत्तराधिकारियों के आचरण के कारण बुरी हालत है।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में मुद्दा न्यायाधीशों की अनाहूत टिप्पणियों के कारण जनचर्चा में तीक्ष्ण हुआ।
शाहबानो के प्रसिद्ध मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पति के विरुद्ध पत्नी को भरणपोषण आदि का अधिकार वैध तथा लागू करार दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने अफसोस किया कि यह अनुच्छेद 44 तो मृत प्रावधान हो गया है।
सरकार ने उस सिलसिले में अब तक कुछ नहीं किया। यह अहसास लेकिन कराया ही नहीं गया कि इस संबंध में मुस्लिम समुदाय को पहल करनी है।
वैसे दायित्व तो सरकार और संसद का है। बाद में सरला मुदगल के दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा मुखर होकर समान सिविल कोड के विधायन की जरूरत महसूस की। जस्टिस कुलदीप सिंह ने यहां तक कह दिया कि सिक्ख, बौद्ध, जैन और हिन्दुओं ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने पारंपरिक कानूनों में बदलाव मंजूर कर लिया है, जबकि कुछ समुदायों में अब भी गहरा एतराज है।
कई हाईकोर्ट्स ने भी गहराई में उतरे बिना संहिता समर्थक सिफारिशें तो की हैं।
कुछ पश्चिमी विचारकों ने सुप्रीम कोर्ट के मजहब आधारित वर्गीकरण की कड़ी आलोचना भी की है। न्यायमूर्ति सहाय ने भी सुप्रीम कोर्ट के इसी पीठ में बैठकर समान सिविल कोड की पैरवी की।
सांस्कृतिक समाज की रचना में धर्म के आग्रहों को दरकिनार कर राजनीतिक नस्ल के विधायन के संभावित परिणाम केवल सुप्रीम कोर्ट की सलाह के सहारे बूझे नहीं जा सकते।
बहुलधार्मिक और बहुलवादी संस्कृति का, विश्व में भारत एक विरल उदाहरण है। हालांकि कई प्रगतिशील मुस्लिम विचारकों ने भी पारिवारिक कानूनों के बदलाव की बात की है।
इस सवाल की तह में सांप छछूंदर वाला मुहावरा बहुत आसानी से दाखिल दफ्तर होने वाला नहीं है। वक्त आ गया है जब बाबा साहब के आश्वासनों को ताजा सन्दर्भ में वस्तुपरक ढंग से परीक्षित किया जाए।
किसी भी पक्ष या समाज को संविधान की निष्पक्ष व्याख्याओं की हेठी नहीं करनी चाहिए।
सभी को याद रखना चाहिए कि देश हर धर्म से बड़ा है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.