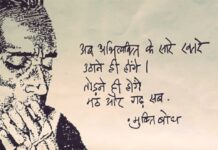— ध्रुव शुक्ल —
कहते हैं कि चन्द्रमा पृथ्वी का मन है। जब पूर्णिमा का चांद समुद्रों के जल को आंदोलित करके उनकी उंची उठती लहरों पर डोलता है तो लगता है कि जैसे पृथ्वी का मन डोल रहा है। फिर डोलता हुआ सागर शान्त हो जाता है। बिलकुल इसी तरह हमारी देह में बसा सागर भी पछाड़ें मारता है। अपने ही तट को तोड़ता है और उसे भी शान्त होना पड़ता है। बाढ़ आयी नदी भी शान्त हो जाती है। आंधियां थक कर शान्त होती देखी जाbbyeती हैं। अशांति जीवन का स्थायी भाव नहीं है।
कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी की आत्मा है। जीवन पर उजली-शान्त धूप छाई हुई है। कई तरह की हवाओं में उड़ती धूल इस उजली धूप को मैला भी करती है। आंखों में फैले उज्ज्वल आकाश को धुन्ध से भरती है। जीवन में बसी आग को कामनाओं की बयारें उकसाती ही रहती हैं। पर आग में भड़क कर शान्त हो जाने का गुण भी तो है।
कहते हैं कि आग, पानी और हवा कुसंगति में फंस जायें तो वह वर्षा चक्र बाधित होता है जो बादल बनकर सबके लिए वरदान बन जाता है। वही सबका पालनहार है। राज-काज बदलते रहते हैं पर सृष्टि अपना नियम नहीं बदलती। इस नियम के विपरीत जीवन को ढालना संभव नहीं। पर लगता तो यही है कि इस नियम से बेपरवाह होकर समाज और राज्य व्यवस्था खूब मनमानी कर रहे हैं। अब तो इस मनमानी में वैश्विक साझेदारी का बाज़ार भी गर्म है।
कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप के संतुलन से ही सबका जीवन चलता है पर हमारे शरीर, देवत्व और प्रकृति के बीच तापमान का संतुलन बिगड़ता ही चला जा रहा है और इसके लिए सब जिम्मेदार ठहरते हैं। वे भी जो दूसरों पर दोष लगाकर अपना बचाव किया करते हैं। दूसरों को दोषी ठहराकर अपने-अपने पाप छिपाने की प्रवृत्ति ने ही धरती को एक बड़े घूरे में बदल दिया है। जल और औषधियां देने वाले पर्वत दरककर धंस रहे हैं। हम जीने के लिए दूसरी पृथ्वी कहां से लायेंगे?
क्या वे लोग अपने बारे में अब भी नहीं सोचेंगे जिनका इस्तेमाल कुटिल राजनीतिक ताक़तों ने धरती पर आतंक के बीज बोने के लिए किया है और वे धरती पर कचरे की तरह लाशें बिखराते रहे हैं, आज भी बिखरा रहे हैं। आखिर इस हिंसा से उन्हें अब तक क्या मिला — बेबसी, भूख और कचरे की तरह धरती पर बिखरा पड़ा उन लोगों का घरबार जो जीना चाहते हैं।
पृथ्वी पर नदी, पेड़, पहाड़ और मनुष्य सहित सभी प्राणियों का जीवन परस्पर आश्रित है। इसे सॅंभाले रखने के लिए बड़ी इन्सानी बिरादरी चाहिए जो आपस में मिलकर सच्ची खुदाई ख़िदमतगार होने की जिम्मेदारी निभा सके। पृथ्वी पर वृक्षों की उखड़ती जड़ों को उन हाथों का इंतज़ार है जो उन पर थोड़ी-सी मिट्टी डाल सकें। फटे हुए मन के आकाश को रफ़ूगरों की तलाश है।
बहनें-बेटियॉं
वे अभी भी विष-अमृत के खेल से उबर नहीं पायी हैं….
वे साहुन के महीने में आमों की डाली पर झूला झूल रही हैं। आंगन में लंगड़ी थप्प खेल रही हैं। किसी घने बरगद की छाया में गुड्डे-गुड़ियों का ब्याह रचा रही हैं। वे पराये घर की अमानत की तरह किसी और घर में सयानी हो रही हैं।
वे आंगन में उतरी चिड़ियों-सी चहचहाती हैं और घर की देहरी पार कर किसी अजनबी देश जाने की तैयारी करती-सी लगती हैं–लै बाबुल घर आपनों, मैं चली पिया के देस।
वे यात्राओं के बीच अपने बच्चों के साथ किसी बस स्टैण्ड या स्टेशन पर मिल जाती हैं और हमसे कुछ कहना चाहती हैं पर जल्दी ही उनकी बस आ जाती है, उन्हें कोई तेज भागती रेल खींच ले जाती है। उनका खिड़की से हिलता अकेला हाथ भर दीखता है जैसे कह रही हों कि हमें कुछ नहीं कहना।
वे जन्म लेते ही दो घरों से बॅंध जाती हैं। जब हम उनकी देहरी से लौटते हैं तो वे हमें दूर तक अकेली निहारती रहती हैं और आंसू पोंछकर अपने हिस्से के दुख को बह जाने से रोक लेती हैं।
ऐसे ही उनका जीवन बीतता रहा है। वे बूढ़ी हो रही हैं पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ रहीं। हर बार किसी वंश वृक्ष पर पत्ती की तरह मुरझाती हैं और फिर पीक उठती हैं — बहनें-बेटियां सदियों से घर-संसार को बचा रही हैं —
रुनुक-झुनुक बेटी अंगना में डोलें
बाबुल लये हैं उठाय भलेंजू।
कै मोरी बेटी तुम सांचे की ढारीं
कै गढ़ी चतुर सुनार भलेंजू।
नें बाबुल हम सांचे की ढारीं
नें गढ़ी चतुर सुनार भलेंजू।
माता की कुखिया सें जनम लये हैं
रूप दये हैं करतार भलेंजू।
बाबुल कहें सबकी बिटियां जीवें
बेटी रहें तो संसार भलेंजू।
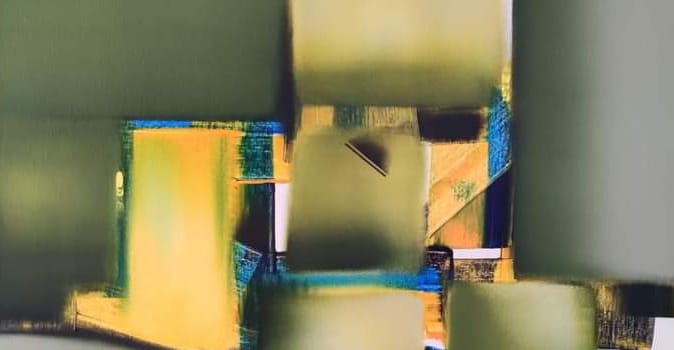
सत्ता हथयाने की मची हाय-हाय
कोई इस दल से उस दल में जाय
कोई उस दल से इस दल में आय
कोई गिनती में आय
कोई गिनती से जाय
यही राजनीति कहाय
सत्ता हथयाने की मची हाय-हाय
कोई तन को दहकाय
कोई मन को भरमाय
कोई जन को बहकाय
भकर-भकर लोकतंत्र खाय
जो सबके सहारे का अंतिम उपाय
सत्ता हथयाने की मची हाय-हाय
जो सुनें नहीं पंचों की राय
वही नेता कहाय
अपनी धूम मचाय
रोज सबको धमकाय
अब कौन करे न्याय
सत्ता हथयाने की मची हाय-हाय
जनता क्या पाय?—
फटे हुए दूध की ठण्डी-सी चाय
सत्ता हथयाने की मची हाय-हाय
लोकतंत्र के डूब क्षेत्र में
बॉंधी जा रही है लोकतंत्र की नदी
बन रहा कोई बहुत ऊंचा बॉंध
रोज़ उठती जा रही दीवार
बस्तियों में बढ़ रहा पानी
डूब रहा घरबार
डूब रहे हैं पूर्वजों के बनाये
लोकतंत्र के घाट
धॅंसती जा रही हैं सीढ़ियाँ
रुॅंधती जा रही नदी के कीचड़ में
फॅंस गयी है लोकतंत्र की नाव
बढ़ता जा रहा डूब क्षेत्र
भाग रहे हैं लोग
नहीं मिल रहा आश्रय
लोकतंत्र की नदी के किनारे
लोकतंत्र के डूब क्षेत्र से दूर
बसायी जा रही हैं चुप्पियों में डूबीं
ऊबे हुए सुखी लोगों की बस्तियां
रचा जा रहा है नया राजभवन
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.