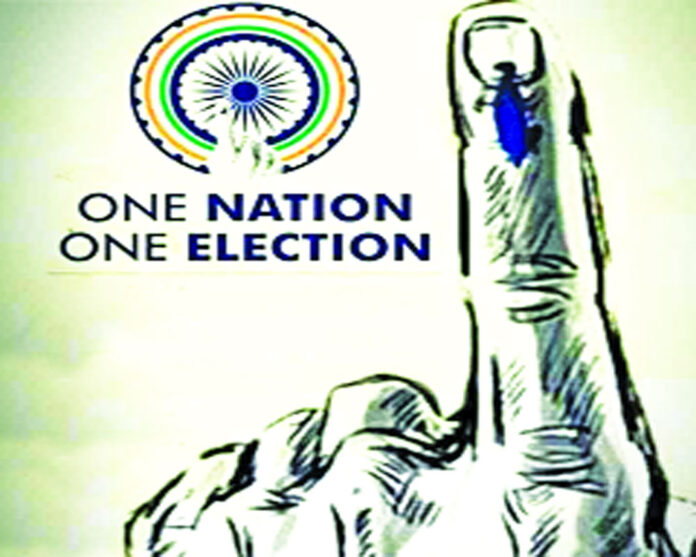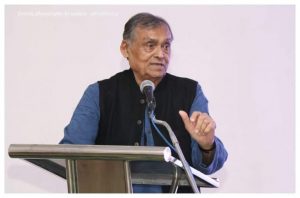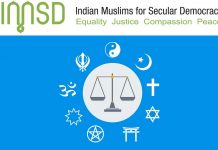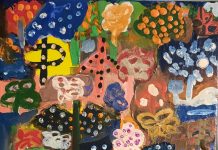— कनक तिवारी —
सनसनी फैली हुई है कि 18 सितम्बर (2023) से लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एजेंडा जाहिर या प्रसारित नहीं है। अलबत्ता नेपथ्य में फुसफुसाहटें हैं। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ सरकार का इरादा है। विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एकसाथ करा दिए जाएं। ऐसा अजूबा आजादी के पंद्रह वर्ष के बाद से विधायिकाओं की घट बढ़ उम्र के चलते कभी नहीं हुआ। आंबेडकर के संविधान सभा में कथन के कारण भी हो नहीं सकता था।
संवैधानिक कहानी 15 जून 1949 से शुरू हुई है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा.बी. आर. आंबेडकर ने चुनाव आयोग की स्थापना तथा अधिकारिता सम्बन्धी अनुच्छेद 324 (प्रारूप में अनुच्छेद 289) को बहस के लिए पेश किया था। आंबेडकर ने खुलासा किया कि चुनाव आयोग के जरिए संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान अब होगा। हमने चुनावी मशीनरी कायम करते चुनाव मैनेजमेंट का प्रावधान किया है। उन्होंने बहुत खुलकर कहा, इसमें शक नहीं कि आमतौर पर चुनाव हर पांच वर्ष बाद ही होंगे। प्रश्न फिर भी रहेगा कि उपचुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। पांच वर्ष के पहले विधानसभा भंग भी हो सकती है। स्थायी मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी मशीनरी के जरिए चुनाव कराना बड़ा बदलाव है। हमने राज्यों (प्रदेशों) को अधिकार नहीं दिया है क्योंकि वहां से गुटबाजी की शिकायतें आ रही हैं। केन्द्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
सजग सदस्य शिब्बनलाल सक्सेना ने प्रारूप के बुनियादी सोच पर हमला करते कहा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करें? केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और उसके मुखड़े प्रधानमंत्री की हर सिफारिश मानना राष्ट्रपति के लिए लाजिमी होगा। प्रधानमंत्री के हुक्म जनता पर चुनाव आयोग के जरिए लादकर चुनाव प्रबंधन उसके हाथ दे देना कहां तक लोकतांत्रिक है? सक्सेना ने नायाब प्रस्ताव किया, वही व्यक्ति प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जिसके पक्ष में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का दो तिहाई बहुमत जरूर हो। लचीला लेकिन विचारोत्तेजक सुझाव आंबेडकर ने नहीं माना। सक्सेना ने कहा, आजाद खयालों और निष्पक्ष आचरण के प्रधानमंत्री नेहरू चाहें तो अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, हालांकि वह कतई नहीं करेंगे। लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं कि आगे प्रधानमंत्री नैतिक और प्रशासनिक पैमाने पर नेहरू की कदकाठी के होंगे। प्रधानमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में समर्थन के लिए थोड़ा सा विरोध होने पर भी संसार के जनमत के सामने उनका सिर झुक जाएगा। सक्सेना ने भी जोर देकर कहा, ‘‘शायद किसी न किसी प्रान्त में हमेशा चुनाव होते ही रहेंगे। देशी रियासतों के शामिल होने पर लगभग तीस प्रान्त हो जाएंगे। मुमकिन है, केन्द्र तथा अलग अलग प्रान्तों के विधानमंडलों के चुनाव एक ही समय पर नहीं हों। दस-बारह वर्ष के पश्चात हर समय किसी न किसी प्रान्त में चुनाव होता रहेगा।”
असम के कुलाधर चालिहा ने ताबड़़तोड़ भाषण में प्रस्तावित प्रावधानों की छीछालेदर करते हुए कहा, राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने से उनके पक्षपाती रहने की इंसानी गुंजाइश है। हृदयनाथ कुंजरू ने अलबत्ता महत्त्वपूर्ण कहा, दुनिया में किसी संविधान को नहीं जानता जहां फेडरल देश में चुनाव की सभी खटपट और जिम्मेदारियां चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ी जाएं। अजूबा केवल भारतीय फेडरल लोकतंत्र में किया जा रहा है।
सदस्यों की आशंका थी, आगे ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है जो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को बंधुआ मजदूर बनाकर अपनी सियासी सेवाटहल कराने हुक्मबजाऊ चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करे। प्रबल तर्काें के लिए मशहूर हरि विष्णु कामथ ने कहा, सवाल है राज्यों के लिए गोलमोल लिखा है कि उन्हें बचा-खुचा अधिकार यानी खुरचन दी जाएगी। नजीरुद्दीन अहमद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव जैसे सदस्य सरकारी प्रस्ताव के समर्थन में रहे। राज्यों का क्षेत्राधिकार बर्फ की सिल्ली की तरह चट्टान होने का धोखा देता है। जैसे ही उस पर केन्द्र की कार्रवाई की गर्मी पड़ती है, पिघलकर पानी हो जाता है।
मई 2024 में लोकसभा चुनाव तय हैं। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का शिगूफा फुसफुसाता है या तो 2023 में होने वाले पांच राज्यों की विधानसभाओं का समय संसदीय हुक्म से बढ़ा दिया जाए। जिससे चुनाव लोकसभा के साथ हो सकें। विकल्प में मौजूदा लोकसभा भंग कर दी जाए और पांचों विधानसभाओं के साथ लोकसभा चुनाव भी करा लिया जाए। तब तक संसद का मुंह बंद हो लेकिन मंत्रिपरिषद संविधान के मुताबिक कायम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व-काल में संविधान की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उसने 2002 में सरकार को सिफारिशों सहित रिपोर्ट पेश कर दी। सिफारिशों के सार संक्षेप के अध्याय 4 में चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर 64 सुझावों में कहीं भी विधानसभा को भंग कर ‘वन नेशन वन इलेक्शन‘ जैसे शगल का सुझाव नहीं है। अब ताकतवर प्रधानमंत्री की हुकूमत संविधान को चुनौती दे रही है। संविधान राजपथ पर पड़ा हुआ रोड़ा लगता होगा। वह जनपथ पर चलने की नसीहत क्यों देता है? ऐसा रोड़ा हटा देना है।
संविधान की उद्देशिका उसका दिल है। उसे छोड़़कर जो किया जाएगा, गैरसंवैधानिक होगा। यह समझना कि संविधान नेताओं ने ही बनाया है, सरासर गलत है। अंधभक्त पीढ़ी भक्तिभाव में संवैधानिक सच नहीं समझ पाती है। लोकतंत्र की बुनियाद नेता, सरकार, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी नहीं हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह सार्वभौम नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, हम भारत के लोग अर्थात जनता ही सार्वभौम है। संविधान भी सार्वभौम नहीं है। चुनने का अधिकार मूल अधिकार है लेकिन सांसद, विधायक बनने चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के तहत बने अधिनियम का है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की आड़़ में केन्द्र सरकार जनप्रतिनिधियों का हुकूमत करने का अधिकार खंडित नहीं कर सकती। ‘वन नेशन वन इलेक्शन‘ लागू करना है तो संविधान में अधिकार मांगते जनमत संग्रह भी करा लें।
जनता ही संविधान बल्कि देश के अस्तित्व की बुनियाद है। 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में डा आंबेडकर ने दो टूक कहा, आजादी की लड़ाई के दौरान कई लोग ‘भारत की जनता‘ शब्द कहने के बदले ‘भारतीय राष्ट्र’ शब्दों को पसंद करते थे। ‘हमारा एक राष्ट्र है‘ कहते हम एक बडे़ मायाजाल में फंस रहे हैं। हजारों जातियों में बंटी जनता किस प्रकार एक राष्ट्र हो सकती है? जातियां सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं। वर्ण और वर्ग भी राष्ट्रीयता के विरोधी हैं। एक राष्ट्र बनना है, तो इन बुराइयों को दूर करना पडे़गा।
रवीन्द्रनाथ टैगौर ने भी विश्व की सांस्कृतिक एकता समझाते धर्म पर संकीर्ण चेहरे का मुखौटा लगाए राष्ट्रवाद की मुखालफत की थी। विवेकानन्द ने राष्ट्र के संकीर्ण ठेकेदारों को लानत भेजी थी। आंबेडकर की ऐतिहासिक चेतावनी ने संविधान सभा में तय किया था भारतीयों के अधिकार क्या होंगे। ‘वन नेशन’ या ‘एक राष्ट्र’ का नारा क्यों थोपा जा रहा है। समीक्षा में फुसफुसाहटें हैं। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ सरकार का इरादा है। विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एकसाथ करा दिए जाएं। ऐसा अजूबा आजादी के पंद्रह वर्ष के बाद से विधायिकाओं की घट बढ़ उम्र के चलते कभी नहीं हुआ। आंबेडकर के संविधान सभा में कथन के कारण भी हो नहीं सकता था।
संवैधानिक कहानी 15 जून 1949 से शुरू हुई है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा.बी. आर. आंबेडकर ने चुनाव आयोग की स्थापना तथा अधिकारिता सम्बन्धी अनुच्छेद 324 (प्रारूप में अनुच्छेद 289) को बहस के लिए पेश किया था। आंबेडकर ने खुलासा किया कि चुनाव आयोग के जरिए संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराने का प्रावधान अब होगा। हमने चुनावी मशीनरी कायम करते चुनाव मैनेजमेंट का प्रावधान किया है। उन्होंने बहुत खुलकर कहा, इसमें शक नहीं कि आमतौर पर चुनाव हर पांच वर्ष बाद ही होंगे। प्रश्न फिर भी रहेगा कि उपचुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। पांच वर्ष के पहले विधानसभा भंग भी हो सकती है। स्थायी मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी मशीनरी के जरिए चुनाव कराना बड़ा बदलाव है। हमने राज्यों (प्रदेशों) को अधिकार नहीं दिया है क्योंकि वहां से गुटबाजी की शिकायतें आ रही हैं। केन्द्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
सजग सदस्य शिब्बनलाल सक्सेना ने प्रारूप के बुनियादी सोच पर हमला करते कहा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करें? केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और उसके मुखड़े प्रधानमंत्री की हर सिफारिश मानना राष्ट्रपति के लिए लाजिमी होगा। प्रधानमंत्री के हुक्म जनता पर चुनाव आयोग के जरिए लादकर चुनाव प्रबंधन उसके हाथ दे देना कहां तक लोकतांत्रिक है? सक्सेना ने नायाब प्रस्ताव किया, वही व्यक्ति प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जिसके पक्ष में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का दो तिहाई बहुमत जरूर हो। लचीला लेकिन विचारोत्तेजक सुझाव आंबेडकर ने नहीं माना। सक्सेना ने कहा, आजाद खयालों और निष्पक्ष आचरण के प्रधानमंत्री नेहरू चाहें तो अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, हालांकि वह कतई नहीं करेंगे। लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं कि आगे प्रधानमंत्री नैतिक और प्रशासनिक पैमाने पर नेहरू की कदकाठी के होंगे। प्रधानमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में समर्थन के लिए थोड़ा सा विरोध होने पर भी संसार के जनमत के सामने उनका सिर झुक जाएगा। सक्सेना ने भी जोर देकर कहा, ‘‘शायद किसी न किसी प्रान्त में हमेशा चुनाव होते ही रहेंगे। देशी रियासतों के शामिल होने पर लगभग तीस प्रान्त हो जाएंगे। मुमकिन है, केन्द्र तथा अलग अलग प्रान्तों के विधानमंडलों के चुनाव एक ही समय पर नहीं हों। दस-बारह वर्ष के पश्चात हर समय किसी न किसी प्रान्त में चुनाव होता रहेगा।”
असम के कुलाधर चालिहा ने ताबड़़तोड़ भाषण में प्रस्तावित प्रावधानों की छीछालेदर करते हुए कहा, राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने से उनके पक्षपाती रहने की इंसानी गुंजाइश है। हृदयनाथ कुंजरू ने अलबत्ता महत्त्वपूर्ण कहा, दुनिया में किसी संविधान को नहीं जानता जहां फेडरल देश में चुनाव की सभी खटपट और जिम्मेदारियां चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ी जाएं। अजूबा केवल भारतीय फेडरल लोकतंत्र में किया जा रहा है।
सदस्यों की आशंका थी, आगे ऐसा प्रधानमंत्री आ सकता है जो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को बंधुआ मजदूर बनाकर अपनी सियासी सेवाटहल कराने हुक्मबजाऊ चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करे। प्रबल तर्काें के लिए मशहूर हरि विष्णु कामथ ने कहा, सवाल है राज्यों के लिए गोलमोल लिखा है कि उन्हें बचा-खुचा अधिकार यानी खुरचन दी जाएगी। नजीरुद्दीन अहमद, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव जैसे सदस्य सरकारी प्रस्ताव के समर्थन में रहे। राज्यों का क्षेत्राधिकार बर्फ की सिल्ली की तरह चट्टान होने का धोखा देता है। जैसे ही उस पर केन्द्र की कार्रवाई की गर्मी पड़ती है, पिघलकर पानी हो जाता है।
मई 2024 में लोकसभा चुनाव तय हैं। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का शिगूफा फुसफुसाता है या तो 2023 में होने वाले पांच राज्यों की विधानसभाओं का समय संसदीय हुक्म से बढ़ा दिया जाए। जिससे चुनाव लोकसभा के साथ हो सकें। विकल्प में मौजूदा लोकसभा भंग कर दी जाए और पांचों विधानसभाओं के साथ लोकसभा चुनाव भी करा लिया जाए। तब तक संसद का मुंह बंद हो लेकिन मंत्रिपरिषद संविधान के मुताबिक कायम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व-काल में संविधान की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उसने 2002 में सरकार को सिफारिशों सहित रिपोर्ट पेश कर दी। सिफारिशों के सार संक्षेप के अध्याय 4 में चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर 64 सुझावों में कहीं भी विधानसभा को भंग कर ‘वन नेशन वन इलेक्शन‘ जैसे शगल का सुझाव नहीं है। अब ताकतवर प्रधानमंत्री की हुकूमत संविधान को चुनौती दे रही है। संविधान राजपथ पर पड़ा हुआ रोड़ा लगता होगा। वह जनपथ पर चलने की नसीहत क्यों देता है? ऐसा रोड़ा हटा देना है।
संविधान की उद्देशिका उसका दिल है। उसे छोड़़कर जो किया जाएगा, गैरसंवैधानिक होगा। यह समझना कि संविधान नेताओं ने ही बनाया है, सरासर गलत है। अंधभक्त पीढ़ी भक्तिभाव में संवैधानिक सच नहीं समझ पाती है। लोकतंत्र की बुनियाद नेता, सरकार, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारी नहीं हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह सार्वभौम नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, हम भारत के लोग अर्थात जनता ही सार्वभौम है। संविधान भी सार्वभौम नहीं है। चुनने का अधिकार मूल अधिकार है लेकिन सांसद, विधायक बनने चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के तहत बने अधिनियम का है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की आड़़ में केन्द्र सरकार जनप्रतिनिधियों का हुकूमत करने का अधिकार खंडित नहीं कर सकती। ‘वन नेशन वन इलेक्शन‘ लागू करना है तो संविधान में अधिकार मांगते जनमत संग्रह भी करा लें।
जनता ही संविधान बल्कि देश के अस्तित्व की बुनियाद है। 25 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के अंतिम भाषण में डा आंबेडकर ने दो टूक कहा, आजादी की लड़ाई के दौरान कई लोग ‘भारत की जनता‘ शब्द कहने के बदले ‘भारतीय राष्ट्र’ शब्दों को पसंद करते थे। ‘हमारा एक राष्ट्र है‘ कहते हम एक बडे़ मायाजाल में फंस रहे हैं। हजारों जातियों में बंटी जनता किस प्रकार एक राष्ट्र हो सकती है? जातियां सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं। वर्ण और वर्ग भी राष्ट्रीयता के विरोधी हैं। एक राष्ट्र बनना है, तो इन बुराइयों को दूर करना पडे़गा।
रवीन्द्रनाथ टैगौर ने भी विश्व की सांस्कृतिक एकता समझाते धर्म पर संकीर्ण चेहरे का मुखौटा लगाए राष्ट्रवाद की मुखालफत की थी। विवेकानन्द ने राष्ट्र के संकीर्ण ठेकेदारों को लानत भेजी थी। आंबेडकर की ऐतिहासिक चेतावनी ने संविधान सभा में तय किया था भारतीयों के अधिकार क्या होंगे। ‘वन नेशन’ या ‘एक राष्ट्र’ का नारा क्यों थोपा जा रहा है। समीक्षा कमेटी में राष्ट्रपति को समीक्षा कमेटी का अध्यक्ष बनाना ऐतिहासिक असंवैधानिक अजूबा है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.