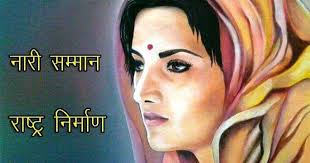— आनंद कुमार —
विश्व मूलत: मानवता के आधार पर संचालित है और मानव संस्कृति विविधताओं का महासंगम है. फिर भी दुनिया के हर स्त्री-पुरुष की एक निश्चित राष्ट्रीयता और अस्मिता होती है. राष्ट्रीयता के दो प्रमुख पहलू हैं – एक तो यह विश्व की राजनीति, आर्थिकी और संस्कृति के सन्दर्भ में बनती-बिगडती है और दूसरे यह राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया को आधार देती है. विविधता में एकता की व्यवस्था स्थापित करना राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय सारांश है. वैसे हम सभी स्त्री-पुरुषों का अस्तित्व जन्म से लेकर मरण तक एक नितांत एकाकी दैहिक प्रक्रिया का परिणाम है. लेकिन हम सभी – लिंग-भेद, विवाह, परिवार, कुटुंब, पड़ोस, जाति-धर्म, भाषा, संस्कृति और राष्ट्र जैसी सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की देखरेख में जीते और मरते हैं. हमारा सम्पूर्ण जीवन ‘अपनत्व’ और ‘अन्यता’ के ताने-बाने से बनता है. अपनत्व में ममत्व का विस्तार और वर्चस्व का निषेध है. अन्यता का आधार परस्पर अलगाव और वर्चस्व है. ‘व्यक्तिगत’ और ‘सामाजिक’ की धूप-छांह के बीच के बीच हमारा व्यक्तित्व-विकास और जीवन-सञ्चालन होता है. इसमें राष्ट्र-निर्माण का विमर्श हमारे जीवन की शर्तों के निर्धारण में अनिवार्य आधारशिला का काम करता है.
राष्ट्रनिर्माण में सफल समाज के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार, आवास, परस्पर सहयोग और आत्मसम्मान के मोर्चे पर अनुकूलता का परिवेश मिलता है. दूसरी तरफ़, राष्ट्रनिर्माण की शर्तों को पूरा करने में असफल समाज के लोगों का जीवन अभावग्रस्त, असुरक्षित और असमानताओं से त्रस्त होने को अभिशप्त रहता है. निरक्षर और सुशिक्षित, दरिद्र और सम्पन्न, अभावग्रस्त और सुपोषित, उपेक्षित और सम्मानित, वंचित और संरक्षित के बीच ‘अपनत्व’ कैसे पनप सकता है? बिना सजगता और सरोकार के विभिन्नताओं की लिंगभेद आधारित, जातिप्रथा द्वारा संरक्षित, सम्प्रदाय भेद और धर्म-भेद पर बनी, भाषा-भेद से टिकी, गरीब-अमीर के बीच के फासलों और राजनीतिक हैसियत के फर्क की खाइयाँ कैसे पटेंगी? इसलिए राष्ट्रनिर्माण में योगदान करना हरेक के व्यक्तिगत और सामूहिक हित में होता है. निजी और सार्वजनिक जीवन के आदर्शो और आचरण के जरिये राष्ट्रनिर्माण में रचनात्मक हिस्सेदारी हरेक वयस्क व्यक्ति का सहज नागरिक धर्म है. भारत में परम्पराओं और स्मृतियों की ऐतिहासिकता के बावजूद नागरिकता का इतिहास २६ जनवरी १९५० से शुरु हुआ है. इसलिए सजगता और प्रतिबद्धता की जादा जरूरत है.
भारत की राष्ट्र-निर्माण यात्रा
भारत का राष्ट्रनिर्माण-रथ हमारे संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तरफ पिछले आठ दशकों से क्रमश: बढ़ रहा है. लेकिन गति संतोषजनक नहीं है. १९३० में ही ‘सभी के लिए सम्मानजनक जीवन संभव बनाने’ को पूर्ण -स्वराज का लक्ष्य घोषित करने वाले और १९७५ में ‘सम्पूर्ण क्रांति’ के लिए समर्पित होनेवाले भारत के लोग बड़े सपने देखने की क्षमता खो रहे हैं. ‘भूख से मुक्ति’, ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ और ‘सम्मानपूर्ण जीवन की जरूरत’ के लिए समाज को जोड़ने का उत्साह नहीं है. आज ‘सबको रोजगार – सबको सम्मान’ देने का सपना हमको उत्साहित नहीं करता. हम अपनी नदियों को निर्मल बनाने और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त बनाने की बेचैनी नहीं महसूस करते. हम सांप्रदायिक नफरत से मुक्त अहिंसक सामुदायिक जीवन को एक असम्भव कल्पना समझने लगे हैं. स्त्री, आदिवासी, दलित और गैर-हिन्दू सम्प्रदायों के लोग न्यायपूर्ण स्वराज की आस लगाए आठ दशकों से प्रतीक्षा कर रहे हैं.
स्त्री के खिलाफ अपराध हमारे जीवन में ‘पुरुष केन्द्रित जीवन व्यवस्था’ का सबसे शोचनीय पक्ष है. स्त्री ‘वंचित भारत’ की सबसे पीड़ित हिस्सा है. स्त्री के साथ हिंसा, जातिगत हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा की तरह, ‘हम’ और ‘अपनत्व’ की भावना पर आघात है. पुरुषवाद का पोषण है. लोकतान्त्रिक राष्ट्रनिर्माण की संभावना का निषेध है. अकेले २०२२-२०२३ में स्त्रियों के खिलाफ ४ लाख ४५ हजार अपराधों की रिपोर्ट दर्ज हुई है. भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात ९३४ स्त्री प्रति १००० पुरुष (२०११) रहा है और स्त्री के खिलाफ अपराध दर ६६ प्रति एक लाख पायी गयी. भारत के १२ प्रदेशों में राष्ट्रीय अनुपात से जादा मामले होते हैं. इनमें दिल्ली और हरियाणा में जादा बर्बरता की जा रही है. कुल मिलाकर २०२० में ३ लाख ७१ हजार मामले और २०२१-२०२२ में ४ लाख २८ हजार से अधिक घटनाएँ पुलिस को दर्ज करायी गई थीं. इनमें से ५० प्रतिशत घटनाएं कुल पांच प्रदेशों – उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में हुई थीं. स्त्री के खिलाफ अपराध के ३१ % मामले पति और ससुराल के अन्य परिवारजनों द्वारा दुर्व्यवहार से सम्बंधित और १९% अपहरण से जुड़े थे. १८% शिकायतें अभद्रता और अपमान की तथा ७% घटनाएं बलात्कार की थीं! आज भी ग्रामीण और कस्बाई परिवेश में स्त्री का स्वराज सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त से समाप्त हो जाता है. जाति-धर्म-भाषा-वर्ग के भेद के बावजूद अधिकांश महिलाओं की यह प्रार्थना है कि ‘अगले जनम मोहें बिटिया न कीजो!’.
यह सब भारत की महिलाओं की नागरिकता के आत्मघाती अधूरेपन का संकेतक है. हमारे आधे देश की बेबसी का बयान है. वैसे उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और यूरोप महाद्वीपों के देशों को छोड़कर वैश्विक विषमताओं के कारण बाकी दुनिया भी चिंताजनक हाल में है. एक तरफ गरीबी और गैर-बराबरी और दूसरी तरफ प्रकृति संहार और मध्यम वर्गों में बढ़ता बेलिहाज भोगवाद आज के भूमंडलीकरण के दो पहलू हैं. पूरी दुनिया में भरोसे लायक विकास के रास्ते की तलाश जारी है जिससे हर स्त्री-पुरुष अपने जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके और हिंसा-मुक्त न्याय आधारित दुनिया रची जा सके. दुनिया में १९३ राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण किया है. इन देशों में जी रहे स्त्री-पुरुष एक शांतिपूर्ण और मानव गरिमा से सुसज्जित भविष्य के लिए संगठित प्रयास में जुटे हैं. हम भारतीय स्त्री-पुरुषों को भी अपना घर संवार के अपना योगदान करना है.
हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य
हमारे क्या सामूहिक राष्ट्रीय लक्ष्य हैं? हम अनेको मतभेदों के बावजूद कम से कम चार प्रश्नों पर राष्ट्रीय सहमति का निर्माण करने में सफल हैं – विकास, लोकतंत्र, स्वराज-रचना (वि-औपनिवेशीकरण), और राष्टीय अखंडता. हमारे संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्र-निर्माण के पांच स्तम्भ हैं – स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व और एकता-अखंडता. इसमें हर स्तम्भ को लगातार मजबूत बनाए रखने की जरूरत है. इसके लिए भारत को अपनी परम्पराओं में निहित संभावनाओं को पहचानना होगा. जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, अहिंसा परमोधर्म, सर्वधर्म समभाव, नारी-सम्मान, करुणा, मैत्री और परोपकार. कई नए आदर्शों को अपनाना होगा. जैसे सहभागी लोकतंत्र, मानव अधिकारों की रक्षा, हिंसा मुक्त पारिवारिक व् सामुदायिक जीवन, समान नागरिक विधियाँ, नागरिक सक्रियता, सहकारी जीवन शैली. इसमें हमें सात स्त्रोतों से आधी-अधूरी मदद मिल रही है – विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, राजनीतिक दल समूह, नागरिक संगठन और शिक्षा और शोध संस्थान.
लेकिन यह भी सच है कि भारत कम से कम सात मोर्चों पर पिछड रहा है – संतुलित विकास, पारदर्शी प्रशासन, वैधता से लैस सत्ता व्यवस्था, लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती, नागरिकता निर्माण, राष्ट्र-निर्माण, और स्वस्थ पर्यावरण प्रबंधन. इसीलिए जीवन दशा में सुधार के वैश्विक मूल्यांकन (२०२३-२४) में हमारा स्थान १३४ के आसपास है जो हमें ‘विकासशील देश’ की दयनीय दशा में रखता है. दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान हमसे आगे निकल गए हैं. चीन(७५वाँ स्थान) तो हमसे ५९ सीढ़ी ऊपर है. भारत सिर्फ पाकिस्तान (१६४) से बेहतर पाया गया. देश के अंदर, जाति-जनजाति- अन्य जातियों के बीच अंतर और अनपढ़ तथा शिक्षित के बीच की दूरियाँ बहुत खतरनाक है. सम्प्रदाय और गाँव-नगर-महानगर के बीच फासले बेहद शर्मनाक हैं. उत्तर और पूर्व तथा दक्षिण और पश्चिम के प्रदेशों के बीच की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार-आमदनी की विषमताएं तो और भी चिन्त्ताजनक हैं.
लेकिन यह संतोष की बात है कि भारतीय समाज में सत्तर के दशक से स्त्री-विमर्श में कई आशाजनक परिवर्तन हुए. अब ‘स्त्री-सशक्तिकरण’ लोकतंत्री-राष्ट्रनिर्माण का अनिवार्य अंग बन चुका है. ‘बेटी बचाओ- बेटी पढाओ’ नयी शताब्दी का उद्घोष है परिवार से लेकर बाजार और सरकार तक ‘हिंसा-मुक्त’ जीवन दशा निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होती जा रही है और इस सांस्कृतिक नवनिर्माण में उसे स्त्री-आन्दोलन का मार्गदर्शन और सजग पुरुषों का सहयोग मिल रहा है. दिल्ली में हुए ‘निर्भया आन्दोलन’ (२०१२) और कलकत्ता विद्रोह (२०२४) के बीच देश बहुत बदला है. स्त्री की सहभागिता के राजनीतिक आयाम के रूप में विधायिका में २०२९ से आरक्षण का निर्णय और मतदानों के अवसर पर स्त्री-मतदाता के निर्णय में स्व-विवेक का संकेत इसका महत्वपूर्ण संकेत हैं. जबकि १९४६ में गठित हमारी संविधान सभा में कुल ३८९ सदस्य थे इनमें मात्र १५ महिलाएं थी. फिर भी संविधान ने ‘पुरुषवाद’ को पीछे छोड़ते हुए नर-नारी समता का आदर्श अपनाया. सर्वोच्च न्यायालय और सेना से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिला को महत्व दिया जाने लगा है. हालांकि सुधार संतोषजनक नहीं है. हमारी लोकसभा के ५४३ सदस्यों में सिर्फ ७८ और राज्यसभा में २०५ में से २६ महिलायें हैं.
इसीबीच आर्थिक मोर्चे पर स्त्री को स्वावलम्बी बनाने के लिए देश के खजाने से सीधी मदद दिलाने में दलों के बीच होड़ शुरू है. ‘लाडली बहना योजना’ से ‘लखपति दीदी योजना’ तक एक नया सिलसिला बन रहा है. इससे हमारा राजनीतिक विमर्श स्त्री-उन्मुख हो चुका है. सांस्कृतिक सन्दर्भ में विवाह व्यवस्था में जाति (दहेज़ प्रथा और विधवाओं की दुर्दशा) और धर्म (बहु-विवाह) से जुडी परम्पराओं में सुधार के अभियान के लिए अनुकूलता बढ़ी हैं. उदाहरण के लिए स्त्री को परिवार की संपत्ति में अधिकार और विवाह-विच्छेद के मामले में बच्चों के अभिभावकत्व के बारे में कानून बनाने के प्रयास में डा. आम्बेडकर को १९५१ में परम्परावादियों द्वारा जबरदस्त विरोध का निशाना बनाया गया था. उन्हें सरकार से इस्तीफ़ा देना पड़ा था. लेकिन तब से अब के बीच परिस्थितियां बेहतरी की ओर मोडी जा चुकी है. संपत्ति में यौन उत्पीडन निषेध कानून (२००३) और घरेलू हिंसा के खिलाफ पारित कानून (परिवारक हिंसा निषेध अधिनियम, २००५) ने स्त्री जीवन को मानवीय बनाने के लक्ष्य से राज्य सत्ता को सहज ही जोड़ दिया है. शिक्षा के उच्च स्तरों में सफलता और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पुलिस-सेना में प्रवेश में सफलता और उपलब्धियों के कारण स्त्री का जीवन पुरुष की धुरी पर नाचने के लिए विवश नहीं रह गया है. सार्थक शिक्षा और आधुनिक रोजगारों के फैलते दायरे ने एक वयस्क स्त्री के लिए विवाह की अनिवार्यता को समाप्त करना शुरू कर दिया है.
एक सांस्कृतिक क्रांति का शुभारम्भ
वस्तुत: हम एक आवश्यक सांस्कृतिक क्रांति के साक्षी और सहभागी बन रहे है. क्योंकि हम समझ चुके हैं कि राष्ट्र निर्माण और स्त्री-अस्मिता दोनों का रास्ता शिक्षा और न्याय से सुसज्जित समाज में ही सुगम होता है. भारतीय समाज स्त्री-शिक्षा को महत्व देकर समाज संचालन की निर्णय प्रक्रिया में हर स्तर पर स्त्री की सहभागिता के प्रयास में जुट गया है. ब्रिटिश राज के दो शताब्दियों के बाद भारत में १९३१ में हुई जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर मात्र ९.१ प्रतिशत थी. ९७ प्रतिशत से अधिक महिलायें निरक्षर के अन्धकार में कैद थीं. लेकिन स्वराज मिलने के सातवें दशक में हुई जनगणना में साक्षरता का प्रकाश ७२ प्रतिशत भारतीयों तक पहुँच गया था. स्त्री-साक्षरता दर भी ६४ प्रतिशत के ऊपर पहुँच गयी थी. २००९ में पारित शिक्षा अधिकार कानून की स्वीकृति से निकट भविष्य में स्त्री-शक्ति शिक्षा शक्ति से लैस हो जाएगी. इससे नागरिकता निर्माण की सबसे बड़ी बाधा दूर होगी और राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया को बल मिलेगा. इस प्रक्रिया में क) स्त्री-आधारित, ख) स्त्री-उन्मुख और ग) स्त्री-केन्द्रित विमर्शपारित शिक्षा अधिकार कानून के बाद निरक्षरता भारतीय स्त्री-पुरुषों के जीवन से शीध्र निर्मूल हो जाएगी. हमारी जनश देश-समाज की सबसे बड़ी जरूरत है. ऐसे परिवेश में स्त्रियों को ‘अबला’ या ‘देवी’ की बजाए ‘वीरांगना’ के रूप में परिभाषित करना और ‘वीरांगना-वाहिनी’ की स्थापना करना एक बुनियादी बदलाव का शुभारम्भ है. इसका देशव्यापी विस्तार और हर प्रकार से समर्थन और संवर्धन हर देशप्रेमी और मानवीयता के प्रत्येक उपासक-उपासिका का सहज कर्तव्य है.
‘रेड ब्रिगेड’ द्वारा एकजुट की गयी युवतियों द्वारा वीरांगना वाहिनी के शुभारम्भ के लिए विदुषी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र्नायिका सरोजिनी नायडू की प्रेरक स्मृति में १९ जनवरी को आयोजित ‘राष्ट्रीय महिला दिवस’ को चुना जाना महत्वपूर्ण है. इससे राष्ट्र को हमारी आज़ादी की लड़ाई में स्त्रियों की हिस्सेदारी और योगदान का स्मरण ताज़ा होता है. लक्ष्मीबाई, चेनम्मा, हज़रत महल, झलकारी देवी, अहिल्या देवी होल्कर से लेकर सावित्री फुले, फातिमा शेख, भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, ग्वैदालो, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, विजया पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, अमृत कौर, दक्षायनी वेलायुधन और लक्ष्मी सहगल तक की यशस्वी श्रृंखला से प्रेरणा मिलती है. स्त्रियों को भी अपनी विरासत, भूमिका और जिम्मेदारी का अहसास करना आसान हो जाता है. आइए, राष्ट्रनिर्माण की चुनौती का समाधान करें. परिवार, बाजार और विद्यालय से लेकर विधायिका, चिकित्सालय और न्यायालय तक स्त्री की सार्थक सहभागिता के लिए वीरांगना वाहिनी को उन्मुक्त सहयोग दें.
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.