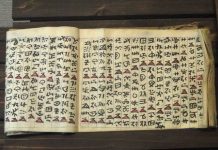— परिचय दास —
हिन्दी का , सच पूछिये तो कोई एक दिन नहीं होता, न कोई एक प्रदेश उसका घर होता है। वह कभी मध्य भारत के मैदानों में झूलती है तो कभी पूर्वांचल की संधियों में सीपी-सीपियों-सी बजती है। कभी लोकगीतों की तरह गूँजती है, कभी सिनेमा के संवादों में आत्मीय हो जाती है। वह जहाँ होती है, अपने होने की घोषणा नहीं करती—बस रहती है, फैलती है, गुँथती जाती है। और यही उसकी शक्ति है।
महाराष्ट्र ने हाल ही में हिन्दी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में मान्यता देकर इसी मौन स्वीकृति को औपचारिक कर दिया है। यह निर्णय कोई तुरन्त लिया गया राजनीतिक उपक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का वह अविरल प्रवाह है, जिसे राज्य की शिक्षा नीति में आत्मसात किया गया है। वर्ष 2024 के अंत में, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि राज्य के सभी गैर-हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों में हिन्दी को अब तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में लिया गया, जो त्रिभाषा सूत्र को पूरे भारत में समान रूप से लागू करने की बात करता है।
यह घोषणा, कुछ के लिए विस्मय का विषय हो सकती है, लेकिन वास्तव में यह उस स्वाभाविकता का विस्तार है जो महाराष्ट्र की भूमि में हिन्दी पहले से ही जीती रही है। मुम्बई शहर हिन्दी की आत्मा को अपने फ़िल्मी लहजे, ग़ज़लों, नाटकों और संवादों में कई दशक से ढोता आया है। पुणे, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद जैसे नगरों में हिन्दी पत्रकारिता, साहित्य और रंगमंच की गहरी परंपरा रही है। लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे, बाबा आमटे—सभी ने हिन्दी को एक सेतु की तरह अपनाया, एक ऐसी भाषा के रूप में जो संवाद को संकीर्णता से बचाती है।
हिन्दी यहाँ ‘थोपी’ नहीं गई, हिन्दी यहाँ ‘उग आई’। जब विद्यार्थी अपने करियर के लिए कोचिंग संस्थानों की ओर रुख करते हैं, जब सिनेमा के टिकट खिड़कियों पर संवाद होता है, जब रिक्शेवाले से लेकर प्रोफेसर तक के बीच कोई भाषा पुल बनती है—तो वह अक्सर हिन्दी होती है। महाराष्ट्र का यह निर्णय उस सहज स्वीकार्यता को संस्थागत करता है जो जनता पहले ही अपना चुकी है।
इसके ठीक विपरीत तमिलनाडु की राजनीति ने हिन्दी को लेकर जिस तरह की ऐतिहासिक दूरी बनाई है, वह अब एक परंपरा की तरह जड़ होती जा रही है। द्रविड़ आंदोलन के आरंभिक दौर में हिन्दी-विरोध आत्मरक्षा का औज़ार था—एक सांस्कृतिक इकाई की पहचान बचाए रखने की आकांक्षा। पर अब जब भारत बदल चुका है, जब भाषाएँ एक-दूसरे के जीवन में घुल-मिल चुकी हैं, तब भी यदि किसी राज्य की राजनीति हिन्दी से घबराती है, तो यह घबराहट भाषायी नहीं, बल्कि वैचारिक हो जाती है।
तमिलनाडु की भाषा-संवेदनशीलता को समझा जा सकता है, पर हिन्दी को डरावनी चीज़ मान लेना उस संवेदनशीलता को कठोर बना देता है। स्टालिन द्वारा हिन्दी-विरोध उस ऐतिहासिक सांचे से निकला है जिसमें हिन्दी को सत्ता का प्रतीक मानकर खारिज किया गया। पर हिन्दी अब सत्ता की भाषा नहीं, वह जनता की आत्मा बन चुकी है। यह जनता ही है जो मेट्रो में, दुकानों में, टोल प्लाज़ा पर, शिक्षण संस्थानों में और सोशल मीडिया पर हिन्दी में संवाद करती है—बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के।
जब महाराष्ट्र हिन्दी को तीसरी भाषा बनाता है, तो वह केवल एक शिक्षा नीति लागू नहीं करता, बल्कि वह एक विचार प्रस्तुत करता है—कि कोई भी राज्य अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए, अन्य भारतीय भाषाओं को आत्मसात कर सकता है। मराठी की गरिमा को छुए बिना हिन्दी को अंगीकार करना भारत की भाषिक सह-अस्तित्व की सुंदरतम मिसाल है।
यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी के पास अब केवल ‘संख्या बल’ नहीं है, बल्कि ‘सांस्कृतिक स्नेह’ भी है। महाराष्ट्र का यह दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा किसी विशाल परिवार में एक नए सदस्य को अपनेपन से जगह दी जाती है—न वह पुरानों को हटाता है, न उन्हें छोटा करता है, बस सभी को जोड़ता है।
हिन्दी आज भारत में केवल संवाद का माध्यम नहीं, वह एक संवेदना है। उसकी उपस्थिति किसी परछाईं की तरह होती है—जो सूरज के संग-संग चलती है, पर कभी अतिक्रमण नहीं करती। यह वह भाषा है, जो तमिल और मलयालम, मराठी और बंगला, उड़िया और असमिया सभी के बीच एक समरसता उत्पन्न कर सकती है, यदि उसके स्वर को विरोध की राजनीति में दबाया न जाए।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी को एक अवसर के रूप में देखें, एक ऐसे माध्यम के रूप में जो तमिलनाडु के विद्यार्थी को राजस्थान के विद्यार्थी से जोड़ सके, जो मणिपुर के कवि को महाराष्ट्र के पाठक से मिलवा सके, और जो यह स्मरण दिला सके कि भारत की आत्मा केवल विविधता में नहीं, बल्कि संवादशील विविधता में है।
महाराष्ट्र ने यह दिखा दिया है कि भाषा का अपनाना अस्मिता का खोना नहीं होता। वह एक उजास है, जो अपने में जोड़ लेने से और भी दीप्त होता है। अब तमिलनाडु को यह उजास देखना है—नकारना नहीं। और जब यह हो जाएगा, तब भारत की भाषाएँ नदियों की तरह एक महासागर में मिल जाएँगी—जहाँ कोई भाषा पहली नहीं, कोई अन्तिम नहीं—सभी एक समान प्रिय।
।। दो। ।
तमिलनाडु में हिन्दी के प्रति जो दृष्टिकोण है, वह ऐतिहासिक रूप से विरोधात्मक रहा है। यह विरोध केवल भाषा तक सीमित नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक योजना का हिस्सा रहा है। द्रविड़ आंदोलन की जड़ें ही इस बात से पोषित होती रही हैं कि हिन्दी का प्रचार ‘उत्तर भारतीय प्रभुत्व’ का प्रतीक है और इस आधार पर हिन्दी को अस्वीकार कर तमिल अस्मिता की रक्षा का झंडा उठाया गया। यही मानसिकता आज भी तमिलनाडु की राजनीति में जीवित है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का हिन्दी-विरोध इसी राजनीतिक परंपरा का विस्तार है।
यह विरोध केवल हिन्दी के खिलाफ़ नहीं है, यह उस भारतीय भावना के भी खिलाफ़ है जो विविधता में एकता की कल्पना करती है। हिन्दी को थोपे जाने की बात करना एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपनी मातृभाषा के अस्तित्व पर खतरे का आभास कराता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिन्दी आज़ादी के पहले से ही सम्पर्क भाषा के रूप में देशभर में स्वाभाविक रूप से फैलती रही है। महाराष्ट्र में जब हिन्दी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो यह किसी के ऊपर कोई भाषा थोपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी भाषा को अवसर देना था जो देश के कोने-कोने में संवाद की ताक़त रखती है।
यह विचार करना चाहिए कि क्या कोई भी राष्ट्र बिना किसी साझा भाषा के दीर्घकालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता बनाए रख सकता है? क्या किसी राज्य का यह दावा कि वह किसी एक भाषा को अपने युवाओं से दूर रखना चाहता है, उस राज्य के भीतर वैचारिक सीमाओं को नहीं खड़ा करता? जब महाराष्ट्र जैसे राज्य—जहाँ मराठी का स्वाभिमान जीवंत है—हिन्दी को तीसरी भाषा के रूप में अपनाता है तो वह अपनी भाषिक अस्मिता को और मजबूत ही करता है, न कि खो देता है।
तमिलनाडु के लगातार हिन्दी-विरोध को देखने का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि वहाँ की राजनीति ने हिन्दी को एक प्रतीक बना लिया है, जिस पर वार करके वे अपनी जनसंख्या के भावनात्मक हिस्से को जोड़े रखते हैं। यह विरोध अब एक प्रकार का वंशागत राजनीतिक नारा बन चुका है, जिसमें नई पीढ़ी के लिए संवाद के दरवाज़े बंद करने की प्रवृत्ति छिपी हुई है। स्टालिन जब हिन्दी के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वे वास्तव में उस साझा राष्ट्रीय संस्कृति से दूरी बना लेते हैं जो हिन्दी के माध्यम से सहज रूप से विकसित हो सकती है।
यह विरोध ‘भाषिक आत्मनिर्भरता’ का मुखौटा पहनकर ‘संवाद की विफलता’ को जन्म देता है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में संवाद का एक सार्वदेशिक माध्यम होना आवश्यक है। हिन्दी कोई वर्चस्व का औज़ार नहीं, बल्कि वह एक सेतु है जो असम से गुजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली भाषाई विविधता को एक सूत्र में पिरोती है। इसे पढ़ना, जानना और समझना किसी राज्य की संस्कृति के लिए अपमान नहीं, बल्कि आत्मविस्तार का अवसर है।
भारत के युवाओं को यदि वैश्विक मंचों पर पहुंचना है, यदि उन्हें आपस में जुड़ना है, तो उनके पास कम से कम एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उन्हें भारत के अन्य भागों से जोड़े। अंग्रेज़ी इस भूमिका को केवल आंशिक रूप से निभाती है, जबकि हिन्दी उसका मानवीय विकल्प बन सकती है।
इसलिए जब महाराष्ट्र हिन्दी को अपनाता है, वह कोई राजनीतिक दबाव नहीं झेलता—बल्कि वह एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जो अपनी सारी भाषाओं को संजोकर भी एक साझा संवेदना का स्पर्श पा सके। यह वह भारत है जो न तमिल से डरता है, न मराठी से घबराता है, न कश्मीरी या बंगाली से दूरी बनाता है, और न हिन्दी को लेकर अपराध-बोध पालता है। बल्कि यह वह भारत है, जो सभी भाषाओं को सम्मान देकर एक राष्ट्र की कल्पना करता है।
तमिलनाडु को भी इस भारत में उसी गरिमा के साथ जुड़ना चाहिए, जैसा गौरव वह अपनी तमिल भाषा को लेकर अनुभव करता है। हिन्दी से घबराना एक भाषाई आत्मविश्वास की नहीं, एक राजनीतिक रणनीति की निशानी है—और अब समय आ गया है कि भारत की राजनीति भाषा को संघर्ष नहीं, संवाद का आधार बनाए। महाराष्ट्र ने जो राह दिखाई है, वह एक अनुकरणीय उदाहरण है—और वह इस बात का प्रतीक है कि हिन्दी का बढ़ना किसी भाषा का घटना नहीं है, बल्कि भारत का आत्मविस्तार है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.