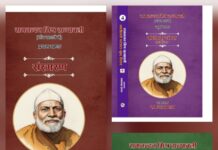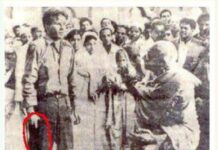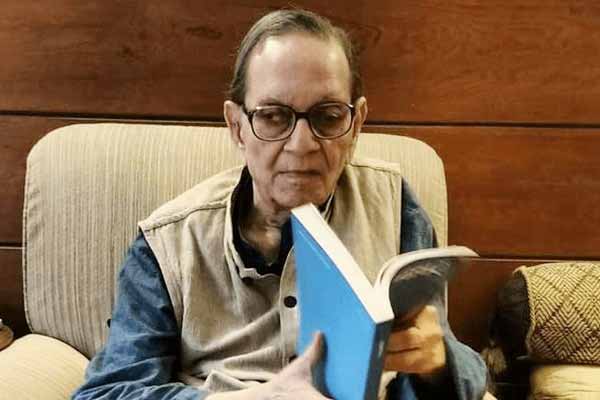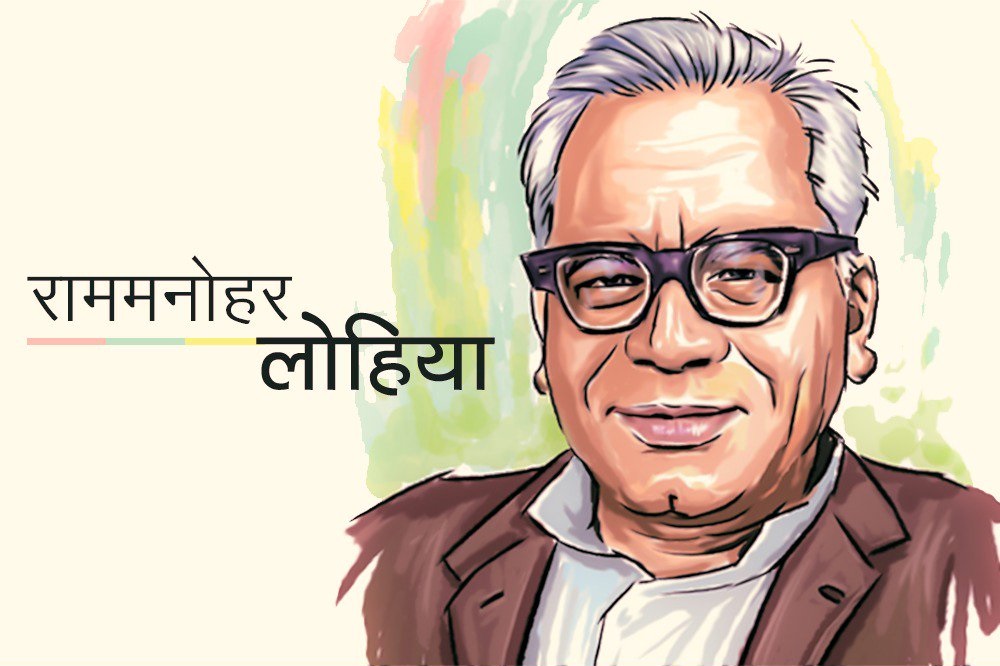माणिकचन्द्र-जैन-ग्रन्थमाला के म॔त्री तथा “ हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर” कार्यालय के मालिक नाथूराम प्रेमी जी के एकलौते पुत्र हेमचन्द्रजी (1909-1942) बहुमुखी प्रतिभासंपन्न लेखक थे। 1930 के दशक मे उन्होंने
“साहित्य शिक्षा का अध्ययन”, “गोदान, शाहजहाँ और बुद्धदेव की आलोचना” हिन्दी का बुनियादी व्याकरण” आदि पुस्तकें लिखीं, “हंस’ और “विशाल भारत” पत्रिका में साहित्यालोचन-विषयक अनेक लेख लिखे और साथ ही अंग्रेजी और बांग्ला की महत्वपूर्ण कृतियों का भी हिन्दी में अनुवाद किया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के जन्मदिवस पर हेमचन्द्र जी पर लिखे उनके संस्मरणात्मक लेख जो ग्यारह खंडों में प्रकाशित “हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली” में भी संकलित नही है, को आपके सामने प्रस्तुत कर पुण्यश्लोक आचार्य जी का स्मृति-तर्पण कर रहा हूं। 1977 में जेएनयू मे सूरदास पर दिये गये आचार्यप्रवर के दो व्याख्यान की स्मृति मेरे मानस-पटल पर अभी भी अंकित है।
—-‐—————–
स्वर्गीय हेमचन्द्रजी
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शास्त्राचार्य (शान्तिनिकेतन)
हेमचन्द्र जी के साथ मुझे सिर्फ दो दिन रहनेका अवसर मिला था। जब वे शान्तिनिकेतन आए थे तो मैं कलकत्ते गया था। लोटने पर मालूम हुआ कि वे गेस्ट हाउसमें ठहरे हैं। मैं उसी समय उनके पास पहुंचा और ‘हिन्दी मवन’ ले आया। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी अनुपस्थिति में उन्हें कष्ट हुआ होगा और आश्रम देखने में असुविधा उठानी पड़ी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनसे पहली बार जो उत्तर पाया उसने मुझे चक्कर में डाल दिया।
मैंने पूछा, “कल आपने आश्रम घूम-फिर कर कुछ देखा ?” उन्होंने बिना भूमिका के उत्तर दिया, “आश्रम क्या देखना है? मैं आश्रम देखने नहीं आया । ”
इस विषय में कुछ और कहे बिना ही उन्होंने उस नवीन पुस्तक के बारे अपनी राय प्रकट की, जिसे वे कल से ही पढ़ रहे थे और आज प्रायः समाप्त कर चुके थे। मैं चुपचाप सुन रहा था और वे उस पुस्तक के वक्तव्य की आलोचना कर रहे थे। मैं थोड़ी देर मे ऊब गया, परन्तु वे उसकी ही बात करते रहे। मैंने हँसकर कहा, “आपको शायद यह भ्रम है कि मैं पुस्तक चर्चा में ही दिन-रात लगा रहता हूं, पर मुझे पुस्तक की चर्चा में रस कम मिलता है, आइए, कुछ गप्प मारें ।” परन्तु हेमचन्द्र को अपने विषय से फुर्सत नहीं थी, गेस्ट हाउस का भृत्य उनका बिस्तर सँभालकर ‘हिन्दी भवन’ की ओर चला और हम दोनों उसी पुस्तक के विषय में उलझे हुए उसके पीछे हो लिये। आधे घंटे के भीतर मैंने आश्वर्य के साथ अनुभव किया कि किसी पुस्तक को वह व्यक्ति कितने अभिनिवेशके साथ पढ़ता है। मैने यह भी लक्ष्य किया कि वे पुस्तक से अभिभूत नहीं हैं। उसकी अगल-बगल की युक्तियों को देखते रहने के अभ्यस्त हैं, परन्तु ठीक उसके विरुद्ध से आनेवाली युक्ति की ओर से बेखबर हैं। मैंने उनको उस पुस्तके विषय से बाहर खींच लाने के लिये ही ठीक उल्टी दिशा से आक्रमण किया। मैंने हँसते हुए कहा, “भाई, गलत जगह किए हुए, गलत दिशा को जानेवाले और गलत ढंग से समाप्त होने वाले इन विषयों को इतना तूल क्यों देते हो? इसके लिये जितनी भी सूक्ष्म युक्तियाँ आप ढूँढते रहें, यह गलत ही रहेगा। ऋण स॔ख्या को हजारों-लाखों धन स॔ख्या से गुणा करते रहें, फल ऋण ही होगा।” और फिर मैं जोर से हँस पहा। मेरा उद्देश्य शास्त्रार्थ करना नहीं था। केवल पुस्तक के तर्क से उन्हें दूर हटा लाना ही अभिप्रेत था। वे जरूर कुछ चकराये, थोड़ी देर तक चुप रहकर बोले, “सही आपके मतसे क्या है?” मैंने रस लेते हुए कहा “यही भक्ति, प्रेम, पूजा।” मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ। हेमचन्द्रजी के सिर से उस पुस्तक का नशा उतरने लगा। अत्यन्त बालकोचित सरलताके साथ उन्होंने स्वीकार किया कि भक्ति बड़ी चीज है। उनका अध्ययन विशाल था और यद्यपि स॔ग्रहीत विचार उनके मस्तिष्क में अभी तक सामञ्जस्य नहीं बना सके थे, पर उनके अपने हो चुके थे। मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है कि किस एक बात पर उन्होंने दो परस्पर विरोधी बातें कहीं और याद दिलाने पर सरलता पूर्वक मान गए कि उन्होंने दोनों तरह की बातें पढ़ीं है और दोनों ही उनके विचारों में दाखिल हो चुकी है।
हेमचन्द्र का यह प्रथम परिचय बिलकुल अप्रत्याशित ढंग से हुआ। ये आश्रम देखने नहीं आए थे, शान्तिनिकेतन में चलनेवाली शिक्षापद्धतिके गुण-दोषों की परख को उत्सुक नहीं थे, यहाँ के उन विद्वानों से मिलनेकी भी उन्हें कोई बेचैनी नहीं थी, जो बाहर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। मैं हैरान था कि ये फिर किस उद्देश्य से इतनी दूर आये थे। असल में उनमें एक अजीब भोलापन था। वे अब शान्तिनिकेतन के लिये चल पड़े तो निश्चय ही कोई न कोई उत्सुकता उनके चित्त में थी, पर जब नई पुस्तक में उलझ गये तो यह उत्सुकता गौण हो गई और पुस्तकगत उत्सुकता प्रधान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि पढने में उनका नैसर्गिक अनुराग था। वे किसी पुस्तक को उसकी प्रत्येक विशेषताके साथ पढ लेते थे। यहाँ तक कि उन्हें याद था कि किस प्रसिद्ध पुस्तकमाला की पुस्तकों पर सीरीज की पुस्तकों की सख्या लिखी रहती है और किस पर नहीं लिखी रहती। कौन विलायती प्रकाशक पुस्तक का दाम किस पृष्ठ पर छापता है और जब नहीं छापता तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उन्होंने पुस्तकों के अन्य पहलुओं पर भी विचार किया था। मुझे उनकी बातों में बाद में बहुत रस आने लगा। उनके दिमाग में कई योजनाएँ थीं । दुर्भाग्यवश ये कार्यरूप में परिणत होनेसे रह गई।
मैं कह चुका हूँ कि उनसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा ही हुआ था। उतने परिचय को मैं व्यक्तित्व के अध्ययन के लिये पर्याप्त नहीं समझता। फिर हेमचन्द्रका व्यक्तित्व तो अभी कलिका की अवस्था में ही था। फिर मी मुझे लगा कि इस आदमी में एक लापरवाही की मस्ती है।
‘विशाल-भारत ‘में मेरी एक पुस्तक की आलोचना निकली थी। आलोचक महाशय ने पुस्तक के विषय की कोई आलोचना न करके भाषा और शैली की ही निन्दा या प्रशंसा की थी। मुझे इस बात का खेद जरूर था, क्योंकि आलोचना के पांडित्य पर मेरा विश्वास था और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी बातों से गर्भारतापूर्वक विचारने योग्य नहीं समझा है, केवल ऊपरी बातों की चर्चा करके छुट्टी ले ली है। मैंने हेमचन्द्रजी से यह बात कही; उन्होंने आलोचना देखी नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि पुस्तक की कठोर निंदा हुई है और मुझे इसी बात की चिन्ता है। बोले, “परवाह क्या है! यही तो ठीक है। होने दीजिये न निंदात्मक आलोचना। थोड़ी गर्मागर्म चर्चा होनी ही चाहिये।” मैंने उन्हें फिर से अपनी बात समझाई। कहा कि मुझे इस बातका दुख नहीं है कि पुस्तक की निंदा हुई। वह तो कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण बात नहीं, पर विद्वान लोगों की हिन्दी के प्रति उपेक्षाभाव का दुख मुझे जरूर है। वे विषय की गहराईमें जो नहीं उतरते, वह उपेक्षा के कारण ही। गहराई में उतरकर कोई मेरी पुस्तक की धज्जियाँ उडा दे तो भी मैं दुःखित नही होऊंगा। पर उपेक्षा तो समूची हिन्दी-माषी जनता के कल्याण की बाधक है। हेमचन्द्रजी ने मेरी बात ध्यानसे सुनी। और जो बयान दिया यह उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का सुन्दर परिचय है। ” हमलोग यदि ग॔भीर और शक्तिशाली साहित्य लिखेंगे और फिर भी लोग उपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा करनेवाले ही उपेक्षित हो जायेंगे।” मुझे यह वाक्य शायद इसलिये ज्यादा पसन्द आया कि मैं स्वयं भी इसी विचार से सहमत हूँ। जो लोग प्रवर्द्धमान हिन्दी-साहित्य की उपेक्षा कर रहे हैं, वे बुरी तरह उपेक्षित होंगे। हिन्दीका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस भाषाने जो शक्ति अर्जित की है वह किसी राजशक्ति की उँगली पकड़कर नहीं। अपने आपकी शक्ति से निरन्तर शक्तिशाली बननेवाली इस भाषा का आश्रय लिये बिना अब कोई भी हिन्दुस्तानी अपने शान, कर्म या सेवा को देशव्यापी नहीं बना सकता। हेमचन्द्र ने इस सत्यको पाया था। मैं सोचता हूँ कि इतने बडे सत्य का साक्षात्कार अब भी बड़े-बडे विद्वान कहे जानेवाले लोग क्यों नहीं कर पाते ?
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.