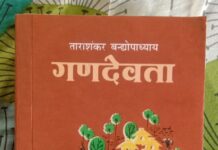— अनामिका सिंह —
यह ललित निबंध संग्रह मात्र नहीं है बल्कि अपने आप में पूरी विविधताओं से भरी हुई दुनिया है। प्रश्नाकुल नीलिमा में विषयों की विविधता, भाषा का सहज प्रवाह, ग्रामीण जीवन का जीवंत चित्रण और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली का प्रभाव यह दर्शाता है कि संजय गौतम की पकड़ अपनी जड़ों पर बहुत मजबूत है। पूरी किताब आकाश पटल पर छाए हुए इंद्रधनुष के समान लगती है जिसके विविध रंग पाठक की चेतना को सराबोर कर देते हैं और उन विषयों पर गंभीरता से सोचने को मजबूर कर देते हैं जो लेखक का अभीष्ट है।
‘प्रश्नाकुल नीलिमा’ पाठक के समक्ष कई प्रश्न रखती है। यह प्रश्नाकुलता आगे चलकर दायित्व बोध में बदल जाती है। पाठक महसूस करता है कि एक सभ्य देश का नागरिक होते हुए भी वह कितना किंकर्तव्यविमूढ़ है। स्वयं को शिक्षित, अभिजात्य और तर्कशील माननेवाला समाज न जाने कितने प्रश्नों को अनदेखा और अनसुना कर अपने में मगन है। लेकिन संजय गौतम उन सभी प्रश्नों के प्रति न केवल सजग हैं बल्कि उनका उत्तर ढूंढ़ने के लिए प्रयासरत भी। उनकी प्रवृत्ति समस्याओं को देखकर आगे बढ़ जाने की नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने की है। संग्रह के निबंध पाठक की चेतना को झिंझोड़ते हैं, सोए हुए दायित्व बोध को जगाने का प्रयास करते हैं।

हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पश्चिमी चकाचौंध और अंग्रेजीयत से ग्रसित होनेवाला सबसे बड़ा तबका यही है। बाकी प्रदेशों की बात करें तो अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने बखूबी सहेजा है। अंग्रेजी प्रभाव के बावजूद वे अपनी भाषा और साहित्य के प्रति सजग हैं। हिंदी प्रदेश की स्थिति ठीक इसके उलट है। भाषाई स्तर पर अंग्रेजी का महिमामंडन इस कदर हुआ है कि उसके सामने हिंदी की चमक खो गई है। महज कुछ जयंतिया और हिंदी दिवस मनाकर हिंदी प्रदेश साहित्य के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है। लेकिन अपने नौनिहालों को हिंदी की समृद्ध परंपरा से वैसे नहीं जोड़ पाता जैसे बंगालियों ने खुद को रवींद्रनाथ या शरतचंद्र से जोड़े रखा है।
संजय गौतम न केवल इस उदासीनता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं बल्कि एक नई शुरुआत का उत्साह भी जगाते हैं। ‘आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के गांव में’ को पढ़ते हुए शुरू में पाठक उसे महज एक यात्रा वृत्तांत या उनकी जयंती मनाने के एक आयोजन के रूप में देखता है। लेकिन निबंध का उत्तरार्ध हिंदी प्रदेश की अपने साहित्यकारों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता की पराकाष्ठा का दुखद रूप प्रस्तुत करता है। कैसे हिंदी के महान साहित्यकार, ललित निबंध के प्रणेता को न केवल हिंदी प्रदेश बल्कि उनका गाँव भी भूल चुका है। जिस आचार्य ने हिंदी का परचम लहराया उसी आचार्य का गाँव उनके साहित्यिक अवदान से अपरिचित तो है ही, महज संयोगवश हुई दुर्घटनाओं के कारण उनकी जयंती मनाने से परहेज भी करता है। ‘आहत सपनों का गान’ प्रवर्तक नवगीतकार ठाकुर प्रसाद सिंह के जीवन संघर्ष के साथ ही उनके रचनात्मक अवदान की गहराई में उतरता है। सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर के प्रति उपेक्षा का ही भाव है कि प्रकृत कवि केदारनाथ सिंह नदी की भेजी चिट्ठियों को तो बाँच लेते हैं लेकिन उनकी अपनी चिट्ठियों को उनके गांव के लोग ही नहीं बाँच पाते। संजय गौतम इस उपेक्षा से आहत तो दिखते हैं पर वो निराश नहीं हैं। उनकी कोशिश सतत जारी है कि जो सूत्र हाथ से छूटते जा रहे हैं उन पर पकड़ मजबूत की जाए और नई पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत के साथ जोड़ा जाए।
‘शिक्षा भूसा तो नहीं’ आजकल के माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाओं पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अभिभावकों के सपनों का बोझ अपने मासूम कंधों पर लादे हुए बच्चों के लिए शिक्षा बोझ बन गई है। आज एक मासूम बच्चे के लिए स्कूल कुछ नया सीखने का स्थान नहीं बल्कि मैराथन दौड़ की ट्रैक बन चुका है जहां किसी भी हाल में उसे बस जीतना है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे विद्यालय बच्चे के मानसिक विकास की सीमा का ध्यान रखे बिना पाठ्यक्रम को जटिल बनाते जा रहे हैं। महत्त्वाकांक्षा के बोझ तले मुरझाते हुए बचपन को लेखक अपने सपनों के टूटने के दर्द से जोड़कर देखता है, वह ऐसी व्यवस्था चाहता था जिसमें भारतीयता और देशी संस्कार व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जहाँ सर्वग्रासी अंग्रेजी के बजाय हिन्दी की प्रधानता हो पर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का मकड़जाल इतना मजबूत है कि एक शिक्षक के रूप में सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं।
अशोक सेकसरिया जी पर लिखा गया संस्मरण ‘कहीं गया नहीं हूं मैं’ संग्रह की उत्कृष्ट और मर्मस्पर्शी रचनाओं में से एक है। उनके व्यक्तित्व के अनेक रूप लेखक की कलम के द्वारा साकार हो उठे हैं। एक अभिभावक, मार्गदर्शक, साहित्य सेवी के रूप में अशोक जी ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है।
सामाजिक और राजनीतिक विद्रूप के ऊपर लेखक की प्रश्नाकुलता अत्यंत गंभीर, सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती चली गई है। ‘कमरे में खिड़की’ अपनी जड़ों से दूर उन प्रवासी मजदूरों के दर्द को बयान करती है जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो हैं लेकिन अपना जीवन गंदी, तंग बस्तियों के दड़बेनुमा घरों में गुजारने को अभिशप्त हैं। हरक्यूलिस की भांति उपभोक्तावादी समाज का भार ढोते श्रमिक महानगर की भीड़ और चकाचौंध के बीच ताजी हवा तक को तरस रहे हैं। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं के पहिए तले आम जनता के कुचले हुए सपनों की कहानी है ‘दुःस्वप्न’ जहां प्रकृति को वश में कर लेने की उद्दाम लालसा अट्टहास करती हुई दिखाई देती है। ‘सपने की ठोकर’, ‘संस्कृति के बन्द दरवाजे’, ‘देवी दर्शन’ पाठक की चेतना को झकझोरते हैं। लोकतंत्र का सतहीपन, गंगा जमुनी तहजीब का अस्त होता सूरज, नारी की असुरक्षा के स्वर यहां मुखर हैं।
व्यंग्यात्मक रचनाओं में लेखक की कलम की धार पैनी और शैली चुटीली हो जाती है। ‘एक दिन का जोग’ तथा ‘ईश्वर अल्ला खतरे में है, बचाओ’ अपनी व्यंग्यात्मकता में परसाई जी की याद दिलाते हैं। व्यावसायिकता और उपभोक्तावाद के इस दौर में योग को भी व्यावसायिक लाभ का साधन बना दिया गया है। पर जो भी हो, एक दिन के जोग ने लगभग विस्मृत हो चुकी इस साधना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तो किया ही है।
‘रामप्रसाद बिस्मिल : बजरिए आत्मकथा’ शौर्य, त्याग और देश के प्रति अटूट प्रेम का दस्तावेज है। इसे पढ़ते हुए पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसी आत्मकथाएं आज पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं हैं? सोशल मीडिया की चकाचौंध में दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण के लिए पाठ्यक्रम में इनका समावेश अत्यंत आवश्यक है।
भाव, भाषा, विषय सभी स्तरों पर ‘प्रश्नाकुल नीलिमा’ के बहुरंगी स्तर हैं। इसकी प्रश्नाकुलता पाठक को सतही वैचारिकता से ऊपर उठकर गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित करती है।
किताब- प्रश्नाकुल नीलिमा; लेखक- संजय गौतम; मूल्य- 250.00; प्रकाशक- इंडिया नेटबुक्स प्राइवेट लिमिटेड, सी-122, सेक्टर 19, नोएडा-201301 फोन-120437693, मो.9873561826
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.