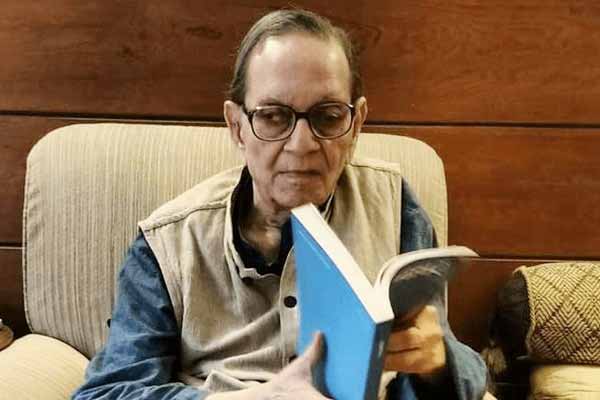— राजकिशोर —
ठीक ही कहा गया है कि समाज में रहनेवाले एक-एक व्यक्ति की जितनी ताकत होती है, समाज की ताकत उसके जोड़ से ज्यादा होती है। दो का बीस गुना गणित में हमेशा चालीस होता है– कम से कम अभी हम ऐसा ही जानते हैं, भविष्य में हो सकता है कि यह जानकारी खंडित हो जाए; लेकिन समाज में यह जोड़ साठ या अस्सी भी हो सकता है। यह अतिरिक्त ताकत समाज में कहाँ से आती है? संभवतः उसकी नैतिक सत्ता से, जो भौतिक सत्ताओं की तुलना में हमेशा ज्यादा आदरणीय और आज्ञा-पालन के योग्य होती है। समाज में यह नैतिक सत्ता न रहे, तो उसकी बात का वजन क्या रह जाएगा?इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ समाज टूट रहा है या प्रभावहीन हो रहा है, वहाँ नैतिक सत्ता भी छीज हो रही है। यह छीजनेवाली सत्ता सामूहिक नैतिकता की है, जिसका स्थान निजी नैतिकताएँ ले सकती हैं या ले रही हैं। इन नैतिकताओं में कुछ अनैतिकताएँ भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ नैतिकता की साझा परिभाषाएँ धूमिल हो रही हों, वहाँ निजी नैतिकता के बारे में फैसला कौन करेगा कि वह नैतिकता है भी या नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज अपनी नैतिक सत्ता का हमेशा नैतिक इस्तेमाल ही करता है। यह इस्तेमाल अनैतिक भी हो सकता है, इसके उदाहरण अनेक हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। कुछ बहुत स्थूल उदाहरण देने हों, तो सती की बाध्यमूलक घटनाओं और अस्पृश्यता का उल्लेख किया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में अंतरजातीय प्रेमी-प्रेमिकाओं के साथ जो क्रूर सलूक हो रहा है, वह भी समाज की नैतिक सत्ता की अभिव्यक्ति नहीं है।
जो बात समाज पर लागू होती है, वह कुछ हद तक भीड़ पर भी लागू होती है। भीड़ भी एक तरह का समाज है या कह लीजिए कि समाज की एक अभिव्यक्ति है। जो लोग समाज बनाते हैं, उन्हीं का एक हिस्सा भीड़ का निर्माण करता है। लेकिन दोनों के बीच एक महत्त्वपूर्ण फर्क है। समाज जैसा भी हो, कम या ज्यादा अनुशासित होता है। इसीलिए वह अपने सदस्यों को भी अनुशासित कर पाता है। वस्तुतः इस अनुशासन के बल पर ही कई तरह के अन्याय जारी रह पाते हैं, तो कुछ दूसरे अन्यायों का प्रतिरोध भी हो पाता है। लेकिन भीड़ स्वभाव से ही निरंकुश होती है।
निस्संदेह सारी भीड़ एक तरह की नहीं होती। रेलवे के प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ एक सामूहिक पहचान भले ही बनाए, पर कुछ घंटों में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी को एक जगह नहीं जाना था और जो लोग एक ही रेलगाड़ी में जाकर बैठ गए हैं, उन्हें भी अलग-अलग स्टेशनों पर उतरना है। कहा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म की यह भीड़ अनेक उपभीड़ों का समुच्चय है। इसके विपरीत, मेले की भीड़, सिनेमा हॉल के सामने की भीड़ या जनसभा की भीड़ प्रायः एकमुखी या एकलक्ष्यीय होती है। प्रायः इसलिए कि भीड़-भाड़ की ऐसी जगहों में ही जेबकतरों, उठाईगीरों तथा औरतों के साथ बदतमीजी करनेवालों की बन आती है। मंदिरों में जूतों की चोरी आम बात है।
सामान्य लक्ष्य होने पर भी, या शायद इसी वजह से, भीड़ में एकात्मकता नहीं होती। लगाव से प्रतिद्वंद्विता का जन्म होता है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी कई बार इतने व्याकुल हो जाते हैं कि एक-दूसरे की देह पर चढ़कर भी अपना लक्ष्य पाने में उन्हें संकोच नहीं होता। इस तरह की धक्कमपेल में हर साल अनेक लोगों की जान जाती है। ‘पहले आप’ की जगह ‘पहले हम’ की प्रवृत्ति का यह एक शोकपूर्ण उदाहरण है। शायद यह अराजकता भीड़ की प्रकृति या संरचना में ही निहित है। ‘भीड़ में अकेला’ को एक दुखमय स्थिति माना जाता है, पर भीड़ में क्या सभी अकेले नहीं होते?जितने एक सामान्य लक्ष्य की ओर उन्मुख उससे ज्यादा अपने निजी लक्ष्य के लिए व्यग्र, जिससे एक प्रकार की अंतरंग शत्रुता पैदा होती है और भीड़ का हर सदस्य सोचता है कि दूसरे लोग भीड़ बढ़ाने चले आए हैं– वे घर पर रहते, तो मेरा काम कितना आसान हो जाता! भीड़ की एक सिफत यह है कि जो ऐसा सोचते हैं, उनमें से कुछ ही घर लौट जाने का फैसला करते हैं, ताकि शेष लोगों की असुविधा कम हो सके। जो डटे रहते हैं, वे भीड़ की अंतर्निहित आक्रामकता को ईंधन मुहैया करने का काम करते हैं। यह ट्रेजडी ही कही जाएगी कि इनमें से अनेक स्वयं इस आक्रामकता की लपटों में घिर जाते हैं। जो आत्मघाती नहीं हुई, वह भीड़ क्या!
इसके साथ ही, मानव स्वभाव की विचित्रता यह है कि जो अपने को अकेला पाते हैं, वे, अकसर, दूसरों के अकेलेपन का अनुभव नहीं करते। क्या अकेलापन भी स्वार्थी होता है? या, स्वार्थीपन ही अकेलेपन का गर्भाशय है?
यह भीड़ का व्यक्तिवादी और कमजोर पक्ष है।
प्रकटतः भीड़ का एक मजबूत और ताकतवर पक्ष भी होता है। यह पक्ष तब सामने आता है, जब भीड़ उन्मादग्रस्त हो। यह उन्माद सांप्रदायिक भी हो सकता है, जातिवादी भी और विचारधारा से चालित भी। ध्यान से देखा जाए, तो इन सबका चरित्र एक ही है, जिसे बहुत संक्षेप में फासिस्ट कहा जा सकता है। फासिज्म का लक्षण यह दुष्ट विचार है कि हम बड़ी तादाद में हैं और संगठित हैं तथा झुंड बल से अपनी बात मनवा कर रहेंगे। सारी जुल्मी भीड़ें ऐसी ही होती हैं। यहाँ भीड़ का जो लक्ष्य होता है, वही लक्ष्य भीड़ में शामिल हर शख्स का होता है, इसलिए उनमें प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। या, होती है, तो यह दिखाने की कि कौन कितने दुस्साहस या क्रूरता का परिचय दे सकता है।
जैसे हर कायर दूसरे कायर से ज्यादा तेज रफ्तार से भागने की कोशिश करता है, वैसे ही भीड़ में शामिल हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने को ज्यादा दम-खम वाला साबित करने की कोशिश करता है। इससे भीड़ में साहस और उत्साह का, दोनों ही बुरे अर्थों में, संचार होता है। भीड़ के सदस्यों की एकलक्ष्यीयता उन्हें जोड़ती है और संगठित करती है, तो दुस्साहस की प्रतिद्वंद्विता भीड़ की ताकत को उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है जितनी उसमें मूलतः होती है। सच पूछा जाए तो वीर और क्रूर का फर्क यहीं प्रकट होता है।
वीर अकेले में भी वीर ही होता है, जबकि क्रूर अकसर अकेले में कायर होता है, पर अपने जैसों के समूह में उसकी क्रूरता, तीव्रतर और मुखर हो उठती है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान मानव स्वभाव की जो बीभत्सताएँ प्रकट होती हैं, उनका उत्स भीड़ का यह उन्मादी स्वभाव ही है। मानव स्वभाव की शायद ही कोई अच्छाई हो, जो इस तरह की ‘मारो-काटोवाली’भीड़ में प्रकट होती हो।
यह सामूहिकता का अश्लील पक्ष है। यह पक्ष अकसर बहुसंख्यकवाद में प्रकट होता है, जो लोकतंत्र के लिए एक सतत खतरा है। लेकिन मौका पड़ने पर अल्पसंख्यक समूह भी इससे मुक्त नहीं रह पाते। कहा जा सकता है कि ऐसे अवसर उन्हीं स्थानों पर और ऐसे ही समय आते हैं, जहाँ और जब अल्पसंख्यकों की हैसियत बहुसंख्यक जैसी हो जाती है। क्रूरता पर समाज के किसी भी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होता, यद्यपि हम अल्पसंख्यकों की हिंसा को बहुसंख्यकों की हिंसा से अलगा कर एक प्रतिक्रियामूलक कार्रवाई के रूप में देखते हैं। इसका उद्देश्य उसका औचित्य प्रमाणित करना नहीं, बल्कि उस श्रृंखला को समझना है जिससे हिंसा-प्रतिहिंसा की आग भड़कती जाती है।
जैसे नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, वैसे ही उन्मादग्रस्त भीड़ किसी भी हद तक जा सकती है। नशा आदमी का रासायनिक संतुलन बिगाड़ देता है (मद्यप मित्रों की भावनाओं का खयाल रखकर कहा जा सकता है कि बिगाड़ नहीं, बदल देता है, जिसका अच्छा और बुरा दोनों अर्थ हो सकता है), उन्माद तब पैदा होता है जब किसी विचार या भावना की उग्रता के परिमाणस्वरूप ये संतुलन विकृत होता जाता है। पहली स्थिति में नशे से मन बदलता है, दूसरी स्थिति में मानसिक बदलाव से नशा पैदा होता है। बाबरी मस्जिद का ध्वंस करनेवाले इसी नशे के शिकार थे।
लेकिन उनका उन्माद एक ऐसी स्थिति में फलीभूत हुआ, जब पूरा वातावरण उनके अनुकूल था। वे जानते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं, उसकी सजा उन्हें नहीं भुगतनी पड़ेगी। राज्य की सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी थी। सीआरपीएफ केंद्र द्वारा भेजी गयी थी, पर वह राज्य शासन की अनुमति बगैर हरकत में नहीं आ सकती थी। क्रूरता हमेशा सुरक्षित वातावरण खोजती है। इसकी तुलना 1991 की अयोध्यावादी भीड़ से करें, जब ‘मौलाना’ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और शासन के आदेश से गोली चली थी, तो बात और साफ हो जाएगी। तब दो-चार ध्वंसमार्गी परिषदियों को गोली लगते ही राम मंदिर का निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध भीड़कों में भगदड़ मच गयी थी।
दरअसल, उन्हें जान लेने की ट्रेनिंग दी गयी थी, जान देने की नहीं। इससे पता चलता है कि एकलक्ष्यीय उन्मत्त भीड़ प्रकटतः जितनी ताकतवर दिखाई दे, अंततः वह भी कायर ही होती है। जैसे पुलिस को देखकर बहुत से नशेड़ियों का नशा हिरन हो जाता है, वैसे ही वास्तविक खतरा आने पर उन्मादग्रस्त भीड़ भी उलटे पाँव दौड़ने लगती है। अयोध्यावासियों की गत सप्ताह की भीड़ में इसके तत्त्व देखे जा सकते हैं।
जो लोग महात्मा गांधी को इसलिए दोषी मानते हैं कि चौरी-चौरा कांड के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, वे यह देख नहीं पाते कि भीड़ के हिंसक, अराजक और कायर स्वभाव को हमारे देश में सबसे पहले गांधीजी ने ही पहचाना था।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.