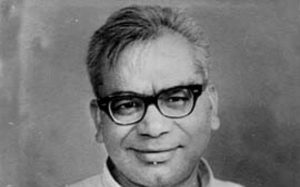
कृष्ण की सभी चीजें दो हैं : दो माँ, दो बाप, दो नगर, दो प्रेमिकाएँ या यों कहिए अनेक। जो चीज संसारी अर्थ में बाद की या स्वीकृत या सामाजिक है, वह असली से भी श्रेष्ठ और अधिक प्रिय हो गई है। यों कृष्ण देवकीनन्दन भी हैं, लेकिन यशोदानन्दन अधिक। ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कृष्ण की असली माँ, पेट-माँ का नाम न जानते हों, लेकिन बाद वाली दूध वाली, यशोदा का नाम न जानने वाला कोई निराला ही होगा। उसी तरह, वसुदेव कुछ हारे हुए से हैं, और नन्द को असली बाप से कुछ बढ़कर ही रुतबा मिल गया है। द्वारका और मथुरा की होड़ करना कुछ ठीक नहीं, क्योंकि भूगोल और इतिहास ने मथुरा का साथ दिया है। किन्तु यदि कृष्ण की चले, तो द्वारका और द्वारकाधीश, मथुरा और मथुरापति से अधिक प्रिय रहे। मथुरा से तो बाललीला और यौवन-क्रीड़ा की दृष्टि से, वृन्दावन और बरसाना वगैरह अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रेमिकाओं का प्रश्न जरा उलझा हुआ है। किसकी तुलना की जाए, रुक्मिणी और सत्यभामा की, राधा और रुक्मिणी की, या राधा और द्रौपदी की। प्रेमिका शब्द का अर्थ संकुचित न कर सखा-सखी भाव को ले के चलना होगा। अब तो मीरा ने भी होड़ लगानी शुरू की है। जो हो, अभी तो राधा ही बड़भागिनी है कि तीन लोक का स्वामी उसके चरणों का दास है। समय का फेर और महाकाल शायद द्रौपदी या मीरा को राधा की जगह एक पहुँचाए, लेकिन इतना संभव नहीं लगता। हर हालत में, रुक्मिणी राधा से टक्कर कभी नहीं ले सकेगी।
मनुष्य की शारीरिक सीमा उसका चमड़ा और नख हैं। यह शारीरिक सीमा, उसे अपना एक दोस्त, एक माँ, एक बाप, एक दर्शन वगैरह देती रहती है। किन्तु समय हमेशा इस सीमा से बाहर उछलने की कोशिश करता रहता है, मन ही के द्वारा उछल सकता है।
कृष्ण उसी तत्त्व और महान् प्रेम का नाम है जो मन को प्रदत्त सीमाओं से उलाँघता-उलाँघता सबमें मिला देता है, किसी से भी अलग नहीं रखता।
क्योंकि कृष्ण तो घटनाक्रमों वाली मनुष्य लीला है, केवल सिद्धांतों और तत्त्वों का विवेचन नहीं, इसलिए उसकी सभी चीजें अपनी और एक की सीमा में न रहकर दो और निरापनी हो गयी हैं। यों दोनों में ही कृष्ण का तो निरापना है, किन्तु लीला के तौर पर अपनी माँ, बीवी और नगरी से परायी बढ़ गयी है। परायी को अपनी से बढ़ने देना भी तो एक मानी में अपनेपन को खतम करना है। मथुरा का एकाधिपत्य खतम करती है द्वारका, लेकिन उस क्रम में द्वारका अपना श्रेष्ठत्व जैसा कायम कर लेती है।
भारतीय साहित्य में माँ हैं यशोदा और लला है कृष्ण। माँ-लला का इनसे बढ़कर मुझे तो कोई संबंध मालूम नहीं, किन्तु श्रेष्ठत्व भर ही तो कायम होता है। मथुरा हटती नहीं और न रुक्मिणी, जो मगध के जरासंध से लेकर शिशुपाल होती हुई हस्तिनापुर के द्रौपदी और पाँच पांडवों तक एक-रूपता बनाये रखती है। परकीया स्वकीया से बढ़कर उसे खतम तो करती नहीं, केवल अपने और पराये की दीवारों को ढहा देती है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय इत्यादि की चहारदीवारी से अपना या स्वकीय छुटकारा पा जाता है। सब अपना और अपना सब हो जाता है। बड़ी रसीली लीला है कृष्ण की, इस राधा-कृष्ण या द्रौपदी–सखा और रुक्मिणी–रमण की कहीं चर्म सीमित शरीर में, प्रेमानन्द और खून की गर्मी और तेजी में, कमी नहीं। लेकिन यह सब रहते हुए भी कैसा निरापना।
कृष्ण है कौन? गिरधारी, गिरधर गोपाल! वैसे तो मुरलीधर और चक्रधर भी है, लेकिन कृष्ण का गुह्यतम रूप तो गिरधर गोपाल में ही निरखता है। कान्हा को गोवर्धन पर्वत अपनी कानी उँगली पर क्यों उठाना पड़ा? इसलिए न कि उसने इन्द्र की पूजा बंद करवा दी और इन्द्र का भोग, खुद खा गया, और भी खाता रहा। इन्द्र ने नाराज होकर पानी, ओला, पत्थर बरसाना शुरू किया, तभी तो कृष्ण को गोवर्धन उठाकर अपने गो और गोपालों की रक्षा करनी पड़ी। कृष्ण ने इन्द्र का भोग खुद क्यों खाना चाहा?
यशोदा और कृष्ण का इस संबंध में गुह्य विवाद है। माँ, इन्द्र का भोग लगाना चाहती है, क्योंकि वह बड़ा देवता है, सिर्फ वास से ही तृप्त हो जाता है, और उसकी बड़ी शक्ति है, प्रसन्न होने पर बहुत वर देता है और नाराज होने पर तकलीफ। बेटा कहता है कि वह इन्द्र से भी बड़ा देवता है, क्योंकि वह तो वास से तृप्त नहीं होता और बहुत खा सकता है और उसके खाने की कोई सीमा नहीं है। यही है कृष्ण-लीला का गुह्य-रहस्य। वास लेने वाले देवताओं से खाने वाले देवताओं तक की भारत-यात्रा ही कृष्ण लीला है।
कृष्ण के पहले, भारतीय देव, आसमान के देवता हैं। निस्संदेह अवतार कृष्ण के पहले से शुरू हो गये। किंतु त्रेता का राम ऐसा मनुष्य है जो निरंतर देव बनने की कोशिश करता रहा। इसीलिए उसमें आसमान के देवता का अंश कुछ अधिक है।
द्वापर का कृष्ण ऐसा देव है, जो निरंतर मनुष्य बनने की कोशिश करता रहा। उसमें उसे संपूर्ण सफलता मिली। कृष्ण संपूर्ण और अबोध मनुष्य है, खूब खाया-खिलाया, खूब प्यार किया और प्यार सिखाया, जनगण की रक्षा की और उसका रास्ता बताया, निर्लिप्त भोग का महान् त्यागी और योगी बना।
इस प्रसंग में यह प्रश्न बेमतलब है कि मनुष्य के लिए, विशेषकर राजकीय मनुष्य के लिए राम का रास्ता सुकर और उचित है या कृष्ण का। मतलब की बात तो यह है कि कृष्ण देव होता हुआ निरंतर मनुष्य बनता रहा। देव और निस्व और असीमित होने के नाते कृष्ण में जो असंभव मनुष्यताएँ हैं, जैसे झूठ, धोखा और हत्या, उनकी नकल करने वाले लोग मूर्ख हैं, उसमें कृष्ण का क्या दोष। कृष्ण की संभव और पूर्ण मनुष्यताओं पर ध्यान देना ही उचित है, और एकाग्र ध्यान। कृष्ण ने इन्द्र को हराया, वास लेने वाले देवों को भगाया, खाने वाले देवों को प्रतिष्ठित किया, हाड़, खून, मांस वाले मनुष्य को देव बनाया, जन-गण में भावना जागृत की कि देव को आसमान में मत खोजो, खोजो यहीं अपने बीच, पृथ्वी पर। पृथ्वी वाला देव खाता है, प्यार करता है, मिलकर रक्षा करता है।
कृष्ण जो कुछ करता था, जमकर करता था, खाता था जमकर, प्यार करता था जमकर, रक्षा भी जमकर करता था : पूर्ण भोग, पूर्ण प्यार, पूर्ण रक्षा। कृष्ण की सभी क्रियाएँ उसकी शक्ति के पूरे इस्तेमाल से ओत-प्रोत रहती थीं, शक्ति का कोई अंश बचाकर नहीं रखता था, कंजूस बिलकुल नहीं था, ऐसा दिलफेंक, ऐसा शरीरफेंक चाहे मनुष्यों से संभव न हो, लेकिन मनुष्य ही हो सकता है, मनुष्य का आदर्श, चाहे जिसके पहुँचने तक हमेशा एक सीढ़ी पहले रुक जाना पड़ता हो। कृष्ण ने खुद गीत गाया है स्थितप्रज्ञ का, ऐसे मनुष्य का जो अपनी शक्ति का पूरा और जमकर इस्तेमाल करता हो। “कूर्मोअंगानीव” ने बताया है ऐसे मनुष्यों को। कछुए की तरह यह मनुष्य अपने अंगों को बटोरता है, अपनी इन्द्रियों पर इतना संपूर्ण प्रभुत्व है इसको कि इन्द्रियार्थों से उन्हें पूरी तरह हटा लेता है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो भोग का उलटा हुआ। ऐसी बात नहीं। जो करना, जमकर भोग भी, त्याग भी। जमा हुआ भोगी कृष्ण, जमा हुआ योगी तो था ही। शायद दोंनों में विशेष अंतर नहीं। फिर भी, कृष्ण ने एकांगी परिभाषा दी, अचल स्थितप्रज्ञ की, चलस्थित प्रज्ञ की नहीं। उसकी परिभाषा तो दी जो इन्द्रियार्थों से इन्द्रियों को हटाकर पूर्ण प्रभुता निखरता हो, उसकी नहीं, जो इन्द्रियों को इन्द्रियार्थों में लपेटकर, घोलकर। कृष्ण खुद तो दोनों था, परिभाषा में एकांगी रह गया।
जो काम जिस समय कृष्ण करता था, उसमें अपने समग्र अंगों का एकाग्र प्रयोग करता था, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाता था, अपना तो था ही नहीं कुछ उसमें। “कूर्मोअंगानीव” के साथ-साथ “समग्र-अंग-एकाग्री” भी परिभाषा में शामिल होना चाहिए था। जो काम करो, जमकर करो, अपना पूरा मन और शरीर उसमें फेंक कर।
देवता बनने की कोशिश में मनुष्य कुछ कृपण हो गया है, पूर्ण आत्मसमर्पण वह कुछ भूल-सा गया है। जरूरी नहीं है कि वह अपने-आप को किसी दूसरे के समर्पण करे। अपने ही कामों में पूरा आत्मसमर्पण करे। झाड़ू लगाए तो जमकर, या अपनी इन्द्रियों का पूरा प्रयोग कर युद्ध में रथ चलाये तो जमकर, श्यामा मालिन बनकर राधा को फूल बेचने जाए तो जमकर, जीवन का दर्शन ढूँढ़े और गाए तो जमकर। कृष्ण ललकारता है मनुष्य को अकृपण बनने के लिए, अपनी शक्ति को पूरी तरह और एकाग्र उछालने के लिए। मनुष्य करता कुछ है, ध्यान कुछ दूसरी तरफ रहता है। झाड़ू देता है फिर भी कूड़ा कोनों में पड़ा रहता है।
एकाग्र ध्यान न हो तो सब इन्द्रियों का अकृपण प्रयोग कैसे हो। “कूर्मोअंगानीव” और “समग्र-अंग-एकाग्री”मनुष्य को बनना है। यही तो देवता की मनुष्य बनने की कोशिश है। देखो, माँ, इन्द्र खाली वास लेता है, मैं तो खाता हूँ।
आसमान के देवताओं को जो भाग्य उसे बड़े पराक्रम और तकलीफ के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी कृष्ण को पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उँगली पर उठाना पड़ा। इन्द्र को वह नाराज कर देता और अपनी गउओं की रक्षा न करता, तो ऐसा कृष्ण किस काम का। फिर कृष्ण के रक्षा-युग का आरंभ होने वाला था। एक तरह से बाल और युवा-लीला का शेष ही गिरिधर लीला है। कालिया-दहन और कंस वध उसके आसपास के हैं। गोवर्धन उठाने में कृष्ण की उँगली दूखी होगी, अपने गोपों और सखाओं को कुछ झुँझलाकर सहारा देने को कहा होगा। माँ को कुछ इतराकर उँगली दूखने की शिकायत की होगी। गोपियों से आँख लड़ाते हुए अपनी मुसकान द्वारा कहा होगा। उसके पराक्रम पर अचरज करने के लिए राधा और कृष्ण की तो आपस में गंभीर और प्रफुल्लित मुद्रा रही होगी। कहना कठिन है कि किसकी ओर कृष्ण ने अधिक निहारा होगा, माँ की ओर इतराकर, या राधा की ओर प्रफुल्ल होकर। उँगली बेचारे की दुख रही थी। अब तक दुख रही है, गोवर्धन में तो यही लगता है। वहीं पर मानस गंगा है। जब कृष्ण ने गऊ वंश रूपी दानव को मारा था, राधा बिगड़ पड़ी और इस पाप से बचने के लिए उसने उसी स्थल पर कृष्ण से गंगा माँगी। बेचारे कृष्ण को कौन-कौन से असंभव काम करने पड़े हैं। हर समय वह कुछ न कुछ करता रहा है दूसरों को सुखी बनाने के लिए। उसकी उँगली दुख रही है। चलो, उसको सहारा दें। गोवर्धन में सड़क चलते कुछ लोगों ने, जिनमें पंडे होते ही हैं, प्रश्न किया कि मैं कहाँ का हूँ?
मैंने छेड़ते हुए उत्तर दिया, राम की अयोध्या का।
पंडों ने जवाब दिया, सब माया एक है।
जब मेरी छेड़ चलती रही तो एक ने कहा कि आखिर सत्तू वाले राम से गोवर्धन वासियों का नेह कैसे चल सकता है। उनका दिल तो माखन-मिसरी वाले कृष्ण से लगा है।
माखन-मिसरी वाला कृष्ण, सत्तू वाला राम कुछ सही है, पर उसकी अपनी उँगली अब तक दूख रही है।
एक बार मथुरा में सड़क चलते एक पंडे से मेरी बातचीत हुई। पंडों की साधारण कसौटी से उस बातचीत का कोई नतीजा न निकला, न निकलने वाला था। लेकिन क्या मीठी मुसकान से उस पंडे ने कहा कि जीवन में दो मीठी बात ही तो सब कुछ है। कृष्ण मीठी बात करना सीख गया है, आसमान वाले देवताओं को भगा गया है, माखन-मिसरी वाले देवों की प्रतिष्ठा कर गया है। लेकिन उसका अपना कौन-कौन सा अंग अब तक दूख रहा है।
कृष्ण की तरह एक और देवता हो गया है, जिसने मनुष्य बनने की कोशिश की। उसका राज्य संसार में अधिक फैला। शायद इसलिए कि वह गरीब बढ़ई का बेटा था और उसकी अपनी जिंदगी में वैभव और ऐश न था, शायद इसलिए कि जन-रक्षा का उसका अंतिम काम ऐसा था कि उसकी उँगली सिर्फ न दूखी, उसके शरीर का रोम-रोम सिहरा और अंग-अंग टूटकर वह मरा। अब तक लोग उसका ध्यान करके अपने सीमा बाँधने वाले चमड़े के बाहर उछलते हैं। हो सकता है कि ईसूमसीह दुनिया में केवल इसलिए फैल गया है कि उसका विरोध उन रोमियों से था जो आज की मालिक सभ्यता के पुरखे हैं। ईसू रोमियों पर चढ़ा। रोमी आज के यूरोपियों पर चढ़े। शायद एक कारण यह भी हो कि कृष्ण-लीला का मजा ब्रज और भारत भूमि के कण-कण से इतना लिपटा है कि कृष्ण की नियति कठिन है। जो भी हो, कृष्ण और क्रिस्टोस दोनों ने आसमान के देवताओं को भगाया। दोनों के नाम और कहानी में भी कहीं-कहीं सादृश्य है। कभी दो महाजनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। दोनों अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है। फिर भी, क्रिस्टोस प्रेम के आत्मोत्सर्गी अंग के लिए बेजोड़ और कृष्ण संपूर्ण मनुष्य-लीला के लिए। कभी कृष्ण के वंशज भारतीय शक्तिशाली बनेंगे, तो संभव है उसकी लीला दुनिया भर में रस फैलाए।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


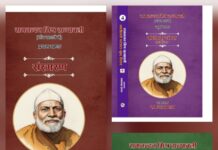

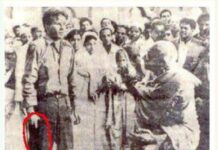













शुक्रिया..