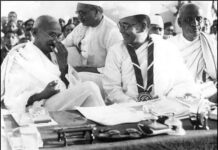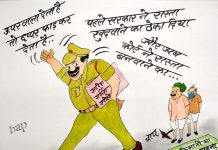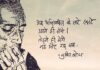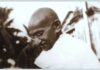— डॉ. राममनोहर लोहिया —
किसी पंथ या विचारधारा पर विचार करते समय आमतौर पर हमारी नजर अंतिम लक्ष्य पर जाती है। मार्क्सवाद के भी अपने अंतिम लक्ष्य हैं। इनमें मानव जाति के भविष्य के संबंध में, यदि यह विचारधारा लागू हुई तो, बहुत कर्णमधुर वाक्य कहे गए हैं, जैसे : आदमी द्वारा आदमी का शोषण समाप्त होगा, आदमी के व्यक्तित्व का विकास मानव-जाति के विकास की जरूरी शर्त है, आदमी पर शासन नहीं करेगा किंतु वस्तुएँ शासित होंगी। ये सब ऊँचे और कानों में बजने वाले वाक्य हैं। किंतु यदि हम अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो क्रोपोटकिन, मार्क्स, गांधी और एडम स्मिथ तक सब एक ही परिवार के चिंतक ठहरेंगे क्योंकि इन सबने ऐसी स्थिति की कल्पना की जिसमें मानव-जाति को शोषण से मुक्ति मिले और शांति स्थापित हो और जिसमें सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण इस प्रकार हो कि मानव-व्यक्तित्व का विकास हो सके।
अतः किसी विचारधारा को समझने के लिए विशेषकर मार्क्सवाद को समझने के लिए हमें अंतिम लक्ष्य के बजाय उस तक पहुंचने की विधि या उसके विश्लेषण का अध्ययन करना चाहिए। मार्क्सवाद के प्रति एक विशेष प्रकार के मन और विशाल जनता का आकर्षण इसलिए है कि इसने पूंजीवाद का जो विश्लेषण किया वह निश्चित रूप से उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। एक प्रकार से यह नियति का आदेश है कि ऐसा ही होगा और इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। पूंजीवाद का विश्लेषण करते समय मार्क्स ने मानव-विकास के कुछ आधार बताए जो किसी मानव-इच्छा पर निर्भर नहीं हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और इसलिए वे अंततः वह स्थिति बनाएंगे जिसकी कल्पना मार्क्स या अन्य व्यक्तियों ने की। मार्क्सवाद का विचित्र आकर्षण इस बात में है कि इसकी अनिवार्य सफलता किसी व्यक्ति या पार्टी की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। यह पूंजीवाद के विकास में ही निहित है और नियति के आदेश की तरह मानव-जाति उस स्थिति को प्राप्त करेगी जिसका वर्णन मार्क्सवाद साम्यवाद के रूप में करता है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख भाग पूंजीवाद के इस विकास से ही संबंधित है। पूंजीवादी विकास के कुछ नियमों की खोज की गई है। अतः मार्क्सवाद को समझने के लिए पूंजीवादी विकास के इन नियमों की सरसरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी होगा।
मार्क्स इस बात से शुरू करता है कि मानव-श्रम के, अन्य वस्तुओं से भिन्न, दो मूल्य होते हैं, एक उपयोग-मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। मैं जटिल शब्दावली का प्रयोग नहीं करूंगा, जब तक कि यह बहुत जरूरी नहीं होगा। मानव-श्रम के दो मूल्य होते हैं। एक तो वह जो श्रमिक को मजदूरी के रूप में मिलता है और दूसरा वह जो कुछ उत्पादन के हिस्से के रूप में मालिक को मिलता है। ये दोनों मूल्य भिन्न-भिन्न हैं। श्रमिक को वह सब नहीं मिलता जिसे वह पैदा करता है और इसलिए श्रम के परिणाम (उत्पादन) और श्रमिक की मजदूरी के बीच अंतर रहता है अर्थात् वह हिस्सा जो मजदूर को मजदूरी के रूप में मिलता है और वह हिस्सा जो मालिक को लाभ के रूप में मिलता है। इन दोनों के बीच के अंतर को मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। इस विभाजन के कारण हर मालिक या नियोक्ता श्रम के कुछ उत्पादन का एक हिस्सा अपने लिए ले लेता है।
अतिरिक्त मूल्य की इस कल्पना के साथ मार्क्स यह दिखाता है कि पूंजीवाद अपनी पूंजी में वृद्धि करते-करते श्रमिक वर्गों में ऐसी स्थितियां पैदा करता है जो पूंजीवाद को नष्ट करने वाली होती हैं। मालिक लाभ कमाता है उससे नए कारखाने लगाता है, पहले से बड़ा और नया कारखाना। अधिकाधिक पूंजी निवेश से बड़ी-बड़ी मशीनों को लगाना संभव होता है जिनमें श्रमिकों का हिस्सा उत्तरोत्तर कम होता जाता है और पूंजीपति का हिस्सा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसका परिणाम होता है कि एक तरफ पूंजी का भारी संचय हो जाता है और दूसरी तरफ श्रमिक-वर्ग की गरीबी बढ़ती जाती है और साथ ही श्रमिकों का समाजीकरण भी बढ़ता जाता है। अधिकाधिक पूंजी, अधिकाधिक निर्धनता और अधिकाधिक समाजीकरण के तीन कारक एक साथ काम करते लगते हैं।
इसके अतिरिक्त मार्क्सवाद पूंजीवादी विकास के एक और नियम का जिक्र करता है। श्रमिक वर्गों की बढ़ती निर्धनता और उत्पादकों द्वारा अपने सारे उत्पादन की बिक्री न कर पाने के कारण जिसकी वजह भी श्रमिकों की निर्धनता के कारण उनकी क्रय शक्ति का ह्रास होता है, एक संकट पैदा होता है। इस संक्रमणकालीन संकट को व्यापार संकट कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी के अलावा व्यापार संकट पैदा होता है : व्यापार घट जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है और उद्योगों में मंदी आती है। इस प्रकार के औद्योगिक संकट लोभ की वजह से बढ़ते जाते हैं और तब पूंजीवाद का व्यापक संकट पैदा होता है। बार-बार आने वाले औद्योगिक संकटों के कारण पूंजीवाद का व्यापक संकट आता है ठीक अतिरिक्त मूल्य की वजह से। सारा उत्पादित माल बिक नहीं पाता, इसलिए मंदी अवश्य पैदा होगी।
इसके बाद मार्क्स एक और नियम पर आता है जिसमें पूंजीवाद के पतन का आलंकारिक भाषा में वर्णन किया जाता है जिसकी मुख्य बात यह है कि पूंजीवाद अपने विकास की प्रक्रिया में अपनी कब्र खोदने वाले को, अपने अजेय शत्रु को जन्म देता है। अपने विकास में, अपनी संभावनाओं और क्षेत्रों को बढ़ाते हुए वह सर्वहारा वर्ग की सेना तैयार करता है जो बड़े-बड़े कारखानों में एक साथ काम करते हैं। उन्हें अपने धन और अपनी संपत्ति से वंचित किया जाता है और उनकी हालत बिगड़ती जाती है, इसलिए उनके और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष चलने लगता है। यह संघर्ष किसी की इच्छा से नहीं चलता क्योंकि पूंजीवादी विकास में इच्छा भी स्थितियों से निर्देशित होती है। इच्छा करने वाले कुछ व्यक्ति होंगे, संघर्ष में हिस्सा लेने वाले लोग होंगे और सर्वहारा के ग्रुप या पार्टियां होंगी जो सर्वहारा को संगठित होने के लिए कहेंगी। यह कुछ ऐसा होगा जिससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि सर्वहारा की संख्या लगातार बढ़ रही होगी। यह वर्ग अपना समाजीकरण करेगा और उसके रहन-सहन का स्तर भी गिरता जाएगा और इस प्रकार पूंजीवाद अपनी कब्र खोदने वालों को स्वाभाविक रूप से तैयार करता जाएगा, और फिर एक समय आएगा जब यह वर्ग पूंजीवाद के व्यापक संकट के समय उसे ऐसा धक्का देगा कि वह खत्म हो जाएगा, संगठित मजदूर वर्ग उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर देगा, उसके कारखानों आदि उत्पादन साधनों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। यहां फिर कानों में बजने वाले वाक्य का प्रयोग हुआ है :शोषणकारियों को संपत्ति से वंचित किया जाएगा।
अब उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों की चर्चा की जाए। उत्पादन की शक्तियों का मतलब है कारखाने, मशीनीकृत फार्म आदि जो कृषि तथा उद्योगों पर विज्ञान के प्रयोगों का फल है। उत्पादन की ये असंख्य मशीनें और औजार विज्ञान के प्रयोग के परिणाम हैं। ये उत्पादन की शक्तियां हैं। उत्पादन-संबंधों का मतलब है मालिक-मजदूरों के बीच या किसान-जमींदार के बीच संपत्ति के संबंध। पूंजीपति-मजदूर संबंधों के टकराव में उत्पादन-शक्तियों और उत्पादन-संबंधों का टकराव निहित है। उत्पादन शक्तियाँ लगातार वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण बढ़ती जाती हैं जबकि उत्पादन-संबंध उत्पादन-शक्तियों के रास्ते में बाधक बनते हैं और उन्हें अपनी पूर्णता में विकसित नहीं होने देते क्योंकि पूंजीपति राष्ट्र के वार्षिक उत्पादन का हिस्सा अपने पास रख लेता है और इससे संकट पैदा होता है। उत्पादन-संबंध वृद्धि में सतत बाधा उपस्थित करते हैं, शाश्वत तथा सतत वृद्धि उत्पादन-शक्तियों की, और इससे टकराव इतना बढ़ जाता है कि कवच ध्वस्त हो जाता है। मार्क्स ने इसे समूचा खोल कहा है जिसमें उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के साधन दोनों सम्मिलित हैं। तब संपत्ति, स्वामित्व के संबंध मौलिक रूप में बदल जाते हैं, नए संबंध बनते हैं और उत्पादन-शक्तियों का सहज ढंग से विकास होने लगता है।
पूँजीपतियों को संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है। सामंती अवशेषों को भी संपत्ति से वंचित किया जाता है। श्रमिक वर्ग कुल उत्पादन से अपना हिस्सा ले सकता है, बिना अतिरिक्त मूल्य के रूप में उसे किसी को दिए। औद्योगिक मंदी और व्यापक मंदी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। राष्ट्र में जो भी उत्पादन साल में होता है वह तो बिक जाता है या सामाजिक निवेश में चला जाता है। इस प्रकार जब शोषणकारियों को संपत्ति से वंचित किया जाता है तो मानव-जाति उस अवस्था को प्राप्त करती है जब आदमी के द्वारा आदमी का शोषण समाप्त हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का विकास सारे समाज के विकास का कारण बनता है, जहाँ आदमी को किसी शासक की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ वस्तुओं का प्रबंध करना पड़ता है।
मार्क्स द्वारा पूंजीवाद के विश्लेषण का संक्षेप में यही स्वरूप है। यह सारांश है। केंद्रीय विचार है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि भारत में कुछ लोग हैं जो मार्क्सवाद को उलझाकर अस्पष्ट प्रकार की बातें करते हैं और क्रांति की सामान्य भावनाएं जगाते हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि मार्क्सवादी सिद्धांत का सार पूंजीवादी विकास के इस विश्लेषण में हैं कि कैसे प्रशासन और सरकारों के कानूनों से बड़ी शक्ति इस प्रक्रिया में है। पूंजीवाद के सामाजिक नियम की यह मूल शक्ति ही समाज की वह तस्वीर बनाती है जिसकी कल्पना मार्क्स और एंगेल्स ने की। यदि पूंजीवादी विकास का यह विश्लेषण सही है तो मार्क्स और एंगेल्स की भविष्यवाणियाँ कितनी ही गलत क्यों न सिद्ध हों, यह विश्लेषण हमें आचरण और कर्म का मजबूत आधार देता है जिसके आगे हम अपनी सारी शक्ति तथा साधनों को समर्पित कर सकते हैं। किंतु क्या यह ठोस रूप से सही है?
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.