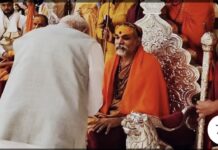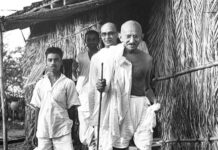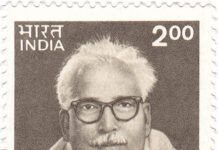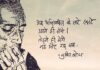— सत्यनारायण साहु —
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने हाल में एक विवादास्पद लेख लिखा, जिसे एक प्रमुख बिजनेस अखबार ने, हैरत की बात है कि किसी और दिन नहीं, स्वाधीनता दिवस पर ही प्रकाशित किया। देबराय अपने उस लेख में शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के एक अध्ययन का हवाला देते हैं, जो कहता है कि 1789 से दुनिया भर में लिखित संविधानों की ‘औसत आयु’ 17 साल रही है। वर्ष 2009 के इस अध्ययन के आधार पर देबराय यह निष्कर्ष पेश करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपने संविधान को अलविदा कह दे और उसकी जगह नया संविधान लाए।
शिकागो लॉ स्कूल का अध्ययन यह हरगिज नहीं कहता कि लिखित संविधान को फिर से लिखना या उसके स्थान पर नए संविधान बनाना हमारा लक्ष्य या आदर्श होना चाहिए। दरअसल, यह अध्ययन वो वजहें बताता है कि क्यों अनेक संविधान ‘अल्पप्राण’ हैं और ऐसे पहलुओं की व्याख्या करता है जो उन संविधानों को दीर्घजीवी बना सकते हैं। उपर्युक्त अध्ययन के मुताबिक ऐसे तीन पहलू हैं – समावेशिता, अनुकूलन-क्षमता और विशिष्टता, जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई लिखित संविधान अल्पजीवी होगा या दीर्घजीवी।
मसलन, यह अध्ययन कहता है, “जहाँ तक समावेशिता की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता की अभिपुष्टि अधिक टिकाऊ संविधान देती है, लेकिन तानाशाही व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता।” दूसरे शब्दों में, संवैधानिक प्रक्रिया में सहभागिता जितनी अधिक होगी, संविधान उतना ही दीर्घजीवी होगा। दूसरे, आखिरकार किसी देश के लोग ही यह तय कर सकते हैं कि उनके देश के संविधान की आयु कितनी होगी। इसके अलावा, “संवैधानिक मानदंडों का सामूहिक क्रियान्वयन” तानाशाही के बजाय लोकतंत्र में बेहतर होता है।
तीसरे, एक लिखित संविधान में संशोधन आसान है या कठिन, इस पर भी उसकी दीर्घजीविता निर्भर करती है। और जिन संविधानों का दायरा बड़ा होता है वे दीर्घस्थायी होते हैं, बशर्ते उनके प्रावधान सिर्फ शब्दों की भरमार न हों, बल्कि विशिष्ट हों। दरअसल, उपरोक्त अध्ययन यह चेतावनी देता है कि जो संविधान 1945 के बाद लिखे गए उनकी विदाई की संभावना अधिक है, चाहे वह पुनर्लेखन के जरिए हो या नए सिरे से नया संविधान बनाकर।
फिर सवाल उठता है कि देबराय क्यों सोचते हैं कि अब भारत के संविधान को रद्द कर दिया जाए या थोक में उसे फिर से बनाया जाए। आखिरकार शिकागो लॉ स्कूल का अध्ययन कहता है कि दुनिया के आधे से कुछ ही अधिक संविधान युद्ध, गृहयुद्ध और तख्ता पलट जैसी विपदाओं के बाद भी बने रहते हैं। क्या देबराय यह सोचते हैं कि भारत में हालात इतने खराब हैं जितने पहले कभी नहीं थे? नहीं।
दरअसल ऐसा लगता कि देबराय उन पुरानी और परस्पर विरोधी धारणाओं के प्रभाव में हैं जो बताती हैं कि क्या चीज ‘भारतीय’ है और क्या नहीं। वह कहते हैं कि भारत का संविधान उसके औपनिवेशिक अतीत को प्रतिबिंबित करता है – जबकि संविधान की हर चीज पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा हुई थी और वह संविधान सभा हमारे नेताओं और समाज सुधारकों से बनी थी।
उनकी एक भ्रामक दलील यह भी है कि हमारा संविधान “मुख्य रूप से 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है।”
अब देखते हैं कि देबराय की निगाह में भारतीय या देशी क्या है। वह लिखते हैं कि सेंगोल, जिसे हाल ही में नए संसद भवन में स्थापित किया गया, “विस्मृत (भारतीय) विरासत” का एक प्रतीक है। जो वह नहीं बताते वह यह कि केवल हिन्दुत्ववादियों या मौजूदा सरकार के समर्थकों की निगाह में सेंगोल ब्रिटेन से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इतिहास के अभिलेखों में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति में सेंगोल की कोई भूमिका प्रमाणित हो। इसके अलावा, सेंगोल सेकुलर संविधान के ऊपर धार्मिक सत्ता की ओर इशारा करता है।
अब देबराय की अगली दलील पर आते हैं। वह कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से इसमें इतने संशोधन हो चुके हैं कि हमारा संविधान वही नहीं रह गया है जो मूल रूप से था। लेकिन यह कहकर वह अपनी ही इस दलील को पलीता लगा देते हैं कि भारत का संविधान औपनिवेशिक युग का अवशेष है।
शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के जिस शोध की बात ऊपर आयी है उसके लेखक हैं थामस गिन्सबर्ग, जैचरी एटकिन्स और जेम्स मेल्टन। इन्होंने लिखित संविधानों की उन आंतरिक विशिष्टताओं की पड़ताल की है जो उन्हें लचीला और वक्त के थपेड़ों को झेलने में समर्थ बनाती हैं। उनके मुताबिक ये गुण हैं – संविधान निर्माण की खुली प्रक्रिया, जो कि तमाम विषयों पर व्यापक रूप से पारदर्शी हो और जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर तर्कसंगत संशोधनों के लिए गुंजाइश हो।
दरअसल, उपरोक्त शोधपत्र के लेखकों के मुताबिक लिखित संविधान के लचीला होने का सकारात्मक परिणाम होता है। वे कतई इस बात की वकालत नहीं करते कि एक ‘कमजोर’ संविधान को कगार पर से ढकेल दिया जाए, जिसके लिए देबराय आमादा दीखते हैं। लेकिन देबराय क्यों उस शोधपत्र की चेतावनियों और सलाह की अनदेखी करते हैं, जिस शोधपत्र की 17-साल वाली बात से वह चिपके हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद संविधान के उन पहलुओं में छिपा हुआ है जिनको लेकर देबराय सबसे ज्यादा असहज हैं और इसे वे जाहिर भी करते हैं।
वह लिखते हैं कि संविधान में किये गए संशोधन हमेशा बेहतरी के लिए ही नहीं थे। इस संदर्भ में वह खासकर केशवानंद भारती मामले में 1973 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं। इसी फैसले ने संविधान के बुनियादी ढाँचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी संविधान का बुनियादी ढाँचा नहीं बदला जा सकता। देबराय इस सिद्धांत को मरोड़ते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र की आकांक्षाएँ संसद द्वारा अभिव्यक्त होती हैं और बुनियादी ढाँचे का सिद्धांत इसे कमजोर करता है। और लोकतंत्र यही चाहता है, जैसा कि वह दावा करते हैं, कि मौजूदा संविधान को रुखसत कर दिया जाए।
असल में, सत्तारूढ़ दल के नेता, मसलन किरन रिजीजू, न्यायपालिका के साथ रह-रह कर तकरार करते रहे हैं, इस बात को लेकर कि संसद की शक्तियां और भूमिका सर्वोच्च मानी जानी चाहिए। पार्टी नेताओं के अलावा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत का हवाला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की।
इस कोरस में देबराय भी शामिल हो गये, और सरकार को बच निकलने का रास्ता भी सुझा दिया। वह लिखते हैं कि मौजूदा संविधान को हटाकर नया संविधान लाने से बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत से पिंड छूट जाएगा, जिससे कार्यपालिका को नागरिकों के ऊपर निर्बाध सत्ता हासिल हो जाएगी।
अस्पष्ट ढंग से लिखे गए एक वाक्य में देबराय यह इशारा करते हैं कि राज्यसभा को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह ‘चुनाव सुधार’ की राह में रोड़ा है। वे यह भी सुझाते हैं कि नयी स्थितियों में, जिसमें बाजार के मुकाबले भारतीय राज्य की भूमिका दोयम दर्जे की रह गयी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थहीन हो गए हैं। लेकिन देबराय सयानापन दिखाते हुए यहीं रुके नहीं रहते। वह कहते हैं कि “हमारी अधिकांश बहस संविधान के साथ शुरू होती है और संविधान पर ही खत्म हो जाती है।” इसलिए वह जड़मूल से समाधान सुझाते हैं कि इस संविधान से ही छुटकारा पा लिया जाए।
इस वक्त भारत के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो संविधान को रद्द करना चाहते हैं, कभी भी यह नहीं बताते हैं कि इसमें क्या खामियाँ हैं। इसके बजाय वे इसकी असाधारण खूबियों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करते हैं। उदाहरण के लिए, देबराय संविधान की प्रस्तावना की इस घोषणा को लेकर असहज हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य और “सोशलिस्ट, सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य” है जो न्याय, स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के बीच समानता के प्रति प्रतिबद्ध है।
देबराय की समस्या संविधान को लेकर नहीं बल्कि संविधान के मूल आदर्शों को लेकर है, जिन आदर्शों से संघ परिवार, बीजेपी, इसके समर्थकों और इसके विचारकों को शुरू से ही, 1950 के दशक से ही, घोर एतराज रहा है।
लेकिन देबराय की दलीलें ज्यादा छलपूर्ण हैं। वह कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के – सोशलिस्ट, सेकुलर, लोकतांत्रिक, न्याय, समानता – इन शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। किस प्रकार बदल गए हैं यह वे नहीं बताते, लेकिन वह लिखते हैं कि “हमें शुरुआत सिद्धांतों से करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि – सोशलिस्ट, सेकुलर, लोकतांत्रिक, न्याय, समानता – का अब क्या अर्थ है।”
साफ है कि इन शब्दों का वही अर्थ है जो तब था जब भारत आजाद हुआ था, जब संविधान सभा ने संवैधानिक प्रावधानों पर बहस की थी, या जब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द बाद के बरसों में जोड़े गए थे, इस पर जोर देने के लिए कि भारत किन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है।
बड़े पैमाने पर हुई आलोचना के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सफाई दी है कि संविधान को लेकर देबराय ने जो लिखा है वह उनके निजी विचार हैं, न कि भारत सरकार के। लेकिन तथ्य यह है कि केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार ने भी दिसंबर 2017 में कहा था कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। उनके मुताबिक, लोग अपने आप को सेकुलर नहीं कहते, बल्कि धर्म या जाति से जोड़कर देखते हैं – ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, ईसाई आदि। उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अपने माता-पिता और अपने खून की पहचान खो देते हैं।
अनंत कुमार के उस बयान पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गयी थी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने यह रुख अख्तियार किया था कि एक मंत्री जिसने संविधान की शपथ ले रखी है उसे यह कतई अधिकार नहीं है कि वह संविधान का उल्लंघन करे और अपने पद पर बना भी रहे। कांग्रेस ने हेगड़े के बयान को भारत की समावेशी अस्मिता पर सीधा हमला करार देते हुए यह आरोप लगाया था कि बीजेपी-आरएसएस कट्टरता, घृणा, विघटन, पूर्वाग्रह फैलाने में लगे हैं।
क्या देबराय स्वीकार करेंगे कि ये आरोप उन पर भी लागू होते हैं, क्योंकि उनकी सयानी भाषा के बावजूद, यह जाहिर है कि वह भी समानता, न्याय और सेकुलरिज्म जैसे संवैधानिक सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं?
हेगड़े के मामले में भी सरकार ने एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया था, राज्यसभा में, संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि संविधान में सरकार की पूरी निष्ठा है, इसे बदलने की उसकी कोई योजना नहीं है और वह हेगड़े के बयान से सहमत नहीं है।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 1998 से 2000 के अपने कार्यकाल के दौरान यह चाहते थे कि संविधान की समीक्षा की जाए। उस समय वाजपेयी सरकार ने संसद में राष्ट्रपति केआर नारायणन के अभिभाषण में भी अपनी मंशा का इजहार किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ही हमेशा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है इसलिए उसे बदलना राष्ट्रपति के विवेकाधिकार में नहीं होता। लिहाजा, नारायणन ने वह अभिभाषण संसद में पढ़ा, उस हिस्से को भी, जिसमें सरकार ने संविधान की समीक्षा करने की मंशा जताई थी।
लेकिन जब हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती के अवसर पर नारायणन ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपना भाषण दिया, तो उन्होंने संविधान को फिर से लिखे जाने की कई बार उठ चुकी मॉंग का जिक्र किया और कहा, “हमें सोचना होगा कि हम संविधान की वजह से नाकाम हुए हैं या हमने संविधान को नाकाम किया है।”
वे शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए और देश भर में लोगों ने राष्ट्रपति का समर्थन और संविधान पर पुनर्विचार करने की वाजपेयी सरकार की योजना का विरोध किया। फिर सरकार नरम पड़ गयी और संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बजाय संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोग गठित किया। राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी सरकार को कदम आगे बढ़ाने से रोक दिया था। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने सम्माननीय पूर्ववर्ती की मिसाल पर चलेंगी और संविधान की रक्षा करने की अपनी शपथ के अनुरूप, संविधान को पलीता लगाने के प्रयासों पर सख्ती से विराम लगाएंगी?
संविधान के बारे में देबराय ने जो कुछ कहा है, वह डॉ राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव आंबेडकर समेत उन सभी देश-नायकों का अपमान है जो संविधान सभा में थे और तमाम प्रावधानों पर गहन चर्चा के बाद देश को एक ऐसा संविधान दिया जो वक्त के थपेड़ों और अनगिनत चुनौतियों से पार पाने में सक्षम सिद्ध हुआ है। जो सरकार में ऊॅंचे पदों पर हैं उनका कर्तव्य है कि वे इस दस्तावेज की और संविधान सभा के विधायी उद्देश्य की रक्षा करें। अन्यथा भारत की हमारी संकल्पना (आइडिया आफ इंडिया) और हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता खतरे में पड़ जा सकती हैं।
(लेखक राष्ट्रपति के आर नारायणन के विशेष कार्याधिकारी रह चुके हैं)
अनुवाद : राजेन्द्र राजन
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.