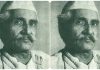— शैलेन्द्र चौहान —
मुक्तिबोध एक समाज चेता रचनाकार हैं। वे अँधेरों से मुँह नहीं फेरते बल्कि अँधेरे की ओर उँगली उठाने का साहस रखते हैं। उसका दुष्परिणाम भी वे जानते हैं क्योंकि अँधेरे के साथी सभी प्रभावशाली लोग हैं फिर भी वे अँधेरे को उजागर करते हैं-
“विचित्र प्रोसेशन/ गंभीर क्वीक मार्च कलाबत्तू वाला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल/ बैंड के लोगों के चेहरे/ मिलते हैं मेरे देखे हुओं से/ लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार/ इसी नगर के/ बड़े-बड़े नाम अरे/ कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में।
भई वाह!
उनमें कई प्रकाण्ड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण/ मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान/ यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद।”
यह है हमारा, हमारी नैतिकता का असली चेहरा, बड़ी-बड़ी बातें करनेवाले साहित्यकार, पत्रकार अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए हत्यारों के साथ हो लेते हैं।

मुक्तिबोध प्रश्न करते हैं अपने आपसे और अपने बहाने समाज से, हम सबसे। हम सब जो अपनी-अपनी खोल में सिमटे हुए हैं, सबके सब दोषी हैं। मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ आत्मालोचन करती हैं-“अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किसके लिए तुम दौड़ गये। करुणा के दृश्यों से हाथ मुँह मोड़ गये। बन गये पत्थर। बहुत बहुत लिया। दिया बहुत कम। मर गया देश अरे जीवित रह गये तुम।” और आलोचना के इन्हीं क्षणों में उन्हें महसूस होता है कि कोई है जो उनसे उम्मीदें रखता है। वह अपना अनुभव शिशु उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता है- “एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर/ मूर्ति की ठठरी/ नाक पर चश्मा हाथ में डंडा/ कंधे पर बोरा, बाँह में बच्चा/ आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे/ मुस्करा उस द्युति पुरुष ने कहा, तब/ मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था/ सँभालना इसको, सुरक्षित रखना।”
और उन्हें लगता है कि अब खतरे उठाने का समय आ गया है। वे संकल्प चाहते हैं देश से, समाज से, खासकर अपने आपको देश और समाज का प्रवक्ता कहनेवाले लोगों से- “अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे/ तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़/ पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार/ तब कहीं देखने मिलेगी बाँहें/ जिसमें कि प्रतिपल काँपता रहता अरुण कमल एक।” वे शोषण-मुक्त अन्याय रहित समाज चाहते हैं। तमाम अँधेरों को भेदकर एक किरण उतारना चाहते हैं, जो खिला सके उम्मीदों का अरुण कमल। मगर अफसोस तो यह है कि कोई साथ नहीं है। सब रक्तपायी व्यवस्था के साथ नाभिनाल आबद्ध हैं- “सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। चिन्तक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके खयाल से यह सब गप है मात्र किवदन्ती। रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल बध्द ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे।”
मुक्तिबोध और लम्बी कविता हिन्दी में एक तरह में समानार्थी शब्द बन गये। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा भी है कि यथार्थ के तत्त्व परस्पर गुम्फित होते हैं और पूरा यथार्थ गतिशील, इसलिए जब तक पूरे का पूरा यथार्थ अभिव्यक्त न हो जाए, कविता अधूरी ही रहती है। ऐसी अधूरी कविताओं से उनका बस्ता भर पड़ा था जिन्हें पूरी करने का वक्त वे नहीं निकाल पाये। अधूरी होने के बावजूद मुक्तिबोध के मन में इनके प्रति बड़ा मोह था और वे चाहते थे कि उनके पहले संग्रह में भी इनमें से कुछ जरूर ही प्रकाशित करा दी जाएं। अपनी छोटी कविताओं को भी मुक्तिबोध अधूरी ही मानते थे।
मेरे खयाल से उनकी सभी छोटी कविताएँ अधूरी लम्बी कविताएँ नहीं हैं। उनकी भावावेशमूलक रचनाएँ अपने आप में सम्पूर्ण हैं जिनमें से कई इस संग्रह की शोभा हैं जैसे ‘साँझ और पुराना मैं’ या ‘साँझ उतरी रंग लेकर’, ‘उदासी’ शीर्षक रचनाएँ। ‘भूरी भूरी खाक धूल’ में संग्रहीत लम्बी कविताएँ ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ की तुलना में कमजोर, शिथिल और बिखरी-बिखरी सी जान पड़ती है। कारण स्पष्ट है। कवि के जीवन के उत्तर-काल की होने के कारण ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ की लम्बी कविताएँ फिनिश्ड रचनाएँ हैं और खाट पकडऩे के पहले कवि ने उनका अन्तिम प्रारूप तैयार कर लिया था। शेष कविताओं पर काम करने का वक्त उन्हें नहीं मिल पाया।
लम्बी कविता को साधने के लिए मुक्तिबोध नाटकीयता के अलावा अपनी सेंसुअसनेस का भी भरपूर उपयोग करते हैं। इस कला में महारत उन्हें अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में ही हासिल हुई। परवर्ती लम्बी कविताओं में उनकी लिरिकल प्रवृत्ति एकदम घुल-मिल गयी है। शायद इसीलिए अपने अन्तिम वर्षों में उन्हें शुद्ध लिरिकल रचनाएँ लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत ‘भूरी भूरी खाक धूल’ में प्रगीतात्मक रचनाओं के अलावा विशिष्ट मन:स्थितियों के भी अनेक चित्र मिल जाएंगे जिनका होना, संभव है कुछ लोगों को चौंकाये लेकिन इनका होना अकारण नहीं है।
मुक्तिबोध के लेखन का बहुत थोड़ा हिस्सा उनके जीवन-काल में प्रकाशित हो सका था। जब उनकी कविता की पहली किताब छपी तब वे होश-हवास खो चुके थे। एक तरह से उनका सारे का सारा रचनात्मक लेखन उनके मरने के बाद ही सामने आया। आता जा रहा है। मरणोत्तर प्रकाशन के बारे में जाहिर है हम जितनी भी एहतियात बरतें, थोड़ी होगी क्योंकि हमारे पास जानने का साधन नहीं होता कि जीवित रहता तो कवि अपने लिखे का कितना हिस्सा किस रूप में प्रकाशित कराने का फैसला करता। खासतौर से मुक्तिबोध जैसे कवि के बारे में तो हम अपने को हमेशा ही संशय और दुविधा की स्थिति में पाते हैं। वे दूसरों को लेकर जितने उदार थे खुद को लेकर उतने ही निर्मम और निर्मोही। जो लोग उनकी रचना-प्रक्रिया से परिचित हैं, जानते हैं कि अपनी हर रचना वे कई-कई बार लिखते थे। कविता ही नहीं गद्य भी।
‘कामायनी : एक पुनर्विचार’ किताब-रूप में उन्होंने सन् 50 के आसपास ही लिख डाली थी और वह मुद्रित भी हो चुकी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं हो सकी। कोई दस बरस बाद जब उसके प्रकाशन का डौल जमा तो मुक्तिबोध ने संशोधन के लिए एक महीने का समय माँग कर पूरी की पूरी किताब नये सिरे से लिखी। ‘वसुधा’ में प्रकाशित डायरी-अंशों और ‘एक साहित्यिक की डायरी’ के प्रारूपों को आमने-सामने रखकर इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। कविता के मामले में तो वे और भी सतर्क और चौकस थे। जब तक पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं कि उनका अभिप्राय शब्द के खाँचे में एकदम ठीक-ठीक बैठ गया है, वे अपनी रचना को अधूरी या ‘अन्डर रिपेयर’ कहते थे। दोबारा-तिबारा लिखी जाने पर उनकी मूल रचना सर्वथा नया रूपाकार पा पाती। मुक्तिबोध की पांडुलिपियों को खँगालते हुए किसी भी दूसरे आदमी के लिए तय करना सचमुच बहुत मुश्किल है कि उनकी रचना का कौन-सा प्रारूप अंतिम है। जीवित होते तो शायद उनके लिए भी यह तय करना बहुत आसान न होता।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.