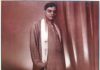हमारे संविधान में सहभागी लोकतंत्र और जनसाधारण की सहभागिता के लिए जरूरी प्रतिबद्धता की कमी रही है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में केंद्र और राज्य सरकार से नीचे जिला परिषद, नगरपालिका और ग्राम-पंचायत तक जाने में संकोचग्रस्त रहा। इस दिशा में किये गये संविधान संशोधनों के बावजूद केंद्र और राज्य के नीचे की सत्ता-व्यवस्था में लोकतंत्र की सुगंध और ऊर्जा नहीं है। राष्ट्रनिर्माण में आत्मविश्वास से जुटे हुए स्त्री-पुरुषों की कतारों की बजाय बेलगाम सत्ताधीशों और नौकरशाही के सामने याचक-भाव से झुके हुए असहाय जनसाधारण ही हमारी अबतक की लोकतंत्र रचना का अंतिम सत्य है।
इस संविधान ने देशवासियों को नागरिक के रूप में मतदान के अधिकार के अलावा कोई और जिम्मेदारी नहीं दी है। जैसे जनप्रतिनिधि वापसी का अधिकार, दलों पर अपने घोषणापत्र के प्रति जिम्मेदारी का अंकुश, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग, आदि। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के सवाल पर निर्गुणता का दोष है। इसलिए सरकारें बदलने के बावजूद इन जरूरी मोर्चों पर संसाधन संवर्धन के प्रति उपेक्षा भाव की निरन्तरता का सच हमारे स्वराज की सीमित सार्थकता को बेपर्दा करता रहता है।
डॉ. लोहिया के लिए इसका यह अर्थ नहीं था कि मौजूदा संविधान को खारिज करते हुए सहभागी लोकतन्त्र को संभव बनाने के लिए एक नयी संविधान सभा के लिए अभियान चलायें। वह स्वतंत्रता, न्याय, समता, सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र और विश्व बंधुत्व के आदर्शों के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर से देखे गये सपनों को साकार करने के लिए संविधान में सुधार के पक्षधर थे…
चौखम्भा राज योजना अर्थात सहभागी राष्ट्रनिर्माण
इस विस्तृत पृष्ठभूमि के आधार पर यह बताना उचित होगा कि चौखम्भा राज की रचना करके भारतीय समाज और राज्य-व्यवस्था में स्वराज का प्रकाश और लोकतंत्र का उत्साह फैलाते हुए सहभागी राष्ट्रनिर्माण का आवाहन करनेवाले डॉ. लोहिया कौन थे? इस जानकारी के बाद चौखम्भा राज की उनकी योजना का संदर्भ, प्रमुख बातें और प्रासंगिकता को समझना आसान होगा।
‘चौखम्भा राज’ की योजना के प्रस्तावक डॉ. राममनोहर लोहिया भारतीय समाजवादी आन्दोलन के अग्रणी नायक और सिद्धांतकार थे। एक मध्यमवर्गीय व्यापारी परिवार में जनमे डॉ. लोहिया को फैजाबाद, मुंबई, बनारस, कोलकाता और बर्लिन में शिक्षित होने का सुअवसर मिला था। बचपन में ही उनकी माँ चन्द्रावती का देहांत हो गया था और पिता हीरालाल 1921 से गांधी के प्रभाव से अपना पारिवारिक व्यवसाय छोड़कर असहयोग आन्दोलन के रचनात्मक पक्ष से जुड़ गये थे। वह 1930 के नमक सत्याग्रह में जेल भी गये थे। वह राममनोहर को बाल्यावस्था से ही कांग्रेस के अधिवेशनों में ले जाते थे। इससे राममनोहर का 1933 तक अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पढ़ना स्वाभाविक था। उन्होंने 1942 के ‘अंग्रेजो,भारत छोड़ो!’ आन्दोलन में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए बम्बई और कलकत्ता से ‘कांग्रेस रेडियो’ के जरिये स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया था।
डॉ. लोहिया इससे पूर्व स्वराज के सिपाही के रूप में 1939 और 1940 में ब्रिटिश राज द्वारा गिरफ्तार किये जा चुके थे। उन्होंने 1946 में ब्रिटिश कैद से रिहाई के बाद उसी साल पुर्तगाली शासन से गोवा की आजादी की मशाल प्रज्वलित करने के लिए भी जून और सितम्बर में दो बार सत्याग्रह किया। लोहिया को भारत की आजादी के कुछ ही महीनों के बाद नेपाल में राणाशाही के खात्मे के आन्दोलन के समर्थन में प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली में जेल में बंद रखा गया। 1948 और 1966 के बीच के वर्षों में उन्होंने किसानों और नौजवानों से लेकर मणिपुर और नगालैंड के लोगों के सवालों पर सत्याग्रह किये। 1964 में उन्होंने अमरीका में रंगभेद के खिलाफ भी गिरफ्तारी दी। नेहरू के कार्यकाल में वह प्रतिपक्ष के सबसे मुखर नेता थे जिन्हें आजादी के बाद भी अनेकों बार कैद किया गया।
डॉ. लोहिया के विचार समग्र को (क) निराशा के कर्तव्य के दर्शन, (ख) इतिहास चक्र के सिद्धांत, और (ग) सप्तक्रांति के कार्यक्रमों की त्रिवेणी में समाहित किया जा सकता है। लोहिया ने देश को खर्च पर सीमा, दाम बाँधो, जाति तोड़ो, नर-नारी समता, अँग्रेजी हटाओ, हिन्द-पाक महासंघ, हिमालय बचाओ, सप्तक्रांति और विश्व-सरकार जैसे क्रांतिकारी कार्यक्रम दिये। द्रौपदी को भारतीय नारी का आदर्श और गांधी को दुनिया के भविष्य का पथप्रदर्शक माना। लोहिया ने गजनी, गोरी और बाबर को विदेशी लुटेरे और रजिया, रसखान, जायसी और शेरशाह को सभी देशवासियों का पुरखा बताया। उनकी प्रार्थना थी कि ‘हे भारतमाता! हमें राम की मर्यादा, कृष्ण का उन्मुक्त ह्रदय और शिव का मस्तिष्क प्रदान करो।’.
उन्हें सत्याग्रही समाजवाद के महानायक के साथ ही ‘गैर-कांग्रेसवाद’ की राजनीति के सफल प्रवर्तक के रूप में भी याद किया जाता है। आजादी, लोकतंत्र, सत्याग्रह, राष्ट्रीयता, विश्वबंधुत्व और समाजवाद उनके मुख्य सरोकार थे। लेकिन वह व्यक्तिकेन्द्रित ‘वादों’ के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने‘मार्क्सवादी’ या ‘मार्क्स विरोधी’ अथवा ‘गांधीवादी’ या ‘गांधीविरोधी’ जैसी खेमेबंदियों से दूर रहने की जरूरत पर बल दिया।
उनके चिंतन की व्यापकता के अनुमान के लिए 9 खण्डों में उपलब्ध राममनोहर लोहिया रचनावली और 16 खण्डों में प्रकाशित ‘लोकसभा में लोहिया’ का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। लोहिया की रचनाओं में से‘मार्क्स, गांधी ऐंड सोशलिजम’, ‘इतिहास चक्र’, ‘जातिप्रथा’, ‘भाषा’, ‘इंटरवल ड्यूरिंग पोलिटिक्स’, तथा ‘भारत, चीन और उत्तरी सीमाएं’ कालजयी रचनाएँ मानी जाती हैं। 23 मार्च 1910 को अकबरपुर (फैजाबाद) में जनमे डॉ. राममनोहर लोहिया का 57 बरस की आयु में 12 अक्तूबर 1967 को नयी दिल्ली में निधन हो गया।
डॉ. लोहिया के चौखम्भा राज की योजना का मूल उद्देश्य नव-स्वाधीन भारत में सहभागी राष्ट्रनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करना था। इसमें राजनीतिक सत्ता, आर्थिक क्षमता, टेकनोलाजी सुधार, स्थानीय संसाधन और जनसाधारण की जिम्मेदारी का संगम किया गया था। इसे वह लोकतन्त्र को समावेशी बनाने और नागरिकता निर्माण की प्रक्रिया में हर देशवासी को शामिल करने का उपाय भी मानते थे।
1951 से 1962 की अवधि में उन्होंने इस विचार को समाजवादी पुस्तिकाओं (1951, 1957) से लेकर सोशलिस्ट पार्टी के दो चुनाव घोषणापत्रों (1957, ’62) के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में बार-बार देश के सामने रखा। इन सबका एकसाथ अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि डॉ. लोहिया द्वारा प्रस्तुत चौखम्भा राज योजना के मुख्यत: सात आयाम थे :
1. देश के समस्त सरकारी राजस्व के 1/4 अंश को गाँव, नगर और जिला पंचायत को दिया जाए और योजना से जुड़े खर्च के 1/4 हिस्से को गाँव, नगर और जिला पंचायत के जरिये किया जाए।
2. पुलिस-व्यवस्था को गाँव, नगर और जिला पंचायत के अंतर्गत उनकी समितियों की निगरानी में संचालित किया जाए।
3. जिले में कलक्टर (जिलाधीश) के पद को समाप्त करते हुए उसकी जिम्मेदारियों को जिले की विभिन्न समितियों को सौंपा जाए। यह भी जरूरी है कि प्रशासन में निर्वाचन की व्यवस्था को बढ़ाने और नामांकन और मनोनयन की व्यवस्था को कम करने पर यथासंभव बल दिया जाय।
4. खेती, उद्योग और अन्य सभी राष्ट्रीयकृत संपदाओं का स्वामित्व यथासंभव गाँव, नगर और जिला पंचायत को सौंपा जाए।
5. आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के कार्य को यथासंभव छोटी मशीनों के अधिकतम उपयोग से संपन्न किया जाए।
6. शासन की स्थानीय इकाई के रूप में गाँव, नगर और जिला पंचायत को औपचारिक तौर पर निर्धारित विषयों के बारे में कानून बनाने और नियोजन का अधिकार मिले।
7. गाँव, नगर और जिला पंचायत के सदस्यों को देश के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार मिले।
इस योजना में भारत के लिए अनुकूल समाजवादी राज्य-व्यवस्था के मूल तत्त्व प्रस्तुत किये गये हैं। यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सत्ताव्यवस्था और अमरीका की पूँजीवादी बाजार व्यवस्था से बिलकुल अलग रखी गयी है। यह स्पष्ट है कि चौखम्भा राज योजना की अपेक्षा है कि स्वराज और लोकतंत्र के प्रकाश को केंद्र और राज्य से आगे जिला, नगर और गाँव तक अविलम्ब पहुँचाने के लिए अविलम्बता (‘इमेडीएसी’) और सहभागिता (हिस्सेदारी) की कसौटियों को आधार बनाया जाए। देश के सुसंचालन के लिए राष्ट्रीय संसद से लेकर गाँव पंचायत तक वयस्क मताधिकार के जरिये चुने जनप्रतिनिधियों के परस्पर सम्बद्ध योगदान की सुविधा की दृष्टि से राज्यसत्ता का एक चार-मंजिला ढांचा निर्मित किया जाए। इस चार-स्तरीय राज्यसत्ता को उत्पादन, स्वामित्व, प्रशासन, नियोजन, शिक्षा आदि की जिम्मेदारी सँभालनी होगी। इसके तकनीकी प्रबंधन को छोटी मशीन की टेकनोलॉजी से संचालित किया जाएगा।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.