— गोपाल प्रधान —
वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित सुषमा नैथानी की किताब अन्न कहाँ से आता है सही अर्थ में हिंदी की उपलब्धि है। लोकोपयोगी विज्ञान श्रृंखला के तहत छपी इस किताब का उपशीर्षक ‘कृषि का संक्षिप्त इतिहास : झूम से जीएमओ तक’ है। किताब में कुल दस अध्याय हैं और उनमें बेहद कसी हुई प्रस्तुति के साथ खेती के अलग अलग पहलुओं का गहन विश्लेषण है। न केवल समूची किताब की योजना में आंतरिक संगति और तर्क नजर आता है बल्कि सभी अध्यायों के भीतर भी बिना किसी भटकाव के बेहद सुलझी हुई भाषा में इस जटिल विषय को आसान बनाकर पेश कर दिया गया है।
किताब की इस गुणवत्ता का स्रोत लेखिका के भाषामूल और पेशेवर दक्षता से है। सुषमा नैथानी का भाषा संस्कार उत्तराखंड का है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के हिंदी लेखकों के पास टकसाली किस्म की साफ-सुथरी हिंदी सहज ही उपलब्ध होती है। सुमित्रानंदन पंत से लेकर मनोहरश्याम जोशी तक लेखकों की लम्बी कतार ने वह हिंदी सुषमा जी को सौंपी है जिसमें उन्होंने हमारे जीवन में व्याप्त व्यवहार का इतिहास खोलकर रख दिया है। कभी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में इस तरह की हिंदी में न केवल विज्ञान बल्कि गणित तक की किताबें हुआ करती थीं। इस काम के लिए लेखिका हिंदीभाषी समाज के आभार की अधिकारी हैं। उनकी इस योग्यता का दूसरा पहलू विज्ञान से उनका लगभग जुनूनी लगाव है। ढेरों सामान्य जानकारी पाने के अतिरिक्त भी इस किताब का तात्कालिक उपयोग है। इस समय खेती-किसानी पर कंपनियों के कब्जे का रास्ता साफ करने की सरकारी मुहिम के समय इस किताब को जरूर देखा जाना चाहिए। इससे पता चलेगा कि वर्तमान मुहिम के स्रोत किन जगहों पर छिपे हैं।

इन योग्यताओं से लैस सुषमा जी ने सबसे पहले यह बात स्थापित की है कि आज जो फसलें उगायी जा रही हैं वे आदिकाल से मौजूद नहीं थीं। उनका यह नजरिया मार्क्स की इस मान्यता के मेल में है कि शुद्ध प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं होती बल्कि पर्यावरण और मनुष्य की आपसी क्रिया से प्रकृति का निर्माण होता है। हजारों साल तक ध्यान से परखने के बाद मनुष्य ने उन फसलों का विकास किया जिनकी उपज से हमारा भोजन बनता-मिलता है। इन सभी फसलों की विविधता को सुषमा जी ने बहुत अच्छी तरह उजागर किया है।
किसानों को सहज उपलब्ध इस जानकारी को रोचक तरीके से लेखिका ने पाठकों तक पहुंचाया है कि खीर और लड्डू तथा भूजे के लिए एक ही तरह के अन्न का इस्तेमाल नहीं होता। इसे मक्का जैसी विदेशी फसलों तक के लिए उन्होंने साबित किया है। पापकार्न से लेकर स्वीटकार्न तक उसके तमाम भेद हैं। नयी प्रजातियों के बीजों के निर्माण की उनकी बतायी प्रक्रिया तो प्रकृति की लीला का रहस्य भेदन है जिसमें आसपास खड़ी फसलें एक दूसरे से लेती देती हैं (स्व-परागण और पर-परागण) तथा इस प्रक्रिया का दूर से सावधानी के साथ मनुष्य पर्यवेक्षण करता रहता है ताकि पोषण प्रदान करनेवाली प्रजातियों का विकास कर सके। ये पर्यवेक्षक बागवानी करनेवाले सामान्य मनुष्यों से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो उनकी किताब में सचमुच रचयिता की तरह चित्रित हुए हैं। संसार भर की फसलों का बीज बैंक तैयार करने के काम में जुटे रूसी वैज्ञानिक निकोलाई वाविलोव और हरित क्रांति के प्रयोगों के साथ जुड़े अमरीकी वैज्ञानिक नार्मन बोरलाग इसके उदाहरण हैं।
खेती के बारे में पाठक के किसी भी रूमानी रुख को तोड़ते हुए लेखिका ने दूसरे ही अध्याय में बागानी खेती के साथ जुड़ी दास प्रथा की क्रूरता की कहानी कही है। इसके जैसी ही कहानी हम हिंदुस्तानियों की रही जिसे दास प्रथा की समाप्ति के बाद शुरू किया गया। उसे हम गिरमिटिया प्रथा के नाम से जानते हैं। खाद्यान्न के बाद की नकदी खेती के बयान में ही चाय की कहानी है जिसके साथ अफ़ीम युद्ध भी जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि इन फसलों की खेती के साथ ही उपनिवेशवाद का लम्बा इतिहास भी चला आया है जिसे आज के वैश्वीकरण का पूर्वज कहा जा सकता है। इस मामले में यह किताब विज्ञान, मानव श्रम, प्रवास और अर्थतंत्र के वैश्विक एकीकरण की कहानी को एकसाथ बयान करती है।
इसके बाद का अध्याय उपज बढ़ाने के लिए खाद के आविष्कार और उसके कारपोरेट विपणन की कथा है। इस आख्यान से हम विस्थापन और संसाधनों की लूट की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लैटिन अमरीका के स्थानीय निवासी चिड़ियों की बीट का इस्तेमाल उपज बढ़ाने के लिए जानते और करते रहे थे। उनके इस इस्तेमाल के बावजूद खाद का स्रोत बचा हुआ था लेकिन जैसे ही इसका पता अंग्रेजों को चला उसके विपणन का एकाधिकार दुनिया भर में एक कंपनी ने हथियाया और कुछ ही समय में वह विशाल प्राकृतिक भंडार खाली हो गया। इस प्राकृतिक खाद का दोहन कर लेने के बाद रासायनिक खाद का खेल शुरू हुआ जिसमें हिटलरी विज्ञान से भी सहायता मिली। विज्ञान के संहारक के साथ ही रक्षक रूप का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जिन गैसों से नरमेध किया जा सकता था उनसे ही खेतों में फसलों की पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है!
पूरी किताब मानव सभ्यता के विकास की भौतिकवादी व्याख्या की तरह है। मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य कुछ भी करने से पहले जीवन यापन के साधनों का इंतजाम करता है। इसके क्रम में ही वह प्रकृति के साथ अंत:क्रिया के जरिये तमाम वस्तुओं का उत्पादन करता है। आबादी में बढ़ोत्तरी के साथ इनकी जरूरत बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में उसे जीवनोपयोगी उत्पादन को विस्तारित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति भी प्रकृति में मौजूद संसाधनों के सहारे ही होती है।
नाइट्रोजन हमारे वातावरण में ही थी। फसलों की उपज में इसके योगदान की जानकारी होने से मनुष्य ने उसका सार्थक उपयोग शुरू किया। भोजन के लिए बढ़ती जरूरत ने खेती की लगभग सभी खोजों की प्रेरणा दी और मनुष्य ने जमीन की सीमित मात्रा में ही अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बहुतेरे प्रयोग किये। संसार में धान, गेहूं और मक्का तीन बुनियादी फसलें हैं जिनके परिष्कार ने आबादी की बढ़ोत्तरी के बावजूद भोजन की कमी नहीं होने दी। इन तीनों के संवर्धन की कहानी हरित क्रांति से जुड़ती है।
खेती से पैदा होनेवाला अन्न केवल पोषण ही नहीं प्रदान करता बल्कि हमारे शरीर में बाहरी तत्त्वों के प्रवेश का रास्ता भी यह अन्न ही होता है। अन्न या फसलों की उपज बढ़ाने के सभी प्रयोगों के साथ खतरे भी जुड़े रहते हैं। जैसे जंगली घासों से विकसित होकर अन्न के बीज निकले उसी तरह इन खतरों से बचाव का रास्ता भी मानव सभ्यता निकालेगी। महात्मा गांधी ने किसानों को सबसे अधिक निर्भय प्राणी कहा था। खेती के लिए हिंसक जानवरों, विषाणुओं और आपदाओं से लगातार जूझना पड़ता है। भोजन की जरूरत मनुष्यों को हमेशा रहेगी। मुनाफे के सौदागर इसलिए खेती पर नजर लगाये रहते हैं। वैसे भी लालच आत्मघाती प्रवृत्ति होती है। इसलिए खेती को बचाने की वर्तमान लड़ाई के समय इस किताब को पढ़ना प्रत्येक हिंदीभाषी का कर्तव्य है। इससे हम अपने पुरखों की ताकत और सृजन की क्षमता को समझ सकेंगे।
किताब : अन्न कहाँ से आता है
लेखक : सुषमा नैथानी
प्रकाशक : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास; नेहरू भवन 5, वसंतकुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2 वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070
मूल्य : 275 रु.












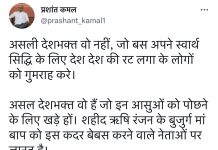





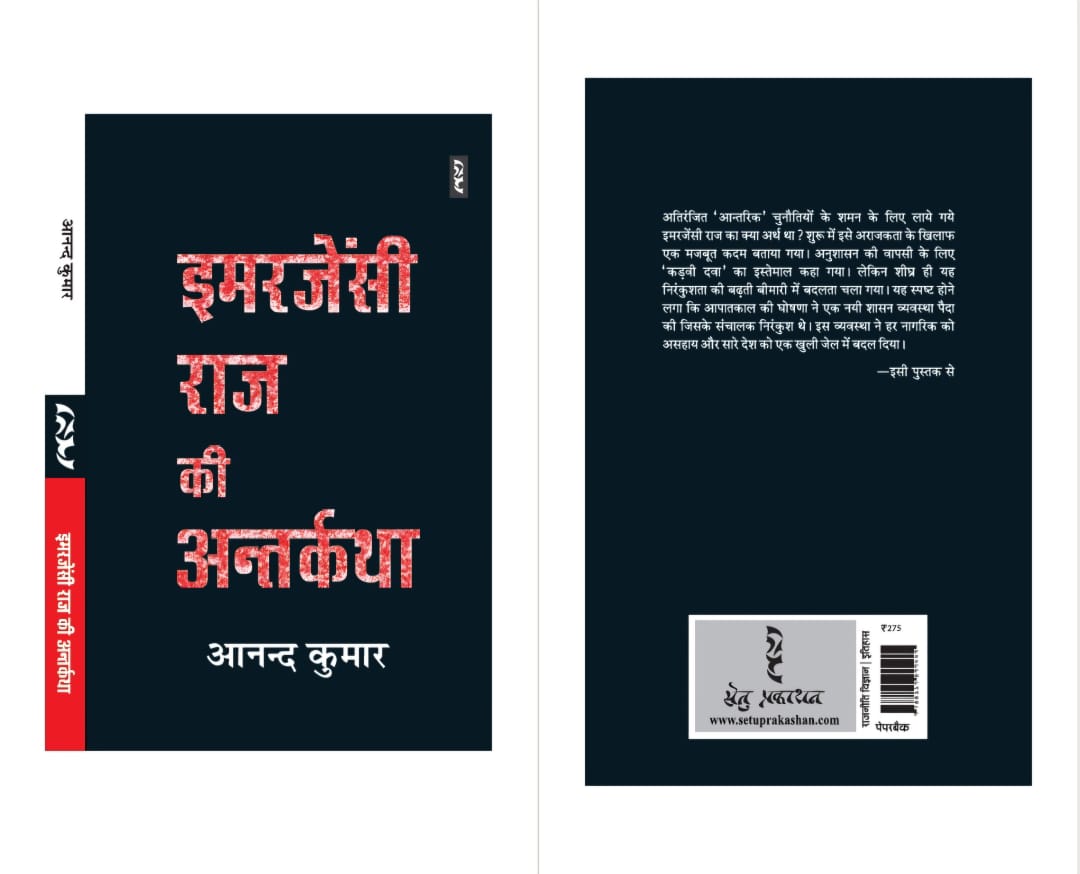
एक उम्दा परिचय के लिए धन्यवाद सर। इस संक्षिप्त लेख में आपने उन महत्पूर्ण आयमो को उजागर किया है जिससे इस पुस्तक की उपयोगिता सिद्ध होती है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ूगा।
आभार।
एक ज़रूरी किताब का सारग्राही विवेचन।
आभार लेखक और समीक्षक का।