— राममनोहर लोहिया —
(लोहिया ने 1936 में नागरिक स्वाधीनता से संबंधित दो लेख लिखे थे- एक, ‘नागरिक स्वाधीनता क्या है’, और दूसरा, ‘भारत में नागरिक स्वाधीनता की अवस्था’ शीर्षक से। दोनों लेख अंग्रेजी में लिखे गये थे। पहली बार जब दोनों लेख एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुए तो उसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। दिनेश दासगुप्ता ने इसे फिर से, हिंदी में, छपवाया था, अक्टूबर 1976 में, यानी इमरजेंसी के दिनों में। तीसरा संस्करण नागपुर के लोहिया अध्ययन केंद्र के हरीश अड्यालकर ने छपवाया था। इस पुस्तिका को ग्वालियर स्थित आईटीएम यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने 23 मार्च 2020 को प्रकाशित करके फिर से उपलब्ध कराने का प्रशंसनीय कार्य किया है। आज देश तो स्वाधीन है लेकिन नागरिक स्वाधीनता पर संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में नागरिक स्वाधीनता पर लोहिया के उपर्युक्त निबंध की प्रासंगिकता जाहिर है। लिहाजा, इसे हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)
नागरिक स्वाधीनता (सिविल लिबरटीज) क्या चीज है? यह जानने के लिए हमें उसके सैद्धांतिक स्वरूप, उसकी उत्पत्ति और उसकी वर्तमान स्थिति पर विचार करने के साथ यह भी सोचना होगा कि उसकी हिफाजत के वास्ते क्या-क्या किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि नागरिक स्वाधीनता के बारे में हमें चार बातों पर विचार करना है- (1) नागरिक स्वाधीनता कितने प्रकार की होती है? (2) उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? (3) उसपर आज किस प्रकार और क्यों प्रहार हो रहा है? (4) उसकी हम किस प्रकार हिफाजत कर सकते हैं और उसकी हमें हिफाजत क्यों करनी चाहिए। इन चार बातों पर विचार करने से हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि नागरिक स्वाधीनता क्या है अर्थात उसकी अवधारणा क्या है?
नागरिक स्वाधीनता कितने प्रकार की होती है? यह जानने के लिए हमें राज्य निर्माताओं की युगांतरकारी घोषणाओं और मूल कानूनों व अदालती फैसलों के बुनियादी सिद्धांतों को एक साथ पिरोना पड़ेगा। ये घोषणाएँ और सिद्धांत नागरिक स्वाधीनता के विभिन्न प्रकारों को निर्धारित और स्पष्ट करते हैं। नागरिक स्वाधीनता के विभिन्न प्रकारों में सबसे ऊपर जिस स्वतंत्रता का नंबर आता है, वह है- व्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता तथा घर की पवित्रता की स्वतंत्रता। 1786 के फ्रांसीसी संविधान में कहा भी गया है कि राज्य का उद्देश्य आदमी के प्राकृतिक या मूल (नैचुरल) अधिकारों की हिफाजत करना है। ये अधिकार हैं- ‘व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और दमन व अत्याचार का प्रतिकार करने का अधिकार।’ इन अधिकारों से यह प्रकट है कि किसी भी नागरिक को कानून की उपयुक्त और उचित प्रक्रिया चलाये बिना गिरफ्तार, नजरबंद और कैद नहीं किया जा सकता। कानून की इन प्रक्रियाओं में धीरे-धीरे जूरी की खुली अदालत की व्यवस्था भी शामिल कर ली गय़ी है। यही नहीं, यह भी तय किया गया है कि जूरी बनाये जानेवाले लोगों में से ज्यादातर लोग उसी वर्ग के होंगे जिसका कि अभियुक्त है। हर आदमी अपने घर में निरापद और निश्चिंत रह सकेगा। उसके घर पर छापा नहीं मारा जा सकता और न ही तलाशी ली जा सकती है। कानून तोड़ने के सुनिश्चित और सुस्पष्ट अभियोग के बिना उसके घर पर छापा नहीं मारा जा सकता और न ही तलाशी ली जा सकती है। देश के भीतर आने-जाने और घूमने तथा विदेश जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने की उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
आज के जन-जागरण और महान जनान्दोलनों के युग में विचार व मत प्रकट करने और सभा करने की स्वतंत्रता उतनी ही महत्त्वपूर्ण व जरूरी है जितनी कि व्यक्तिगत सुरक्षा और घर की पवित्रता की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, जिसका मतलब बोलने और छापने की आजादी है, यह अमरीकी उक्ति सर्वमान्य और मापदण्ड है कि- अगर आदमी विद्रोह की प्रकट कार्रवाई न करे तो उसे उग्र से उग्र और क्रान्तिकारी से क्रान्तिकारी अभिमत व्यक्त करने पर भी कोई सजा नहीं दी जा सकती।
इसी तरह सभा और जलूसों के बारे में यह ब्रिटिश सिद्धांत सर्वमान्य है कि- अगर ट्रैफिक में बहुत ज्यादा बाधा न पड़े तो पुलिस या प्रशासकीय अधिकारी सभा और जुलूस को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इन सिद्धांतों का मतलब राजद्रोह के कानून का खात्मा और प्रेस, पुस्तकों, चिट्ठियों और रेडियो पर सेंसरशिप का न होना होता है। सभाओं और जुलूसों पर रोक नहीं लगायी जा सकती। नगरों और गांवों के सार्वजनिक स्थानों में सभा करने का हरेक व्यक्ति को समान अधिकार है।
व्यक्ति और विचार व मत की स्वतंत्रता के साथ संगठन बनाने की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड ऑरगेनाइजेशन) का मतलब आज बहुत बढ़ गया है। यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राज्य के क्रिया-कलापों और आर्थिक प्रबंध व व्यवस्था में अपनी गहरी दिलचस्पी को संगठित प्रयास रूप दें ताकि मौजूदा बुराइयाँ दूर हों। इसलिए उन्हें किसी भी हालत में संगठन बनाने और हड़ताल व पिकेटिंग करने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह एक अत्यन्त कीमती स्वतंत्रता है। प्रशासन अकसर यह दुहाई देगा और प्रचार करेगा कि इस तरह के संगठनों और हड़तालों से अन्ततः शांति भंग होगी और क्रान्तिकारी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। वह इस कीमती स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करेगा। उसकी ऐसी कोशिशों का प्रतिकार और परदाफाश करना होगा।
संगठन बनाने और हड़ताल करने की स्वतंत्रता से, अगर वह प्रकट रूप में विद्रोह की कार्रवाई का रूप न लेती हो तो किसी भी हालत में छेड़छाड़ बरदाश्त नहीं की जा सकती।
कानून सार्वजनिक इच्छा (जनता की इच्छा) की अभिव्यक्ति है, यह 1786 के फ्रांसीसी संविधान की एक घोषणा है। राज्य की सत्ता का उत्स जनता में है। जनता की इच्छा से ही राज्य को सत्ता मिलती है। इसलिए जनता को सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। इस अधिकार को ही लोकतांत्रिक नियन्त्रण कहा जाता है। इसलिए सरकार पर जनता के लोकतांत्रिक नियंत्रण का अधिकार एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह भी होता है कि सरकार गुप्त रूप से काम नहीं कर सकती और न ही वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संसद की अनुमति बिना कुछ कर सकती है। दुनिया के नागरिक स्वाधीनता यूनियनों (सिविल लिबर्टीज यूनियनों) ने अपने आंदोलन के घोषणापत्रों में सरकार पर किसी न किसी प्रकार के लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात कही है।
अंतःकरण या विवेक, विचार और शिक्षा की स्वतंत्रता को मत की स्वतंत्रता का ही एक अंग माना जाना चाहिए। इस स्वतंत्रता पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के भीतर ही इससे सबसे ज्यादा छेड़छाड़ होती है।
अगर किसी प्राध्यापक या शिक्षक को प्रशासन के प्रतिकूल राय रखने पर बरखास्त कर दिया जाय और राज्य सांप्रदायिक व जातीय संस्थाओं को बढ़ावा देने लगे तो यह अंतःकरण, विचार और शिक्षा की स्वतंत्रता पर ऐसा प्रहार है, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार की सुनवाई की गुंजाइश नहीं रहती।
राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग नागरिक स्वाधीनता का एक और पहलू है।
अभियुक्तों को ज्यादातर ऐसे कानूनी और न्यायिक तंत्र के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, जो सरकार और नागरिक के बीच सरकार की ही तरफदारी करता है। जाहिर है कि इस तंत्र से लड़ने का मतलब इसके द्वारा सताये गये लोगों की रक्षा करना भी होगा। लिहाजा, राजनीतिक बंदियों की रहाई की मांग नागरिक स्वाधीनता की एक मांग है और रिहाई न होने तक बंदियों के खाने-पीने, रहने व पढ़ने से संबंधित अधिकारों के लिए लड़ते रहना आवश्यक है।
आशा है कि नागरिक स्वाधीनता का सैद्धांतिक स्वरूप और दायरा अबतक स्पष्ट हो गया है। नागरिक स्वाधीनता होने का मतलब यह है कि एक नागरिक को जीने की निरापदता और निश्चिन्तता प्राप्त करने के अधिकार के साथ बोलने, लिखने, छपाने, संगठन बनाने, सभा करने, समान न्याय प्राप्त करने, सरकार पर नियंत्रण रखने और राजनीतिक कार्यों के लिए अपराधी न ठहराये जाने के अधिकार प्राप्त करने होंगे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















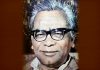


Shaandaar. 👏👏👏👏💐