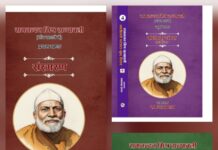(किशन जी चिंतन और कर्म, दोनों स्तरों पर राजनीति में सदाचार, मानवीय मूल्यबोध और आम जन के हित को केंद्र में लाने के लिए सक्रिय रहे। वह मानते थे, जो कि सिर्फ सच का स्वीकार है, कि राजनीति अपरिहार्य है। इसलिए अगर हम वर्तमान राजनीति से त्रस्त हैं तो इससे छुटकारा सिर्फ निंदा करके या राजनीति से दूर जाकर, उससे आँख मूँद कर नहीं मिलेगा, बल्कि हमें इस राजनीति का विकल्प खोजना होगा, गढ़ना होगा। जाहिर है वैकल्पिक राजनीति का दायित्व उठाना होगा, ऐसा दायित्व उठानेवालों की एक समर्पित जमात खड़ी करनी होगी। लेकिन यह पुरुषार्थ तभी व्यावहारिक और टिकाऊ हो पाएगा जब वैकल्पिक राजनीति के वाहकों के जीवन-निर्वाह के बारे में भी समाज सोचे, इस बारे में कोई व्यवस्था बने। दशकों के अपने अनुभव के बाद किशन जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे थे उसे उन्होंने एक लेख में एक प्रस्ताव की तरह पेश किया था। इस पर विचार करना आज और भी जरूरी हो गया है। पेश है उनकी पुण्यतिथि पर उनका वह लेख।)
सन 1950 में भारत का संविधान घोषित हुआ और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार हुआ। इन दो घटनाओं से भारत के सार्वजनिक जीवन, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन की रूपरेखा निर्धारित हो गयी। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय समाज में आर्थिक गैरबराबरी बढ़ती जाएगी और आर्थिक रूप से हम एक कमजोर पूंजीवादी राष्ट्र होकर रहेंगे। हमारे संविधान में भी कुछ गंभीर कमियां रह गयी थीं लेकिन उसमें सकारात्मक संभावनाएं भी थीं। नागरिक आजादी और बालिग मताधिकार के चलते हम यह उम्मीद कर सकते थे कि बहुसंख्यक लोगों की एक भूमिका राजनीति में रहेगी- यदि लगातार नहीं तो बीच-बीच में जनसाधारण की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी- 1977 में आपातकाल को खत्म करने में जनसाधारण की भूमिका इसका उदाहरण है।
इसके अलावा संविधान की सामाजिक दृष्टि काफी सकारात्मक थी। पिछड़ों और दलितों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए स्पष्ट प्रावधान थे। बालिग मताधिकार के चलते पिछड़ों और दलितों के समाज में बहुसंख्यक होने का दबाव राजनीति पर पड़ा, और बड़ी संख्या वाली पिछड़ी तथा दलित जातियां राजनीति की मुख्यधारा में आ गयीं। सदियों के बाद एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया है और जब तक लोकतंत्र का ढांचा रहेगा तब तक इसको पलटने की शक्ति किसी के पास नहीं होगी।
इसको हम सामाजिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं। लेकिन एक समतामूलक जातिविहीन समाज की दिशा में इसकी गति होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो रहा है मानो परिवर्तन अवरुद्ध हो गया है। इसका कारण अवसरवादी राजनीति है।
अवसरवादी राजनीति की चपेट में शूद्र-दलित नेतृत्व भी आ गया है। पूंजीवाद अवसरवादी राजनीति को प्रोत्साहित करता है। शूद्र-दलित राजनीति को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया है। सामाजिक समानता के बारे में संविधान में जिस तरह का प्रावधान है वैसा आर्थिक समानता के बारे में नहीं है। एक अनुपात से अधिक आर्थिक विषमता न बढ़े इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं है।
पंचवर्षीय योजनाओं में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया। फलस्वरूप पूंजीवाद सर्वग्रासी होता गया और राजनीति पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों के नियंत्रण में आ गयी। बाद में समाजवादी-साम्यवादी कहलाने वालों के दल भी पूंजीपतियों पर आश्रित हो गये। अब तो हमारे देश की राजनीति पर अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवाद हावी हो गया है जिसका प्रमाण यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करनेवाला एक भी राजनैतिक दल आज भारत की संसद में नहीं है।
इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैकल्पिक राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य होगा अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवाद के चंगुल से भारत को मुक्त करना और आर्थिक गैर-बराबरी पर रोक लगाना।
ऐसा होने पर दलितों और पिछड़ों की जो शक्ति अभी जातिवादी राजनीति और पूंजीवादी अर्थनीति के द्वारा अवरुद्ध हो गयी है, आर्थिक समानता की लड़ाइयों में वह सक्रिय होकर सामाजिक समानता की दिशा में पुनः गतिशील हो जाएगी। आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय- दोनों लड़ाइयों को संयुक्त ढंग से चलाने की राजनीति नयी राजनीति होगी।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.