(पहली किस्त)

— प्रोफ़ेसर राजकुमार जैन —
फ़िलहाल मुल्क की पहली कतार के बुद्धिजीवी किसान नेता, स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया नामक पार्टी के जन्मदाता जिनकी शीरे जैसी मीठी जुबान, अदब से भरी नफासत हो उनकी कलम इतनी कड़वी हो सकती है, इसका दूर-दूर तक भी अंदाज़ा नहीं था। उनका एक लेख “कुजात लोहियावाद का भविष्य” समता मार्ग में पढ़ने को मिला। मालूम हुआ कि पहले भी कई बार वह छप चुका है। शायद आगे भी छपवाते रहे।
साथी योगेन्द्र यादव, सोशलिस्ट तहरीक से जुड़े रहे हैं। छात्र जीवन में उनको प्रो. आनन्द कुमार की सरपरस्ती तथा बाद में डॉ. राममनोहर लोहिया के शार्गिद किशन पटनायक के वैचारिक अखाड़े (समाजवादी जनपरिषद्) में कई वर्ष इन्होंने रियाज किया है। इसलिए जब ये लोहिया और उनके अनुयायियों पर कुछ लिखते या बोलते हैं तो उस पर ध्यान जाना लाज़मी है। इन्होंने अपने लेख में जहाँ एक ओर आज के दौर में जो लोग अपने को लोहिया अनुयायी मानते हैं, उनकी कमियों को उकेरते हुए उनको उपदेश, सीख या मार्गदर्शन जो भी कहो दिया है। वहीं डॉ लोहिया के वैचारिक दर्शन की कमियों, सीमाओं, अव्यावहारिकता पर प्रकाश डाला है। और लेख के आखिरी हिस्से में लोहिया के विचार और राजनीति की कुछ प्रासंगिकता सार्थकता को कबूल किया है।
लेखक शीर्षक में ही ग़लती कर बैठे। डॉ. लोहिया की नकल कर ‘कुजात लोहियावाद का भविष्य’ दे दिया। राजनीति में कुजात शब्द का इस्तेमाल पहले पहल लोहिया ने ही किया था। 1963 में गांधी जन्म शताब्दी के मौके पर लोहिया ने कहा था कि “आज गांधी जी का कोई भी सार हम लोगों को सीखना है और उसमें से कुछ निकालना है, तो हमें इस समय कितने प्रकार के गांधीवादी हैं, यह जान लेना चाहिए। एक तो हैं सरकारी गांधीवादी, जिनके नेता है श्री नेहरू और गांधीवादियों में आजकल ज्यादातर सरकारी गांधीवादी ही हैं। दूसरे प्रकार के हैं, मठ, मंदिर वाले गांधीवादी, मठाधीश गांधीवादी जिनके नेता आचार्य विनोबा भावे। वे भी अपनी समझ के अनुसार गांधीवाद को सरकारी गांधीवाद के साथ इधर-उधर सहयोग करते हुए बनाए रखना चाहते हैं। एक तीसरी प्रकार के हैं। वह है कुजात गांधीवादी ये तीन प्रकार के गांधीवादी हैं। सरकारी गांधीवादी, मठी गांधीवादी और कुजात गांधीवादी। इन तीनों को अगर हिंदुस्तान की जनता ठीक तरह से समझ जाए तो फिर अभी मैंने जो तीसरा प्रकार बताया है, ये अगर गांधी जी के 100वें जन्मदिवस का हिंदुस्तान में उत्सव मनाएं तो अलबत्ता देश में नई ताकत और नई जान आएगी।
हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि बरतानिया हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जंग कांग्रेस पार्टी के झण्डे तले महात्मा गांधी की रहनुमाई में लड़ी गयी थी। मुल्क के आज़ाद होने पर हिंदुस्तान का आम आदमी कांग्रेस और पं. जवाहरलाल नेहरू की सरकार की शिनाख्त महात्मा गांधी से करता हुआ कांग्रेस का समर्थक बना हुआ था। 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव तक हालात ऐसे बने हुए थे। 1963 में लोहिया ने इस घटाटोप के खात्मे के लिए तीन तरह के गांधीवादियों का जुमला गढ़ा।
1952 से लेकर 1962 तक के तीन आम चुनावों में कांग्रेस की प्रचण्ड बहुमत वाली सरकारें केंद्र से लेकर राज्यों तक में बनी हुई थीं। सरकारी और गैर सरकारी, देशी-विदेशी फण्डों के आधार पर गांधी जी के नाम पर बने बड़े-बड़े संस्थान देश-विदेश में आरामगाह का साधन बने हुए थे। ऊपर से गैरसियासी परंतु अंदर से पूरी तरह कांग्रेस समर्थक कार्य, वैतनिक राजनैतिक संत कर रहे थे, ऐसे हालात में, लोहिया ने अपने को स्थापित गांधीवादियों की जमात से अलग कुजात घोषित किया।
सवाल उठता है कि आज कहाँ सरकारी लोहियावादी हैं? कुल मिलाकर कभी-कभी बिहार, उत्तरप्रदेश में वक्ती तौर पर दूसरों कीबैसाखी पर इनकी सरकार बनी है या बन सकती है, केंद्र में तो दूर-दूर तक इसका नामोनिशान नहीं है। जहाँ तक मठवादी समाजवादियों की बात है तो मठ बनाना तो दूर, छोटी-मोटी वैचारिक संस्था चलाना भी मुश्किल हो रहा है, जिस ‘समता मार्ग’ में यह लेख छपा है, उसको चलाने के लिए, आर्थिक मदद की गुहार रोज-बरोज समाजवादी समागम लगा रहा है।
आज के दौर में अगर नामकरण करना ही है, तो वह दिखावटी समाजवादी तथा विचार आग्रही समाजवादी के रूप में किया जा सकता है। न कि सरकारी, मठी व कुजात के रूप में।
लेख में शिकायत है कि लोहियावादियों में लोहिया के प्रति अंधभक्ति, उनकी आलोचना के प्रति असहिष्णुता का दोष न केवल लोहियावादियों का चारित्रिक दोष है, चाहे गांधीवादी हो या मार्क्सवादी सभी स्थापित ‘वादों’ के अनुयायी कमोबेश इसी परंपरा का पालन करते हैं। समाजवादियों में यह दोष लोहिया के अनुयायियों में अधिक रहा है। यहाँ पर लेखक ने ईमानदारी बरतते हुए, बिना लाग-लपेट के हर वैचारिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को संदेश दिया है कि कभी भी किसी वैचारिकता अथवा दार्शनिक चिंतक से मत बंधो, स्वच्छंद रहो, अपने को स्वतंत्र रखो, सुविधानुसार जहाँ सुख सुविधा मिले, वो रास्ता खोलकर रखो। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि मुत्तलिफ तंजीमों में तमाम उम्र खपाने वाले कारकून जो केवल विचार और किसी दार्शनिक को घोषित रूप से मानकर चलते हैं, वे सब बेबकूफ है।
लोहिया के गांधी से रिश्ते को पारिभाषित करते हुए लेखक ने लिखा है कि लोहिया ने गांधी जी से अपने अनूठे रिश्ते को पारिभाषित किया था। न अंध श्रद्धा, न तिरस्कार उनके प्रति एक गुरु जैसा सम्मान-भाव। परंतु लेख में पाठक को समझाने के लिए एक भी उदाहरण नहीं दिया गया। इस लेख में गांधी लोहिया के रिश्ते की पूरी तफसील तो नहीं लिखी जा सकती परंतु लोहिया गांधी जी के प्रति कितनी अंध श्रद्धा रखते थे, किसी विषय पर अलग राय होने पर भी अंतत: वे गांधी की सलाह को अंतिम मानकर चलते थे, इसकी कुछ मिसाल दी जा सकती है।
“दूसरे महायुद्ध के शुरू होने के कुछ दिन पहले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक विशेष अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रश्न उठा था। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय वहाँ रद्दी कानूनों के प्रति सदा संघर्ष करते रहे हैैं। गांधी जी ने खुद ही प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया था जो कांग्रेस कमेटी के सामने रखा गया। लोहिया को यह प्रस्ताव मंज़ूर नहीं था। उन्होंने गांधी जी द्वारा लिखित प्रस्ताव पर दो संशोधन पेश कर दिये। गांधी जी संशोधनों से बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कहलवाया कि या तो अ. भा. कां. क. का पूरा प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार करें या वापिस कर दे। लोहिया इसके लिए तैयार नहीं थे।
लोहिया लिखते हैं कि मैंने महादेव देसाई (गांधी जी के सचिव) की ओर देखा और कहा “आपका (गांधी जी का) तर्क मुझे मंज़ूर नहीं फिर भी एक सवाल रहता है कि न तो यह (कांग्रेस) कार्यकारिणी और न मेरे जैसे अनेक लोग ही दक्षिण अफ्रीका में सिविल नाफरमानी चलाने में समर्थ हैं। यह आंदोलन तो गांधी जी को ही चलाना है, अत: यदि वे हमारी बात स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो सहज ही मुझे भी कम दरजे की सिविल नाफरमानी और बिल्कुल सिविल नाफरमानी न होना, इनमें से ही चुनाव करना होगा। महादेव भाई ने कहा ‘हाँ यही बात है।’ यही सही दृष्टिकोण है। मैंने कहा तब तो मेरे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचता कि वापसी (संशोधन वापिस) मान लूं। संशोधनों को वापिस लिया गया और प्रस्ताव मूल रूप में पास हुआ। केवल बिना किसी बहस के ब्रिटिश भारतीय को भारतीय कर दिया गया।
लोहिया जब सभा से बाहर जा रहे तो, सुभाषचंद्र बोस लोहिया के पास गए तथा व्यंग्य किया। क्या समझे कि शक्तिशाली कौन है, महात्मा गांधी या कांग्रेस दल? तो लोहिया ने कहा “मैं हर समय यह समझता रहता हूँ, और समझ कर ही सब करता हूँ।” गांधी जी की शक्ति कांग्रेस दल से निश्चय ही बड़ी थी। दल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से गांधी की इच्छा अधिक बड़ी थी।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








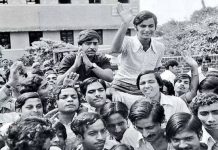







प्रोफेसर राजकुमार जैन जी के लेख “जी हां हम अंधभक्त हैं….” की पहली किस्त के पहले पैरा में कहा गया है कि ‘कुजात लोहियावाद का भविष्य’ शीर्षक से योगेन्द्र यादव का लेख पहले सामयिक वार्ता में छपा था और शायद वो आगे भी इसे छपवाते रहेंगे। यह बात सही है कि वह लेख पहले सामयिक वार्ता में छपा था। आगे कब कौन छापेगा, कौन जाने, लेकिन वह समता मार्ग में छपा तो इसमें योगेन्द्र जी की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने समता मार्ग में छापने के लिए उसे भेजा नहीं था। यह भी नहीं हुआ कि हमने उनसे लेख मांगा हो तथा उन्होंने कोई और लेख देने के बजाय यही लेख पकड़ा दिया हो। यह लेख मेरे पास काफी पहले से था और मैंने सिर्फ मैसेज भेजकर उन्हें सूचित किया था कि उनके उपर्युक्त लेख को हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। वह समता मार्ग में छपा तो इसमेें उनका कोई हाथ नहीं है। उनका लेख छापे जाने के बारे में आनंद जी (डॉ आनंद कुमार) को बताया था, लेकिन वह लेख उन्होंने देखा नहीं था। इसलिए इसे छापने के बारे में उनकी सहमति या असहमति का सवाल ही नहीं उठता। इसे छापने के लिए शत-प्रतिशत मैं जिम्मेवार हूं। बाकी बातों की बहस में फिलहाल मैं नहीं पड़ना चाहता।