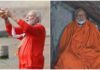सामाजिक समता की स्थापना के लिए विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को गांधीजी आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार ऐसा ही विकेंद्रीकरण देश के आर्थिक जीवन में भी होना चाहिए। वे बड़े-बड़े कल-कारखानों की स्थापना के विरुद्ध थे। उनके विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का विस्तार यदि पर्यावरण के क्षेत्र में करें तो विशाल बांधों की स्थापना के बजाय छोटे-छोटे स्टॉप डैम्स की स्थापना और तालाबों के संरक्षण तथा संवर्धन का सिद्धांत सामने आता है। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर्यावरण मित्र जीवन शैली की आदर्श अवस्था को दर्शाती है।
ग्राम स्वराज्य के विषय में उन्होंने लिखा- “ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुत सी ऐसी दूसरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह हर एक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिए जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के लिए मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बंदोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें उगाए जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके।” (हरिजन सेवक, 2 अगस्त 1942)
गांधीजी के सपनों के गांव में सामाजिक समरसता ही वह ताना-बाना होगी जिस पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करनेवाली राष्ट्र एवं विश्व व्यवस्था कायम होगी। वे कहते हैं- “आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके। ——- इस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। ——– जिस समाज का हर एक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए। ऐसे समाज की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है।
“मेरी राय है कि जब तक ईश्वर पर जीता-जागता विश्वास ना हो तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है।——– ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ल में होगा।
“जिंदगी मीनार की शक्ल में नहीं होगी जहां ऊपर की तंग चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहां तो समुद्र की लहरों की तरह जिंदगी एक के बाद एक घेरे की शक्ल में होगी और व्यक्ति उसका मध्य बिंदु होगा। इस समाज में सबसे बाहर का घेरा या दायरा अपनी ताकत का उपयोग भीतर वालों को कुचलने के लिए नहीं करेगा बल्कि उन सब को ताकत देगा और उनसे ताकत पाएगा। ——— यूक्लिड की परिभाषा वाला बिंदु कोई मनुष्य खींच नहीं सकता फिर भी उसकी कीमत हमेशा रही है और रहेगी। इसी तरह मेरी इस तस्वीर की भी कीमत है।

“जिस चीज को हम चाहते हैं उसकी सही-सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिए तभी हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज पाने की आशा रख सकते हैं। इस तस्वीर में उन मशीनों के लिए कोई जगह नहीं होगी जो मनुष्य की मेहनत का स्थान लेकर कुछ लोगों के हाथों में सारी ताकत इकट्ठी कर देती हैं। सभ्य लोगों की दुनिया में मेहनत की अपनी अनोखी जगह है। उसमें ऐसी ही मशीनों की गुंजाइश होगी जो हर आदमी को उसके काम में मदद पहुंचाए।” (हरिजन सेवक, 28 जुलाई 1946) ———-ग्राम उद्योगों का यदि लोप हो गया तो भारत के सात लाख गांवों का सर्वनाश ही समझिए।
“अनेक आलोचकों ने तो मुझे यह सलाह दी है कि मनुष्य की अन्वेषण बुद्धि ने प्रकृति की जीवनी शक्तियों को अपने वश में कर लिया है, उनका उपयोग करने से ही गांवों की मुक्ति होगी। उन आलोचकों का यह कहना है कि प्रगतिशील पश्चिम में जिस तरह पानी, हवा, तेल और बिजली का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है उसी तरह हमें भी इन चीजों को काम में लाना चाहिए। इस रास्ते अगर हम हिंदुस्तान में चले तो मैं बेधड़क कह सकता हूं कि हमारे प्रत्येक मनुष्य की गुलामी बेतहाशा बढ़ जाएगी।
“यंत्रों से काम लेना उसी अवस्था में अच्छा होता है जब किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हों या नपे-तुले हों। पर यह बात हिंदुस्तान में तो है नहीं। यहां काम के लिए जितने आदमी चाहिए उनसे कहीं अधिक बेकार पड़े हुए हैं। इसलिए उद्योगों के यंत्रीकरण से यहां की बेकारी घटेगी या बढ़ेगी? हमारे यहां सवाल यह नहीं है कि हमारे गांवों में जो लाखों-करोड़ों आदमी पड़े हैं, उन्हें परिश्रम की चक्की से निकालकर किस तरह छुट्टी दिलाई जाए बल्कि यह है कि उन्हें साल में जो कुछ महीनों का समय यूं ही बैठे-बैठे आलस में बिताना पड़ता है उसका उपयोग कैसे किया जाए? कुछ लोगों को मेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी पर दरअसल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः आज गांव की जनता के लिए त्रासरूप हो रही है। उनकी रोजी पर यह मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं। (हरिजन सेवक 23 नवंबर 1934)।
गांधीजी द्वारा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण और मशीनों के नकार का आग्रह अनायास नहीं था। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि लोकतंत्र मशीनों यानी कि प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन के केंद्रीकृत विशाल संसाधनों यानी कि उद्योग का दास होता है। गांधीजी यह जानते थे कि लोकतंत्र पर अंततः कॉर्पोरेट घरानों और टेक्नोक्रेट्स का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था बिग बिज़नेस हाउसेस के हितों की रक्षा के लिए समर्पित हो जाएगी।
गांधीजी का आर्थिक और राजनीतिक दर्शन भी अहिंसा की बुनियाद पर टिका हुआ है। मुनाफे और धन पर अनुचित अधिकार जमाने की वृत्ति आर्थिक हिंसा को उत्पन्न करती है। जबकि धार्मिक-सांस्कृतिक तथा वैचारिक-राजनीतिक-सामरिक आधिपत्य हासिल करने की चाह राज्य की हिंसा को जन्म देती है। गांधी राज्य की संगठित शक्ति को भी हिंसा के स्रोत के रूप में परिभाषित करते थे। यही कारण था कि वे शक्तियों के विकेंद्रीकरण के हिमायती थे।
व्यक्तिगत स्वातंत्र्य उनके लिए सर्वोपरि था। किंतु उन्हें पश्चिम के अराजकतावादियों की श्रेणी में रखना ठीक नहीं है। वे एनलाइटेंड अनार्की के समर्थक थे। उनके मतानुसार जब मनुष्य नैतिक रूप से इतना विकसित हो जाएगा कि स्वयं पर शासन कर सके तब राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता राज्य की जरूरत बनी रहेगी।
गांधीजी आधुनिक सभ्यता के उदारवाद से भी कभी सहमत नहीं हो पाये। उदारवाद का पूरा दर्शन अमूर्त व्यक्ति के लिए निरपेक्ष स्वतंत्रता की स्थापना पर आधारित है। किंतु जैसा अभय कुमार दुबे और विश्वनाथ मिश्र जैसे गांधी के आधुनिक व्याख्याकार स्पष्ट करते हैं कि समाज में न तो अमूर्त व्यक्ति होता है, न ही निरपेक्ष स्वतंत्रता। गांधी आधुनिक सभ्यता की समानता की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि यह केवल भौतिक संसाधनों के समान वितरण तक सीमित रह जाती है। गांधीजी की समानता और समरसता की अवधारणा मानव मात्र की समानता और बंधुत्व तक सीमित नहीं है अपितु इसका विस्तार मानवेतर जगत तक है जिसमें पशु-पक्षी-लता-पादप आदि सभी जीवित अजीवित अस्तित्व सम्मिलित हैं।
(समाप्त)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.