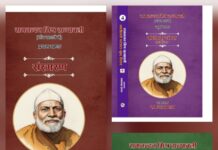वकालत के पेशे में मेरा मन न था। नागपुर के अधिवेशन में जब असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया तो उसके अनुसार मैंने तुरंत वकालत छोड़ दी। इस निश्चय में मुझे एक क्षण की भी देर न लगी। मैंने किसी से परामर्श भी नहीं किया, क्योंकि मैं कांग्रेस के निर्णय से अपने को बँधा हुआ मानता था। मैंने अपने भविष्य का भी ख्याल नहीं किया। पिताजी से एक बार पूछना चाहा, किंतु यह सोच कर कि यदि उन्होंने विरोध किया तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकूँगा, मैंने उनसे भी अनुमति नहीं माँगी। किंतु पिताजी को जब पता चला तो उन्होंने कुछ आपत्ति न की। केवल इतना कहा कि तुमको अपनी स्वतंत्र जीविका की कुछ फिक्र करनी चाहिए और जब तक जीवित रहे, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होने दी।
असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद एक बार पण्डित जवाहरलाल फ़ैजाबाद आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बनारस में विद्यापीठ खुलने जा रहा है। वहाँ लोग तुम्हें चाहते हैं। मैंने अपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसादजी को पत्र लिखा। उन्होंने मुझे तुरंत बुला लिया। शिवप्रसाद जी मेरे सहपाठी थे। और विचार-साम्य होने के कारण मेरी-उनकी मित्रता हो गयी। वह बड़े उदार हृदय के व्यक्ति थे। दानियों में मैंने उन्हीं को एक पाया जो नाम नहीं चाहते थे। क्रांतिकारियों की भी वह धन से सहायता करते थे। विद्यापीठ के काम में मेरा मन लग गया। श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास ने मुझ पर विश्वास कर मुझे उपाध्यक्ष बना दिया। उन्हीं की देखरेख में मैं काम करने लगा। मैं दो वर्ष तक छात्रावास में ही विद्यार्थियों के साथ रहता था। एक कुटुंब-सा था। साथ-साथ हम लोग राजनीतिक कार्य भी करते थे। कराची में जब अलीबंधुओं को सजा हुई थी, तब हम सब बनारस के गाँवों में प्रचार के लिए गये थे। अपना-अपना बिस्तर बगल में दबा, नित्य पैदल घूमते थे। सन् 1926 में डाक्टर साहब ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया और मुझे अध्यक्ष बना दिया।
बनारस में मुझे कई नये मित्र मिले। विद्यापीठ के अध्यापकों से मेरा बड़ा मीठा संबंध रहा है। श्री श्रीप्रकाशजी मेरा विशेष स्नेह हो गया। यह अत्युक्ति न होगी कि वह स्नेहवश मेरे प्रचारक हो गये। उन्होंने मुझे आचार्य कहना शुरू किया। यहाँ तक कि वह मेरे नाम का एक अंग बन गया है। सबसे वह मेरी प्रशंसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलाल जी से होमरूल आंदोलन के समय से था, तथापि श्री प्रकाशजी द्वारा उनसे तथा गणेश जी से मेरी घनिष्ठता हुई। मैं उनके घर में महीनों रहा हूँ। वह मेरी सदा फिक्र उस तरह करते हैं, जैसे माता अपने बालक की। मेरे बारे में उनकी राय यह है कि मैं अपनी फिक्र नहीं करता हूँ। शरीर के प्रति बड़ा लापरवाह हूँ। मेरे विचार चाहे उनसे मिलें या न मिलें, उऩका स्नेह घटता नहीं। सियासत की दोस्ती पायदार नहीं होती। किंतु विचारों में अंतर होते हुए भी हम लोगों के स्नेह में फर्क नहीं पड़ा है। पुराने मित्रों से वियोग दुःखदायी है। किन्तु यदि शिष्टता बनी रहे तो संबंध में बहुत अंतर नहीं पड़ता, ऐसी मिसालें हैं, किंतु बहुत कम।
नेता के मुझमें कोई भी गुण नहीं हैं। महत्त्वाकांक्षा भी नहीं है। यह बड़ी कमी है। मेरी बनावट कुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हूँ और न अंधभक्त अनुयायी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अनुशासन में नहीं रहना चाहता। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ। नेताओं की दूर से आराधना करता रहता हूँ। उनके पास बहुत कम जाता रहा हूँ। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है। आत्म-प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता; अच्छा पद पाकर किसको प्रसन्नता नहीं होती। किंतु मैंने कभी इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति होने के लिए मैंने अनिच्छा प्रकट की। किंतु अपने मान्य नेताओं के अनुरोध पर खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मुझसे वर्किंग कमेटी में आने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। किंतु उनके आग्रह करने पर मुझे निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा।
मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए किसी नये आंदोलन या पार्टी का आरम्भ नहीं कर सकता। सन् 1934 में जब जयप्रकाश जी ने समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और मुझे सम्मेलन का सभापति बनाना चाहा तो मैंने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि समाजवाद को नहीं मानता था, अपितु इसलिए कि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था। उनसे मेरा काफी स्नेह था और इसी कारण मुझे अंत में उनकी बात माननी पड़ी। सम्मेलन पटना में मई, 1934 में हुआ था। बिहार में भूकंप हो गया था। उसी सिलसिले में विद्यार्थियों को लेकर काम करने गया था। वहाँ पहली बार डाक्टर लोहिया से परिचय हुआ। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि जब पार्टी का विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पक्ष में थे कि उद्देश्य के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिए। अंत में हम लोगों की विजय हुई। श्री मेहर अली से एक बार सन् 1928 में मुलाकात हुई थी। बम्बई के और मित्रों को मैं उस समय तक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियों के साथ काम करते मुझको घबराहट होती है। किंतु प्रसन्नता की बात है कि सोशलिस्ट पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शीघ्र ही एक कुटुंब के सदस्य की तरह हो गए।
यों तो मैं अपने सूबे में बराबर भाषण किया करता था, किंतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मैं पहली बार पटना में बोला। मौलाना मुहम्मद अली ने एक बार कहा था कि बंगाली और मद्रासी कांग्रेस में बहुत बोला करते हैं; बिहार के लोग जब औरों को बोलते देखते हैं तो खिसककर राजेन्द्र बाबू के पास जाते हैं और कहते हैं कि “रौवां बोली न”, और यू.पी. के लोग खुद नहीं बोलते और जब कोई बोलता है तो कहते हैं, “क्या बेवकूफ बोलता है!” हमारे प्रांत के बड़े-बड़े नेताओं के आगे हम लोगों को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक समय पण्डित जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे। किंतु 1934 में मुझे पार्टी की ओर से बोलना पड़ा। यदि पार्टी बनी न होती तो शायद मैं कांग्रेस में बोलने का साहस भी नहीं करता।
पण्डित जवाहरलाल जी से मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी। इस कारण तथा उनके ऊँचे व्यक्तित्व के कारण मेरा मन उनके प्रति सदा आकर्षण रहा है। उनके संबंध में कई कोमल स्मृतियाँ हैं। यहाँ केवल एक बात का उल्लेख करता हूँ। हम लोग अहमदनगर के किले में एक साथ थे। एक बार टहलते हुए कुछ पुरानी बातों की चर्चा चल पड़ी। उन्होंने कहा– नरेन्द्रदेव! यदि मैं कांग्रेस के आंदोलन में न आता और उसके लिए कई बार जेल की यात्रा न करता तो मैं इंसान न बनता। उनकी बहन कृष्णा ने अपनी पुस्तक में जवाहरलाल जी का एक पत्र उद्धृत किया है जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। पं. मोतीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपनी बहनों को लिखा कि पिता की संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका ट्रस्टी मात्र हूँ। उस पत्र को पढ़कर मेरी आँखों में आँसू आ गये और मैं जवाहरलाल जी की महानता को समझा। उनको अपने साथियों का बड़ा ख्याल रहता था और बीमार साथियों की बड़ी शुश्रुषा करते थे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.