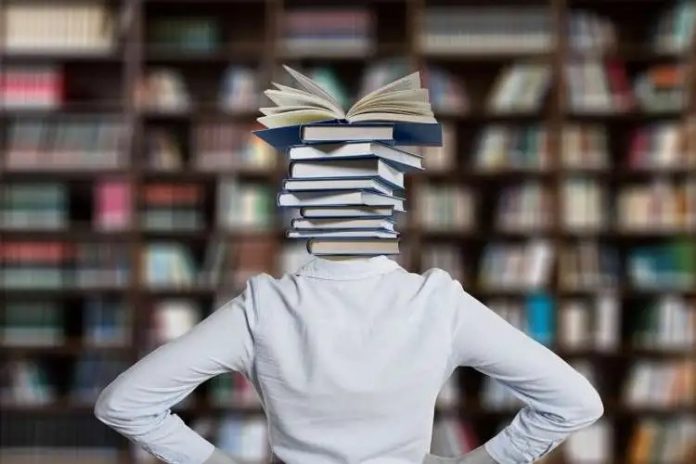— पंकज पुष्कर —
तुलसीदास रचित रामचरितमानस की शुरुआत बहुत रोचक है। तुलसीदास संस्कृतवादी ब्राह्मणों का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें बार-बार नमस्कार करते हैं। भक्त कवि ‘खल वंदना’ और निर्विघ्न आगे बढ़ने की मंगलकामना करता है। तुलसीदास का अपराध इतना भर था कि उन्होंने रामकथा को ‘देवभाषा’ के सिंहासन से उतार कर अवधी भाषा की जमीन पर ला पटका था। भले ही कहानी वर्ण व्यवस्था की समर्थक, नारी को आदर्श पढ़ानेवाली और आर्य श्रेष्ठता का मिथक रचनेवाली ही क्यों न हो लेकिन उसे अपात्र और असंस्कृत जनता तक पहुँचाना अक्षम्य था! संस्कृत से अवधी जैसी बोलियों में आते ही राम, राम के भक्त और राम का शास्त्र सब कुछ थोड़ा-बहुत जरूर बदल गया। उस समय के संस्कृतवादियों के क्रोध के कारणों को समझा जा सकता है।
यह किस्सा हमें समाज चिंतन और भाषाओं के सवाल पर सोचने की प्रेरणा देता है। समाज विज्ञान का कोई भी छात्र समझ सकता है कि जब धर्म और समाज से किसी तरह के बदलाव की माँग नहीं करनेवाली तुलसीकृत रामकथा तक को जनभाषा में आने पर इतना विरोध सहना पड़ा तो समाज के शास्त्र पर कायम अंग्रेजी की इजारेदारी हटा लेने से क्या होगा। यकीनन समाज चिंतन पर छाया अंग्रेजी का प्रभामंडल धूमिल पड़ जाएगा। तमाम नीति-नियम, विधि-विधान और बौद्धिक विमर्श अंग्रेजी में दैवीय और पावन लगता है लेकिन भाषाओं में आते ही ढोल की पोल खुल जाती है। ज्ञान के आधार पर बनी दीवारों में खिड़कयाँ खुलने लगती हैं। धीरे-धीरे खिड़कियाँ दरवाजे और रास्तों में बदल जाती हैं और दीवार पर्दों में।
हालाँकि भाषाओं में और खासतौर से हिंदी में समाज विज्ञान के मुद्दे पर मंथन होते ही बहुत सारे सवाल सतह पर आ जाते हैं। आखिर हिंदी में समाज विज्ञान के मायने क्या है और हम किस हिंदी की बात कर रहे हैं? हम हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा या जनभाषा। याद रखें कि भारत में राजकाज की भाषा और कामकाज की भाषा हमेशा अलग रही है। शासक वर्ग के लिए जरूरी होता है कि सत्ता को लोक से दूर रखा जाए। हिंदी में समाज विज्ञान की किसी नयी पहल से पहले हमें स्वयं से पूछना होगा कि हमें हिंदी कैसी चाहिए?
हमें यह भी साफ करने की जरूरत होगी कि हमें हिंदी की साधना करनी है या हिंदी की मदद से कुछ साधना है। इतिहास बताता है भाषाओं की पीठ पर चढ़कर अमूर्त राष्ट्रवाद की अस्मितापरक राजनीति भी की जा सकती है। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर भाषा का अपना सामाजिक भूगोल होता है। हम एक भाषा संसार से संवाद करते हुए ही उस संसार की उलझन और अंतर्विरोधों को समझ सकते हैं। हिंदी की तमाम सह-भाषाओं में सोचने और जीनेवाले समाजों में छुपे ज्ञान और कौशल को खोज सकते हैं।
हमारे सामने समाज विज्ञानों से जुड़ी कुछ मान्यताएँ और तजुर्बे भी हैं। एक मान्यता रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान किस भाषा में विकसित हुआ है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि जब कोई ज्ञान-विज्ञान किसी खास भाषा में विकसित होता है तो वह शुद्ध निरपेक्ष सत्य नहीं रह जाता वरन उस भाषा से जुड़ी राजनीति, आर्थिकी और संस्कृति ज्ञान-विज्ञान को अपने रंगों में रँग देती है। इस प्रस्ताव को जाँचने की जरूरत है कि अँग्रेजी में सोचा और लिखा गया समाज विज्ञान किस सीमा तक अँग्रेजी भाषी जगत के अनुभवों से प्रभावित है और किस सीमा तक सार्वभौमिक सत्य है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कोई इस निष्कर्ष पर भी पहुँच सकता है कि समाज विज्ञान में कुछ भी शुद्ध और सत्य नहीं होता। यानी अँग्रेजी में समाज विज्ञान और हिंदी में समाज विज्ञान दो बिलकुल अलग चीजें हैं। यह दूसरी तरह की अति है।
आजादी के बाद भारत में उच्च शिक्षा का काफी फैलाव हुआ। इसी के साथ समाज-विज्ञान पढ़ने-पढ़ाने का कारोबार भी फला-फूला। पढ़ने-पढ़ाने के लिए किताबों का या यूँ कहें कि पाठ्य-पुस्तकों का संसार बनना लाजिमी था। लेकिन पुस्तकों का हरा-भरा संसार नहीं बना वरन मुनाफाखोरी भर के लिए एक बाजार बना। बाजार भी ऐसा बना जिसमें गुणवत्ता की चीजों को ढूँढ़ना और घटिया चीजों से बचना, दोनों ही मुश्किल साबित हुआ। समाज विज्ञान की किताबों को समाज के बारे में समझ साफ करने और आलोचनात्मक चेतना जगाने का काम करना था। यह न हो सका। बहुत लोग कहते हैं कि जिस जगह से शुरुआत हुई वही गलत थी। हर विज्ञान को और खासतौर से समाज के विज्ञान को स्थानीय हवा-पानी-मिट्टी और उस क्षेत्र के इतिहास के अनुसार रूप-रंग लेने की जरूरत होती है।
दरअसल समाज चिंतन की मुख्यधारा भी पंडित नेहरू के एक बड़े प्रोजेक्ट से अछूती नहीं रही। देश के पहले प्रधानमंत्री के आधुनिकता-बोध पर केम्ब्रिज और मास्को का प्रभाव काफी गहरा था। ‘सोशल इंजीनियरिंग’ जैसे शब्द के प्रचलन में आने से बहुत पहले ही नेहरू इसे शुरू कर चुके थे। अपने समय के इस करिश्माई नेता का विश्वास था कि यूरोप में हुए दो सौ वर्ष के विकास को भारत बीस-तीस वर्षों में कर सकता है। यह विश्वास नेकनीयती से तो भरा था लेकिन अपने समाज की बुनावट और खासियत की अनदेखी भी इसमें शामिल थी। इसमें देश की ‘अकुशल’, ‘अवैज्ञानिक’ और ‘पिछड़ी’ जनता में ‘वैज्ञानिक चेतना’ भरने और ‘प्रशिक्षित’ करने का दंभ भी था।
देशभर की लघु-परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं में छुपे ज्ञान और कौशल की अवहेलना कर शुरुआती नेतृत्व ने औद्योगिक देशों में विकसित ज्ञान को सर-आँखों पर लिया। नेहरू ने गांधी की दृष्टि को तो ‘एक बूढ़े की सनक’ कहकर खारिज किया ही, जेपी और लोहिया जैसे अपने शुरुआती समाजवादी मित्रों को पूरी तरह अनदेखा किया। परिणाम यह हुआ कि देश के राजनीतिक अभ्यास में लोकतंत्र के ब्रितानी-अमरीकी तजुर्बे को मानक और आदर्श मानने की एक गलत शुरुआत हो गयी। विकास का रास्ता बहुत करके वही अपनाया गया जो यूरोप में तय हो गया था। राजनीति की इस विवशता को राजनीति के शास्त्र ने अपनी सीमा बना लिया।
इस प्रकार आजादी के बाद से ही जो समाज विज्ञान भारत भर में पसरा वह भारत जैसे समाजों का अपना विज्ञान था, कहना मुश्किल है। असल में यह एक ऐसा समाज विज्ञान था जो बाहरी तौर से तो अँग्रेजी में था ही, अंदरूनी तौर से भी था। समाज विज्ञान और खासकर राजनीति के जो पाठ्यक्रम और किताबें प्रचलन में हैं उन पर बहुत गहरा असर ब्रितानी-अमरीकी दबदबे का है।
यूरोपीय समाज में विज्ञान की बुनियाद पश्चिमी समाज और राजनीति के सैकड़ों बरसों के अनुभव पर पड़ी। भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपना समाज विज्ञान पाश्चात्य जगत के अनुभवों पर ही खड़ा किया। अपने समाज का राजनीतिक तंत्र बनाने के लिए वैचारिक स्वतंत्रता और रचनात्मकता की जरूरत होती है। अपने समाज से सापेक्ष समाज की भाषा में चिंतन और एक देशज समाजशास्त्र गढ़ने की कोशिश इस दिशा में मददगार हो सकती थी लेकिन उपनिवेशवाद के इस मोर्चे पर लड़ने से पहले ही आत्म-समर्पण कर दिया गया।
पश्चिमी शैक्षिक जगत से समाज विज्ञानों को जस का तस उठा लेना तात्कालिक रूप से सुविधाजनक माना गया लेकिन इसके कुछ दूरगामी नुकसान हुए। अपने समाज को सामने रख उसका शास्त्र विकसित करना चुनौती भरा काम था। वर्ण व्यवस्था की गोद में पली आधुनिक जड़ता और काहिली ने इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। नकलची पीढ़ियों को पैदा करने का आसान लेकिन आत्मघाती रास्ता चुन लिया गया। इस पूरे समर्पण के बदले हमें स्वयं को पश्चिम की नजरों से देखनेवाला एक चश्मा मिला। समर्पण करने में नाक इस कदर घिस गयी थी कि यह चश्मा भी ठीक से टिक न सका। इस चश्मे को लगातार दोनों हाथों से पकड़े रहने की जरूरत आ पड़ी।
इसके फलस्वरूप बिना कुछ काम किये ही हाथों में दर्द और दृष्टि में दोष पैदा हो गया। हाथों में हुए इस दर्द के कारण हाथों से किये जानेवाले सभी काम और उन कामों को करनेवाले लोग समाज विज्ञान के फोकस से कमोबेश बाहर हो गये और समाज चिंतन करने के लिए आरामकुर्सी का होना अनिवार्य हो गया। दृष्टिदोष का परिणाम यह हुआ कि भारत में समाज विज्ञान को जाति-धर्म, भाषा-बोली, गाँव-समुदाय, घर-परिवार और ‘तेरी औकात क्या है?’ जैसी खास हिंदुस्तानी सामाजिक सच्चाइयों की जटिलताओं को समझने और अध्ययन के केंद्र में लाने में समय लगा और बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अभी भी बहुतों के लिए गाँव पिछड़ेपन के ढेर हैं, धर्म अफीम है, जाति एक विकृति है या कभी हुआ करती थी।
यह कहना वाजिब नहीं होगा कि मात्र अँग्रेजी में रचे होने के कारण समाज विज्ञान इस तरह का बना। असल में तो अँग्रेजी की प्रभुता की नकल में हिंदी ने भी देवत्व पाने की कोशिश की। एक समय अँग्रेजी में हवा भरने के लिए ‘असभ्यों को सभ्य बनाने का कर्तव्य बोध’ था तो हिंदी के पीछे एक ‘देवभाषा’ खड़ी थी। हिंदी की एक नस्ल तो उतनी ही हवाई और अभिजात्य जा बनी जितनी कि विक्टोरियाई युग की अँग्रेजी थी। यह हिंदी अँग्रेजी की टक्कर में राजभाषा बनने को व्याकुल थी। अँग्रेजी का स्थानापन्न बनने के आग्रह ने इस हिंदी के मन में एक गाँठ बना दी। अँग्रेजी सत्ता की भाषा थी तो ये ‘हिंदी’ भी सत्ता के गलियारों में पहुँचने के लिए मचलने लगी। क्योंकि अंग्रेजी शासकों और शोषकों की भाषा थी इसीलिए जाने-अनजाने इस हिंदी ने भी स्वयं को शासितों और शोषितों से थोड़ा दूर ही रखा। इस हिंदी में जब भी समाज विज्ञान रचने की कोशिश हुई तो वह अँग्रेजी के समाज विज्ञान का उल्था या अनुवाद से ज्यादा कुछ नहीं बना। यहाँ हिंदी का ‘वर्ण चरित’ बाँचने का समय नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि बोलियों में जीनेवाले किसानों और कारीगरों को जात-बाहर कर इस हिंदी ने स्वयं को घर-बाहर कर लिया।
आज यह देखकर अचरज होता है कि हिंदी या अँग्रेजी में राजनीति शास्त्र की कोई भी पाठ्य-पुस्तक उठाकर देख लें उसमें ग्रेट (?) ब्रिटेन के राजा-रानी के किस्सों से शुरू होकर अमरीकी संघ की विशेषताओं को गिनानेवाली ज्ञानधारा का प्रवाह एक जैसा ही होता रहा है। राजनीति की किताबों में राजनीति वहीं ठिठकी खड़ी है जहाँ उसे चर्चिल, विल्सन और स्टालिन ने छोड़ा था। कुछ बदला भी है तो उसे थेगली (पैबंद) की तरह टाँग दिया गया। आज भी प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के लंबे, लद्धड़ उद्धरण हिंदुस्तानी किशोरों के दिमाग पर बमबारी सी करते हुए गुजर जाते हैं। राजनीति की इन किताबों में ज्ञान का सूरज आज भी यूरोप के एक शहर में उगकर दूसरे में डूब जाता है।
लोकतंत्र के बनने की कहानी को उदाहरण के रूप में देखें। ब्रिटेन ने डेमोक्रेसी को ‘ग्रो’ किया सो वहाँ डेमोक्रेसी ‘डेवेलप्ड’ है। इसमें वहाँ के अतीत की अटूट परंपरा का आग्रह है। ब्रिटेन में जो कभी राजतंत्र के पहरुए थे वही बाद में धीरे-धीरे लोकतंत्र के भी स्तंभ बने। वहाँ की राजनीति में नयी भर्ती हुई लेकिन ‘आम’ को भी थोड़ा ‘खास’ बनना पड़ा। अमरीका ने ‘डेमोक्रेसी’ की ‘डिजाइनिंग’ की। ‘साइंस और टेक्नोलॉजी’ में साँस लेनेवाले अमरीका के लिए लाजिमी था कि वह ‘डिजाइन’ करने के व्यक्तिवादी आग्रह को आवाज दे। हिंदुस्तान जैसे मुल्क का समाजशास्त्र इसके लिए ‘लोकतंत्र की चिनाई’ जैसा पद गढ़ सकता है। ‘चिनाई’ इमारत बनानेवाले कारीगर, राज-मजदूर करते हैं। वे अनुभव के धनी होते हैं। ‘लोकतंत्र की चिनाई’ कहते ही न केवल लोकतंत्र की बनावट और बुनावट बदल जाती है बल्कि लोकतंत्र को बनानेवाले और बरतनेवाले सब बदल जाते हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र कुछ इस तरह भी करवट लेता है और संभावनाओं के नये स्रोत खुलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में समता खोजना उस पर आदर्शों का बोझा लादने जैसा है। शायद वे सही हों, लेकिन इतना तो है कि लोकतंत्र की ‘ग्रोथ’, ‘डिजाइनिंग’ और ‘चिनाई’ समता के लिहाज से लोकतंत्र को तीन अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है।
इस सारी बातचीत से समझ में यह आता है कि भाषा एक नहीं अनेक होती है और असल में और हर भाषा के अंदर अनेक उप-भाषाएँ होती हैं। यह बुनियादी तौर से महत्त्वपूर्ण है कि इन भाषाओं और उनके समाजों का मानक होने का धर्म निभानेवाली भाषा से कैसा रिश्ता-नाता है। इस रिश्ते-नाते से ही उस भाषा के अंदर चिंतन और सृजन की संभावनाएँ तय होती हैं। साथ ही यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सत्ता की भाषा और समाज की भाषाओं के बीच रिश्ते कैसे हैं- ये रिश्ते जड़ हैं या बदल रहे हैं? क्या राजभाषा ने स्वयं को लोकभाषा का प्रतिनिधि बना लिया है? क्या आगे चलकर राज और लोक के अंतर मिटने की स्थितियाँ बन रही हैं या जैसे एक ही शासक वर्ग में अदला-बदली होती रहती है उसी तरह राजभाषाओं में हो रही है?
इससे भी आगे जाकर देखें तो भाषाओं में समाज चिंतन की संभावनाएँ भाषाओं में जीनेवाले समाज और उनकी आर्थिकी से जुड़ी हैं। हमेशा से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की खोयी हुई चाबी चौराहे पर खोज रहा है क्योंकि घर के बाहर अँधेरा है और चौराहे पर रोशनी। भाषाओं के दरवाजे पर अँधेरा है। ये अँधेरा दूर कैसे होगा? क्या ही बेहतर होगा कि हिंदी जैसी भाषाओं में समाजशास्त्र गढ़ने के लिए किसी बड़े प्रकाश स्तंभ का इंतजार किये बिना शुरुआत की जाए।