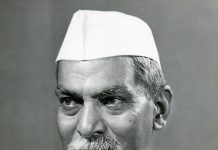(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
विज्ञापन का जादू
एक उदाहरण बालों को सघन और काला रखने की दवाओं तथा तेलों का है। सर्वविदित है कि अभी तक बालों को गिरने या सफेद होने से रोकने का कोई उपचार नहीं निकला है। लेकिन हर रोज ऐसे विज्ञापन निकलते रहते हैं जो लोगों में यह भ्रम पैदा करते हैं कि किसी खास दवा या तेल से उनके बालों की रक्षा हो सकती है और इनसे प्रभावित होकर लोग इन उपचारों पर अंधाधुंध खर्च करते हैं। यही हाल प्रायः दाँत के टूथपेस्टों का है। पत्र-पत्रिकाओं के पृष्ठ चमकीले दाँतोंवाली महिलाओं की तस्वीरों से भरे रहते हैं जो किसी न किसी कंपनी के टूथपेस्ट के चमत्कार के रूप में अपने दाँतों का प्रदर्शन करती होती हैं। एक के बाद एक सभी दाँतों के खराब हो जाने के बाद भी लोग उपचार की दृष्टि से टूथपेस्टों की निरर्थकता नहीं देख पाते। ऐसा गहरा असर इस प्रचार के जादू का होता है। यह स्थिति बिलकुल अशिक्षित समाज में जादू-टोने के प्रति फैले अंधविश्वास से भिन्न नहीं है, लेकिन इस अंधविश्वास के शिकार मूल रूप से शिक्षित कहे जानेवाले लोग ही हैं।
किसी विशेष कंपनी की साड़ी से सजी सुंदर औरत, सूट में खड़ा सुंदर नौजवान, कोकाकोला की बोतलें लिये समुद्रतट के रमणीक माहौल में खड़े सुंदर स्त्री-पुरुष, विशेष कंपनी के बाथिंगसूट में समुद्रतट पर क्रीड़ा करती बालाएँ- इन सबके भड़कीले इश्तहार एक ऐसा मानसिक माहौल तैयार करते हैं कि लोग मॉडलों (इश्तहार के सुंदर स्त्री-पुरुष) की सुंदरता का राज़ विभिन्न तरह के परिधानों और कोकाकोला में देखने लगते हैं। क्विंटल भर वजनवाली महिलाएँ और बड़ी तोंदवाले पुरुष भी इन कंपनियों का सूट या बाथिंगसूट पहने विज्ञापन के मॉडलों जैसे अपने रूप की कल्पना करने लगते हैं। फिर दुकानों में इन कंपनियों के परिधानों और कोकाकोला की तलाश शुरू हो जाती है। इस तरह धीरे-धीरे सुंदरता का अर्थ, मनुष्य की स्वाभाविक सुंदरता, जो उसके स्वास्थ्य और स्वभाव से आती है, न रहकर खास-खास कंपनियों के बने मोजे से लेकर टोपी तक में सजावट बन जाता है। सुंदर का मतलब खास तरह के परिधान में सजना या खास तरह के क्रीम पाउडर से पुता होना बन जाता है। सुंदर शब्द भी अब फैशन से बाहर होता जा रहा है, उसका स्थान ‘स्मार्ट’ ने ले लिया है जिसका सीधा संबंध लिबास, सजधज और अप-टु-डेट अदा से है। प्रचलित फैशन से सुंदरता की परिभाषा कैसे बदल सकती है, इसका एक उदाहरण हम रंग की मैचिंग में देख सकते हैं। सौंदर्य की दृष्टि से रंग की मैचिंग यानी एक ही रंग का सारा लिबास रखना, भोंडी चीज है।
सौंदर्य रंगों की विविधता और उनके उपयुक्त संयोजन से आता है। इसी कारण राजस्थान की सरल ग्रामीण महिलाएँ अपने सस्ते लिबास में भी रंगों के उचित संयोजन से जहाँ भी इकट्ठा होती हैं फूलों की क्यारियों सी सज जाती हैं। लेकिन मैचिंग का पागलपन सवार हो जाने से जहाँ एक हैंडबैग, एक जोड़ा जूता या चप्पल तथा एक रंग की लिपस्टिक से काम चल सकता था वहाँ अब हर कपड़े के रंग के साथ सब कुछ उसी रंग का होना चाहिए। इस तरह अब एक की जगह आधा दर्जन सामान खरीदने की जरूरत हो जाती है। पर सबसे हास्यास्पद तो यह होता है कि काले या नीले कपड़ों से मैच करने के लिए लाल होंठों वाली सुंदरियाँ अपने होंठ काले या नीले रंग में रँगने लगती हैं। इस तरह की मूर्खतापूर्ण सजावट का फैशन फैलाने से लिपस्टिक बनानेवाली कंपनियों को अपना व्यापार बढ़ाने का सीमाहीन सुयोग प्राप्त हो जाता है।
यह सोचा जा सकता है कि अगर भिन्न रंग के कपड़े इकट्ठे हो गये तो वे ही कपड़े अदल-बदलकर ज्यादा दिन पहने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक सुनियोजित ढंग से फैशन-प्रदर्शनों और प्रचार के द्वारा ऐसा मानसिक वातावरण तैयार कर दिया जाता है कि फैशन जल्दी-जल्दी बदलते जाएँ। इस साल की चलन का कपड़ा अगले साल तक के फैशन से बाहर हो जाता है और लोग यह साहस नहीं कर पाते कि ‘संभ्रांत’ लोगों की मंडली या दफ्तर में ‘आउट ऑफ डेट’ लिबास में पहुँचें। इस तरह धड़ल्ले से कपड़ों, जूतों, टोपी आदि में बदलाव होता रहता है। लोग मजबूरी में ही एक-दो साल पहले की चलन का कोई कपड़ा पहनते हैं। पश्चिमी देशों में तो एक तरह की ‘थ्रो अवे’ संस्कृति, जिसकी छाया हमारे यहाँ भी पड़ रही है, फैल रही है, यानी ऐसी चीजों का उत्पादन और प्रयोग बढ़ रहा है जिन्हें कुछ समय या एक ही बार उपयोग में लाकर फेंक दिया जाए।
लेकिन इस संस्कृति को फैलाने के लिए की जानेवाली विज्ञापनबाजी का बोझ भी वे ही लोग ढोते हैं जिनके सिर पर यह संस्कृति लादी जाती है। सबसे पहले तो कंपनियों द्वारा प्रचारित वस्तुओं की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर खर्च होता है। कभी-कभी तो कपनियाँ उत्पादन से अधिक खर्च अपनी वस्तुओं को प्रचारित करने में करती हैं। इस विज्ञापनबाजी के लिए काफी खर्चीले शोध होते रहते हैं। पर परोक्ष रूप से विज्ञापन का बोझ फिर दुबारा उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। विज्ञापन पर किये गये खर्च को अपनी लागत में दिखलाकर कंपनियाँ आयकर में भारी कटौती करा लेती हैं। कंपनियों पर कर की कटौती से आमलोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इस तरह विज्ञापनबाजी से लोगों पर दुहरी आर्थिक मार पड़ती है।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.