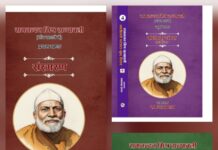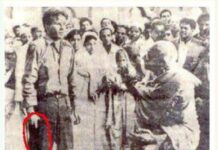(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि वह उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक मजदूर से सृजन का सुख छीन लेती है। यह विशेषता इसे शोषण पर आधारित सभी पिछली उत्पादन प्रणालियों से अलग कर देती है। गुलामी की व्यवस्था, सामंती या भारत की जाति व्यवस्था में भी असली उत्पादक शोषण के शिकार थे और समाज में निरादर के पात्र थे। फिर भी इन व्यवस्थाओं में शिल्पी मजदूर वस्तुओं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर अधिकार रखते थे। इस तरह वे अपनी रुचि और कौशल के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते थे और इसमें उन्हें एक सीमा के भीतर सृजन का सुख मिलता था। जीवन के अन्य क्षेत्रों में कुंठित उनकी आकांक्षाएँ, संवेदनशीलता और कल्पना सभी इन वस्तुओं में समाहित होती थीं। उदाहरण के लिए एक कुम्हार की सारी संवेदना और कल्पना उसकी उँगलियों के स्पर्श से उसके घड़े या अन्य बरतनों के आकार में व्याप्त हो एक आत्मीय रूपाकार देती थी। फिर वह अपनी रुचि से उन्हें पकाने के पहले विभिन्न रंगों और रूपों से सजाता था। फलस्वरूप उसके बरतनों में एक वैयक्तिक अभिव्यक्ति होती थी। ऐसे ही कारणों से यूनान, मध्ययुगीन यूरोप या प्राचीन भारत की स्थापत्यकला, मूर्तिकला या रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं में हम किसी न किसी स्तर की कलात्मकता पाते हैं। कहीं-कहीं तो यह कलात्मकता चरम बिंदु को छू लेती है।
इसके विपरीत पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली ने शुरू से ही जल्द और थोक उत्पादन की पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं के खंडित उत्पादन की प्रक्रिया अपनायी। इसमें एक ही वस्तु के निर्माण के विभिन्न स्तरों को विभिन्न लोगों में बाँट दिया गया और किसी भी निर्माता श्रमिक का नियंत्रण पूरी वस्तु के स्वरूप के निर्माण पर नहीं रहा। उत्पादक अब पूँजीपति थे जो तय करते थे कि क्या निर्मित होगा और अपनी योजना के हिसाब से वे काम का बँटवारा विभिन्न श्रमिकों में करते थे। ‘शिल्पियों’ का स्थान अब श्रमिकों ने ले लिया। पूँजीवादी व्यवस्था के प्रारंभ में पूँजीपति स्वतंत्र श्रमिकों को काम बाँटते थे, बाद में उन्हें एक जगह कारखाने में आकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। कालांतर में जब भाप और बिजली से चालित मशीनों का आविष्कार हुआ तब से मजदूर मशीनों के गुलाम बन गये और उन्हें अपना काम और अपनी गति मशीनों के अनुरूप बनानी पड़ी।
उत्पादन प्रक्रिया में अब श्रमिकों के निजी कौशल का स्थान एकरसता ने ले लिया। उत्पादन का प्रधान गुण ‘स्टैंडर्डाइजेशन’ (एक मानक के भीतर उत्पादन) बन गया। वस्तुओं की विविधता भी श्रमिकों की सृजनात्मकता के साथ समाप्त हो गयी। उत्पादित वस्तु और उत्पादक मजदूर दोनों से उनकी अपनी विशिष्टता छीन ली गयी।
इस उत्पादन पद्धति का सबसे विकसित रूप आधुनिक कारखाने की एसेंबली लाइन है। ये कारखाने ‘कान्वेयर बेल्ट’ का जाल होते हैं जिसके जरिए विभिन्न हिस्सों से मशीन के पुर्जों के हिस्से प्रवाहित होते रहते हैं। अलग-अलग बिंदुओं पर अलग-अलग मजदूर विभिन्न औजारों से पुर्जों में थोड़ा कुछ जोड़ते जाते हैं। इस तरह यह पुर्जा तैयार होकर उस बिंदु पर पहुँचता है जहाँ से उसे कोई दूसरा मजदूर किसी और पुर्जे के साथ जोड़ता है। इस प्रक्रिया के अंत में पूरी मशीन, मोटरगाड़ी, साइकिल आदि हमें तैयार रूप में मिलते हैं। पूरी मशीन की रूपरेखा कुछ विशेषज्ञों द्वारा तैयार किसी ब्लूप्रिंट (नक्शे) में होती है। कारखाने में काम करनेवाले मजदूर कठपुतलियों की तरह चंद सेकेंड या चंद मिनट तक मशीन की गति के हिसाब से कुछ यांत्रिक क्रिया अपने पूरे कर्यकाल में दोहराते जाते हैं। मजदूरों को इस तरह एक यंत्र के रूप में परिवर्तित कर देने का एक फायदा पूँजीपति वर्ग को यह हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार वे मजदूरों की जगह कंप्यूटर से अधिकाधिक काम करा सकते हैं। मजदूर रखे जाएँ या कंप्यूटर, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सस्ता पड़ता है।
इस उत्पादन प्रणाली में मजदूरों को न तो साँस लेने की फुरसत मिलती है और न ही सृजन का सुख क्योंकि उन्हें मशीन की गति से चलना होता है, और दूसरे, उन्हें अपने काम की रूपरेखा की भी कोई जानकारी नहीं होती। इसी प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक उद्योगों के प्रारंभिक काल में ‘एलियेनेशन’(आत्म-दुराव) की संज्ञा दी थी जिसमें मजदूरों का निजत्व जो उनकी श्रम-प्रक्रिया से जुड़ा है उनसे अलग हो जाता है और यह श्रम जब उत्पादन के जरिए पूँजी का रूप ग्रहण कर लेता है तो फिर मजदूरों के शोषण का औजार बन जाता है।
( जारी )
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.