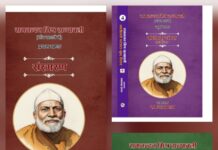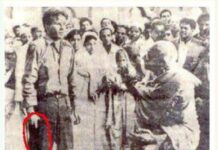(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
वस्तुओं को जमा करने की लत
पहले उत्सवों में आनंद के लिए शराब पी जाती थी। अब जीवन की नीरसता और ऊब से छुटकारे के लिए शराब पी जाती है। इस तरह उन समूहों में जिनका काम सबसे नीरस है या जिनकी जिंदगी अर्थहीन बन गई है, उनमें शराबीपन सबसे अधिक फैल रहा है। लेकिन शराब, चाय, कॉफी या कोकाकोला का नशा थोड़ा सीमित है। जो सबसे बड़ी अफीम लोगों को अपनी स्थिति को भूलने के लिए इस संस्कृति ने दी है वह उपभोग की वस्तुओं को जमा करने की लत। यह अधिक से अधिक समय लोगों को व्यस्त रख सकती है। कुछ समय दुकानों की सजी खिड़कियों में झाँककर नई वस्तुओं के ‘अन्वेषण’ में लगता है, फिर कुछ समय उन्हें उपलब्ध करने या उसके लिए साधन जुटाने की योजना में और अंत में घर में लाने पर उनके रख-रखाव में। धर्म नहीं, जैसा मार्क्स ने कहा था, आधुनिक युग की अफीम तो उपभोक्तावादी हविस है। इस हविस के अधीन होने पर वस्तुओं को पाने की कल्पना में मजदूर भी अपनी सामाजिक स्थिति भूल जाता है और अपने वर्ग-स्वार्थ की रक्षा के लिए शोषकवर्ग से संघर्ष करने के बजाय उस वर्ग की जीवन पद्धति की ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगता है और एक हद तक उसका प्रशंसक बनकर उसके मूल्यों को आत्मसात कर लेता है। पश्चिमी दुनिया में इस हविस के कारण समाज परिवर्तन की शक्ति बनने के बजाय, उपभोक्तावादी मूल्यों का शिकार मजदूर अब पूँजीवादी व्यवस्था का जबरदस्त स्तंभ बन गया है।
समता और बंधुत्व के मूल्यों का लोप
मजदूरवर्ग की क्रांतिकारिता का क्षरण समता और बंधुत्व के मूल्यों को लाँघकर उपभोक्तावादी मूल्य अपनाने से ही हुआ है। उपभोक्तावादी समाज ने दो मान्यताओं को जन्म दिया है। एक तो यह कि उपभोग की जो वस्तुएँ आज कुछ लोगों को उपलब्ध हैं वे धीरे-धीरे सबों को उपलब्ध हो सकती हैं, और दूसरी तरफ यह कि समता अपने आप में कोई साध्य नहीं है। इस तरह समता और संपन्नता को दो विसंगतियों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। चूँकि इस मत के अनुसार पूँजीवादी समाज संपन्नता दे सकता है अतः समता की बात अप्रासंगिक हो गई है। कहा जाएगा कि यह ठीक है कि कुछ लोग सीढ़ी के उच्चतम स्तरों पर हैं और बाकी के लोग नीचे की सीढ़ियों पर, लेकिन चूँकि ये सीढ़ियाँ ‘स्केलेटर’ (चलती हुई यांत्रिक सीढ़ी जिस पर चढ़ते ही अपने आप आदमी ऊपर पहुँचने गलता है।) की हैं सारे लोग ऊपर जा रहे हैं – नीचेवाले भी और जो ऊपर हैं वे भी। अगर इन दोनों के बीच की दूरी नहीं मिटती, अगर उनके बीच बीसियों स्तरों के भेद हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सच तो यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति, समाज को किसके पास क्या उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध हैं, इस आधार पर असंख्य वर्गों में बाँटती जाती है और उनके बीच भावनात्मक भेद पैदा करती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मार्क्स की कल्पना के विपरीत पश्चिम के विकसित पूँजीवादी समाज में, जहाँ उपभोक्तावाद पूरी तरह से हावी है, मजदूरों की वर्ग-चेतना नष्ट हो गई और बड़ी तादाद में मजदूर अपने को भावना के स्तर पर मध्यमवर्ग में शामिल करने लगे हैं क्योंकि मालिक मजदूरों के भेद के बजाय उपभोक्तावादी मानक के हिसाब से, मजदूरों के आपसी भेद रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा उजागर होते रहते हैं।
मजदूरों की चेतना पर उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव का एक आँख खोलने वाला परिणाम 1968 में फ्रांस में देखने को मिला। उस समय पश्चिमी देशों के युवावर्ग और खासकर छात्रों में पूँजीवाद और उससे जुड़े उपभोक्तावादी मूल्यों के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह की लहर दौड़ गई थी। इसका एक ऐसा विस्फोट 1968 के मई महीने में फ्रांस में हुआ कि वहाँ की हुकूमत गहरे संकट में पड़ गई थी। सौरबोन विश्वविद्यालय के छात्रों ने पेरिस में ‘बैरिकेड’ (विद्रोह के समय ईंट-पत्थर तथा अन्य वस्तुओं का अवरोध खड़ा कर एक तरह की अस्थायी किलेबंदी, जिसकी यूरोप की क्रांतियों में एक लंबी परंपरा रही है।) खड़ा करना शुरू किया। विद्रोह की शुरुआत उपभोक्तावादी मूल्यों की प्रतीक मोटरगाड़ियों को जलाने से हुई। लेकिन मजदूरवर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों उपभोक्तावादी समाज के दबावों से पक्षाघात का शिकार हो जाने के कारण अनिर्णय की स्थिति में रहे या आंदोलन के विरोध में रहे। इस तरह मजदूरों के समर्थन के अभाव में यह विद्रोह क्रांति का रूप ले सके इसके पहले ही समाप्त हो गया।
अगर हम अपने समाज पर ही नजर डालें तो पाएँगे कि कैसे उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से लोगों का आपसी विभाजन गहरा हो रहा है। जाति-व्यवस्था के तमाम दोष अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ दशक पहले तक कम से कम जाति-बिरादरीवालों में आपस में एक बराबरी का संबंध रहता था जिसका प्रतीक साथ का हुक्का-पानी हुआ करता था। लेकिन जैसे-जैसे इस नई संस्कृति ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, गाँवों में भी कुछ संपन्न लोगों के घरों में सोफासेट, टेलीविजन आदि आऩे लगे हैं। अब चटाई पर बैठने वाले और सोफा पर बैठनेवाले एक ही बिरादरी के लोगों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो रही है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि बिरादरी के बाहर सोफासेट वालों की एक अलग बिरादरी खड़ी हो रही है। इस तरह जहाँ थोड़ा-बहुत समुदाय का भाव था वह भी नष्ट होता जा रहा है। वस्तुओं की दीवारों से लोग एक–दूसरे से कटते जा रहे हैं। इसका एक परिणाम यह होता है कि आध्यात्मिक खोखलेपन से पैदा जिस ऊब से उबरने के लिए वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, वह ऊब और भी बढ़ती जाती है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.