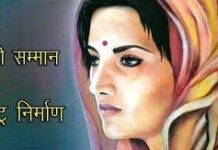— मेधा —
बिहार में हिंदी के प्राध्यापक के घर जन्म लेने के कारण हिंदी से मेरा जन्मजात रिश्ता है। लेकिन पिता हिंदी को भ्रष्ट बनाने के लिए हिंदी की बोलियों को जिम्मेदार मानते हैं। इस मान्यता के लिए उनके पास वाजिब कारण थे। मातृभाषा के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करनेवाले छात्रों की कॉपियां जाँचते वक्त बोलियों की मिलावट से हिंदी के एक से एक भ्रष्ट नमूने उन्हें देखने को मिला करते थे। हमारे भाषाई विकास के लिए सजग और तत्पर पिता हमें भी ऐसे नमूने दिखाया करते थे। यही कारण था कि बोलियों के विविधवर्णी संसार में रहते हुए भी रूप, गंध और भाव से भरी किसी बोली को अपनी मातृभाषा बनाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल सका।
मगही का मायका और बज्जिका की ससुराल वाली माँ ने पिता के आदेश पर हमें खड़ी बोली हिंदी में ही तुतलाना सिखलाया। हालाँकि घर में खड़ी बोली का प्रयोग करने पर दादी माँ को अँग्रेजी बोलने का ताना दिया करती थीं। इस तरह दो-दो बोलियों की विरासत वाले घर में हम भाई-बहनों की मातृभाषा बनी हिंदी और हमें बज्जिका तथा मगही से दूर रखा गया।
बहुत समय तक मैं भी पिताजी की मान्यता पर विश्वास करती रही लेकिन जब रेणु के रचना-संसार में आंचलिकता के प्रभाव से पात्रों ही नहीं पूरे परिवेश को धड़कते पाया और अपने क्षेत्र की कवयित्री अनामिका की सरस, सजीव और भावप्रवण भाषा में स्थानीय बोली की केन्द्रीय भूमिका को पहचाना तो लगा कि यदि मेरा बचपन बोलियों से हरा-भरा होता तो मेरी हिंदी का बाग विविधवर्णी स्थानीय अभिव्यक्तियों के फूलों से सदाबहार होता। हो सकता है कि उसमें व्याकरण की अशुद्धियों के कुछ खर-पतवार भी आ जाते लेकिन उसे तो प्रयास से दूर किया जा सकता था। बोलियों को अपने जीवन में शामिल करना केवल समृद्ध हिंदी के लिए ही जरूरी नहीं अपने समाज को जानने-समझने के लिए भी जरूरी है, यह एहसास भी वक्त के साथ बड़ा होता गया। खैर!

हिंदीभाषी समाज ने अपनी बोलियों की शक्ति को उस तरह नहीं पहचाना और न ही उस शक्ति का उपयोग अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति की समृद्धि के लिए किया। कुछ अपवादों को छोड़ दें। लेकिन कई समाजों के लिए आज भी मातृभाषा इतने गौरव का विषय है कि कोई जब अपने शत्रु के विनाश की कामना करता है तो उसे शाप देता है- ‘अल्लाह! तुम्हारे बच्चों को उनकी माँ की भाषा से वंचित कर दे’। भाषा के ऐसे ही गौरव को जीने वाला पहाड़ी समाज है- दागिस्तान। लेखक रसूल हमजातोव ने अपनी किताब ‘मेरा दागिस्तान’ में एक संस्मरण का जिक्र किया है। एक बार लेखक की मुलाकात दागिस्तान छोड़कर फ्रांसीसी लड़की से शादी कर फ्रांस में बस गये एक दागिस्तानी से होती है। अपने देश लौटकर लेखक ने उस मुलाकात का जिक्र उस व्यक्ति की माँ से किया। लेखक की बात खत्म होने पर माँ ने पूछा- ‘तुम दोनों ने अवार भाषा में तो बात की होगी?’ लेखक के न कहने पर माँ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उसने अपने को सँभालते हुए कहा- ‘लेखक आप किसी और से मिले होंगे मेरा बेटा तो कब का मर चुका है।’
हमें बज्जिका से दूर रखनेवाले पिताजी अपनी ईया से बज्जिका में ही बात करते थे हालाँकि दादी अच्छी हिंदी जानती थीं। हिंदी हम भाई-बहनों की तो मातृभाषा थी लेकिन हमारे परिवेश में रह रहे अन्य लोगों के लिए वह बोलने-बरतने की भाषा नहीं थी। वहाँ हिंदी को ‘जीवन की भाषा’ का दर्जा प्राप्त नहीं था। वहाँ उसकी हैसियत बाहरी की थी। एक औपचारिक भाषा जिसमें लिखत-पढ़त का काम किया जाता था। इतनी ही भर थी हिंदी की हैसियत। ऐसे में हम भाई-बहनें जब अपनी बोलचाल के लिए हिंदी का प्रयोग करते तो सारा परिवेश हमें अचरज और व्यंग्य से देखता। हमारे पड़ोसी फब्तियाँ कसते- ‘देशी मुर्गी विलायती बोल’।

हम जिस सहजता से समस्त उत्तर भारत के लिए ‘हिंदी पट्टी’ पद का प्रयोग करते हैं, उसके एक बहुत बड़े हिस्से के लिए ‘हिंदी’ सचमुच ही ‘विलायती बोल’ के समान है। लिखत-पढ़त की भाषा यह जरूर है; लेकिन जीवन आज भी बोलियों में धड़कता है। बोलियों को हिंदी के लिए अछूत बनाकर शुद्धतावादियों ने बोलियों से अधिक हिंदी का नुकसान किया है। जो बात हिंदी की राजनीति करनेवाले बहुतेरे बुद्धिजीवी नहीं समझ पाये उसे बाजार ने बहुत अच्छी तरह समझा। यही कि लोगों के दिलों में अपनी बात बसानी है तो लोक भाषाओं का सहारा लेना ही होगा। इसका प्रमाण है विज्ञापन की भाषा।‘चलत मुसाफिर ले गयो रे पिंजड़े वाली मुनिया’ और गढ़वाली लोकगीत ‘बेडू पाको बारामासा’ की तर्ज पर बनाये गये विज्ञापनों की अपार सफलता इस बात की पुष्टि करते हैं।
बोलियों में जीनेवाले सभी समाजों के लिए किताबी हिंदी दूसरी भाषा है, पहली नहीं। यह बात तब और भी पुष्ट हुई जब कुमाऊँनी बोलनेवाले एक ग्रामीण अंचल में कुछ साल रहने का अवसर मिला। वहाँ के छात्रों के लिए हिंदी सीखना उतना ही कठिन था जितना कि हिंदी बोलनेवाले के लिए अँग्रेजी। वहाँ के कॉलेज में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक अपना विषय पढ़ाने से पहले भाषा सिखाना ज्यादा जरूरी समझते थे। उनके साथ मुश्किल यह थी कि एक साझी भाषा के बिना वह अपने छात्रों से विषय पर चर्चा कैसे करते?
आज महसूस होता है कि पिताजी का फैसला कई पीढ़ियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि आज मैं चाहूँ भी तो अपनी बेटी को किसी बोली की सौगात नहीं दे सकूँगी।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.