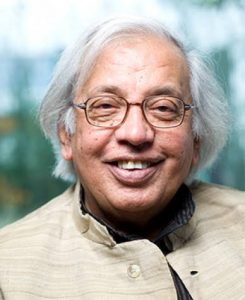
1. थोड़ा-सा
अगर बच सका
तो वही बचेगा
हम सबमें थोड़ा-सा आदमी-
जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता,
अपने बच्चे के नम्बर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर,
जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर
सबसे पहले अस्पताल पहुँचाने का जतन करता है,
जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता-
वही थोड़ा-सा आदमी –
जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता,
जो अपनी बेटी के अच्छे फ्राक के लिए
दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता,
जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है,
जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है,
वही थोड़ा-सा आदमी-
जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं ऊबता
जो अपने घर को चीजों का गोदाम बनने से बचाता है,
जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है
और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता।
जिसे ख़बर है कि
वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान,
आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य,
पक्षी आँगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण –
वही थोड़ा-सा आदमी –
अगर बच सका
तो वही बचेगा।
1987
2. वे
वे एक पिंजड़ा लाएँगे,
अदृश्य,
पर जिसे छोड़कर फिर
उड़ा नहीं जा सकेगा।
वे वचन देंगे आकाश का,
वे उल्लेख करेंगे उसकी
असीम नीलिमा का,
पर वे लाएँगे पिंजड़ा –
फिर वे धीरे-से समझाएँगे
कि आकाश में जाने से पहले
पिंजड़े का अभ्यास ज़रूरी है।
फिर वे कहेंगे कि आकाश में बहुत ख़तरा है,
कि कहीं नहीं है आकाश,
कि आकाश भी अंततः पिंजड़ा है।
फिर वे पिंजड़े में
तुम्हें छोड़कर
आकाश में
अदृश्य हो जाएँगे।
1987

3. अगर वक़्त मिला होता
अगर वक़्त मिला होता
तो मैं दुनिया को कुछ बदलने की कोशिश करता।
आपकी दुनिया को नहीं,
अपनी दुनिया को,
जिसको सँभालने-समझने
और बिखरने से बचाने में ही वक़्त बीत गया।
वैसे वक़्त का टोटा नहीं था
– कुल मिलाकर ठीक-ठाक ही मिल गया
पर पता नहीं क्यों पूरा नहीं पड़ा।
अनन्त पर इतना एकाग्र रहा
कि शायद इतिहास पर नज़र डालना भूल गया।
उस वक़्त में प्रेम किया, भोजन का जुगाड़ किया,
छप्पर नहीं जुटा लेकिन लोगों के संग-साथ की गरमाहट ने सहारा दिया,
कविताएँ लिखीं, कुछ दूसरों की मदद की थी –
कुछ बेवजह विवाद में फँसा :
नौकरी की और शिखर पर पहुँचने में सफल नहीं हुआ,
झंझटों से बिना कुम्हलाए निकल आया
पर न बहुत सुख दे सका, न पा सका।
हँसने के लिए महफ़िलें बहुत थीं
रोने के लिए कंधे कम मिले।
जब-तब भीड़ में पहचान लिया गया
पर इसीलिए चेहरे के सारे दाग़ जग-ज़ाहिर होते रहे।
पुरखों को याद करने का मौक़ा कम आया
और पड़ोस के कई लोगों के चेहरे
ग़ैब में गुम होते रहे –
मुझे कोई भ्रम नहीं है
कि मेरे बदले
दुनिया ज़रा भी बदल सकती है।
पर अगर वक़्त मिलता
तो एक छोटी सी कोशिश की जा सकती थी,
हारी होड़ सही
लगाई जा सकती थी।
दुनिया यों बड़ी मेहनत-मशक्कत से
बदलती होगी
फ़ौज-फाँटे और औजारों-बाज़ारों से,
लेकिन शब्दों का एक छोटा सा लुहार
और नहीं तो
अपनी आत्मा की भट्टी में तपते हुए
इस दुनिया के लिए
एक नए क़िस्म का चका ढालने की
जुर्रत कर ही सकता था –
अगर वक़्त मिला होता
तो दुनिया की हरदम डगमगाती सी गाड़ी में
एक बेहतर चका लगाकर उसका सफ़र आरामदेह बनाने की,
उसे थोड़ा सा बदलने की गुस्ताख़ी तो की ही जा सकती थी।
1997
4. वृक्ष ने कहा
इधर-उधर भटकने-खोजने से क्या होगा?
अपनी जड़ों पर जमकर रहो,
वहीं रस खींचो,
वहीं आएँगे फूल, फल, पक्षी,
धूप और ओस,
वहीं झुकेगा आकाश –
वहीं पृथ्वी करेगी पूतस्पर्श –
वहीं जहाँ जड़ें हैं
और उन पर जमे तुम हो,
वहीं।
2003
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















