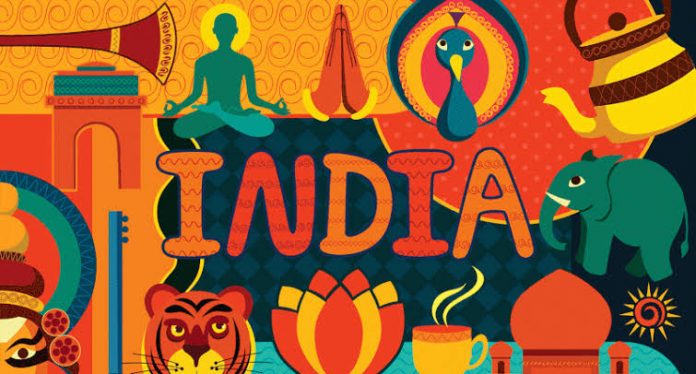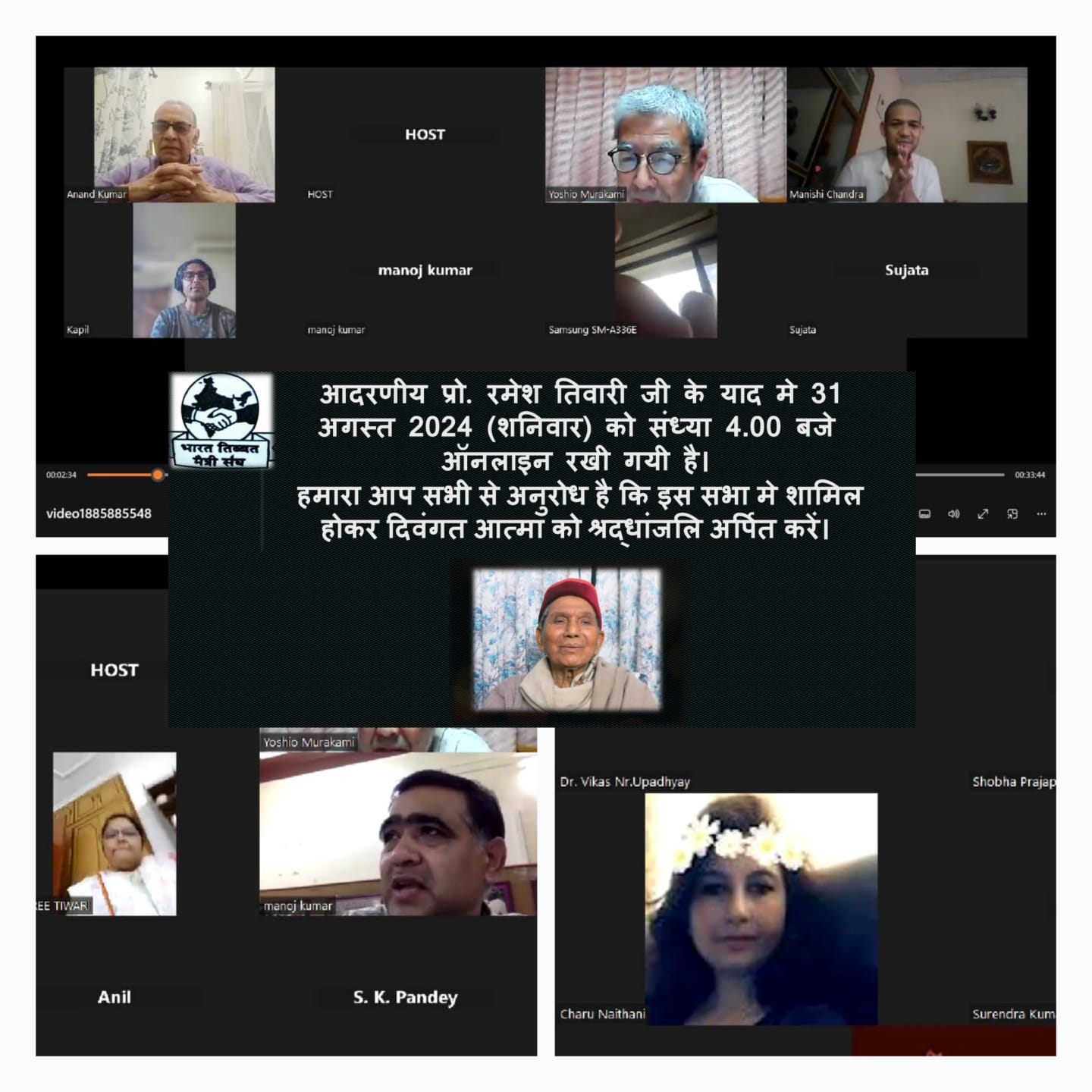हमने अपनी विरासत की उपेक्षा की है- इस हद दर्जे की उपेक्षा कि इसे भारत नाम के राष्ट्र-राज्य की सबसे बड़ी नाकामियों में गिना जाएगा। आधुनिकता के नाम पर हमने सांस्कृतिक रूप से अनपढ़ों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है।
प्रगतिशीलता के नाम पर हमने अपनी नयी पीढ़ियों को सिखाया है कि रीति-रस्म कुछ और नहीं बल्कि अंधविश्वास ही हैं और यह भी कि संस्कृति का कोई भी नेह-बंध अगर तुमसे जुड़ा है तो उसे अपने पिछड़े होने की निशानी मानो। आज नयी पीढ़ी का कोई आधुनिक, उच्चशिक्षित हिंदुस्तानी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो भारत-भूमि की कोई भाषा इस खूबी से जानता हो कि अपने ड्राइवर या घर में काम करनेवाली बाई के अलावा किसी और से बोल सके या भारत-भूमि की भाषाओं में अपने जरूरी सोच-विचार को लिख सके। कपड़े की किस बुनावट को पटोला कहा जाए और किसको फुलकारी या चिकनकारी- यह नयी पीढ़ी के उच्चशिक्षित शायद ही बता पायें आपको। ऐसे उच्चशिक्षितों ने हमारी संस्कृति के गौरवग्रंथों के नाम पर बस अमर चित्रकथा को पढ़ा है और भारत-भूमि में चहुंओर जो विविध किस्म के व्यंजन बनते-मिलते हैं उससे भी यह पीढ़ी अब मुंह फेर रही है, बस रोटी या भात भर से नाता रह गया है।
हम अपनी संस्कृति को जितना हेय समझते हैं उतना ही अपनी नजरों में और जिन्हें हम अपने लिए जरूरी समझते हैं उन लोगों की नजरों में हमारी कीमत बढ़ती जाती है। सांस्कृतिक अज्ञानता की गजब की भांग तैयार हुई है इस देश की नयी पीढ़ियों के बीच कि इसके औद्धत्य का नशा अब चहुंओर चढ़ रहा है।
आधुनिकता के जामे में इतरानेवाले इस औद्धत्य का एक रूप और है- यह रूप कहीं ज्यादा महीन है। इस आधुनिकतावादी उच्चवर्गीय औद्धत्य का शिकार होने पर आप अपनी सांस्कृतिक विरासत की अवहेलना नहीं करते बल्कि उससे जुड़े होने का गर्व पालते हैं लेकिन शर्तों के साथ।
संस्कृति का जो हिस्सा आपको अपनी आधुनिक भाव-संवेदना के अनुकूल लगता है, उसे आप मूल्यवान समझते हैं और जब-तब सभा-सोसाइटियों में दिखाये-झमकाये जानेवाले गहने की तरह पहन लेते हैं। नेहरू या फिर अमर्त्य सेन की तर्ज पर हम अपनी संस्कृति में उपलब्ध किसी अमूर्त दार्शनिक अवधारणा को जब-तब अपने लिखे-बोले में मोरपंख की तरह सजा देते हैं और इस बात का गर्व पालते हैं। हम फैबइंडिया के कपड़े पहनकर तो सहज महसूस करते हैं लेकिन अजायबघरों (म्यूजियम) से बाहर लोक-संस्कृति की कोई चीज हमें दिख या भेंट जाए तो इसे लेकर हमारी असहजता देखते ही बनती है।
अब यहां कह लेने दीजिए कि जो सांस्कृतिक गर्व-गर्जना आजकल हिंदुत्व के नाम पर हमें अपने चारों तरफ सुनायी देने लगी है वह कुछ और नहीं बल्कि इस सांस्कृतिक शून्य के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का ही नाम है। और, जैसा कि तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ होता है, हिंदुत्व नाम की यह प्रतिक्रिया भी उसी की एक प्रतिच्छवि है जिसके विरोध की यह दावेदारी करती है। अपने को भारतीय संस्कृति के संरक्षक और पैरोकार बतानेवाले हिंदुत्व के हिमायती भारतीय संस्कृति के बारे में उतने ही अनजान हैं जितने कि उनके विरोधी। हिंदुत्व के इन हिमायतियों को भी पश्चिम का अनुमोदन चाहिए सो भारतीय संस्कृति की कोई चीज इनके खोजे से कहीं दिखी नहीं कि फट से उसकी औनी-पौनी वैज्ञानिक व्याख्या पेश कर देते हैं।
हिंदुत्व के इन हिमायतियों के सांस्कृतिक अज्ञान की हद तो ये है कि इसी के सहारे ये लोग जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता से पैदा उत्पीड़न के सबसे जघन्य रूपों पर भी चमकदार पन्नी चढ़ाने का भी काम कर लेते हैं और दूसरे धर्म-मत या धर्म-विश्वास को माननेवालों के प्रति नफरत फैलाने की तो यहां बात ही क्या करें— वो तो इनका प्रिय शगल ही है। अपनी शरारतों में दयनीय और अपनी खुराफातों में डरावने नजर आनेवाले भारतीय परंपराओं के ये पैरोकार, भारत नाम की महादेशीय सभ्यता की विरासत को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना तो हमारी इस सभ्यता के निंदकों और आलोचकों ने भी नहीं पहुंचाया।
क्या कोई बीच का रास्ता भी है?
हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ सकें और सहजता के भाव के साथ जुड़ सकें, कुछ ऐसे कि ना तो इस जुड़ाव में हमें शर्मिंदगी महसूस हो और ना ही किसी किस्म का अटपटापटन- ना तो अपनी परंपराओं से हमारा जुड़ाव इतना आक्रामक हो कि हम हर हाल में उसके संरक्षण में तैनात नजर आएं और ना ही इतना ढीला-सीला कि हमारी परंपरा का हर रेशा हमारे हाथ से फिसलता जाए और हम इस नुकसान के बावजूद चैन की वंशी बजाते रहें। क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता हो सकता है?
मुझे लगता है, बस यही एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर न सिर्फ हम नामुराद हिंदू राष्ट्रवाद से निपट सकते हैं बल्कि यही रास्ता हमें सच्चे स्वराज की तरफ भी ले जा सकता है। के.सी. भट्टाचार्य के विचारों ने इस तीसरे या कह लें बीच के रास्ते का दार्शनिक घोषणापत्र तैयार किया है और राममनोहर लोहिया ने इसे एक राजनीतिक विभावन के रूप में गढ़ा। आशिष नंदी ने आधुनिकतावादी औद्धत्य की इस सांस्कृतिक आलोचना के लिए एक मजबूत सामाजिक-वैज्ञानिक बुनियाद तैयार की है। देवदत्त पटनायक ने हिंदू-देवमाला से जुड़ी कथाओं का जो पुनर्पाठ प्रस्तुत किया है या फिर टीएम कृष्णा और सिंह के पारलौकिक स्वाद वाले गायन को भी मैं इसी श्रेणी में रखता हूं। अनुपम मिश्र ने हमारे देश में जल-निकासी और संरक्षण-संवर्धन की जो पुरानी पद्धति प्रचलित थी- उसकी गहन खोज-बीन की है। उनका यह काम भी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के इस तीसरे और जरूरी रास्ते पर ले जानेवाला माना जाएगा। अफसोस कि अपनी जड़-जमीन से जुड़ी और कहीं ज्यादा गहरी इस वैकल्पिक आधुनिकता के रास्ते पर चलने को हम तैयार हो ही रहे थे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक छिछली, नकलची और बड़बोली शय ने हमारा रास्ता रोक लिया।
प्रोफेसर जी. एन. देवी की नयी किताब महाभारत : द एपिक एंड द नेशन हमें एक रास्ता दिखाती है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मौजूदा हमले के बरक्स हम विचारों के जगत में अपने स्वराज पर कैसे दावा ठोकें। सांस्कृतिक रूप से अपने स्व-भाव और स्व-राज को हासिल करने के प्रयासों की अगुवाई करने के लिए जिस साख की जरूरत है, वह सब जी.एन.देवी में प्रत्यक्ष है।
ताउम्र अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर रहे जी.एन. देवी प्रसिद्ध साहित्य समालोचक हैं। लेकिन उन्हें एक भाषा-विज्ञानी, पीपल्स लिंग्विटस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और भाषाई विविधता के पैरोकार के रूप में विशेष तौर पर जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछिए तो वे कहेंगे कि जी.एन. देवी सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले सिरे पर मौजूद खानाबदोश और विमुक्त समुदाय के दिली दोस्त हैं। देवी दक्षिणायन चलाते हैं- यह आरएसएस के प्रतिपक्ष में खड़े लेखकों का एक आंदोलन है। फिलहाल, जी.एन. देवी राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरएसएस के दृढ़ प्रतिकार में खड़े मुहिमों में एक है राष्ट्र सेवा दल। जी.एन. देवी उन चंद भारतीयों में एक हैं जिनके जीवन और कर्म में हम टैगोर, गांधी और आंबेडकर की झलक पाते हैं।
प्रोफेसर देवी की पतली किताब ‘महाभारत : द एपिक एंड द नेशन ‘ का तर्क जितना सीधा है उतना ही सधा हुआ कि महाभारत एक काव्य है और इस काव्य का रिश्ता इतिहास-लेखन से है, भले ही इसमें इतिहास का अर्थ वह न लिया गया हो जो अर्थ पेशेवर इतिहासकारों में प्रचलित है।
महाभारत सहस्राब्दियों के इतिहास का लेखा-जोखा है और भारतीय सभ्यता वैदिक काल से लेकर महान साम्राज्यों के बनने तक जिन-जिन पड़ावों से गुजरी है- उसके छाप-चिह्नों को महाभारत दर्ज करता है और ऐसा करते हुए महाभारत में पौराणिक अतीत और ऐतिहासिक अतीत को एक आख्यान में बुन दिया गया है। महाभारत की लोकप्रियता बरकरार है तो इसलिए कि वह अपने अतीत से जुड़ने के निमित्त हमारे लिए एक मानचित्र की तरह है। प्रोफेसर देवी ने अपनी इस किताब में एक जगह लिखा है : ‘महाभारत ने अतीत के स्मरण की एक अनोखी पद्धति बनायी। भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्मृति को संरक्षित करने के लिए इस पद्धति को आत्मसात कर लिया है। महाभारत इसी अर्थ में हमारा राष्ट्रीय काव्य है। यह राष्ट्र का आख्यान रचता महाकाव्य नहीं वरन राष्ट्र को सुमिरने का जो हमारा तरीका है, उसका आख्यान रचता महाकाव्य है।’ (पृष्ठ112)
बीसवीं सदी में महाभारत की जो अनेकानेक टीकाएं आयी हैं (और बीसवीं सदी के हमारे ज्यादातर चिंतकों ने महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है) उनकी तरह प्रोफेसर देवी ने अपनी किताब में अपना चिंतन-मनन सिर्फ भगवदगीता पर केंद्रित नहीं किया। वे महाभारत की दार्शनिक पीठिका को नहीं बल्कि उसकी कथा को अपने विवेचन का आधार बनाते हैं।
महाभारत अगर पौराणिकता, चमत्कार, दैवीयता, असंभाव्यता और अबूझेपन के तत्त्वों से भरा पड़ा है तो प्रोफेसर गणेश देवी इनसे मुंह नहीं मोड़ते बल्कि वे किंवदंतियों और पुराण-कथाओं के अर्थ ढूंढ़ते हैं। वे आपको बताते हैं कि कहां दार्शनिक जिज्ञासा थक कर विराम लेती है कि कहां महाभारत में इतिहास दर्ज है और अगर महाभारत में कोई बात किसी रूप में है तो उसके होने का औचित्य क्या है- असल में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी अभिव्यक्ति में महाभारत में कोई पंक्ति किसी खास रूपाकार में दर्ज की गयी।
देवी के मुताबिक ‘महाभारत नाम के काव्य की परिणति शांत-रस में होती है- वह स्थितप्रज्ञता का विभावन रचता है, महाभारत आपको साक्षी-भाव देता है।’ (पृष्ठ 45)
इसी कारण प्रोफेसर देवी ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी एक पात्र को महाभारत का नायक नहीं कहा जा सकता। गौर कीजिए कि इस मामले में भी प्रोफेसर देवी अन्य टीकाकार जो कृष्ण, द्रौपदी, अर्जुन, कर्ण या भीष्म को प्रधान मानकर चलते हैं, उनसे अलग प्रस्ताव कर रहे हैं। दरअसल, प्रोफेसर देवी आपसे अपनी इस किताब में यह कहते हुए मिलेंगे कि महाभारत नाम के महाकाव्य में तो आद्योपांत यम ही मौजूद है- वह शुरुआत में भी है और अंत में भी। महाभारत का दार्शनिक महत्त्व इस बात में है कि इसमें काल के जो मुख्य चार विभावन- ऋत, पौराणिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक— किये जाते हैं उन्हें एकसाथ गूंथ दिया गया है।
प्रोफेसर देवी ने अपनी किताब में महाभारत का जो पुनर्पाठ प्रस्तुत किया है उसका सबसे मोहक पक्ष यह है कि वे इस ग्रंथ (महाभारत) पर लगे सामाजिक रूढ़िवाद के आरोपों की अनदेखी नहीं करते बल्कि ऐसे आरोपों से मुठभेड़ करते हैं। जाहिर सी बात है कि महाभारत में आपको जगह-जगह वर्ण-व्यवस्था, छुआछूत और वर्ण-धर्म से जुड़े कर्म के आधार पर पुनर्जन्म की दुहाइयां मिलेंगी। इस संदर्भ में प्रोफेसर देवी का कहना है कि महाभारत में वर्णित धर्म और धर्मशास्त्रों में वर्णित ब्राह्मणवादी वर्ण-धर्म में फर्क किया जाना चाहिए, दोनों अलग हैं। महाभारत में पौराणिक और ऐतिहासिक को एक में पिरोने से एक खासियत पैदा हुई है। खासियत यह कि महाभारत समावेशन, संश्लेषण, स्वीकार और किसी का अपवर्जन किये बगैर आगे की राह चलने की बात कहता है (पृष्ठ 77)। महाभारत की लोकप्रियता अगर निरंतर बनी चली आ रही है तो इसी कारण कि यह धर्म की गैर-ब्राह्मणवादी पुस्तक है, अब्राह्मणवादी धर्म-ग्रंथ है` (पृष्ठ106)।
बेशक महाभारत में महात्मा बुद्ध का प्रत्यक्ष जिक्र नहीं आता लेकिन परोक्ष तौर पर महात्मा बुद्ध की अंतर्दृष्टियों का समावेश किया गया है और इस रूप में महाभारत शौर्य, नैतिक सत्य एवं मुक्ति के महापाठ के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है।
मैं कोई इतिहासकार या इंडोलॉजिस्ट (भारत-विद्याविद्) नहीं जो प्रोफेसर देवी की किताब में आये तर्कों का ऐतिहासिक स्रोतों या फिर अन्य पाठगत सामग्रियों के सहारे परीक्षण-समालोचन कर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेसर देवी की किताब ऐसी समीक्षाओं की अपेक्षा भी नहीं रखती। मेरे जानते, प्रोफेसर देवी की किताब अपने रचाव-गढ़ाव में राजनीति का एक ग्रंथ है जो अपने तर्कों के सहारे उस मौजूदा चलन का प्रतिवाद करती है जिसमें हमारे महाकाव्यों और अन्य गौरव-ग्रंथों का कु-पाठ किया जा रहा है और न्यस्त स्वार्थ के लिए बरता जा रहा है।
प्रोफेसर देवी की किताब अकुंठ भाव से एक रास्ता सुझाती है जिसपर चलकर अपनी सभ्यतागत विरासत पर दावा ठोंका जा सकता है— ऐसा दावा जिसमें न रंचमात्र हीनताबोध हो और ना ही श्रेष्ठता की घोषणा करता कोई दंभ। जैसे प्रोफेसर देवी महाभारत के बताये रास्ते पर चलकर अपने अतीत से जुड़ने के हिमायती हैं वैसे ही मैं उनकी बतायी पद्धति के सहारे अपने राष्ट्रीय महाकाव्यों से जुड़ने का हिमायती, और यह रास्ता यह मानकर चलने का है कि : ‘ना तो हमारे महाकाव्य वस्तुनिष्ठ सत्य के पूर्ण उद्भावक हैं और ना ही उन्हें पूर्ण रूप से गल्प की संज्ञा दी जा सकती है।’ (पृष्ठ 127).
अपने स्वराज पर दावा करने के लिए हमें इसकी ही जरूरत है।
(द प्रिंट से साभार)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.