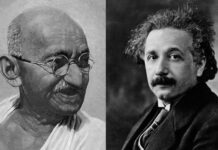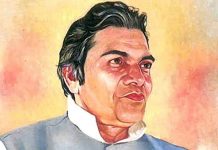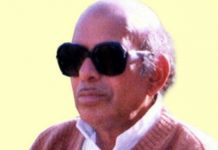नरम पंथ तथा उग्रपंथ
भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का इतिहास बहुत हद तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय और विकास से जुड़ा होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीमाओं के बाहर कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था। कांग्रेस के बाहर भी स्वतंत्रता के पुजारी थे, जिनको मोटे तौर पर आतंकवादी क्रांतिकारियों की संज्ञा दी जाती है। भारतीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए समय-समय पर जिन तौर-तरीकों का इस्तेमाल किया, उनको ऐतिहासिक दृष्टि से तीन हिस्सों में बाँटा जा सकता है :
(1) प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णतया निर्भर करती थी अनुनय-विनय और आवेदन-पत्रों पर। इस चरण में कांग्रेस के नेता यह मानकर चलते थे कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान के साथ जो संयोग हुआ है, वह ईश्वरीय देन है और इस तरह का संबंध बने रहना दोनों देशों के लिए मुफीद होगा। भारतीय नेताओं का यह कहना था कि अंग्रेज सद्भाव से प्रेरित होकर हमारे देश पर राज कर रहे हैं, हमें आधुनिक विद्याओं और सभ्यता से अवगत करा रहे हैं और जैसे-जैसे हम लोगों में योग्यता होती जाएगी, वैसे-वैसे प्रशासन के अधिकार वे हमारे हाथों सौंपते जाएंगे। लेकिन भविष्य में भारत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा, इसकी कल्पना भी इस चरण के भारतीय नेता नहीं कर पाए थे। यानी मोटे तौर पर जिनको उदारवादी कहा जाता है, उनके हाथों में भारतीय कांग्रेस का नेतृत्व था। जैसे फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले आदि।
(2) द्वितीय चरण में कांग्रेस में नयी शक्तियों का उदय हुआ। इन्होंने अनुनय-विनय की जगह हिंदुस्तानियों का मनोबल ऊंचा उठाने पर जोर दिया। लोकशिक्षण और लोक जागरण ये उनके हथियार थे। नयी-नयी सार्वजनिक प्रवृत्तियों को चालू कर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास नए उग्रवादी राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। ये लोग भी पूर्णतः वैध और संवैधानिक तरीकों से अपने आंदोलन को चलाना चाहते थे हालांकि राजनिष्ठा इनकी विशेषता नहीं थी। न इस शब्द से वे अपने को गौरवान्वित समझते थे। इस चरण के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में हम लोकमान्य तिलक को मान सकते हैं। वेलेंटाइन चिरोल नाम के लेखक ने तिलकजी के विभिन्न आंदोलनों का अध्ययन किया था। चिरोल का यह निष्कर्ष गलत नहीं है कि भारत में उनके सारे आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के प्रति असंतोष भड़काने के उद्देश्य से प्रेरित थे। इसीलिए उनको “भारतीय असंतोष के जनक” की सार्थक उपाधि चिरोल साहब ने दी– फादर आफ इंडियन अनरेस्ट।
(3) तीसरा चरण था आतंकवादियों अथवा क्रांतिकारियों का रास्ता। इसकी विशद चर्चा हम आगे करेंगे।
अंग्रेजी प्रशासन लोकमान्य तिलक की ओर शंकित दृष्टि से देखता था। साधारण जनता में अपने विचार का प्रसार करने के लिए उन्होंने जान-बूझकर लोक-भाषाओं के माध्यम को अपनाया। उनके द्वारा जो दो समाचार-पत्र चलाए जाते थे, उनमें से एक ‘मराठा’ अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। लेकिन इसको वे प्रचार का मुख्य साधन नहीं समझते थे, सिर्फ गैरमराठी भाषियों को वे इसके माध्यम से अपने विचारों से परिचित कराते थे। उन दिनों हिंदी का महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में प्रसार नहीं था, हालांकि आगे चलकर लोकमान्य तिलक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। मराठी में ‘केसरी’ नाम की जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, वही उनका प्रमुख माध्यम था, उपकरण था। तिलक जी की शैली में ओजस्विता थी। उनकी भाषा साधारण लोगों के आकलन से परे नहीं थी। इसका नतीजा हुआ कि महाराष्ट्र के प्रत्येक कोने में रहनेवाले लोग उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए।
तिलकजी की ख्याति मुख्यतः इस बात को लेकर बढ़ी की उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता के उद्देश्य को भारतीयों के सामने एक लक्ष्य के रूप में रखा। उसके लिए उन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेकर रहूंगा” यह मंत्र तिलकजी ने देशवासियों को दिया। उदारमतवादी विचारकों में ज्यादातर अंग्रेजों के कृपापात्र लोग थे। उनमें से बहुत सारे लोग न सिर्फ अंग्रेजों की खुशामद करते थे, बल्कि अंग्रेजों द्वारा दी गयी पदवियां और खिताब आदि उनको बहुत लुभावने लगते थे। परंतु सभी उदार मतवादी लोग स्वार्थी और कायर नहीं थे। उनमें फिरोजशाह मेहता जैसे आत्मसम्मान को सर्वोपरि माननेवाले और अंग्रेजों के साथ बराबरी के व्यवहार का आग्रह करनेवाले नेता भी थे। इन लोगों में दादाभाई नौरोजी जैसे भारतीय एकता के समर्थक भी थे जिन्होंने अपनी प्रदीर्घ आयु में राष्ट्र को जाग्रत और शिक्षित करने के लिए अखंड प्रयास किए। इतना ही नहीं, सीधे इंग्लैण्ड जाकर वहां के राजनीतिज्ञों को हिंदुस्तान की समस्याओं से अवगत कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी उन्होंने किया।
इंग्लैण्ड की जनता के मन में हिंदुस्तान के प्रति रुचि उत्पन्न करने में दादाभाई को कितनी सफलता मिली, उसका सबसे अच्छा सबूत यह है कि वहां फिंसबेरी चुनाव क्षेत्र से वे इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में लिबरल पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। तत्कालीन कंजरवेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री लार्ड साल्सबरी ने उनकी उम्मीदवारी का उल्लेख दुष्टतापूर्वक किया था और उन्हें ‘काले आदमी’ की संज्ञा दी थी हालांकि दादाभाई गौरवर्ण ही थे, जैसे दक्षिण और मध्य यूरोप के लोग। फिर भी उनके बारे में किया गया यह शब्द प्रयोग इंग्लैण्ड के प्रगतिवादी लोकमत को अच्छा नहीं लगा और फिंसबेरी के लोगो ने दादाभाई को वोट देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया था।
उदार मतवादी लोगों में गोपालकृष्ण गोखले जैसे दिन-रात भारतमाता के वैभव की आकांक्षा रखनेवाले और देशवासियों की सेवा में रत देशप्रेमी भी थे। उन्होंने इंपीरियल कौंसिल में जो अविस्मरणीय काम किया, उसका लोहा राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता भी खुले दिल से मानते थे। भारतमाता की सेवा के लिए समर्पित जीवन बितानेवाले, स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करनेवाले सेवकों का एक संघ ‘सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी’(भारत सेवक समाज) का गठन इन्होंने किया था। इसी संस्था ने श्रीनिवास शास्त्री, हृदयनाथ कुंजरू, एन.एस.जोशी, ठक्कर बापा आदि महान लोगों को सार्वजनिक जीवन में लाने का काम किया था। श्री जोशी मजदूर आंदोलन और ठक्कर बापा आदिम जातियों के उत्थान के प्रणेता रहे हैं।
तिलकजी और इन ऊँचे दर्जे के उदार मतवादी नेताओं में ज्वलंत मतभेद देशभक्ति की भावना को लेकर नहीं थे। दोनों ही देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे। जो मतभेद था, वह साधनों को लेकर था। जन-जागरण के लिए तिलकजी ने न केवल अखंड प्रयास किया, उसके लिए उन दिनों विरले साहस और हिम्मत का परिचय दिया था। 19वीं शताब्दी समाप्त होने से पहले ही दो बार तिलकजी ने देश की खिदमत में कारावास भोगा था। दूसरी दफा तो राजद्रोह के मुकदमे में ही उनको कठोर कारावास की सजा हुई थी। इतना ही नहीं, आगे चलकर उनके ऊपर तीसरी बार जो मुकदमा चला तो उसमें उनको न सिर्फ छह साल की सजा फरमाई गई, बल्कि उन्हें इस देश के बाहर दूर बर्मा में मांडले की जेल में बंद करके रखा गया था।
स्वराज्य की लड़ाई में तिलकजी ने निःस्वार्थ भाव और हिम्मत का यह जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसको लेकर साधारण जनता के दिल में उन्हें उच्च स्थान मिला। जनता के द्वारा उन्हें ‘लोकमान्य’ की उपाधि दी गई, जो अंग्रेजों, द्वारा अपने खुशामद करनेवाले सेवकों को दी गई पदवियों और खिताबों से निःसंदेह मूल्यवान थी।