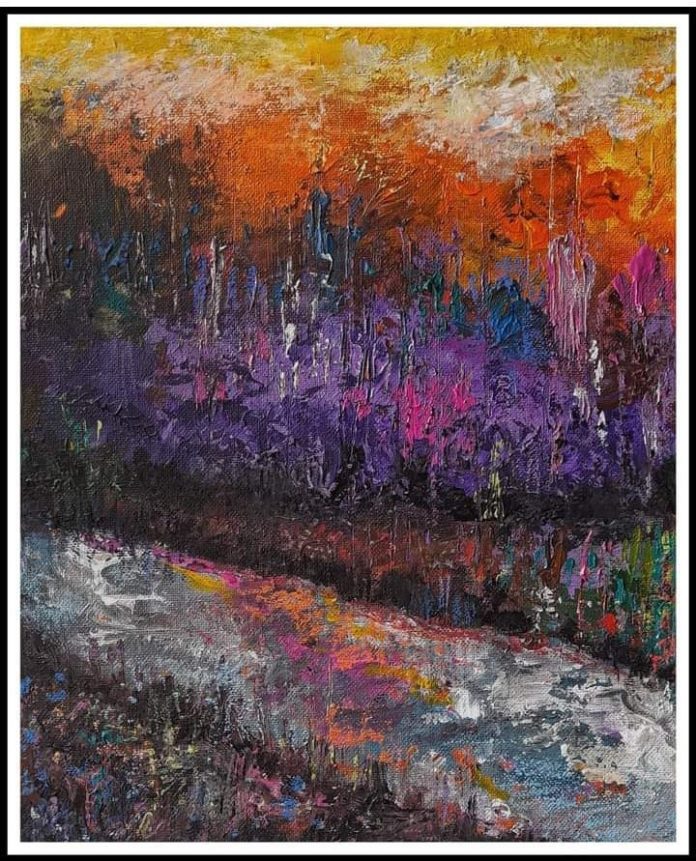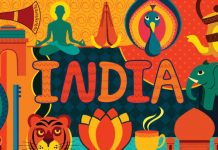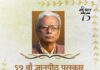— नंदकिशोर आचार्य —
सामान्यतया जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन घटनाओं की खोज और अध्ययन से होता है जो अतीत में घटित हुईं। अध्ययन की प्रक्रिया में हम घटनाओं की पृष्ठभूमि में काम कर रहीं कुछ विशेष प्रवृत्तियों को भी लक्षित कर पाते हैं और इस तरह मनुष्य की यात्रा की प्रकृति और उसके लक्ष्य को पहचानने की कोशिश भी करते हैं। सामान्य अर्थों में इसे ही इतिहास-दृष्टि कहा जाता है। प्रत्येक दर्शन पद्धति एक इतिहास-दर्शन का भी विकास करती है यानी इतिहास को समझने की एक दृष्टि हमें देती है। इसे यों भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से ही एक जीवन-दर्शन का बोध विकसित होता है क्योंकि इतिहास वस्तुतः मनुष्य के होने का इतिहास है और इसलिए मनुष्य की अपनी पहचान भी इतिहास में से ही उभरती है।
ऐसी स्थिति में यह बड़ा अजीब लगता है कि हम एक पूर्व निर्धारित दृष्टि के अनुसार इतिहास की व्याख्या करें- क्योंकि दृष्टि का विकास तो इतिहास के अध्ययन का परिणाम होना चाहिए, उसका कारण नहीं।
लेकिन फिलहाल मैं इतिहास के अध्ययन की विविध दृष्टियों के औचित्य पर बहस में नहीं पड़ना चाहता, न ही इस बहस में कि इतिहास की मूल दिशा क्या है।
एक और बात है जो अकसर मेरे मन में उठती रही है। इतिहास के अध्ययन-अध्यापन और अपने लेखन-कर्म के दौरान भी अकसर मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है और उसका कोई आपत्तिरहित हल मुझे नहीं सूझ पाया है। समस्या यह है कि इतिहास के अध्ययन में हम घटना या तथ्य किसे मानें? ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक तथ्य का वास्तविक तात्पर्य क्या है?
सामान्यतया हम केवल उन घटनाओं और तथ्यों को ही इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण मानते हैं जिनका पूरे मानव समाज या उसके किसी एक अंश – देशबद्ध या कालबद्ध अंश – पर कोई बुनियादी असर पड़ा। वैसे तो छोटी-से-छोटी और पूर्णतया निजी घटना तक में भी किसी-न-किसी सामान्य ऐतिहासिक प्रवृत्ति को पहचाना जा सकता है क्योंकि किसी भी मनुष्य के माध्यम से घटित कोई भी घटना मानवीय चेतना की ही किसी-न-किसी प्रकार की अभिव्यक्ति है।
लेकिन जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उन तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं जिन्होंने स्वयं चेतना को प्रभावित किया हो या जिनके माध्यम से हम चेतना की यात्रा के किसी नए कदम को देख पाते हैं। इसलिए इतिहास सिर्फ राजाओं की विरुदावली या साम्राज्यों के उत्थान-पतन की कहानी ही नहीं है- बल्कि अब शायद उनका इतना महत्त्व भी नहीं है जितना संस्कृति और विज्ञान के विकास के इतिहास का। विद्यालयों में चाहे किसी भी तरह का इतिहास हम अब भी पढ़ाते रहें।
यदि ऐतिहासिक तथ्य का तात्पर्य वह तथ्य है जिसने मानव की चेतना को प्रभावित किया हो तो हमें अपनी ऐतिहासिक सामग्री पर पुनर्विचार करना होगा और यह प्रकारांतर से हमारी इतिहास-दृष्टि का भी पुनः परीक्षण करना होगा। एक इतिहास वह है जो पुरातात्त्विक और पुरालेखीय सामग्री के आधार पर समझा जाता है। विविध ऐतिहासिक ग्रंथों, दस्तावेजों, अभिलेखों और अन्य प्राचीन कलाकृतियों-औजारों आदि के आधार पर हम ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करते हैं और उन्हीं का अध्ययन कर मनुष्य की यात्रा को, उसकी गति को तीव्र करनेवाली और उसमें बाधा डालनेवाली दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों को समझने का यत्न करते हैं।
लेकिन ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो मानव-समाज की चेतना में तो रहती हैं लेकिन उनके लिए कोई पुरातात्त्विक या पुरालेखीय आधार हमें प्राप्त नहीं होता। क्या इस तरह की बातों को भी हम ऐतिहासिक तथ्य या घटना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों?
इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन का दावा करनेवाले इतिहासकार उन तथ्यों या घटनाओं को कपोलकल्पित या किंवदंती मानते हैं जिनका कोई पुरातात्त्विक या पुरालेखीय प्रमाण नहीं मिलता – चाहे लोकमानस में उनकी कितनी ही गहरी छाप पड़ी हो। ऐसा क्यों? इतिहास का अध्ययन यदि मनुष्य की चेतना की यात्रा और उस पर पड़े प्रभाव का अध्ययन है तो हमें उन घटनाओं को अधिक महत्त्व देना होगा जो हमारी चेतना में अभी भी अस्तित्वमान हैं और इसलिए हमारे कार्यों को अब भी प्रभावित करती हैं। इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य है अपने वर्तमान को अपने अतीत में से गुजारना क्योंकि अतीत और वर्तमान की द्वंद्वात्मक संबंधप्रक्रिया में से ही भविष्य की संभावना खुलती है – भविष्य अतीत और वर्तमान की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का फल है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए आज उस अतीत का अधिक महत्त्व है जो अब भी हमारी चेतना में जीवित है, अतः हमारे वर्तमान और उससे फूटनेवाले हमारे भविष्य का एक प्रमुख प्रेरक तत्त्व है।
इतिहासकारों द्वारा अकसर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिकता को लेकर संदेह प्रकट किया जाता रहा है। लेकिन भारतीय मानस पर उसका असर किसी भी ऐतिहासिक घटना की तुलना में अधिक है। लोकचेतना में अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क आदि महान सम्राटों की तुलना में विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य और भोज जैसे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण समझे जानेवाले राजाओं की स्मृति अधिक जीवित है।
इतिहासकारों की राय में भारत से बौद्ध धर्म का लोप मुसलिम आक्रमणकारियों के कारण हुआ जबकि भारतीय स्मृति में इसका कारण शंकराचार्य के शास्त्रार्थ थे। गोरखनाथ भारतीय लोकचेतना में जितने जीवित हैं, शंकराचार्य के अलावा अन्य कोई दार्शनिक उस स्थान का दावा नहीं कर सकता। वशिष्ठ और विश्वामित्र की जो स्मृति अनायास ही निरक्षर भारतीय मानस में बनी रह सकी, वह शायद निरक्षर यूरोपीय समाज में प्लेटो और अरस्तू की नहीं रही होगी। ऐसा क्यों है?
क्यों लोकमानस कुछ घटनाओं को भूल जाता है – चाहे आज का इतिहासकार उन्हें कितना ही महत्त्वपूर्ण समझता हो- और कुछ ग्रंथों या अभिलेखों-मुद्राओं में ही उनका उल्लेख बच रहता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि इस तरह की घटनाएँ लोकस्मृति में मर जाती हैं। लोक की दृष्टि में वे स्मरणीय नहीं रहतीं। इस तरह की घटनाएँ लोक के इतिहास का अंग नहीं रहतीं – वे लोक के वर्तमान में जीवित नहीं होतीं।
यदि ऐसा है तो सवाल उठना चाहिए कि लोकमानस का इतिहासबोध या इतिहास-चेतना क्या वैज्ञानिक अध्ययन का दावा करनेवाली दृष्टि से बुनियादी रूप से भिन्न है। वैज्ञानिक दृष्टि पुरातात्त्विक या पुरालेखीय प्रमाणों के बिना तथ्य का अस्तित्व नहीं मानती। दूसरी ओर, लोकचेतना में पुरालेख और पुरातत्त्व का नहीं, अपनी स्मृति का महत्त्व अधिक है क्योंकि किसी वस्तु के स्मृति में न रहने का मतलब है उसका हमारे लिए अस्तित्वहीन हो जाना। कौन-सी दृष्टि अधिक सही और सार्थक है इतिहास के अध्ययन के लिए?
क्या सिक्कों, अभिलेखों तथा दस्तावेजों में वर्णित उन तथ्यों का महत्त्व अधिक है जिन्हें लोकमानस ने भुला दिया, या उन ‘सत्यों’ का, जो बिना किसी पुरातात्त्विक या पुरालेखीय प्रमाण के, हमारी स्मृति में, हमारी चेतना में जीवित हैं और इस प्रकार हमारे वर्तमान अस्तित्व का भी एक अविभाज्य अंग है।
यह हो सकता है कि सिक्कों-दस्तावेजों के आधार पर कुछ तथ्यों का निरूपण कर उन्हें आज हम अपनी चेतना का अंग बना लें, लेकिन ऐसा करके भी क्या वास्तव में हम उस इतिहास का अध्ययन कर रहे होंगे जो हमारी चेतना को आज तक प्रभावित करता रहा अथवा कुछ तथ्यों को आज अपनी चेतना में अस्तित्व देकर अपने भविष्य को उससे प्रभावित करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे होंगे? इस तरह के प्रयत्नों के औचित्य और उपयोगिता का अलग से विचार भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमें क्या अपनी इतिहास-दृष्टि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है?
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.