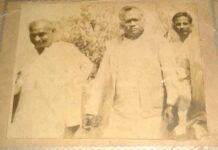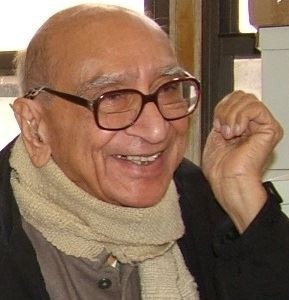
— नारायण देसाई —
जो दूसरी सामुदायिक गतिविधि थी, खासकर साबरमती आश्रम में, वह थी सामूहिक साफ-सफाई। सदियों से, शायद सामंती जमाने से या और भी पहले से भारत में सफाई के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। यह काम करने वाले अछूत समझे जाते थे। हालांकि प्रत्येक मां बच्चों का साफ-सफाई करती है और सारी स्त्रियां घर में झाडूं-बुहारू करती हैं, लेकिन सड़कों और शौचालयों की सफाई का काम एक खास जाति के मत्थे मढ़ दिया गया, और उसे अछूत माना जाता रहा। बचपन से ही, गांधी ने अस्पृश्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। फीनिक्स आश्रम की स्थापना के समय से ही उन्होंने परिसर की साफ-सफाई को हरेक के लिए एक साझी गतिविधि बना दिया था।
शौचालयो की सफाई, जोकि सबसे तुच्छ काम समझा जाता था, उसे गांधी ने खुद खुशी-खुशी अपने हाथ में ले रखा था, जब तक कि वह साफ-सफाई की संपूर्ण प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग नहीं बन गया। साबरमती में आश्रम में गुजारे मेरे जीवन की सबसे खुशनुमा यादों में से एक वह है जब हर सुबह प्रेमाबेन कंटक की देखरेख और अगुआई में कोई पौने एक घंटे तक व्यवस्थित ढंग से साफ-सफाई होती थी। सेवाग्राम में मुझे कुछ महीनों तक शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। यह एक ऐसा काम था जिसे ऊंची जातियों के हिंदू सदियों से हेय या घृणित काम मानते आए थे। गांधी ने शौचालय की सफाई दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। जब वे साबरमती और सेवाग्राम आए, तो शौचालयों की सफाई की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक गतिविधि में तब्दील हो गई।
आश्रम में विभिन्न प्रकार के शौचालयों के साथ प्रयोग भी किए गए ताकि सफाई की प्रक्रिया को बदबू रहित बनाया जा सके और मल को खेतों के लिए खाद में बदला जा सके। इसे एक ऐसी प्रक्रिया में विकसित किया गया जो स्वच्छता के लिहाज से माकूल थी और आर्थिक दृष्टि से उत्पादक भी। लेकिन इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका सामाजिक आयाम था। जिस काम को ऊंची कही जाने वाली जातियों के हिंदू घृणित समझते थे, गांधी ने उसे अपने आश्रम में एक दैनिक अनुष्ठान में बदल दिया। नए आने वालों को अपने आश्रम से परिचित कराने के गांधी के तरीकों में एक यह था कि वे शौचालय–सफाई का काम सौप देते। यह आश्रम जीवन में दीक्षित करने का एक तरीका तो था ही, नए आने वालों का इम्तहान भी था कि अपनी जीवन शैली को बदलने की उनकी तैयारी कितनी है। शौचालयों की सफाई का उत्तरदायित्व पूरा करते हुए मुझे नवागंतुक व्यक्ति के वरिष्ठ साथी की भूमिका निभानी पड़ी थी। मैं बड़ी दिलचस्पी से देखता कि नौसिखिया आदमी शुरू-शुरू में लगभग मानसिक संकट से गुजर रहा होता था। मेरा काम उन्हें इस प्रक्रिया को उतने ही रुचिकर रूप में पेश करना होता था जितनी रुचि के साथ मैं उसे कर सकता था।
साफ-सफाई की ड्यूटी आश्रमवासियों के बीच समय-समय पर बदलती रहती थी, ताकि उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुभव हो सके और वे ऊबें नहीं। झाड़ू बनाना और कंपोस्ट खाद के गड्ढे तैयार करना भी सफाई के काम का हिस्सा होता था। सामुदायिक सफाई दरअसल, सामाजिक बदलाव का गांधी का एक क्रांतिकारी तरीका था, अस्पृश्यता के खिलाफ एक रचनात्मक विद्रोह।
सामूहिक कताई आश्रम में लगभग एक धार्मिक अनुष्ठान में बदल गई थी। सभी आश्रमवासी, युवा और बुजुर्ग, स्त्रियां और पुरुष और बच्चे, सूत कातने के लिए एक केंद्रीय स्थान पर इकट्ठा होते। खादी बनाने के काम में कताई केंद्रीय प्रक्रिया होती थी। इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा समय लगता था, पर इसी काम का सबसे कम मेहनताना मिलता था। गांधी की कताई ने उन्हें भारत के सबसे गरीब लोगों से जोड़ा। गांधी ने सामूहिक कताई को सूत्र यज्ञ कहा था। विचार यह था कि सामुहिक कताई के दौरान सूत कातना सामाजिक उद्देश्यों के लिए समर्पित हो।
गांधी ने ‘यज्ञ’ शब्द को गहरा अर्थ दिया। सामान्य अर्थ यानी आहुति की अग्नि, जोकि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए जलाई जाती थी, उसके बजाय गांधी ने यज्ञ को ऐसा अर्थ दिया, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने श्रम का एक हिस्सा या कौशल या अपने स्वामित्व की चीज समाज को समर्पित करता था। सूत्र-यज्ञ समाज के लाभ के लिए था। सूत कातते हुए आप रोजाना अपने को देश के सबसे गरीब कत्तिनों से जोड़ने की कोशिश करते। सामुदायिक कताई में सबसे दीन-हीन व्यक्ति के साथ समरसता कायम करने के उद्देश्य को एक दूसरे से साझा करने का तत्व भी शामिल रहता। हर सदस्य की रोजाना की कताई का नियमित रूप से हिसाब रखा जाता था। यह आश्रम के दैनिक अनुशासन का भी अंग था।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.