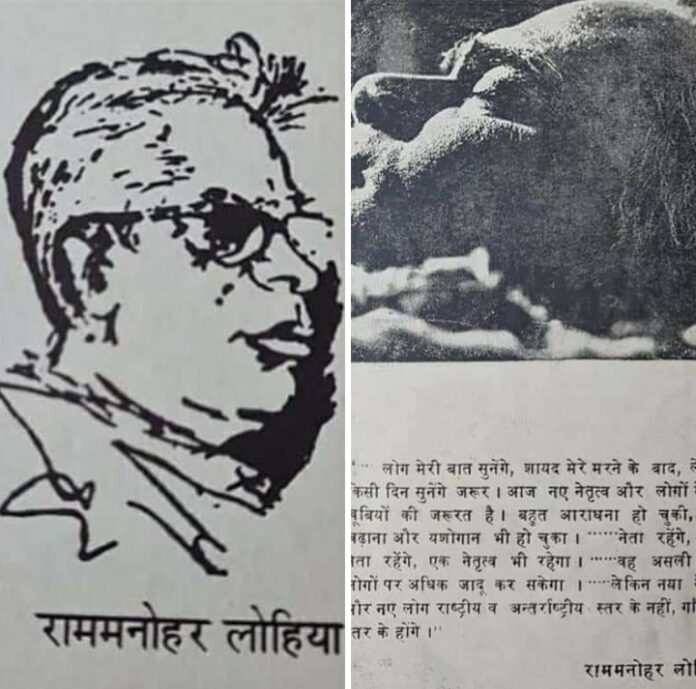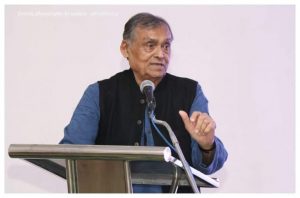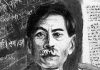— कनक तिवारी —
गणेश मंत्री की समझ में लोहिया की उनकी विचार-प्रणाली के मूल में तीन तत्व प्रमुख थे। पहला तत्व था समता को, सत्य और सौंदर्य की तरह एक सार्वभौम मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने की अदम्य आकांक्षा। इस आकांक्षा से प्रेरित होकर लोहिया ने निर्गुण और सगुण सभ्यता, पूर्ण और संभव बराबरी में तालमेल बिठाने और समता के आंतरिक तथा बाह्य के साथ-साथ मौलिक आध्यात्मिक अर्थों को समझने-समज्ञाने की लगातार कोशिश की। आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तनों के लिए लोहिया ने चौखंभा राज, छोटी मशीन की उत्पादन प्रणाली, न्यूनतम और अधिकतम आमदनी खर्च में, 1 और 10 के अनुपात खर्च पर सीमा जैसे जो अनेक कार्यक्रम दिये, उनके पीछे भी समता के निर्गुण सिद्धान्त को सगुण कार्यक्रम का रूप देने की ही इच्छा थी।.
/…….लोहिया की विचार-दृष्टि का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था– अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की मनुष्य की क्षमता और उसकी उन्नति में सीमा सम्बन्ध। जिस राष्ट्र या समुदाय में यह क्षमता नहीं है, उसकी पराजय या पतन निश्चित है। इसीलिए लोहिया ने आंतरिक अत्याचारियों के विरुद्ध व्रिद्रोह करने की जनता की क्षमता के साथ देश की स्वतंत्रता का भी सम्बन्ध जोड़ा था।..
….इसी के साथ जुड़ा हुआ लोहिया की विचार दृष्टि का तीसरा महत्वपूर्ण तत्वः परिवर्तन की शक्ति के रूप में जन-साधारण में प्रबल आस्था। लोहिया की राजनीति मूलतः साधारण जन की राजनीति थी, छोटे आदमी की राजनीति। उनको देश के बड़े लोगों, विशिष्ट वर्गों में अपने समर्थक बनाने की कभी कोई विशेष चिंता नहीं रही। इन विशिष्ट वर्गों को जब वे ‘‘खानदानी-गुलाम‘ या दो नम्बर के राजा‘‘ जैसे नामों से सम्बोधित करते थे, तो उसके पीछे की मान्यता यही थी कि ये वर्ग समाज को बदलने वाली, या उसका नव-निर्माण करने वाली शक्ति के सर्जक ही नहीं हैं। ये तो शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति के निर्माता और सर्जक तो साधारणजन हैं, जो किसी युगान्तरकारी विचार से प्रेरित होकर खेतों-कारखानों, सड़कों-चौराहों, पर संगठित होते हैं और उस विचार के लिये सब कुछ करने, मरने-मारने के लिये तैयार होते हैं।
मधु लिमये का यह सार संक्षेपित कथन है कि लोहिया ने कांग्रेस को अन्यायी यथास्थितिवाद के स्तम्भ की भांति देखा। इसका अन्त करना उनका प्राथमिक लक्षण था। इसकी पराजय तथा समाजवादी पार्टी की स्थापना से उन्हें चरम आनन्द मिलता। किन्तु सन् 1963 में अशोक मेहता तथा जे.पी.की राजनीति तथा उनके कार्यों ने उस आशा को ध्वस्त कर दिया था। पलटकर परिदृष्य को देखने पर सदैव ऐसा महसूस हुआ।
उन्होंने अपने स्तर से कार्य करने की चेष्टा की। किन्तु वह जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, यह कार्य उसकी क्षमता के परे था। लोहिया तुच्छ महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी और उसमें स्वार्थ का एक कण भी न था। इसी कारण से उन्होंने गैर-कांग्रेसवाद का आविष्कार किया ताकि गतिरोध को तोड़ा जा सके और एक प्रगतिशील आन्दोलन प्रारम्भ हो सके तथा निराशा के बादल छटें। उनकी दृष्टि से यह मात्र परिवर्तन का कारक था, न कि सत्ता का मार्ग।
लोहिया के नेहरू विरोध को लेकर शीर्ष कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संतुलित मूल्याकंन किया है कि, ‘‘जिस लोहिया से मेरी मुलाकात सन् 1934 ई. में पटना में हुई थी और जो लोहिया संसद में आये, उन दोनों के बीच भेद था। सन् चौंतीस वाला लोहिया युवक होता हुआ भी विनयी और सुशील था, किन्तु संसद में आने वाले प्रौढ़ लोहिया के भीतर मुझे क्रान्ति के स्फुलिंग दिखाई देते थे। राजनीतिक जीवन के अनुभवों ने उन्हें कठोर बना दिया था और बुढ़ापे के समीप पहुंचकर वे उग्रवादी बन गये थे। उनका विचार बन गया था कि जवाहरलाल जी से बढ़कर इस देश का अहित किसी ने नहीं किया है तथा जब तक देश मेें कांग्रेस का राज है, तब तक देश की हालत बिगड़ती ही जायेगी। अतएव उन्होंने अपनी राह बड़ी निर्दयता से तैयार कर ली थी और वह सीधी राह यह थी कि जवाहरलाल जी का जितना ही विरोध किया जाय, वह कम है और कांग्रेस को उखाड़ने के लिए जो भी रास्ते दिखाई पड़े, उन्हें जरूर आजमाना चाहिए।‘‘
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.