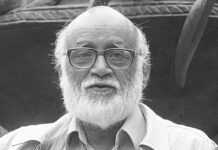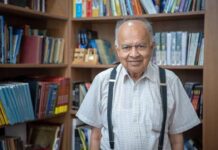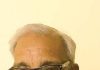— संजय श्रमण —
कला और कला से जुड़ी समाज दृष्टि को हर दौर में पुनर्परिभाषित करना होता है। कला सृजन का ही नहीं बल्कि संवाद और संप्रेषण का भी सबसे सशक्त आयाम है। हर देश में हर संस्कृति में कलाकार ही तत्कालीन समाज को परिभाषित करते आये हैं। कोई देश और समाज कैसे निर्मित हुआ और कैसे आगे बढ़ा – इस बात को कलात्मक अभिव्यक्तियों से ही जाना जाता है। जिसे हम ऐतिहासिक साक्ष्य, लेखन, काव्य, महाकाव्य, प्रस्तर शिल्प, स्थापत्य, वाचिक परम्परा, गीत इत्यादि इत्यादि कहते हैं – वो सब कला ही है।
आज जब तकनीक और संचार क्रांति ने कला को सुलभ बना दिया है तब कला से जुड़े विमर्शों की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस होती है। सभ्यता के आरंभ से ही नाट्य और रंग ने समाज की सबसे सृजनात्मक और ज़िंदा अभिव्यक्तियों को आकार देना शुरू किया। हर सभ्यता में रंग-कर्म और रंगमंच से जुड़े अपने नियम-क़ायदे और प्रस्तावनाएँ हैं। भारत में बौद्ध जातक कथाओं, जैन कथाओं से लेकर कालांतर में रामायण और महाभारत में मंचन योग्य कथाओं उपकथाओं का सृजन होता रहा है।
श्रमण बौद्ध और जैन परम्परा में बीज रूप में जो जातक कथाएँ थीं, वे आगे चलकर ब्राह्मण परंपरा में वृक्ष का रूप लेने लगीं। जीवित बुद्धों, स्थविरों तीर्थंकरों, श्रावकों के उज्ज्वल चरित्रों को देखकर महाकाव्यों के नायकों की कल्पना हुई। धीरे धीरे बुद्ध, महावीर आदि जैसे ऐतिहासिक पुरुषों के वास्तविक चरित्रों के विवरणों के आधार पर उज्जवल चरित्र नायकों के जीवन चरित्र बनने आरंभ हुए। कलात्मक अभिव्यक्ति आगे बढ़ी। बाद के कवियों नाटक-कारों गीतकारों ने इन नायकों के चरित्रों में वे सारे तत्व शामिल कर दिये जिनकी चर्चा बुद्ध और महावीर जैसे लोगों के योग-बल, तप-बल की कहानियों से जुड़ी थीं। बुद्ध जब अंगुलिमाल से बात करते हैं तो एक इंसान से दूसरे इंसान की बात हो रही है। लेकिन सैकड़ों साल बाद जब युधिष्ठिर जब यक्ष से बात करते हैं तो मिथकीय कल्पना कला और मनोविज्ञान की शक्ति लेकर नये आख्यान गढ़ने लगती है। धीरे धीरे महाकाव्य अस्तित्व में आने लगते हैं।
जातक कथाओं में जो राम, रावण, कृष्ण आदि लोग सामान्य मनुष्य थे, वे आगे चलकर काव्यों-महाकाव्यों में राजा-महाराजा, चक्रवर्ती सम्राटों में परिवर्तित हो गये – ये नये कवियों की कला का परिणाम है। जैसे जैसे आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ, इन नायकों में देवत्व का प्रक्षेपण बढ़ता गया। तत्कालीन कलाकारों कवियों ने इनके चरित्रों में कई कई आयाम जोड़े, समाज की तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप समाज को नैतिकता और धर्म-अधर्म शुभाशुभ की धारणा में दीक्षित करने के क्रम में ‘जय’ जैसा काव्य अंत में ‘महाभारत’ बन गया। बुद्ध और महावीर जैसे ऐतिहासिक सत्पुरुषों ने जिन चरित्रों के माध्यम से नैतिक प्रबोधन किया, वे काल्पनिक चरित्र आगे चलकर मिथकीय महानायक बन गये। आज उन्हीं के परितः बुना गया धर्म और धार्मिकता भारत में नज़र आती है।
ये सब कला का चमत्कार है।
कला की शक्ति को आप जातक कथाओं से महाभारत और पुराण तक आने वाले धर्म की यात्रा के ज़रिए समझिए। यही काम यहूदी, ईसाई और इस्लामिक परंपरा में हुआ है। थेरवाद के ऐतिहासिक बुद्ध के बाद महायान और वज्रयान ने मिथकीय बोधिसत्वों को जन्म दिया। इसके पीछे भी वही कारण था – ऐतिहासिक सत्पुरुषों से सीखे गये उज्ज्वल जीवन को काल्पनिक नायकों में प्रक्षेपित करके सभ्यता और संस्कृति का महा-आख्यान निर्मित करना। आगे चलकर बोधिसत्वों और स्त्री बोधिसत्वों तक जन्म लेने लगे। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की कल्पना हुई, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग एक हज़ार साल बाद अनेकों बोधिसत्वों की कल्पना आरंभ हुई।
इन्ही अवलोकितेश्वर को भारत की एक परंपरा ने शिव और दूसरी ने विष्णु के रूप में अपना लिया। इसी अवलोकितेश्वर के एक अवतार ने तिब्बत में दलाई लामा की परंपरा को जन्म दिया। भारत में वैष्णव परंपरा को जन्म दिया। स्त्री बोधिसत्वों से श्याम तारा श्वेत तारा महाकाली दुर्गा आदि का जन्म हुआ। एक बार फिर ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्रों से मिथकीय महानायकों, देवी देवताओं और ईश्वर तक का जन्म हुआ। धीरे धीरे ऐतिहासिक सत्पुरुषों के धर्म खो गये, लेकिन कलाकारों की कूँची से निकले महानायकों के धर्म शक्तिशाली बन गये।
ये सब कला की ताक़त है। ईश्वर और देवी देवता और धर्म असल में इंसानी कला के पुत्र पुत्रियाँ हैं।
ये आख्यान आम जनता को सुशिक्षित और (कुशिक्षित भी) करने के लिए खूब इस्तेमाल हुए। ये सारे आख्यान हज़ारों साल तक नाटक, नाच, नौटंकी और खेला इत्यादि के ज़रिए चलते रहे। राजप्रासादों से लेकर गली मुहल्लों के नुक्कड़ तक यही आख्यान अलग-अलग रूप-आकार में परोसे जाते रहे। फिर धीरे धीरे बिजली, भाप इंजन और रेलगाड़ी पर सवार होकर ‘लाइट, कैमरा और एक्शन’ हमारी ज़िंदगी में आ गया। रंगमंच और चित्रों की एक -आयामी दुनिया ने रूपहले पर्दे पर दो-आयामी दुनिया में छलाँग लगा ली।
इस छलांग की ताक़त को तत्कालीन शासकों धन्नासेठों और कलाकारों ने पहचाना। उन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिया जो जातक कथाओं के साथ हुआ था। ब्लैक एंड वाइट के जमाने में तकनीक अविकसित थी। इसलिए एकदम आम आदमियों की आम जीवन की बातों कि फ़िल्में बनीं। शुरुआती फ़िल्मों में एक इंसान दो या चार लोगों को ही पीट पाता था। बाद में चलकर नायक अतिशक्तिशाली होने लगे। यही क्रम हमें जातक कथाओं से महाभारत और पुराण तक नज़र आता है। फिर धीरे धीरे तकनीक आगे बढ़ी – स्पेशल विज़ुअल इफ़ेक्ट और साउंड इफ़ेक्ट आने लगे। अब सिनेमा में मिथक गढ़ने की शक्ति आने लगी। अब एक हीरो पचास लोगों को पीटने लगा।
फिर सिनेमा में वही हो गया जो तीन हज़ार साल पहले भारत के धार्मिक-कलात्मक सृजन और विमर्श में हुआ था। वास्तविक से काल्पनिक की तरफ़ यात्रा आरंभ हो गई। अब भारत का धर्म और भारत का सिनेमा दोनों काल्पनिक मिथकों में रंग गये हैं।
अब ऐसे में कल्पना कीजिए आचार्य वसुबंधु की, आचार्य नागार्जुन की, आचार्य कुंदकुंद की या पतंजलि की। ये लोग काल्पनिक और मिथकिय विस्तार में जाये बिना जीवन और जगत के गूढ़ सूत्रों को एकदम सीधे शब्दों में रख रहे हैं। वसुबंधु की विमशटिका, नागार्जुन की मूलमध्यमकारिका, जैनाचार्य कुंद-कुंद की ‘समयसार’, पतंजलि ये योगसूत्र आदि को देखिए – ये ऐतिहासिक पुरुषों द्वारा ऐतिहासिक सृजन है। फिर आगे की शताब्दियों में बौद्ध जैन और पौराणिक धर्म में मिथकिय आख्यानों की बाढ़ आने लगती है, फिर धीरे धीरे ऐतिहासिक सत्पुरुषों की जीवन से जुड़ी ठोस शिक्षाओं की जगह काल्पनिक देवी देवताओं और महानायकों की कहानियाँ समाज पर हावी हो जाती हैं।
फिर धीरे धीरे सारे धर्म कथाकारों और व्याख्याकारों के हाथ की कठपुतलियों बनकर आम इंसान की फ़िक्रो-तलब और बेहतरी से मुँह मोड़ लेते हैं। ये सारे धर्म फिर राजा, पुरोहित और धन्नासेठ के हाथों के खिलौने बन जाते हैं।
धर्मों के इस पतन को सिनेमा से जोड़कर देखिए।
सिनेमा भी आम इंसान की आम ज़िंदगी से शुरू हुआ, फिर उसमें देवी देवता और चमत्कार घुसने लगे। आज कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिना ईश्वर और आत्मा का कोई धर्म हो सकता है। उसी तरह आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिना स्पेशल इफ़ेक्ट और जादुई ताक़त या बुद्धि वाले हीरो के बिना कोई फ़िल ब्लॉकबस्टर कैसे हो सकती है।
धर्म और सिनेमा – दोनों ब्लॉक बस्टर होने के चक्कर में आम आदमी की ज़िंदगी से दूर निकाल गये।
लेकिन इस देश में कुछ फ़िल्मकारों ने लोगों ने पौराणिक कथाकारों और व्याख्याकारों की बुद्ध, महावीर, नागार्जुन और कुंदकुंद होना पसंद किया। उन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते। सत्यजीत रॉय, ऋत्विक घटक, शांताराम, गोविंद निहलानी, और श्याम बेनेगल उनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। बाक़ी पैसा कूटने और पब्लिक को लूटने भटकाने वालों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि अब क्या बताएँ।
भारत में आज़ादी के पहले ही सिनेमा ने धूम मचा दी थी। मिथकों की कहानियों को सुन सुनकर जनता की ‘वास्तविक मुद्दों’ को सुनने समझने की ताक़त कमजोर हो चुकी थी। भारत में सिनेमा में आम आदमी से जुड़े मुद्दे शुरू में फ्लॉप रहे, फिर सिनेमा को प्रसिद्ध करने के लिए हज़ारों साल पुराना फ़ॉर्म्युला लाया गया। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा आई, धीरे-धीरे अन्य मिथकीय कथाएँ आईं। ग़ुलाम भारत में चालीस पचास के दशक में आज़ादी के संघर्ष ने आम इंसानों को आम इंसानों के मुद्दों से जोड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ग़रीबी, शोषण, संघर्ष, नर-नारी समानता, छूआछूत विरोध से जुड़ी फ़िल्में बनने लगीं। लेकिन अस्सी के दशक में और ख़ास कर उदारीकरण के बाद आम जीवन से जुड़ा सिनेमा बिरजू के गाँव और सुक्खी लाला के खेत से निकलकर स्विट्ज़रलैंड में छलांग लगा देता है। हमारा सिनेमा तब से वहीं है, वो वहीं से अपने स्टंट, गीत और डांस हमें भेजता रहता है। उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि भारत के भगतराम की आज क्या हालत है और उसके खेत खलिहान नौकरी प्रमोशन परीक्षा और सिलेक्शन आदि का क्या हो रहा है।
धर्म में चमत्कार के प्रवेश ने धर्म को आम आदमी का दुश्मन बना दिया।
सिनेमा में चमत्कार के प्रवेश ने सिनेमा को आम आदमी का दुश्मन बना दिया।
धर्म की दुनिया में जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे कुछ नाम हैं जो अध्यात्म और धर्म को आम आदमी से जोड़कर उम्मीद ज़िंदा रखें हुए हैं। इसी तरह सिनेमा की कहानी में कुछ नाम आज भी हैं जो सिनेमा को आम आदमी से जोड़ते रहे हैं।
तो मित्रों, सिनेमा के नागार्जुन, कुंदकुंद या कृष्णमूर्ति को आज सलाम कीजिए। श्याम बेनेगल को सलाम कीजिए। श्याम बेनेगल के सिनेमा में अवदान को भारत की कला को आम आदमी तक लाने के लिए एक मिशन के रूप में देखिए।