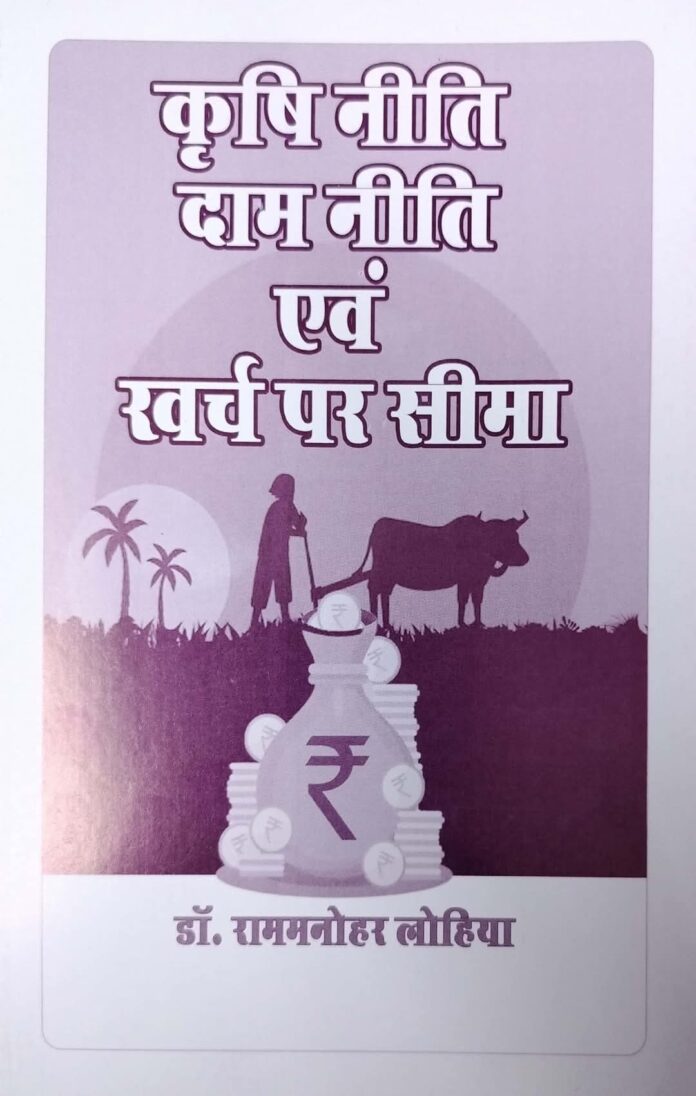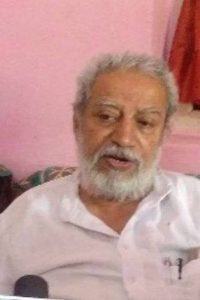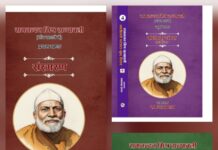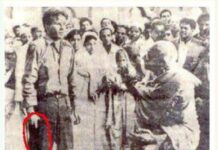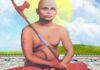— रघु ठाकुर —
स्वामीनाथन की रपट यह उनकी खोज नहीं है बल्कि इसका मूल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 1950 के भाषण और ससोपा की कृषि नीति और राजनीतिक कार्यक्रमों में है डॉ लोहिया ने यह बात सबसे पहले उठाई थी कि किसानों को लागत मूल्य में 50% जोड़कर यानी लागत मूल्य का डेढ़ गुना देना चाहिए परंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि जो बाजार के उत्पादों की दर है वह भी अधिकतम डेढ़ गुना हो – रघु ठाकुर
******
कृषि नीति, दाम नीति एवं खर्च सीमा पर एक नई पुस्तक समता ट्रस्ट कार्यालय भोपाल और नई दिल्ली में उपलब्ध हैl इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक श्री रघु ठाकुर जी ने लिखी है जो निम्न हैl
*****
भूमिका –
हिन्द किसान पंचायत का राष्ट्रीय अधिवेशन रीवा में 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इस अधिवेशन के उदघाटक और नेतृत्वकर्ता समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया थे। इस राष्ट्रीय किसान रैली में किसानों के संगठन और आंदोलनकारियों के समूह संयुक्त रूप से शामिल हुये थे। यह एक नई दिशा भी थी और उस दौर की महत्वपूर्ण घटना भी थी। डॉ. लोहिया का यह भाषण बहुत समय बाद पटना से प्रकाशित हो सका।
अपने भाषण में डॉ. लोहिया ने समूची दुनिया में किसानों के आंदोलन और घटनाओं को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा और उसकी व्याख्या की। इस लंबे भाषण में लोहिया ने समूचे देश के किसानों से निम्न 6 उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न होने की अपेक्षा की थी।
1. अध्यादेश द्वारा जमीन पर अधिकार जोतकर्ता का होगा।
2. अजोत जमीनों का सर्वे हो।
3. छोटी मशीनों द्वारा औद्योगिकीकरण।
4. पुर्नवितरण द्वारा प्रत्येक परिवार के पास 20 एकड़ जमीन और एक गाय हो।
5. व्यावसायिक एवं ग्रांस्तिक मूल्यों की समानता। (ग्रांस्तिक शब्द का प्रयोग घरेलू उपयोग के सामान के लिये किया गया है।)
6. चतुस्पदीय राज्य।
दरअसल यह 6 लक्ष्य वह थे जो बाद में समाजवादी आंदोलन और संयुक्त समाजवादी पार्टी के लक्ष्य बने।
समाजवादी आंदोलन ने बाद में जो नारा लगाया ‘जो जमीन को जोते बोये, वह जमीन का मालिक है’ और इस नारे का जन्म लोहिया के इस भाषण से हुआ था।
यद्यपि 1950 में सरकारी खाली जमीनों का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था, परंतु डॉ लोहिया का अनुमान था 100 करोड एकड़ जमीन ऐसी होगी जिसे वगैर किमी नुकसान के खेती के लिये खेतिहर मजदूरों में बाँटी जा सकती है। और आजीविका विहीन खेतिहर मजदूर इस जमीन को आबाद कर खेती योग्य बनाकर रोजगार भी पा सकते और देश को भूख से बचाने में सहयोग कर सकते हैं।
अपने इस भाषण में डॉ. लोहिया ने छोटी मशीन जिसे उन्होंने बाद में लघु इकाई तकनीक बताया, के माध्यम से ग्रामों को उद्योगीकृत करने और रोजगार पैदा करने, की गांधीवादी कल्पना को सामयिक रूप देकर प्रस्तुत किया था।
इन लक्ष्यों में लोहिया ने व्यावसायिक और राजनीतिक मूल्यों के बीच जो समानता की बात उठाई थी उसे न केवल देश की सरकारों, बल्कि समाज व किसानों तथा किसान आंदोलनों को भी समझने की आवश्यकता है। आजकल हमारे देश के किसान आंदोलन और कभी-कभी न समझ या चालाक राजनैतिक दल कृषि उपजों के बाजार दाम तय करने के लिये डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों को आधार बनाते हैं। मैं लगातार दो बातें कहता रहा हूँ, एक-स्वामीनाथन की रपट यह उनकी खोज नहीं है बल्कि इसका मूल डॉ. लोहिया के 1950 के भाषण और संसोपा की किसान नीति और राजनैतिक कार्यक्रमों में है। डॉ. लोहिया ने सबसे पहले यह बात उठाई थी कि किसानों को लागत मूल्य में 50 प्रतिशत जोड़कर यानि लागत मूल्य का डेढ़ गुना देना चाहिये परंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि जो बाजार के उत्पादों की दर है वह भी अधिकतम डेढ़ गुना हो। याने अन्न उत्पादकों की लागत का डेढ़ गुना मिले तो कृषि उत्पादकों के मिलने वाले घरेलू सामान के मूल्यों में समानता होना चाहिये। उस समय उन्होंने इसे गृहस्थ मूल्य कहा था, याने घर-गृहस्थी के सामान मूल्यों में सभी का इसी आधार पर निर्णय हो।
डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रपट तो एक प्रकार से बाजार को मुक्त छोड़ने की रपट है और एकागी है जिसमें किसानों की उपज का लागत मूल्य निकालकर तथा उसमें 50 प्रतिशत जोड़कर किसान को देने की सिफारिश है, परंतु इसकी कीमत आमजन या आम उपभोक्ता के लिये ही चुकानी होगी। सरकारें, सरकार के खजाने याने जनता के पैसे से उसे खरीदकर 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति बांटेगी और जो शेष 40 से 50 करोड़ लोग सामान्य मध्यमवर्ग के होंगे उन्हें अनाज खरीदने में यह कीमत चुकानी होगी। और दूसरी तरफ बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तथा बाजार घर-गृहस्थी के जरूरत के सामानों को मनमाने दाम पर अपना उत्पाद कारखाने वाला बेचेगा और किसान व आमजन की लूट करेगा। जिन किसानों को भी लागत का डेढ़ गुना दाम मिलेगा वह भी बाजार के राक्षसी पेट में समा जायेगा क्योंकि अंततः किसान को भी अपनी फसल को बेचकर अपने जीवन की पूर्ति के लिये बाजार में ही जाना होगा।
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 1950 में जब डॉ. लोहिया ने यह भाषण दिया था तो हमारे देश का मध्य वर्ग मुश्किल से 4-5 करोड़ रहा होगा और उसकी आय भी उस समय बहुत कम थी। सरकारी कर्मचारियों की तन्खा भी बहुत कम थी और शायद शिक्षक की पगार जो अब लाख रुपये के आसपास है उस समय बामुश्किल 30-40 रुपये होती थी। उस मध्य वर्ग को अनाज खरीदना महंगा होता था। अब के मध्य वर्ग व तब के मध्य वर्ग में बड़ा फर्क आया है। अब देश में लगभग 10 करोड़ के आसपास उच्च मध्य वर्ग तैयार हो गया है और 30 करोड़ मध्यवर्ग है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 1950 के दशक में देश का बाजार पारंपरिक बाजार था, जो आमतौर पर लोगों की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिये था, पर अब देश में पारंपरिक बाजार महत्वहीन हो गया है और गैर पारंपरिक या गैर जरूरी सामानों का बाजार बढ़ गया है। इसे दुनिया में उपभोक्तावाद का नाम दिया गया है। हालाँकि मेरी राय में यह उपभोक्तावाद से आगे है। उपभोक्तावाद तो फिर भी जरूरत से ज्यादा परंतु उपभोग की वस्तुओं तक सीमित था अब तो विलासितावाद है। जिसमें जरूरत और उपभोग दोनों की सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं उपभोक्तावाद ने और विलासितावाद ने अब एक नया जुमला गढ़कर बाजार को हजार और लाख गुना फैला दिया है. याने अगर देश में जरूरत के खरीददार 30-40 करोड हो तो उपभोक्तावाद के खरीददार इससे दोगने यानी 60-70 करोड तक होंगे तथा विलासितावाद के खरीददार गरीब से लेकर अमीर तक, भिखारी से लेकर अरबपति तक सभी कार के हरीयाब तो भिखारी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। बाजारवाद ने जो दुनिया को एक नया जुमला दिया है वह है ‘यूज एण्ड थ्रो’ और इस ने भी बाजार को पंख लगा दिये हैं। जहाँ हम पहले साल, दो साल या तीन साल तक एक कलम का इस्तेमाल करते थे वहां अब साल में 20-25 कलम खरीदते हैं, उन्हें कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं व फेंक देते हैं। यह तो मैंने मात्र एक उदाहरण दिया है परंतु यह स्थिति सभी जरूरत की चीजों या गैर जरूरी चीजों के साथ है वह चाहे वस्त्र हो, घर के सामान, गाड़ियाँ, मोबाइल हो, किताबें, कापियां या कोई भी सामान हो।
अभी हाल में भारत सरकार ने डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न के खिताब से नवाजा है। डॉ. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक माने जाते थे और उन्हें दुनिया का वह बदनाम पुरुस्कार जो अमेरिकी पिट्टू रमन मेग्साय की स्मृति में दिया गया था। मेग्साय पुरस्कार, यह पुरुस्कार भी बाजार का अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र है जो उसके प्रवर्तक प्रचारक या अनुकूल लोगों को सम्मानित करता है, उन्हें पैसा देता है और अपनी जरूरतों के लिये उनका इस्तेमाल करता है। ऐसे पुरुस्कार प्राप्त लोगों को मैं बाजार का प्रचारक व दलाल मानता हूँ। निसंदेह मेरी बात कुछ नये देशी-विदेशी अनुदान प्राप्त लोगों को कड़वी लगेगी पर सच यही है। भारत सरकार ने अभी इसी वर्ष डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर अपना राजनैतिक हित साधा है। एक तो यह कि हमारे देश के अज्ञानी किसान आंदोलन या कहा जाये बाजार प्रेरित किसान आंदोलन डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रपट को लागू करने को पवित्र गीता जैसा संदेश मानते हैं। वैसे भी पिछले 3-4 वर्षों में किसान आंदोलन अभी तक देश में कुछ खाते पीते कुछ संपन्न किसानों का आंदोलन है, जो लगातार वर्षों तक वगैर किसी अधिक कठिनाई के धरना आदि कर सकता है।
उसका आर्थिक बोझ सह सकते हैं। यह कभी भी लोहिया के इस नारे की चर्चा नहीं करेंगे कि ‘जो जमीन को जोते बोये, वह जमीन का मालिक है’। क्या यह तथ्य नहीं है कि आज पंजाब में कृषि की बड़े जोते मशीनों और बिहार के गरीबों पर निर्भर हैं? परंतु जब किसी आंदोलन का लक्ष्य केवल किसी राजनैतिक सत्ता को हासिल करना या गिराना हो जाता है तो ऐसे भटकाव होना स्वाभाविक है। भारत सरकार का डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का एक उद्देश्य इस किसान आंदोलन के लोगों को भरमाना भी है और यह बताना भी है कि सरकार किसानों की बड़ी हितैषी है। और वगैर किसी मांग पर कोई ठोस चर्चा के उनके एक हिस्से में व्याप्त आक्रोश को कम करना है। कुल मिलाकर दोनों तरफ बाजार का प्रचार युद्ध है, स्वामीनाथन आयोग कमेटी की सिफारिश के नाम पर, और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के नाम पर। मैं डॉ. स्वामीनाथन के कृषि ज्ञान व कृषि विज्ञान की विशेषज्ञता को चुनौती नहीं दे रहा हूँ मैं तो केवल यह बता रहा हूँ कि कृषि वैज्ञानिक की विशेषज्ञता और देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और किसान की सामाजिक और वास्तविकता विशेषता। दोनों में फर्क होता है।
अपने इस भाषण में लोहिया ने छठवाँ लक्ष्य चतुस्पदीय राज्य कहा था। इसे बाद में चौ-खम्भा राज्य कहा गया था। लोहिया ने गांधी के ग्राम स्वराज्य को जो एक दूरगामी एवं बड़ा लक्ष्य था, को चौ खम्बा राज्य की कल्पना से एक व्यावहारिक स्वरूप देने का प्रयास किया था। याने पहले संविधान के अनुसार राज्य की शक्तियों को चार हिस्सों में उनकी उपयोगिता व जरूरतों के हिसाब से बांटा जाये तथा सत्ता का केंद्रीयकरण जो दिल्ली व सूबाइ राजधानियों के आसपास सिमट रहा था उसे नीचे जनता तक पहुंचाया जाये। संविधान निर्माण के समय पंचायती राज को लागू करने का तत्काल अनिवार्य प्रावधान नहीं किया गया था परंतु उसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर उसे भविष्य के राजकीय लक्ष्य के रूप में रखा गया था। 80 के दशक में इस लक्ष्य को वैधानिक स्वरूप मिला जब स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र और राज्य के अलावा जिला व ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तिमान बनाया गया था। हालाँकि कांग्रेस में सदैव से यह अकृतज्ञता रही है कि वे सच को स्वीकार नहीं करते और अपने दल के दलीय सत्ता केंद्र से इतने भयभीत रहे हैं कि जो सच जानते भी है, वह भी कह नहीं पाते। ऐसा लगता है कि शायद व्यक्ति केन्द्रित दलों व सरकारों का चरित्र ही यह हो गया है।
वर्तमान केंद्र सरकार जो भाजपा की है, इस मामले में वह भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। अगर स्व. राजीव गांधी ने पंचायती राज के संशोधन के समय महात्मा गांधी के स्मरण के साथ-साथ चौ-खम्बा राज्य की कल्पना के जनक डा. राममनोहर लोहिया का उल्लेख किया होता तो यह उनकी ईमानदारी भी होती व कृतज्ञता का भाव भी होता। इसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गाँव में शौचालय निर्माण की योजना के साथ या तीर्थ स्थलों को जन सुविधाओं से लैस करते समय अगर डॉ. लोहिया की चर्चा की होती जिन्होंने 1956 में ही महिलाओं की और ग्राम शौचालयों की व्यवस्था, नदियों को साफ करने की मांग और जनता की भावनाओं, के केंद्र स्थानों (तीर्थ स्थानों) की तरक्की व विकसित करने की बात को उठाने की बात शुरू की थी, का उल्लेख करते समय डॉ. लोहिया का नाम लेते तो यह न केवल सत्यता व कृतज्ञता होती, बल्कि यह उनके लिये गौरव और सम्मान की बात होती। सत्य को छिपाना भी एक मानसिक बौनेपन की निशानी है। यह तो महात्मा गांधी जैसे महान व विशाल व्यक्तित्व का ही गुण हो सकता है कि वे सत्याग्रह की चर्चा करते समय भक्त प्रहलाद व हैनरी थोरो का उल्लेख करते थे। छोटी मशीन और उनकी सीमाओं की चर्चा करते समय सिंगर की याद करते थे।
डॉ. लोहिया का यह भाषण भारतीय किसानों की उस समय की दुरावस्था का चित्रण है, इसके साथ-साथ यह भाषण समाजवादी आंदोलन के मूल आधारों का वर्णन भी है। यह भाषण जहाँ एक तरफ किसान नीति का एक स्थाई दस्तावेज है वहीं देश व दुनिया में उभरती हुई तानाशाही व सांप्रदायिक प्रवृत्तियों का भी संकेत देता है जो उस समय उभर रही थीं और अब अपने पूर्ण विकास पर है। अपने भाषण में डॉ. लोहिया कहते हैं ‘निश्चित नीति और योजना के अभाव में व्यक्ति का शारीरिक व बौद्धिक पतन दिनों-दिन बढ़ता है परिणामस्वरूप अहंकार में लोगों का दिमाग अचेतन रूप से तानाशाही वृत्ति की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में देश हमेशा साधु व पूजा (मूर्तिपूजा) के पीछे भागता है जिससे उसे दुख व पाप से मुक्ति मिले। इसी भाषण में वह आगे कहते हैं कि ‘सचमुच सभी लोगों के बीच नेता है परंतु जब लोग अपने नेता के अंग बन जाते हैं तो केवल उसी समय तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक प्रोग्राम व विचार प्रतिभूत होते रहते हैं। कुछ ही लोग इस नाटक में उपस्थित होते हैं।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म व जाति की आड़ में छिपे रहते हैं। एक प्रकार की तानाशाही की स्थापना इसके मूल में पड़ी रहती है। धर्म के आधार पर प्रतिस्थापित इस प्रकार तानाशाही विरोधी विचारों के प्रयास पूर्व निर्मित, राजनैतिक, मिल मालिकों व जमींदारों की सत्ता के साथ बंधी रहती है। वे आगे कहते हैं कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की तानाशाही स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि इस प्रकार का तानाशाह असफल दुर्भाग्य पैदा करता है इसमें बराबर खतरा रहता है और यह राष्ट्रीय फूट का कारण बन जाता है। वास्तव में धर्म संपूर्ण विश्व में राजनीति के ऊपर प्रभावशाली ढंग से हावी हो रहा है, जहां कहीं भी एशिया और यूरोप में कंर्जवेटिव पार्टियां धर्म पर आधारित हैं, शक्तिशाली बन रही हैं।’ यह एक प्रशंसनीय बात होगी अगर राजनीति भी धार्मिक आधार पर प्रतिस्थापित हो सके लेकिन दुख इस बात का है कि धर्म ही राजनीति बनता जा रहा है। ‘लोहिया ने जो यह बात कही थी अब उसका चरम रूप सामने है।
मैं मानता हूँ कि पंचायती राज चौ खम्बा राज्य और विकेंद्रीयकरण की महान कल्पना जो महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर डॉ. लोहिया ने की थी, वह भी व्यक्ति चरित्र के गिरावट और व्यवस्था के भ्रष्टाचार और विलासिता के लालच के मार्ग पर चलकर अपने पथ से भ्रष्ट हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण, भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीयकरण चौ खम्बा राज्य के भ्रष्टाचार में बदल गया है। मुझे याद है कि लगभग 24-25 वर्ष पूर्व श्री अरविन्द केजरीवाल जो हाल फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय पंचायती राज के लिये अनुदान प्राप्त एनजीओ में कार्यरत थे, श्री संजय सिंह का संदर्भ लेकर मेरे पास दिल्ली के माता सुंदरी वाले दफ्तर में आये थे। उन्होंने मुझसे पंचायती राज के समर्थन के लिये सहयोग मांगा था। उस समय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के दो विधायक राजस्थान से चुनाव जीतकर आये थे और शायद उनको मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ी होगी। मेरी यह समझ थी कि वे सूचना के अधिकार के एनजीओ में काम कर रहे हैं, परंतु उस दिन मालूम पड़ा कि वे पंचायती राज के क्षेत्र में काम करने लगे हैं और शायद, श्रीमती अरुणा राय जो उनकी सूचना के अधिकार की मानसिक और आर्थिक मुखिया थीं उनसे उनका अलगाव हो गया था।
मैंने उनसे कहा था कि मैं गांधी लोहिया को मानता हूँ, पंचायती राज व चौ खम्बा राज को आदर्श कल्पना मानता हूँ। परंतु पंचायत के प्रतिनिधियों का जो चारित्रिक पतन हो रहा है, वह न केवल चिंता का विषय है बल्कि इस समूची कल्पना को बिगाड़ देने वाला है। उसके कुछ दिन पहले ही मैं ग्वालियर का दौरा कर दिल्ली आया था और मुझे मेरे एक साथी गजराज सिंह सिकरवार, जो बाद में भाजपा में चले गये थे, के द्वारा सुनाई गई घटना दिमाग में थी। श्री गजराज सिंह ने मुझे बताया था कि उनके एक परिचित व्यक्ति उनके पास बाम्मोर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिये भाजपा का समर्थन मांगने आये थे। उन्होंने उनसे पूछा था कि आजकल चुनावों में बहुत पैसा लगता है, तुम इतना पैसा कहां से लाओगे ? तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसने सारी योजना बना ली है। उसके शब्दों में, मैं अभी कर्ज लेकर चुनाव लढुंगा और जीतने के बाद बाजार के व्यापारियों के पास दुकानों के सामने जरी बुलवा दूँगा। याने उनकी नपती करवा दूँगा, और उन सबसे पैसा लेकर कर्ज चुका दूँगा व खुद भी कमा लूँगा। कल्पना कीजिये की चुनाव के पहले से ही वक्ति भ्रष्टाचार की संभावनायें तलाश रहा है और बाद में वह क्या करेगा? मैंने श्री केजरीवाल से कहा कि लोगों को इन बातों पर शिक्षित व जागृत करने की आवश्यकता है तभी पंचायती राज का कोई अर्थ होगा। वह समझदार व्यक्ति हैं और मेरी बात का अर्थ बखूबी समझ गये होंगे। उन्हें तो किसी अन्ना को खोजने की जल्दी थी और मैं वह बनने को न तब तैयार था और न अब। और अब तो लगता है कि शायद मेरी सच्चाई व समझ ठीक ही थी जिसे अपने सत्ताकाल के अनुभव में वे भी देख चुके होंगे।
डॉ. लोहिया ने अपने भाषण में अंत में 13 लक्ष्य किसान आंदोलन के सामने रखे थे वे आज भी सभी सिद्धांत रूप में प्रासंगिक हैं। 1950 के आंकड़ों में और आज के आंकड़ों में फर्क हो सकता है। जिस प्रकार बच्चे के जन्म और विकसित पुरुष में कद-काठी और वजन का फर्क होता है परंतु मानव की मूल आत्मा या जीव तो वही होता है।
इस पुस्तक के प्रकाशन से हमारा यह प्रयास है कि किसान आंदोलन सीखें राजनैतिक दल बदलें, नेता समाज ज्ञानी हो और सरकारें नीतियों को अमल करने वाली बनें। आंदोलन सुधरें, दलों की शैली बदले और सरकारें नीति पर अमल करें अन्यथा तीनों को ही देर-सवेर इतिहास के गर्त में जाना होगा।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.