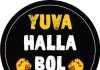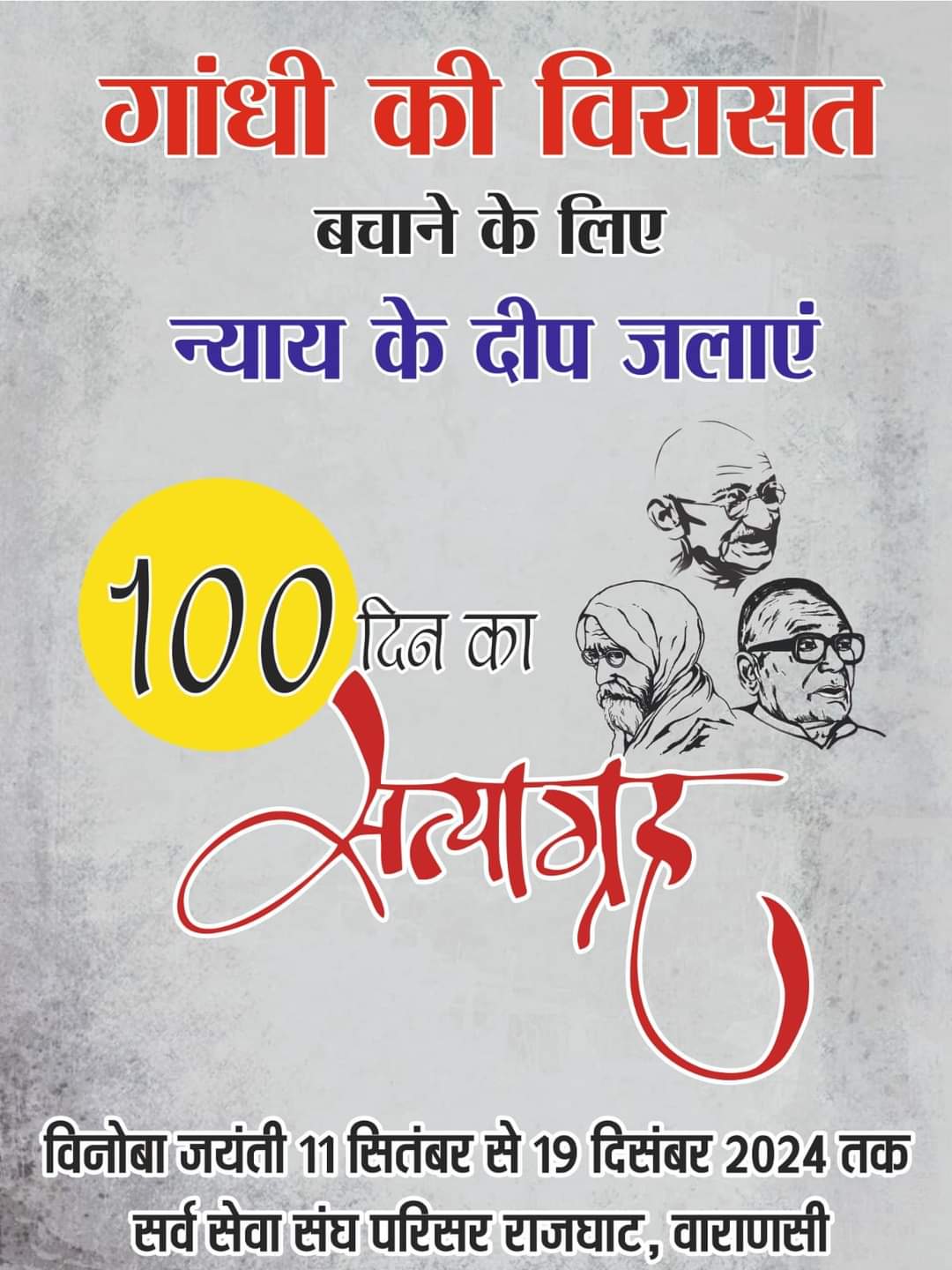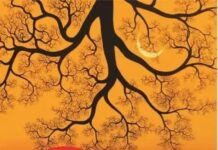— परिचय दास —
अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ हिन्दी साहित्य के उन वरेण्य कवियों में हैं जिनका समस्त सृजन एक समृद्ध सांस्कृतिक चेतना, गहरी काव्यात्मक अनुभूति और सौन्दर्यबोध से अनुप्राणित है। ‘हरिऔध’ उस संक्रमणकालीन समय के कवि हैं जब हिन्दी कविता ने ब्रज और अवधी की पारम्परिक सीमाओं को छोड़ खड़ी बोली में अपनी पहचान गढ़नी आरंभ की थी। वह न केवल खड़ी बोली के पहले महत्त्वपूर्ण कवि हैं बल्कि भाषा को साहित्य की गरिमा तक पहुँचानेवाले रचनाकार भी हैं। उनके साहित्य में संस्कृतनिष्ठ क्लासिकी गाम्भीर्य है, उर्दू-फ़ारसी की रवानी है और आधुनिक हिन्दी की सहजता भी। यह त्रिवेणी उनके काव्य को एक दुर्लभ समृद्धि देती है।
हरिऔध की काव्य चेतना मूलतः भारतीय जीवनमूल्यों से संलग्न है किन्तु उसमें समय की नब्ज़ को पहचानने की भी क्षमता है। वह अपनी कविता को महज नैतिक उपदेश का साधन नहीं बनाते बल्कि उसे अनुभव की एक गहन और चुप बहती नदी की तरह रचते हैं। उनकी रचनाएँ , जैसे- ‘प्रियप्रवास’, ‘वैदेही वनवास’, ‘पारिजात’, ‘रस-कलश’, ‘चुभते चौपदे’ , ‘चोखे चौपदे’ आदि उस युग की साहित्यिक संरचना को समझने के लिए मूलपाठ की तरह हैं। ‘प्रियप्रवास’ को तो हिन्दी का पहला खड़ी बोली महाकाव्य कहा जाता है जो काव्य सौंदर्य, भावप्रवणता और भाषा-शिल्प के स्तर पर एक मौलिक और मील का पत्थर कहा जा सकता है। यह रचना रामकथा पर आधारित होते हुए भी अपने शिल्प, भाषा और भावबोध के कारण परंपरागत रामायण से भिन्न एक नवीन दृष्टि का उद्भाव करती है।
‘प्रियप्रवास’ की भाषा में जो संस्कृतनिष्ठता है, वह आज के पाठक को कठिन लग सकती है पर हरिऔध के समय में यह भाषा एक सांस्कृतिक आत्मगौरव की तरह प्रयुक्त हुई थी। उनकी पंक्तियाँ जैसे – “अमल सी सुधा-सी वाणी, विरल सी विमल कहानी” – न केवल एक सौंदर्यबोध का निर्माण करती हैं बल्कि यह भी दिखाती हैं कि खड़ी बोली भी ब्रज की कोमलता और काव्यशीलता को प्राप्त कर सकती है। हरिऔध की भाषा एक आन्तरिक अनुशासन से बँधी हुई है, जिसमें अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक का इतना कोमल और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है कि पाठक उसमें रम जाता है।
उनकी कविता का एक पक्ष शास्त्रीय है तो दूसरा लोकानुभव से जुड़ा हुआ। वे केवल पुराकथा के कवि नहीं हैं बल्कि लोकभावना और जनमन की सहजता को भी अपने काव्य में उतारते हैं। वह जीवन के हर पक्ष को कविता के योग्य मानते हैं। यही कारण है कि उनके यहां वैराग्य, प्रेम, नीति, प्रकृति, लोकजीवन, इतिहास और सामाजिक यथार्थ – सब एक साथ उपस्थित हैं। उनका साहित्य जैसे हिन्दी मानस का हिस्सा बन गया है जो अपने भीतर संघर्ष, आत्मबल और जीवन के प्रति आस्था की घोषणा करता है।
हरिऔध की कविता में ‘शिल्प’ एक गंभीर विषय है। वे काव्य के लिए भाषा की एक ऊँचाई चाहते हैं। कविता उनके लिए मन की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है बल्कि वह उसे एक कलात्मक अनुशासन में गढ़ते हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में एक ओजपूर्ण माधुर्य है जो न तो केवल भावुकता है, न केवल विचार बल्कि दोनों के बीच की एक संतुलित तान है। उनका काव्य रीतिकालीन वर्णनात्मकता से हटकर भाव की गहराई में उतरता है किन्तु उसमें एक सूक्ष्म शैलीगत विन्यास उपस्थित रहता है जो उनके रचनाकार की कला-बोध को प्रमाणित करता है।
एक आलोचक के रूप में जब हम हरिऔध को देखते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वे केवल कवि नहीं थे, वे भाषा के मूर्तिकार थे। उनकी कविता में शब्द चुन-चुनकर आते हैं, जैसे वह कोई प्रतिमा गढ़ रहे हों। उनके लिए कविता एक ‘दृष्टि’ है, केवल ‘दृश्य’ नहीं। वे राम को केवल पूज्य नहीं बनाते, बल्कि उन्हें उस मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं जो पीड़ा, विरह और कर्तव्य के द्वंद्व में जीता है। ‘प्रियप्रवास’ का राम एक त्रासद नायक है जो आत्मसंयम के पथ पर चलता हुआ भी मानवीय वेदना से ओतप्रोत है। यह छवि उन्हें परंपरागत रामकाव्य से अलग करती है।
हरिऔध के साहित्य में एक विराट भारतीयता है पर वह संकीर्ण नहीं है। उसमें वह ‘विस्तार’ है जो प्रकृति, समाज और आत्मा के बीच सेतु बनाता है। उनकी कविताओं में जो प्रकृति चित्रण है, वह केवल दृश्यावली नहीं है बल्कि एक जीवित संवेदना है। फूल, चाँदनी, वसंत, पवन, जल – सब जैसे उनके काव्य में एक अंतर्मन की भाषा बोलते हैं। उनकी कविताएँ कभी-कभी इस सीमा तक सूक्ष्म हो जाती हैं कि वे छायावादी पूर्वाभास प्रतीत होती हैं। यद्यपि हरिऔध छायावाद से पूर्व के कवि हैं पर उनकी भाषा, बिम्ब और कल्पना शक्ति उस दिशा में संकेत करती है जहाँ कविता आत्मा की अनुगूंज बन जाती है।
हरिऔध का साहित्य केवल हिन्दी के विकास की गाथा नहीं है, वह साहित्य के सौंदर्यशास्त्र का भी इतिहास है। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि हिन्दी में भी वह काव्यात्मक गरिमा संभव है जो संस्कृत, उर्दू या अंग्रेजी में पाई जाती है। उनकी यह भूमिका हिन्दी साहित्य के आत्मविश्वास को एक नया आयाम देती है। वह किसी वाद के नहीं, आत्मा की आवाज़ के कवि हैं। उन्होंने कविता को जीवन की सच्चाइयों, लोक की गहराइयों और भाषा की ऊँचाइयों से जोड़ा। वे परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम रचते हैं – बिना किसी शोर के, बिना किसी उग्रता के।
हरिऔध के साहित्य में जो गहन आत्मीयता है, जो अन्तःसलिला प्रवाह है, वह उन्हें हिन्दी साहित्य में कालजयी बनाता है। उनके काव्य में भव्यता है पर उसमें एक करुण लय भी है। वह शब्दों से केवल चित्र नहीं बनाते, वे पाठक के भीतर एक ध्वनि जागृत करते हैं – एक ऐसा भाव-संगीत जो जीवन की करुणा, सघनता और सौंदर्य से पाठक को भर देता है। हरिऔध की यह ललित साहित्यिक उपस्थिति हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक अलभ्य संवेदना की तरह है, जिसे जितना पढ़ा जाए, वह उतना ही भीतर उतरती है।
इस प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ का साहित्य एक निरंतर स्पंदनशील आत्मा की उपस्थिति है – जिसमें भारत की काव्य परंपरा, संस्कृति, नैतिकता और सौंदर्य की सम्मिलित छवि है। उनकी कविता में समय का सन्नाटा नहीं बल्कि एक अनुगूंज है जो हर युग में सुनाई देती है। वे उस दुर्लभ पीढ़ी के कवि हैं जिन्होंने कविता को भाषा की परंपरा से उठाकर आत्मा की लय में ढाला। यही उन्हें अमर बनाता है।
हरिऔध की कविताओं में एक गहरी नैतिक चेतना विद्यमान है किन्तु यह उपदेशात्मकता में नहीं बल्कि एक सहज आंतरिक अनुशासन में प्रकट होती है। वह मनुष्य के भीतर के मूल्यबोध को संबोधित करते हैं—ऐसे मूल्य जो जीवन को गरिमा देते हैं जो आत्मबल और संकल्प के सहारे जीवन के संघर्षों का सामना करना सिखाते हैं। उनकी काव्य-दृष्टि जीवन को द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखती है—एक ओर करुणा है तो दूसरी ओर कर्तव्य; एक ओर प्रेम है तो दूसरी ओर वैराग्य; एक ओर सौंदर्य है तो दूसरी ओर त्याग। इस द्वंद्व में हरिऔध का काव्य न तो किसी एक पक्ष का एकतरफ़ा गान करता है, न ही उसे निष्क्रियता में बदलता है बल्कि वह एक सामंजस्य की खोज करता है जो आत्मा को संतुलन प्रदान करे।
यह संतुलन हरिऔध की भाषा-शैली में भी दिखता है। वे भाषा को अलंकरण से लादते नहीं बल्कि उसे संगीत की तरह सजाते हैं। उनकी कविता में छंद की कसावट है पर वह शुष्क अनुशासन नहीं बनता। उनकी लेखनी शब्दों से राग रचती है। वे जब ‘प्रियप्रवास’ में राम और सीता के प्रणय और वियोग की कथा कहते हैं, तो वह केवल कथा नहीं रहती—वह एक ऐसी अनुभूति बन जाती है जिसमें पाठक स्वयं को उस समय, उस क्षण और उस भाव में समाहित पाता है। यह उनकी भाषा की अद्वितीय क्षमता है—वह समय के आवरण को भेदकर पाठक तक सीधे पहुँचती है।
हरिऔध केवल काव्य नहीं रचते, वे एक नैतिक भूगोल निर्मित करते हैं—एक ऐसा भूगोल जिसमें जीवन की ऊँचाइयाँ और गहराइयाँ साथ-साथ दिखाई देती हैं। वह किसी एक भाव में ठहरते नहीं बल्कि विविध भावों की अन्तःप्रवाही धारा बनाते हैं। वह भारतीय संस्कृति की उस धारा के कवि हैं जो वेदों से लेकर तुलसी और कबीर तक बहती आई है परन्तु उन्होंने उसमें आधुनिक चेतना की ध्वनि भी जोड़ दी। यही कारण है कि उनकी कविता इतिहास की स्मृति बनकर नहीं, एक जीवित संवेदना बनकर हमारे सामने आती है।
उनके काव्य में स्त्री की छवि भी अत्यंत संवेदनशील ढंग से उकेरी गई है। सीता का चित्रण हो या अलका की कल्पना—हरिऔध स्त्री को केवल श्रद्धेय रूप में नहीं देखते बल्कि एक पूर्ण, अनुभूतिशील, स्वायत्त व्यक्तित्व के रूप में चित्रित करते हैं। ‘प्रियप्रवास’ की सीता अपने वियोग में निष्क्रिय नहीं है, वह स्मृति, करुणा, प्रतीक्षा और आत्मबल की जीवित प्रतिमा है। हरिऔध की यह दृष्टि उस समय की पुरुष-प्रधान सोच से अलग एक व्यापक सौंदर्यबोध का संकेत देती है।
उनकी एक और विलक्षण विशेषता यह है कि वे इतिहास को केवल भूतकाल की वस्तु नहीं मानते बल्कि वर्तमान के भीतर उसकी अनुगूंज को सुनने की क्षमता रखते हैं। जब वे किसी पौराणिक कथा को उठाते हैं, तो उसमें आज का मनुष्य, आज का संघर्ष और आज की चेतना झलकने लगती है। उनकी कविता जैसे यह कहती है कि पुराना कभी केवल ‘बीता हुआ’ नहीं होता, वह जीवन की अन्तर्धारा में समाया रहता है और वही उसे कालजयी बनाता है।
हरिऔध का साहित्य केवल हिन्दी साहित्य का गौरव नहीं, वह समूचे भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। वे हिन्दी कविता के उस स्वर को गढ़ते हैं जो न तो उर्दू की तरह शायरी है, न संस्कृत की तरह श्लोकात्मक; वह एक अलग ही मिठास, एक अलग ही गंभीरता और एक अलग ही रागात्मकता से भरी हुई होती है। उनकी कविता न तो केवल भाव की है, न केवल विचार की बल्कि वह दोनों को एक साथ रचती है। यही रचनात्मक संतुलन उन्हें एक ललित कवि बनाता है—ललित न केवल शिल्प के कारण बल्कि अनुभूति के कारण भी।
हरिऔध की काव्य-दृष्टि में एक गहरा आशावाद है पर वह सतही नहीं। वह जीवन की विडंबनाओं को जानता है, उसे दुःख की गहराई का भान है, पर वह उनमें डूबता नहीं, उनसे ऊपर उठता है। उनकी कविताएँ जैसे कहती हैं कि जीवन एक युद्ध है किन्तु उसमें सौंदर्य है, धर्म है, प्रेम है और अर्चना भी। यह कविता को आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक उच्च मानवीय धरातल पर प्रतिष्ठित करती है। यही हरिऔध की शक्ति है—वे कविता को जीवन के सहचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि केवल मनोरंजन या अलंकार के रूप में।
इस समग्रता में हरिऔध का साहित्य उस विरल संवेदना का वाहक है, जिसकी खोज हर युग का पाठक करता है। वह न केवल अपने युग के कवि हैं, न केवल खड़ी बोली के प्रवर्तक—बल्कि वे उस काव्यधारा के प्रतीक हैं जो भाषा, भाव और विचार के उच्चतम सम्मिलन से उत्पन्न होती है। उनकी कविता न किसी सीमा में बंधती है, न किसी काल में। वह चिरंतन है—जैसे भारतीय आत्मा की कविता।
हरिऔध का साहित्य केवल काव्य-रचना की उत्कृष्टता नहीं है, वह भारतीय काव्य-परंपरा के भीतर एक वैचारिक और भावनात्मक नवोन्मेष का अद्भुत उदाहरण भी है। उनकी रचनाओं में केवल सौंदर्य का अनुशीलन नहीं होता, वहाँ एक प्रकार की गहरी वैचारिकता और सर्जनात्मक अनुशासन भी व्याप्त है। वे भाषा और विचार को कभी अलग नहीं करते; उनके यहाँ भाषा विचार की गूंज बन जाती है, और विचार भाषा का स्वभाव। यही कारण है कि हरिऔध की कविता में शब्द केवल अर्थ नहीं देते, वे एक सम्पूर्ण भावलोक की रचना करते हैं।
उनकी रचनाओं में भारत की सांस्कृतिक आत्मा बार-बार मुखर होती है, पर वह आत्मा किसी परंपरागत आग्रह या रूढ़ि से नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना की तपस्या से प्रकाशित होती है। वे परंपरा को केवल पुनरावृत्त नहीं करते, उसे नवीन अर्थों में रूपांतरित करते हैं। यही कारण है कि ‘प्रियप्रवास’ जैसे काव्य का कथा-विषय पौराणिक होते हुए भी अपने भाव और प्रस्तुति में अत्यंत आधुनिक प्रतीत होता है। राम और सीता का प्रेमविवश वियोग उस समय की नैतिकता और कर्तव्यबोध का बिम्ब तो है ही पर वह आधुनिक पाठक के लिए भी उतना ही जीवंत और अनुभूतिपरक है।
हरिऔध की भाषा शुद्धता और माधुर्य की प्रतीक है, पर वह कभी कृत्रिम नहीं लगती। उसमें एक प्रकार की ‘जीवित क्लासिकी’ मौजूद है। वे अलंकारों का चयन बड़े संयम से करते हैं और छंदों की अनुशासनशीलता के भीतर भी भावों को सहज बहने देते हैं। यह संतुलन दुर्लभ है—जहाँ कविता पाठ्य-गुणों के कारण भी समादृत हो और भाव-विस्तार के कारण भी प्रिय लगे। उनकी भाषा न केवल काव्य के लिए है, वह जैसे जीवन के राग को स्वर देने के लिए ही जन्मी हो।
हरिऔध का सौंदर्यबोध केवल प्रकृति-चित्रण या नारी-सौंदर्य तक सीमित नहीं है। उनका सौंदर्य एक गहरी नैतिकता, एक गरिमा और एक आत्मिक आभा से भरा होता है। वह सौंदर्य जो सहनशीलता में है, त्याग में है, कर्तव्य में है और उस वियोग में भी है जिसमें प्रेम की गहराइयाँ अपने सबसे पारदर्शी रूप में व्यक्त होती हैं। ‘प्रियप्रवास’ की समूची संरचना इसी भाव-सौंदर्य की गवाही देती है। वह केवल एक प्रेमकथा नहीं, वह आत्मा की कविता है—एक ऐसी आत्मा जो धर्म, प्रेम और स्मृति से गुँथी हुई है।
उनकी कविताओं में बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी गहराई से किया गया है पर वह किसी प्रदर्शन या चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि अर्थ की सांद्रता और अनुभूति की सघनता के लिए होता है। फूल, दीप, नदी, पथ, अंधकार—ये सब उनके यहाँ केवल दृश्य नहीं, भाव के वाहक बन जाते हैं। वे दृश्य को इतना पारदर्शी बना देते हैं कि उसमें से अनुभूति झलकने लगती है। यही गुण उन्हें एक ललित कवि के साथ-साथ एक गम्भीर चिन्तक भी बनाता है।
हरिऔध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कविता में जीवन की संपूर्णता को रचते हैं—केवल सुख या केवल दुःख नहीं, केवल प्रेम या केवल धर्म नहीं बल्कि सब कुछ एक दूसरे में रचता-बुनता चलता है। उनकी कविता में जीवन एक सतत प्रवाह है जो भाषा, स्मृति, प्रेम, संघर्ष और चेतना के जल से बहता है। यह प्रवाह कविता को एक काव्य-गंगा बनाता है जो पाठक के मन को न केवल छूती है बल्कि उसमें गहराई तक उतर जाती है।
उनके काव्य का यह नैतिक और भावनात्मक विस्तार उन्हें अन्य समकालीन कवियों से अलग करता है। वे न तो केवल परंपरा के गायक हैं, न केवल नवजागरण के प्रवक्ता बल्कि वे एक ऐसे काव्य-सेतु के निर्माता हैं जो अतीत और वर्तमान, भाव और विचार, सौंदर्य और धर्म, व्यक्ति और समाज के बीच गहरा संवाद स्थापित करता है। हरिऔध की कविता किसी बाहरी चकाचौंध या आधुनिकता की चपेट में नहीं आती, वह भीतर से जलती हुई लौ है—शांत, स्थिर और उजली।
हरिऔध का साहित्य उस आत्मा की आवाज़ है जो शब्दों में नहीं, अनुभव में बोलती है; जो भाषा के माध्यम से मनुष्य की गहराइयों तक पहुँचती है; जो कविता को केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, एक जीवित नैतिक अनुभव बना देती है। इस अर्थ में, हरिऔध की कविता न केवल पढ़ी जाती है, वह भीतर तक अनुभव की जाती है—जैसे कोई गहरी याद, कोई पुराना स्वप्न, कोई आत्मीय स्पर्श। यही ललित आलोचना की कसौटी पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है—कि वे कविता में जीवन भरते हैं और जीवन को कविता बना देते हैं।
हरिऔध के साहित्य की व्याप्ति उनके समकालीनों के बीच उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती है किंतु उनका महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और काव्यात्मक स्तर पर भी अत्यंत प्रासंगिक है। वे एक ऐसे कवि हैं जो कविता को केवल भाव की अभिव्यक्ति नहीं मानते बल्कि उसे आत्मा के तप से जन्मी एक गहन साधना मानते हैं। उनके काव्य में भारतीय संस्कृति का वह पक्ष उभरता है जो एक ओर कालजयी है, दूसरी ओर परिवर्तनशील जीवन के साथ गहराई से संवाद करता है। वे शब्दों को केवल संप्रेषण का साधन नहीं बनाते, उन्हें आत्मिक ऊर्जा का स्रोत बना देते हैं।
हरिऔध की काव्य-दृष्टि में गहरी समरसता है—समरसता समय के साथ, संस्कृति के साथ, जीवन के अनिवार्य कष्टों और सौंदर्य के साथ। वे न केवल हिंदी को गहराई देते हैं बल्कि उसे एक ऐसी गरिमा और विनम्रता भी प्रदान करते हैं जो केवल अनुभूत कवियों के भाग्य में आती है। उनकी कविता में कहीं कोई शोर नहीं है, कोई लाउडनेस नहीं है, वह जैसे धीमी आवाज़ में कोई अनुभवी ऋषि जीवन के रहस्यों को कह रहा हो—संकोच और संयम के साथ, लेकिन पूरी पारदर्शिता और आत्मविश्वास के साथ।
उनका सौंदर्यबोध, शिल्प और विषयवस्तु इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे न केवल भाषा के सजग रचनाकार हैं, बल्कि विचार के गहन साधक भी हैं। ‘प्रियप्रवास’ में उनके द्वारा प्रयुक्त छंद और गद्यात्मक शैली के बीच का संतुलन यह दिखाता है कि वे केवल छंदशास्त्र के अनुयायी नहीं हैं, वे छंद को भी अपने काव्य के अनुसार ढालते हैं, उसमें स्वभाव भरते हैं। यह केवल छंदों की महारत नहीं, यह छंदों की साधना है।
हरिऔध की काव्य-संवेदना एक प्रकार से भारतीय मानस की प्रतिध्वनि है। वह मानस जो सहिष्णु है, संवेदनशील है और गहराई में जाने को आतुर है। हरिऔध की कविता इस आत्मा की तरह है जो किसी भी समय, किसी भी परिवेश में अपनी सच्चाई के साथ उपस्थित हो सकती है। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिक स्मृति और वर्तमान की बेचैनी साथ-साथ चलती हैं। वे भारतीयता की खोज किसी अतीत की पुनरावृत्ति में नहीं करते बल्कि स्मृति, संवेदना और आत्मिक ताप में करते हैं।
उनकी भाषा में जो माधुर्य है, वह केवल ध्वनि का नहीं, वह आत्मीयता का माधुर्य है। वे भाषा से पाठक को बाँधते नहीं, उसे खोलते हैं—जैसे एक पुराना चित्रपट धीरे-धीरे खुलता हो, और उसमें से जीवन की सुगंध आती हो। उनकी कविता में अनुभवों की सुगंध है—वह सुगंध जो पुरानी मिट्टी से आती है, जो वियोग के आँसुओं में घुलती है, और स्मृति की परतों में उगती है।
हरिऔध का साहित्य इसलिए अमर नहीं कि उन्होंने सुंदर लिखा बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस सुंदरता को रचा जो पीड़ा से निकली है, और जिस पर धर्म, प्रेम, कर्तव्य और संस्कार की छाया है। उनके शब्दों में आत्मा की रोशनी है और आत्मा की रोशनी कभी पुरानी नहीं होती। वह हर युग में नई होती है।
आज जब कविता कई बार अपने स्वरूप, उद्देश्य और दिशा को लेकर उलझी हुई-सी लगती है, तब हरिऔध जैसे कवि की ओर लौटना न केवल एक सौंदर्यात्मक अनुभव है, बल्कि एक नैतिक यात्रा भी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि कविता केवल कहन नहीं है, वह एक आत्मान्वेषण है—एक यात्रा भीतर की ओर।
हरिऔध के साहित्य का महत्व इसीलिए भी है कि वह केवल इतिहास नहीं, वर्तमान की एक आलोचना और भविष्य की एक संभावना है। वे एक पुल हैं—जिस पर खड़े होकर हम अपने अतीत को समझ सकते हैं, और अपने वर्तमान को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। उनका साहित्य किसी एक काल या एक मूल्य का नहीं, वह जीवन के उस शाश्वत मूल्य का साक्ष्य है जो समय के परे होता है—जिसे न कोई रेखा बाँध सकती है, न कोई वाद सीमित कर सकता है।
हरिऔध का साहित्य उस गहरी ललितता का नाम है जो केवल कविता में ही नहीं, जीवन में भी अभिव्यक्त होती है—और इसी कारण वह हमारे समय में भी उतना ही महत्त्वपूर्ण, उतना ही आलोकमय और उतना ही आत्मीय है।
हरिऔध का साहित्य हिंदी काव्य परंपरा में उस शांत, गहन और आत्मीय स्वर की तरह है जो समय के कोलाहल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है—नम्रता से पर अत्यंत प्रभाव के साथ। उनका काव्य किसी आंदोलन या प्रदर्शन का शोर नहीं करता, वह आत्मा के सघन क्षणों को भाषा देता है, अनुभूति को आकार देता है और स्मृति को एक ललित रूप में रचता है। वे कविता को महज़ कलात्मकता नहीं, एक गहरी नैतिकता और आंतरिक सौंदर्य का माध्यम मानते हैं। यही कारण है कि उनके काव्य में शब्द आत्मा की तरह दीप्त होते हैं—संयमित पर उज्जवल।
‘प्रियप्रवास’ जैसे ग्रंथ को पढ़ते हुए यह अनुभव होता है कि कविता केवल पढ़ी नहीं जाती—वह भीतर बहती है, चुपचाप, जैसे कोई पुरानी नदी स्मृतियों के घाटों को छूती हो। हरिऔध का साहित्य उसी बहाव का नाम है—जो एक साथ भावुकता और विचार, परंपरा और नवता, भाषा और आत्मा, सबको समाहित करता है। वे काव्य-शिल्पी हैं पर भाव के भी उतने ही साधक हैं। उनकी कविता में प्रज्ञा और करुणा का अद्भुत संतुलन है जो हिंदी साहित्य को केवल समृद्ध नहीं करता, उसे गहराई भी देता है।
हरिऔध ने हिंदी भाषा को एक नई प्रतिष्ठा दी—एक आत्मगौरव, एक संस्कृति का कंठस्वर और एक वैचारिक आभा। वे उन दुर्लभ रचनाकारों में हैं जिन्होंने परंपरा को बोझ नहीं बनने दिया, उसे एक रचनात्मक संसाधन बनाया। उनकी काव्य-दृष्टि में वह शक्ति है जो समय की परतों को चीरकर आने वाले युगों तक पहुँच सकती है।
हरिऔध का साहित्य केवल एक कवि की उपलब्धि नहीं, वह हिंदी की सांस्कृतिक स्मृति, उसकी रचनात्मक चेतना और उसकी नैतिक ऊँचाई का साक्ष्य है। यह साहित्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची कविता वही है, जो समय से परे जाकर भी आत्मा से जुड़ी रह सके। हरिऔध की रचनाएँ इसी अमरता की संवाहक हैं—शब्दों में बसकर भी, शब्दों से आगे जाती हुई।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.