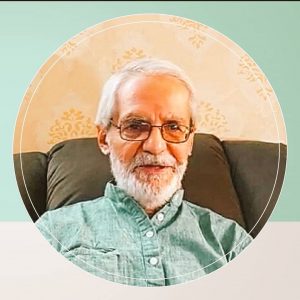— सुरेश पंत —
आज संचार माध्यमों के विभिन्न स्वरूपों- टीवी, अखबार, रेडियो, एफएम इत्यादि- में चुटीली चटपटी, मनोरंजनकारी, बिकने योग्य अर्थात बाज़ारू हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है जो चिन्ता का विषय है। प्रायः मीडिया में पाठक, श्रोता और दर्शक को उपभोक्ता मानकर चलने की प्रवृत्ति देखी जाती है और यह माना जाता है कि उसको जो ‘माल’ परोसा जाए वह चटपटा, रोचक होना चाहिए; जिस रैपर से लपेटा जाए वह घटिया भी हो तो चलेगा। शायद इसी तर्क के आधार पर मीडिया में उपभोक्ताओं को सोचविहीन तथा चिंतनविहीन सामग्री परोसने की प्रवृत्ति बढ़ती गयी है।
समाचार पत्रों की भाषा विशुद्ध साहित्यिक नहीं होती, किंतु वह गली- चौराहे की आमफहम भाषा भी नहीं होती। इन दोनों के बीच में ही कहीं मीडिया की भाषा की स्थिति होनी चाहिए।
माना कि मीडिया साहित्य, आलोचना और चिंतक और सृजनशील साहित्यकारों के गोष्ठीबाज़ संसार से अलग तरह का क्षेत्र है। उसे अपनी अलग भाषा चाहिए किंतु इसका आशय यह नहीं है कि जो सृजनशील साहित्य नहीं है उसमें अंग्रेजी को खुली छूट मिले। एक सीमा तक उसमें अंग्रेजी के आम शब्द आना स्वाभाविक है क्योंकि देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। शिक्षा में, चिकित्सा में, न्यायालयों में और संसद में भी, हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है।
जिसका बोलबाला होता है लोग उसकी नकल करते हैं। किंतु ऐसी भी क्या नकल कि केवल क्रियापद के अतिरिक्त कथित हिंदी वाक्य में सारे शब्द अंग्रेजी के ठूँसे हुए हों। स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त अंग्रेजी और ठूँस-ठूँस कर डाली हुई अंग्रेजी में यही अंतर है और यह अंतर पहचाना जाना चाहिए। मीडिया शायद यह भूल जाता है कि ऐसी हिंदी से लपेटकर परोसी जानेवाली सामग्री के प्रति पाठक में भी अरुचि पैदा होती है।
भाषा का ज्ञान पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है। यह बात जितनी महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में सच और प्रासंगिक थी, उतनी ही आज भी है। आज पत्रकार के सामने विषय विविध हैं, पाठकों की रुचि और बौद्धिक क्षमता भी बहुमुखी है किंतु पत्रकार इनके बीच सहज भाषा का सेतु बनाने की चुनौती को निभा नहीं पा रहे हैं।
परंपरागत मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि भाषा की मर्यादा से किसी तरह का कोई समझौता न हो, उसके लिए इसमें सेवारत पत्रकार एवं लेखक व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गंभीर अध्ययन करते थे ताकि भाषा को लेकर स्थापित मानकों के साथ कोई समझौता न हो।

प्रारंभिक दौर में द्विवेदी युग में पत्रकारिता में सहज, बोलचाल की हिंदी का ही रास्ता था। उस हिंदी की बुनावट में शब्दों को अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पश्तो आदि से भी ऐसे शब्दों को लिया गया जो आम लोगों के दैनिक व्यवहार का हिस्सा थे। पिछली सदी के सातवें-आठवें दशक तक भी आमफ़हम भाषा से आशय यही था कि जो भाषा चाय के ढाबे में, मजदूरों की टोली में, बाज़ार में ख़रीद-बिक्री कर रहे लोगों की समझ में आए और साथ ही साथ पढ़े-लिखे मध्यमवर्ग को भी उससे जुड़ाव महसूस हो। आज स्थितियां बदल गयी हैं। यदि हिंदी को आम लोगों के करीब लाना है तो वह परिष्कृत हिंदी या किताबी हिंदी नहीं हो सकती, जो बोलचाल की हिंदी से अपने को दूर रखती आयी है। मीडिया की बढ़ी ताकत ने उसे एक जिम्मेदारी भी दी है कि नयी पीढ़ी को भाषा के संस्कार भी दे।
पर कुछ अखबार अपनी श्रेष्ठता दिखाने अथवा युवा पाठकों का ख्याल रखने के नाम पर हिंग्लिश परोस रहे हैं और इससे एक नयी किस्म की भाषा जनम रही है जो न तो हिंदी है और न अंग्रेजी है। ये पत्र रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स में अपने अखबार का पंजीयन कराते हैं तो नाम के साथ घोषणापत्र में यह भी बताया जाता है कि यह अखबार किस भाषा में निकलेगा। ये सभी हिंग्लिश प्रेमी अख़बार हिंदी के नाम पर पंजीकृत हैं, द्विभाषी के नाम पर नहीं। फिर भाषाओं के घालमेल का छल क्यों? बहस लंबी हो सकती है। यहाँ हमें तो बस यह कहना है कि संचार माध्यमों में परिष्कृत हिंदी का समर्थक न होने का अर्थ हिंग्लिश जैसी विद्रूप हिंदी का समर्थक होना नहीं है।
मीडिया की भाषा की समस्या केवल अंग्रेजी के अंधाधुंध प्रयोग की समस्या ही नहीं है, उसके कुछ अन्य आयाम भी हैं, जैसे अनुवाद। समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों में दोषपूर्ण अनुवाद के अनेक उदाहरण आसानी से मिल जाते हैं। अनुवाद में सरल, तद्भव और प्रचलित देशज शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दावली के प्रति आग्रह के कारण अख़बारों की भाषा कठिन और बोझिल हो जाती है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के कोशीय अनुवाद ही लेना आवश्यक नहीं है। यदि पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा का अधिक प्रचलित है तो उसे कोशीय अनुवाद से बदला जाना चाहिए।
हिंदी व्याकरण के मनमाने प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। कुछ तो संस्कृत से आए हुए शब्दों की बनावट को न समझने से होते हैं। इन्हें क्षम्य माना जा सकता है किंतु कुछ रिपोर्ट या टिप्पणी लिखने वालों की अपनी नासमझी से भी। कभी अच्छे शब्द भी चल पड़ते हैं तो उन्हें शुद्धता की चासनी में लपेटने के लालच में भ्रष्ट कर दिया जाता है। जैसे डिमॉनेटाइजेशन के लिए नोटबंदी अच्छा शब्द बना था। शुद्धतावादियों ने इसे विमौद्रीकरण विमुद्रीकरण, विमुद्रिकिकरण आदि बना दिया। अब मॉनेटाइजेशन के लिए भी मौद्रिककरण, मुद्रकीकरण मौद्रिकिकरण, मुद्रीकरण आदि चल रहे हैं। इसी प्रकार समाजीकरण- समाजिकीकरण, सशक्तिकरण- सशक्तीकरण आदि का भ्रम भी देखा जाता है। ये उदाहरण केवल एक प्रत्यय ‘-करण’ के प्रयोग को न समझने के हैं। प्रत्यय और भी अनेक हैं और उनसे जन्मने वाली भूलें भी अनेक प्रकार की हैं।
अनुवाद से ही जुड़ी एक अन्य समस्या है दूसरी भाषा के शब्दों (प्रायः नामों) को हिंदी की नागरी लिपि में रूपांतरित करके बोलना या लिखना। इसमें मनमाने प्रयोग देखे जाते हैं। असल में समाचार-एजेंसियों से मूल समाचार अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं और प्रायः उन्हें अंग्रेजी उच्चारण के आधार पर लिपि बदलकर लिख दिया जाता है जो कभी सही होते हैं और कभी नहीं। परिणामस्वरूप निर्मला सीतारमन ‘सीतारमण’ हो जाती हैं, फड़नबीस – ‘फड़ नबिस’, सौरव गांगुली – ‘सौरभ गांगुली’, अर्जन सिंह- ‘अर्जुन सिंह’, सबरी मलै – ‘शबरी मलाई’, जो बाइडन – ‘जो बिडेन’।
ऐसे अनेक उदाहरण प्रायः रोज ही देखने-सुनने को मिलते हैं।
पाना, लेना, देना जैसी सरल क्रियाओं की जगह प्राप्त करना, ग्रहण करना, दान करना जैसे प्रयोगों की क्या आवश्यकता है? रिपोर्ट करने वाले संवाददाता या समाचार संस्था की अप्रतिबद्धता और निर्वैयक्तिकता जताने के लिए भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। पर इसके लिए सदा ‘के द्वारा’ जोड़कर कर्मवाच्य में लिखे गए वाक्य रूखे, उबाऊ और लंबे होते हैं। किए जाने, लिए जाने और दिए जाने जैसे प्रयोग करने पड़ते हैं। मेरा अनुभव है कि ‘के द्वारा’ वाले वाक्य के स्थान पर केवल ‘ने’ वाक्य से काम चल सकता है; जैसे ‘अमुक के द्वारा कहा गया’ के लिए ‘अमुक ने कहा’ पर्याप्त है। मंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जाना है > मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार छोटे और सरल वाक्य बनते हैं।
मुद्दे और भी हैं।