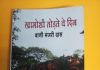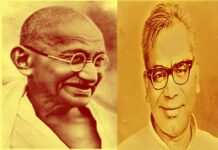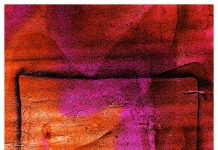— परिचय दास —
।। एक ।।
लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप वह होता है जहाँ प्रतिनिधि और जनता के बीच एक जीवंत, पारदर्शी और सजीव संवाद बना रहता है परंतु आज का यथार्थ इसके एकदम उलट दीख पड़ता है। आज लोकतंत्र एक चुनावी अनुष्ठान तक सीमित होता जा रहा है, जिसमें मतदाता की भूमिका मतदान केंद्र तक पहुँचने और उँगली पर स्याही लगवाने भर की रह गई है। इसके बाद जैसे ही जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है, उसके और जनता के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है—यह दीवार केवल भौगोलिक नहीं, मानसिक, वैचारिक, अनुभवगत और भाषाई भी होती है। वह जनप्रतिनिधि जो कल तक जनता के बीच खड़ा होकर ‘आपका सेवक हूँ’ कह रहा था, वही बाद में भाषाशैली, देहभाषा और विचार की दिशा बदल लेता है। अब उसका शब्दकोश ‘हम’ से ‘मैं’ की ओर, ‘सेवा’ से ‘शासन’ की ओर और ‘जनता’ से ‘व्यवस्था’ की ओर खिसकने लगता है।
इस दूरी के कई कारण हैं और ये केवल राजनीतिक नहीं हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं। लोकतंत्र के पहले चरण में—जब यह प्रणाली भारत में नवागत थी—नेता जनता के बीच से ही निकलते थे, उन्हीं के दुःख-सुख में शामिल होते थे, उन्हीं के त्योहारों में, मृत्यु भोजों में, खेतों में, विद्यालयों में और चौपालों में उनका नियमित आना-जाना रहता था। उनकी राजनीति एक जीवंत अनुभव का परिणाम होती थी परंतु धीरे-धीरे जब राजनीति एक पेशा बन गई, तब इसमें आमजन से कटे हुए, प्रशासन से जुड़े या केवल संगठनात्मक कौशल से ऊपर चढ़े हुए लोग आने लगे। ये लोग जनजीवन के तात्कालिक अनुभवों से वंचित थे और इसलिए जनता की आवाज़ को केवल आँकड़ों, रिपोर्टों या मीडिया की सुर्खियों के ज़रिए समझने लगे।
यह दूरी केवल भौतिक नहीं है। आज के जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए जनता को ‘टाइम’ लेना पड़ता है, ‘प्रोटोकॉल’ का पालन करना पड़ता है और यदि भाग्य अच्छा हो तो किसी बड़े अधिकारी के हस्तक्षेप से प्रतिनिधि एक बैठक में दो मिनट का समय दे देता है। यह दृश्य दर्शाता है कि राजनीति अब प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, लोक से तंत्र की ओर और संवाद से आदेश की ओर बढ़ चली है। यह वही देश है जहाँ कभी एक सांसद पैदल चलकर गाँव-गाँव जाता था, जहाँ मंत्री आमसभा में जनता की शिकायतें सुनता था और जहाँ जनप्रतिनिधि को जनता का ऋणी माना जाता था।
इस दूरी के गहराते जाने का एक बड़ा कारण मीडिया और प्रचार माध्यमों की भूमिका भी है। पहले जो संवाद सीधा जनता और प्रतिनिधि के बीच होता था, अब वह ‘कवरेज’ और ‘इमेज बिल्डिंग’ की प्रक्रिया में बदल गया है। जनप्रतिनिधि अब जनता से मिलने के लिए नहीं, उनके बीच अपनी छवि स्थापित करने के लिए जाता है। वह मंच पर खड़ा होता है, कैमरे के सामने बोलता है, और फिर एक विशिष्ट समूह को संबोधित कर वापस लौट आता है। जनता इस पूरे दृश्य की ‘दर्शक’ बनकर रह जाती है, संवाद की ‘सहभागी’ नहीं। इस परिवर्तन ने राजनीति को ‘नाटकीयता’ से भर दिया है और उसका ‘जन-संवेदनात्मक’ स्वरूप समाप्त कर दिया है।
दूरी का एक और आयाम है—भाषा। प्रतिनिधि की भाषा और जनता की भाषा के बीच अब स्पष्ट अंतर है। पहले नेता गाँव की बोली में बात करता था, अब वह आंकड़ों, योजनाओं और अमूर्त लक्ष्यों की भाषा बोलता है। जनता बेरोजगारी और महँगाई की बात करती है, नेता ‘GDP’ और ‘Ease of Doing Business’ की। इस भाषा का अंतर एक चेतन दूरी को जन्म देता है, जिसमें जनता को लगता है कि जो उसकी बात है, वह प्रतिनिधि की भाषा में है ही नहीं। यह दूरी केवल भाषाई नहीं, वैचारिक भी है, जहाँ जनचिंता का कोई मूल्य नहीं, केवल जनभावना का दोहन होता है।
कुछ लोग इसे ‘राजनीतिक अपरिपक्वता’ कह सकते हैं लेकिन यह एक सुनियोजित प्रवृत्ति का परिणाम है। जब राजनीति में केवल जीतने की कला ही प्रमुख हो जाती है, तब हारने के भय से नेता जनता से दूर भागता है। वह ‘संवाद’ को जोखिम मानता है, क्योंकि संवाद में प्रश्न होते हैं और प्रश्नों में जवाबदेही। आज के जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी सफलता यही मानी जाती है कि वह जनता से बगैर टकराए, उसे अपने पक्ष में बनाए रखे और यह काम प्रचार माध्यमों, सोशल मीडिया और कार्पोरेट जनसंपर्क संस्थाओं की मदद से किया जा रहा है। इस सबके बीच असली जनता खो जाती है, उसकी वास्तविकता एक ‘डेटा’ में तब्दील हो जाती है।
यह दूरी केवल चुनावों तक नहीं सीमित है, यह संसद और विधानसभा के कार्य व्यवहार में भी झलकती है। जनप्रतिनिधियों के बहस में भाग लेने की संख्या लगातार घट रही है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है और लोकहित के विधेयकों पर चर्चा के स्थान पर ‘हंगामा’ और ‘वॉक आउट’ को राजनीतिक मुद्रा बना लिया गया है। जब प्रतिनिधि खुद अपनी संस्था की गरिमा के प्रति लापरवाह हो जाए, तब जनता उससे किस गरिमा की अपेक्षा रखे? इससे वह सोच पैदा होती है कि प्रतिनिधि चुन लेना ही लोकतांत्रिक कर्तव्य की इतिश्री है और प्रतिनिधि भी मान लेता है कि पाँच साल तक वह सवालों से मुक्त है।
।। दो ।।
जिस समाज में प्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व का संबंध केवल ‘सत्ता’ और ‘सामर्थ्य’ के आधार पर देखा जाने लगे, वहाँ यह दूरी अपरिहार्य हो जाती है। भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति उस समय से शुरू हो गई थी जब राजनीति एक आंदोलन नहीं, एक करियर बन गई। स्वतंत्रता संग्राम के समय या उससे कुछ दशकों बाद तक जो नेता जनसंघर्षों से तपकर आए थे, उनकी प्राथमिकता जनसेवा थी—वे राजनीति को ‘कर्मभूमि’ मानते थे। लेकिन बदलते समय के साथ राजनीति में प्रवेश करने के कारण बदलते गए—अब वह सत्ता का रास्ता है, संपर्क और साधन अर्जित करने का एक माध्यम है, एक प्रतिष्ठा और वैभव का मार्ग है। इस बदलाव ने प्रतिनिधियों को ज़मीन से उठाकर मंच पर खड़ा कर दिया—इतना ऊँचा कि वे अब नीचे देख ही नहीं पाते।
यह मनोवैज्ञानिक दूरी अनेक रूपों में सामने आती है। जब कोई जनप्रतिनिधि जनता की शिकायत को ‘नकारात्मकता’ कहकर खारिज कर देता है, तब वह दरअसल उस वास्तविकता से भाग रहा होता है, जिससे वह असहज है।
इस मानसिकता को पोषित करने में सत्ता के केंद्रीकरण ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले विधायक या सांसद भी जनता के लिए सुलभ होता था, अब वह केवल पार्टी नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी हो गया है। जनता की अपेक्षा अब वह पार्टी की नीति, पार्टी फंडिंग और पार्टी छवि के प्रति अधिक चिंतित रहता है। प्रतिनिधित्व की आत्मा, जो जनता की आवाज़ थी, अब संगठन के एजेंडे में समाहित हो गई है। इससे एक नया प्रकार का ‘जन-विमुख प्रतिनिधि’ तैयार हुआ है—जो जनता के नाम पर सत्ता में तो है, पर जनता की बातों से डरता है।
आज का प्रतिनिधि ‘प्रोजेक्ट’ और ‘स्कीम’ की भाषा में सोचता है—उसके लिए गाँव एक ‘डिजिटल ग्राम योजना’ है, स्कूल एक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ है, किसान एक ‘डेटा यूनिट’ है, और बेरोजगार युवा एक ‘उद्यमिता प्रशिक्षण लक्ष्य’ है। जबकि जनता आज भी रोटी, नौकरी, शिक्षा और न्याय की भाषा में जी रही है। यह भाषिक दूरी, जो विकास की नई परिभाषाओं से उपजी है, जनता को अजनबी बना देती है। उसे लगता है कि वह उस राज्य की नागरिक है, जहाँ उसकी ज़रूरतें ‘अतीत’ बन चुकी हैं और नीतियाँ किसी और ‘भविष्य’ के लिए बनाई जा रही हैं।
जनप्रतिनिधि और जनता के बीच यह दूरी लोकतांत्रिक संस्कृति के ह्रास की ओर भी संकेत करती है। नागरिकों का राजनैतिक साक्षरता से कट जाना, पंचायतों और निकायों की उपेक्षा, और राजनीति में विचारधारा की जगह रणनीति का हावी हो जाना, इस दूरी के सामाजिक आधार हैं। जब प्रतिनिधि यह समझता है कि जनता केवल ‘भीड़’ है, जिसे ‘प्रबंधन’ करना है, तब वह संवाद की आवश्यकता नहीं समझता। और जब जनता यह मान लेती है कि प्रतिनिधि ‘अपनों’ में नहीं आता, तो वह भी धीरे-धीरे राजनीति से कटने लगती है—सवाल पूछने छोड़ देती है, भागीदारी से पीछे हट जाती है, केवल मौन दर्शक बन जाती है।
इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह दूरी किसी विशेष समय की उपज नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें सत्ता के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र और संवेदना में परिवर्तन आता गया। रामराज्य के आदर्श में राजा जनसंवाद का आदी था, अशोक ने धम्म लेखों के माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश की थी, अकबर की नवरत्न सभा भी जनता के विविध स्वरों को सुनने का प्रतीक थी। स्वतंत्र भारत में भी जयप्रकाश नारायण या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं में यह लोकसंवेदना स्पष्ट रूप से दिखती थी परंतु समय के साथ संवाद की यह परंपरा एकतरफा वक्तव्यों में बदलती चली गई। अब मंच पर एक व्यक्ति बोलता है और लाखों लोग चुपचाप सुनते हैं—यह संवाद नहीं, ‘प्रसारण’ है।
जनता और प्रतिनिधि के बीच यह दूरी जितनी राजनैतिक है, उतनी ही सांस्कृतिक भी। प्रतिनिधि जिस वर्ग, जिस भाषा, जिस जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करता है, वह अक्सर उस समाज से भिन्न होती है, जहाँ वह चुना जाता है। वह पाँच साल में एक बार उस इलाके में आता है, ‘सरोकार’ का अभिनय करता है और फिर अपने उच्चवर्गीय, नगरीय, नियंत्रित परिवेश में लौट जाता है। इस विसंगति ने ‘प्रतिनिधित्व’ की अवधारणा को खोखला कर दिया है—जनता अब ‘अपना प्रतिनिधि’ चुनती नहीं, केवल ‘कम बुरा’ विकल्प चुनती है। और चुनाव, जो कभी परिवर्तन का अवसर हुआ करता था, अब विवशता का उत्सव बन गया है।
राजनीति में यह दूरी जनतंत्र के मूल उद्देश्य—जनता की भागीदारी—को ही नष्ट करती है। यह भागीदारी केवल मतदान से नहीं आती, यह संवाद, सवाल, आलोचना और संपर्क से आती है। जब इन चारों का लोप होता है, तब प्रतिनिधि नाम मात्र का होता है—वह जनता के बीच नहीं, जनता के ऊपर होता है। और एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ प्रतिनिधि ऊपर और जनता नीचे हो, वह लोकतंत्र नहीं, एक सीमित प्रशासनिक ढाँचा भर रह जाता है, जिसकी आत्मा जा चुकी होती है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.