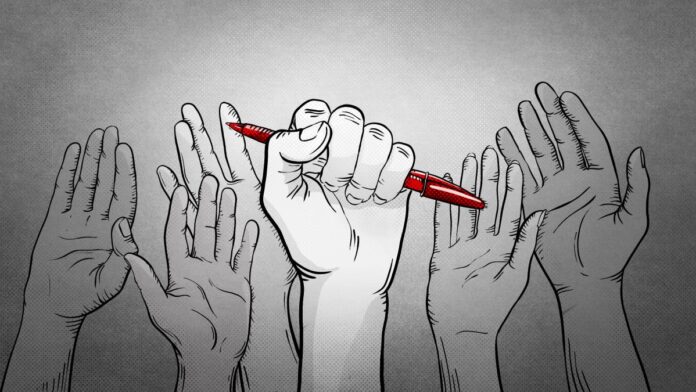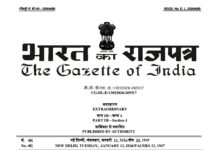— परिचय दास —
जो शब्द नहीं कहे जा सके, वे छपते रहे। जो छप न सके, वे दीवारों पर लिखे गए और जो दीवारों से भी खिसक गए, वे हवाओं में बिखरकर हमारे साँसों में समा गए। किसी युग का सबसे साहसी क्षण वह होता है जब एक अकेला पत्रकार, एक छोटी सी छपाई मशीन, एक निष्पक्ष कलम और एक डगमगाते अक्षर या सोशल मीडिया साथ प्रपंचों के विरुद्ध खड़ा होता है। उसी क्षण से स्वतंत्रता का बीज अंकुरित होता है और उसी क्षण से प्रेस नामक वृक्ष को कुल्हाड़ी की धार सहने की नियति प्राप्त होती है।
प्रेस स्वतंत्रता का अर्थ महज़ एक लेख का छप जाना नहीं होता, न ही किसी नेता की आलोचना करने का मौका मिल जाना ही इसका परचम होता है। यह वह सुगंध है जो हर भोर अखबार के भीगे पन्नों से उठती है; यह वह कंपन है जो किसी टीवी स्टूडियो की चुप्पियों के पीछे मौजूद होती है; यह वह साहस है जो कैमरे के पीछे की आँखों में पलता है और यह वह उत्तरदायित्व है जो हर शब्द, हर विराम चिह्न, हर शीर्षक और हर मौन के भीतर छिपा होता है।
यह दिवस कोई उत्सव नहीं, एक स्मृति है—उन शहीद पत्रकारों की जो कभी किसी टोल नाके पर मार दिए गए, किसी जंगल में लापता हो गए या फिर किसी धूप भरे कमरे में पूछताछ के नाम पर दम तोड़ बैठे। यह उन खबरों की समाधि है जो कागज़ पर आने से पहले ही जला दी गईं और उन कलमों का चिह्न है जो अब भी जेल की अंधेरी कोठरी में किसी ईश्वर की तरह वाणी को खोज रही हैं।
पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है, यह बात बार-बार दुहराई गई, लेकिन रीढ़ झुक भी सकती है, टूट भी सकती है और जब रीढ़ ही लचीली हो जाए तो लोकतंत्र का क़द भी घटता जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता कोई स्वीकृति नहीं, कोई उपहार नहीं—यह जनतांत्रिक संघर्ष का अर्जित अधिकार है, जो न मिलने पर छीन लिया जाता है और जो मिलने के बाद भी सहेजा जाना पड़ता है, हर एक सुबह, हर एक संवाद, हर एक क्लिक, हर एक प्रकाशन के साथ।
आज, जब दुनिया ‘डिजिटल’ हो चुकी है, तब प्रेस की स्वतंत्रता का दायरा भी विस्तृत हुआ है। अब सिर्फ पत्रकार ही नहीं, आम नागरिक भी सूचनाओं के संवाहक बन चुके हैं किंतु इस नवविकसित परिदृश्य में जब ‘फेक न्यूज़’ का अरण्य फैल चुका है, तब सच्ची खबर एक साधना बन गई है—जो मात्र डेटा नहीं, दृष्टि मांगती है; जो सनसनी नहीं, संवेदना से सिक्त होती है।
इस दिवस पर हम उस पारदर्शिता के सामने खड़े हैं, जिसमें हमारे समाज का चेहरा प्रतिबिंबित होता है। यदि प्रेस स्वतंत्र है तो हम अपनी चेतना में भी स्वतंत्र हैं। यदि प्रेस डरता है, तो यह डर धीरे-धीरे हमारी आत्मा को भी सोखने लगता है। यह दिवस उस अलक्षित भय के विरुद्ध प्रतिरोध का उत्सव है जो अखबार की हेडलाइन में नहीं दिखता पर रिपोर्टर के घर लौटने में देर हो जाने से स्पष्ट हो जाता है।
पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, यह एक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में प्रतिदिन सत्य को यज्ञ में आहुति दी जाती है। हर रिपोर्टिंग एक व्रत है—व्रत निष्पक्षता का, व्रत निर्भीकता का, व्रत सत्यनिष्ठा का और जैसे हर व्रत तप मांगता है, वैसे ही पत्रकारिता भी केवल कलम नहीं, कर्म से फलीभूत होती है।
आज, जब हम प्रेस की स्वतंत्रता का स्मरण कर रहे हैं, हमें उन स्वरों की भी सुनवाई करनी चाहिए जो इस ‘स्वतंत्रता’ के बाहर खड़े हैं। वे छोटे गाँवों के संवाददाता, जो बिना किसी संसाधन के, केवल अपने नैतिक साहस पर खबरें लिखते हैं। वे वेब पोर्टल्स, जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जाता है, पर जिनके माध्यम से सच्चाई की असुविधाजनक किरणें हमारे ड्रॉइंग रूम तक पहुँचती हैं।
प्रेस की स्वतंत्रता केवल नीति का विषय नहीं, यह भाषा की, दृष्टि की, और स्वप्न की स्वतंत्रता है। यह विचारों की वह चहचहाहट है जो सत्ता के बंद दरवाजों में डर पैदा कर देती है। यह वह खिड़की है जिससे आम जनता, सत्ता की आलमारी में पड़े सच को देख सकती है।
यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कोई स्थिर अवस्था नहीं, यह एक सतत संघर्ष है। कभी संपादकीय दबाव से, कभी कॉर्पोरेट मालिकान की मुनाफे की आकांक्षा से, कभी सरकार की नीतिगत सेंसरशिप से और कभी जनता की असहिष्णु प्रतिक्रियाओं से इसे बचाकर रखना होता है। यह संघर्ष चुपचाप चलता है, ठीक उसी तरह जैसे एक रिपोर्टर कैमरा बंद कर भी रिकॉर्ड करता है, एक संपादक कट की हुई पंक्तियों को मन में बसा लेता है, एक स्तंभकार अपने निष्कासित लेखों को डायरी में सहेज लेता है।
प्रेस की स्वतंत्रता, एक उजाले की तरह है—जिसे यदि ढक दिया जाए तो अंधकार बढ़ता है, और यदि खुला छोड़ दिया जाए तो आँखें चुभने लगती हैं। इस संतुलन को बनाए रखना ही हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। न तो ऐसा प्रेस जो जनता से डरता हो और न ही ऐसा प्रेस जो जनता को डराए—जरूरत उस पत्रकारिता की है जो आलोचक हो, संवादी हो, संवेदनशील हो और सबसे ज़रूरी—स्वतंत्र हो।
इस दिवस पर यह भी स्मरणीय है कि पत्रकारों को केवल ‘प्रेस कार्ड’ नहीं, ‘सुरक्षा कार्ड’ भी चाहिए। उन्हें न केवल प्रश्न पूछने की आज़ादी मिले बल्कि उत्तरों के पीछा करने की सुरक्षा भी। लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान से नहीं, सवाल पूछने की संस्कृति से आती है और जब तक सवाल पूछने वाले डरते रहेंगे, तब तक जवाब देने वाले और अधिक असंवेदनशील होते जाएँगे।
प्रेस स्वतंत्रता का यह दिवस हमें यह नहीं बताता कि पत्रकार क्या छापें बल्कि यह बताता है कि वे क्या न छाप पाने के लिए बाध्य हैं। यह दिन उनकी कठिनाइयों की परछाईं में खड़ा है और उसी छाया में हमारे भविष्य की रोशनी छिपी है।
जब रात के अंतिम प्रहर में एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप दे रहा होता है जब उसकी आँखों में नींद नहीं बल्कि किसी किसान के आँसू होते हैं, जब उसकी कलम किसी मज़दूर की टूटी हथेली की कहानी कहती है—तो उस क्षण, प्रेस की स्वतंत्रता पूर्ण होती है। क्योंकि तब, पत्रकारिता सिर्फ खबर नहीं रहती—वह करुणा बन जाती है।
परत-दर-परत जब समय का मुखौटा उतरता है तब पत्रकारिता के चेहरे पर सच की झुर्रियाँ साफ़ दिखती हैं। यह झुर्रियाँ उसकी पराजय नहीं, उसकी तपस्या की कथा हैं। शब्दों के संसार में जब मौन भारी हो जाए तब स्वतंत्र पत्रकारिता की एक ही पुकार होती है—सुनो, देखो, कहो… भले तुम्हें कोई सुने या न सुने।
आज भी अनेक छोटे नगरों और बस्तियों में एक अकेला संवाददाता, बिना संपादन विभाग, बिना वेतन, बिना संसाधन, केवल अपने अनुभव और आत्मबल से जनसरोकार की बात लिखता है। वह जानता है कि उसकी खबर शायद प्राइम टाइम में न आए, कोई पुरस्कार न मिले पर वह फिर भी लिखता है—क्योंकि यह उसका कर्म है, उसका धर्म है और शायद वही उसका उत्तराधिकार भी।
प्रेस स्वतंत्रता का अर्थ केवल सत्ता से असहमति नहीं, जनता से संवाद है। वह संवाद जो संसद से अधिक ईमानदार, अदालत से अधिक तत्पर और किसी भी भाषण से अधिक मानवीय हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई पत्रकार किसी आदिवासी अंचल से जल-जंगल-जमीन की रिपोर्ट करता है तो वह इतिहास नहीं, भविष्य लिखता है।
यह भविष्य आसान नहीं होता। हर सच्चे संवाददाता के जीवन में एक लंबा काल होता है—जहाँ वह सरकार से डरता है, मालिक से डरता है, कभी अपने पाठकों से भी डरता है। फिर धीरे-धीरे वह डर ख़ुद में पिघल जाता है, और एक नई तरह की निर्भीकता जन्म लेती है—जिसका स्रोत न समर्थन होता है, न पुरस्कार—केवल अंतरात्मा की ध्वनि होती है।
इस स्वाधीनता का मूल्य केवल पत्रकार नहीं चुकाते—उनके परिजन, उनके मित्र, उनके संपादक, यहाँ तक कि उनके पाठक भी चुकाते हैं। जब कोई रिपोर्टर ग़ायब हो जाता है, तो वह खबर से नहीं, हमारे समाज के ज़मीर से ग़ायब होता है। जब कोई न्यूज़ रूम सेंसरशिप के आगे झुकता है तो केवल खबरें नहीं, हमारी लोकतांत्रिक चेतना भी झुकती है।
आज प्रेस की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा ख़तरा केवल सत्ता से नहीं बल्कि बाज़ार से है। न्यूज़ अब उत्पाद है, और दर्शक ग्राहक। इस समीकरण में सच्चाई अक्सर लाभांश की राह में अवरोध बन जाती है। जब एक चैनल का TRP बढ़ता है, तो हो सकता है, किसी पत्रकार की नैतिक ऊँचाई घट रही हो।
इसी बाज़ार के भीतर कुछ आवाज़ें हैं—जिनकी रिपोर्टिंग में परिश्रम नहीं, एक तीर्थ की तरह पवित्रता होती है। वे किसी चमत्कार की तरह पत्रकारिता की आत्मा को बचाए हुए हैं।
हम आज जब प्रेस की स्वतंत्रता पर विचार करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह स्वतंत्रता कोई एक दिन की बात नहीं। यह हर दिन अर्जित की जाती है, हर घंटे खतरे में रहती है और हर क्षण पुनः परिभाषित होती है।
आज जब तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, जब विमर्श को शोर में दबा दिया जाता है और जब किसी भी असुविधाजनक सच को ‘देशविरोधी’ करार दिया जाता है, तब यह दिवस एक प्रतिरोध का घोष बन जाता है। यह घोषणा करता है कि पत्रकारिता न बिकेगी, न रुकेगी, न झुकेगी।
जो पत्रकार दबे स्वर में सच्चाई कहते हैं, वे भी स्वतंत्रता के सैनिक हैं। जो कैमरे के पीछे का सत्य दिखाते हैं, वे इतिहास के निर्माता हैं। और जो अपने कलम से, हर एक विराम चिह्न से, हर एक असहमति से, यह सिद्ध करते हैं कि जनता का जानना आवश्यक है—वे नायक हैं, भले ही वे बिना नाम, बिना मान, बिना पुरस्कार के चलें।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता दरअसल भाषा की स्वतंत्रता है—और भाषा केवल वाक्य नहीं, वह स्वप्न है, विरोध है, और भविष्य का स्वाभिमान भी। जब एक रिपोर्टर झूठ को पहचानकर उसे खारिज करता है, वह भाषा को नई गरिमा देता है। जब वह कुटिल विमर्श के विरुद्ध सरल सत्य रखता है तो वह संवाद की नयी परंपरा बनाता है।
प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम न केवल पत्रकारों को बल्कि पत्रकारिता की आत्मा को भी समझें। यह आत्मा न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, न किसी ओपिनियन पोल में—यह उस नज़र में होती है जो व्यवस्था के भीतर की दरारें देख पाती है; उस आवाज़ में होती है जो नारे से पहले मनुष्यता को रखती है।
जब एक पुराना पत्रकार, अपने पुराने कैमरे के साथ, किसी धूलभरे गाँव में किसी गुमनाम किसान की आत्महत्या की रिपोर्ट करने निकलता है तब वह दरअसल केवल एक घटना नहीं, एक युग का दस्तावेज़ तैयार कर रहा होता है। वह भविष्य के इतिहास को लिख रहा होता है। वह आज की चुप्पियों में कल के प्रश्नों को उकेर रहा होता है।
यह दिवस उसी आत्मिक पत्रकारिता की स्मृति है। एक गाथा है जो न सुर्खियों में आएगी, न पुरस्कारों में पर जिसे जानना, मानना और संभालना हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.