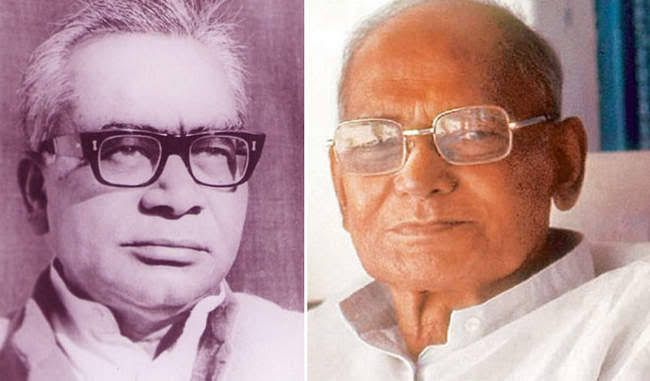— शशि शेखर प्रसाद सिंह —
आजकल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी की निरंतर राजनीतिक सफलता और शक्ति विस्तार से परेशान कुछ राजनीतिक विश्लेषक और प्रगतिशील बुद्धिजीवी इसके लिए समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 के बिहार सहित देश में विद्यार्थी आंदोलन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं जो कई बार बेहद हास्यास्पद लगता है। लोहिया ने 1963 में गैर-कांग्रेसवाद का नारा दिया था और 1967 के लोकसभा के चुनाव तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में गैर -कांग्रेसी दलों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी सहित दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ ने कांग्रेस के खिलाफ सीटों पर तालमेल करके चुनाव लड़ा था और 9 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत न मिलने के कारण इन राज्यों में गैर-कांग्रेसी मिलीजुली सरकारें संयुक्त विधायक दल (संविद) के नाम से बनी थीं।
हालाँकि यह भी सच है कि ये संविद सरकारें अस्थिरता का शिकार हुईं और सरकारें चल नहीं सकीं। लेकिन लोहिया का इस गैर-कांग्रेसवाद की रणनीतिक अवधारणा के पीछे उद्देश्य ये था कि कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के लिए उसे पराजित करना जरूरी है और उसके लिए चुनाव में कुल मतों के बिना स्पष्ट बहुमत के शासन करनेवाली कांग्रेस को विपक्षी मतों के विभाजन को रोक कर हराना आसान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ जब 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकसभा में सीटों की संख्या 283 रह गयी जो 1962 के चुनाव में प्राप्त सीटों की संख्या से काफी कम थी, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, केरल जैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और गैर-कांग्रेसी दलों ने संविद सरकारों का गठन किया। यद्यपि लोहिया की असमय मृत्यु 1967 के चौथी लोकसभा चुनाव के बाद हो गयी और 1969 के कांग्रेस विभाजन के बाद 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे के कारण कांग्रेस(आर) को लोकसभा के साथ- साथ राज्यों में बड़ी सफलता मिली तथा अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। भारतीय जनसंघ पार्टी को 1971 के लोकसभा चुनाव में मात्र 22 सीट मिली और कुल मतों का 7.35 फीसद मत प्राप्त हुआ जो 1967 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 13 सीट कम थी। कांग्रेस (आर) को 352 सीट मिली और उसे 43.68 फीसद मत प्राप्त हुआ।
अतः यह कहना कि लोहिया का गैर-कांग्रेसवाद भारतीय जनसंघ के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक हैसियत के लिए उत्तरदायी था , चुनावी तथ्यों पर आधारित नहीं है।
यह भी कहा जाता है कि बिहार के जेपी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक अंग भारतीय जनसंघ पार्टी को बढ़ने में मदद की। 1973 में गुजरात में कांग्रेस के चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन हुआ और उसके बाद बिहार में कांग्रेस के अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन महंगाई तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रारंभ हो गया। जेपी ने आंदोलनकारी छात्रों के अनुरोध पर आंदोलन का नेतृत्व सम्हाल लिया। इस आंदोलन में अनेक विद्यार्थी तथा युवा संगठनों सहित भारतीय जनसंघ पार्टी की विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी हिस्सा लिया। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून की रात को संविधान के अनुच्छेद 352 का सहारा लेकर आंतरिक गड़बड़ी की आशंका का बहाना बनाकर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के महत्त्वपूर्ण नेताओं तथा आंदोलकारी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर मीसा जैसे काले कानून के अंतर्गत जेल भेज दिया। 19 महीने बाद आपातकाल में ढील देकर इंदिरा गांधी ने 1977 के जनवरी में छठी लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी।
इस समय यह राजनीतिक चर्चा जोर-शोर से होने लगी कि इंदिरा गांधी तथा उनकी पार्टी कांग्रेस (आर) को हराने के लिए सभी गैर-कांग्रेसी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जेपी को लगता था कि इंदिरा गाँधी ने आपातकाल लगाकर नागरिक स्वतंत्रता को छीना था और देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की थी इसलिए देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी गैर-कांग्रेसी दलों को मिलकर एक मजबूत विपक्षी दल बनाना चाहिए और समान चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ना चाहिए तभी देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। उनका यह भी मानना था कि देश के पहले चुनाव से लेकर पांचवें लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को कभी भी कुल मतों का स्पष्ट बहुमत अर्थात 50 फीसद से अधिक मत नहीं मिला है और विपक्षी राष्ट्रीय दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन हो जाता रहा है, परिणामतः कांग्रेस चुनाव जीतती रही है। अतः यदि सभी विपक्षी दल मिलकर एक हो जाएं तो कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन रुक जाएगा और कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। जेपी की यह भी मान्यता थी कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष न होने से निर्वाचित सरकार के अधिनायकवादी होने का खतरा बढ़ जाता है और भारत में आजादी के बाद के प्रथम चुनाव से लेकर अबतक कभी कोई मजबूत विपक्षी दल नहीं रहा है।
जेपी की इस सोच का परिणाम था कि कांग्रेस ( संगठन), भारतीय लोकदल, समाजवादी दल, स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय जनसंघ पार्टी आदि के विलय से एक नई पार्टी जनता पार्टी का गठन हुआ और 1977 के मार्च में संपन्न छठी लोकसभा के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की हार हुई तथा जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में जनता पार्टी की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। निःसंदेह भारतीय जनसंघ के जनता पार्टी में विलय के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक प्रभाव तो बढ़ा और संघ की हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी विचारधारा को माननेवाले सांसदों की संख्या भी बढ़ गयी किंतु ऐसा जनता में आपातकाल के विरुद्ध व्यापक आक्रोश और विपक्षी मतों के एकीकरण के कारण संभव हुआ। उसी वर्ष कई राज्यों की विधानसभाएं भंग कर चुनाव कराए गए तो उन सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें बनीं तथा पूर्व जनसंघ पार्टी के विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई। चार राज्यों में पूर्व जनसंघ पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री भी बनने का अवसर मिला। यद्यपि जनता पार्टी की सरकार आपसी कलह के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और ढाई साल के बाद जनता पार्टी का एक धड़ा गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में पार्टी छोड़ निकल गया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से सरकार का गठन किया।
समाजवादियों ने दोहरी सदस्यता का मामला उठाया
यहाँ यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि जनता पार्टी में टूट का एक महत्त्वपूर्ण कारण दोहरी सदस्यता का मामला भी था। पार्टी के कुछ महत्त्वपूर्ण पूर्व समाजवादी नेताओं मधु लिमये, राजनारायण आदि भारतीय जनसंघ पार्टी के नेताओं के आरएसएस से संबंध को लेकर चिंतित थे और चाहते थे कि सांप्रदायिक संगठन आरएसएस से जनता पार्टी के सदस्यों का कोई संबंध न रहे इसलिए उन्होंने जनता पार्टी में यह मांग उठाई थी कि जो जनता पार्टी के सदस्य हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं रह सकते। इस बात पर पूर्व जनसंघ पार्टी के नेताओं को आपत्ति थी और अंततः जनता पार्टी टूट गयी। 1980 में सातवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ जिसमें बची हुई जनता पार्टी बुरी तरह हार गयी और इंदिरा गाँधी की कांग्रेस को लगभग तीन साल बाद ही दिल्ली की सत्ता में लौटने का अवसर मिल गया। चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व जनसंघ पार्टी के नेता जनता पार्टी को छोड़कर अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी नाम की नई राजनीतिक पार्टी का 1980 के अप्रैल माह में गठन किया।
अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी राजनीतिक दल के प्रभाव और शक्ति में विस्तार का आधार चुनाव में उसकी सफलता और चुनी हुई विधायी संस्थाओं में उसकी संख्यात्मक बढ़ोत्तरी है तो भारतीय जनसंघ पार्टी के नये अवतार भारतीय जनता पार्टी की उसके गठन के बाद उसकी चुनावी सफलता के कारणों का आकलन करने की आवश्यकता है ताकि लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद और जेपी आंदोलन की भूमिका को संघ की दक्षिणपंथी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने के झूठे, तर्कहीन व तथ्यहीन दावे को नकारा जा सके।
भाजपा का गठन
1980 की छठी लोकसभा के आम चुनाव के बाद पूर्व जनसंघ पार्टी के नेताओं ने जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी नवनिर्मित दल भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। वाजपेयी ने जनसंघ से भाजपा को अलग दिखाने के लिए गांधीवादी समाजवाद को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाने की घोषणा की। 1984 के सातवें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा और मात्र दो सीट जीत पायी। वाजपेयी स्वयं चुनाव हार गए। यद्यपि जानकार यह कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी जन सहानुभूति की लहर के कारण लोकसभा में कांग्रेस को अभुतपूर्व सफलता मिली और कांग्रेस 414 सीट जीत गई इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई महत्त्वपूर्ण सफलता नही मिली।
तब प्रश्न उठता है कि आखिरकार कैसे भाजपा आज राजनीतिक रूप से इतनी ताकतवर बन गयी है और 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राजनैतिक सफलता पाती गयी। इतना ही नहीं, आखिरकार तीन बार 1996, 1998 तथा 1999 में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन में अपने बहुमत के बल पर सरकार बनाने में कामयाब हुई!
सच तो यह है कि भाजपा ने 1984 की भारी पराजय के बाद गांधीवादी समाजवाद का रास्ता त्याग दिया और वाजपेयी की जगह अपेक्षातर कट्टरपंथी लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के अध्यक्ष पद की कमान सम्हाल ली। फिर भाजपा ने 1989 के आम चुनाव से सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रक्षामंत्री के रूप में राजीव गांधी की सरकार के समय स्वीडेन की कंपनी से बोफोर्स तोप की खरीददारी में 64 करोड़ के कमीशन लिये जाने का आरोप लगाया था और बाद में सरकार से इस्तीफा दे दिया और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस यद्यपि सबसे बड़ी पार्टी बनी किंतु राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नाटकीय ढंग से नेता चुन लिये गए तथा वामपंथी दलों व भाजपा के बाहरी समर्थन से नेशनल फ्रंट (राष्ट्रीय मोर्चा) की गठबंधन सरकार का गठन किया !
1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 85 सीटें जीतीं। 1991 के लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने 120 सीटें जीतीं तथा 1996 के 11वें लोकसभा चुनाव में 161 सीट लेकर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने किंतु लोकसभा में विश्वास मत में हार गए और तेरह दिन के बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। 1998 में फिर लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में भाजपा 182 सीटें जीत गई और दूसरी बार भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तेरह महीने के बाद फिर अन्ना द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गयी । 1999 के लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और वाजपेयी तीसरी बार एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री बने तथा पहली बार पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
2004 तथा 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर रही किंतु 2014 की 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीतकर पहली बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और 2019 की 17वीं लोकसभा में 300 की संख्या पार कर 303 सीटें जीत लीं। आज भाजपा की कई राज्यों में भी सरकारें हैं।
लोहिया और जेपी पर संघ को स्वीकार्यता दिलाने का झूठा आरोप
क्या भाजपा की इस राजनीतिक सफलता के पीछे लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोई भूमिका रही है?
भाजपा की सफलता में लोहिया और जेपी के योगदान को ढूंढ़ना तर्कसंगत नहीं, बल्कि पूर्वाग्रह प्रेरित है क्योंकि दोनों समाजवादी स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा सदैव सांप्रदायिकता विरोधी रही और दोनों धर्मनिरपेक्षता के प्रबलतम प्रवक्ता रहे। लोकतंत्र और नागरिक अधिकार के लिए आजीवन संघर्षरत और समर्पित रहे।
यही कारण है कि लोहिया कांग्रेस के वर्चस्व को लोकतंत्र के लिए खतरा मानते थे और किसी भी हालत में एक मजबूत विपक्ष को लोकतंत्र की जरूरत मानते थे। दोनों समाजवादी नेताओं ने आजादी मिलने के बाद नेहरू के द्वारा मंत्रिपद के प्रस्ताव को स्वीकार करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को अलग कर भारत में एक मजबूत विपक्ष के निर्माण की सोच के साथ सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और 1952 के पहले चुनावी दंगल में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को चुनौती दी। लोहिया जीवनभर कांग्रेस और नेहरू की गलत नीतियों की कटु आलोचना करते रहे। नेहरू के खिलाफ चुनाव भी यह जानते हुए लड़ा कि वे जीत नही पाएंगे किंतु जनतंत्र में विरोध न होने से अधिनायकवाद का खतरा बढ़ता है।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करने के अद्भुत नैतिक साहस का परिचय दिया। वह कांग्रेस की नीतियों के विरोध और मजबूत विपक्ष की प्रबल राजनीतिक आकांक्षा के कारण गैर-कांग्रेसवाद को समय की राजनीतिक जरूरत समझते थे किंतु सांप्रदायिकता की राजनीति के सदैव कट्टर विरोधी रहे। जेपी देश में कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को रोक कर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते थे और इसलिए कई परस्पर वैचारिक विरोधी दलों के विलय से कांग्रेस विरोधी मतों का एकीकरण अधिनायकवादी इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पराजय के लिए आवश्यक समझते थे। 1977 में इंदिरा गांधी के चुनावी पराजय से तब देश में लोकतंत्र की रक्षा हुई।
ज्ञात रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आजादी के संघर्ष में जेपी, लोहिया जैसे समाजवादियों ने संगठित आंदोलन के लिए वैचारिक भिन्नता के बावजूद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हुए ही आजादी पाने तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को उसके अंतर्गत वैचारिक संगठन के रूप में रखा और आजादी पाने के तुरंत बाद 1948 में कांग्रेस को त्याग कर समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी समाज के निर्माण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए निकल पड़े।
शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना घातक
सच तो यह है कि संघ और भाजपा की राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने में कांग्रेस के गलत फैसले उत्तरदायी रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1985 में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो मुकदमे में दिये गए फैसले को कानून द्वारा बदलने से जहाँ कट्टरपंथी मुसलमानों को बल मिला वहीं संघ और भाजपा जैसी कट्टरपंथी व सांप्रदायिक ताकतों को राजनीतिक लाभ लेने का अवसर। कांग्रेस ने अयोध्या में अदालत में मुकदमा लंबित होने के बावजूद बाबरी मस्जिद-राम मंदिर का द्वार ही नहीं खुलवाया बल्कि वहाँ पूजा की इजाजत दी जिससे संघ और भाजपा को मंदिर के निर्माण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का अवसर मिला। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की वीपी सिंह की सरकार के समय सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा इसी सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी का हिस्सा थी और आगे चलकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की सांप्रदायिक घटना, जिसने अंततः मुस्लिम संप्रदाय में कट्टरपंथी ताकतों को बल दिया, वहीं इसने भाजपा के लिए कट्टरपंथी हिंदुओं को लामबंद करने में उत्प्रेरक का काम किया। आज जबकि भाजपा अत्यधिक शक्तिशाली हो गयी है और विपक्ष में अत्यधिक बिखराव से उसके अधिनायकवादी होने का खतरा बढ़ता जा रहा है तो गैर-कांग्रेसवाद की तर्ज पर गैर-भाजपावाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.