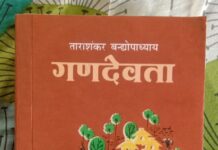— हरिराम मीणा —
बहुत दिनों बाद मेरे हाथों में आदिवासी समाज को लेकर यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक आई है। इस पुस्तक की शुरुआत ‘अधिवास गाथा’ से होती है। आदिवासी लोक में वर्ग, उपवर्ग के आधार पर कोई सामाजिक विभेद, विग्रह और विसंगतियां नहीं रहीं। ‘शासक, नगरसेठ, नौकरशाह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अछूत और अकिंचन जैसे सैकड़ों शहरी विशेषण हैं।’ (पृष्ठ-22) ये सब वर्णवादी समाज में व्याप्त रही हैं, न कि आदिवासी समाज में।
‘एक कुटिल विधायन भारतीय वन अधिनियम के नाम से किया गया। उसमें धीरे धीरे वनों की तरह तरह की परिभाषाएं आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र, आंशिक वन क्षेत्र और बिखरे वन क्षेत्र आदि के नाम होकर वनोत्पादों का मालिकी हक धीरे धीरे सरकार में अंतरित किया जाता रहा। कई अधिनियमों, नियमों, उपनियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के तहत अखंडित चला आ रहा आदिवासी का अधिकार जगह जगह नष्ट करते हुए कुचल दिया गया, जैसे जिस्म के कई अंगों की हड्डियाँ एक के बाद एक कुचल दी जाएँ। आदिवासियों के पुश्तैनी व्याकरण में छूट, कन्सेशन, लाइसेंस, परमिट, अनुमति आदि नए शब्दों को अतिक्रमित करते उनमें अधिकारहीनता, लाचारी, निराशा और लुट जाने का मनोवैज्ञानिक भावबोध इंजेक्ट कर दिया गया।’ (पृष्ठ-25)

आदिवासी के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा जल-जंगल-जमीन का रहता आया है। “सरकारी और प्रशासनिक कुटिलता सियासी सूझबूझ और नागर सभ्यता के नवोन्मेष के प्रहार के कारण आदिवासी इलाकों में भूमि पर सामूहिक अधिकार की पुश्तैनी परंपरा, समझ और चली आ रही मान्यता को दरकिनार कर दिया गया…..भूमि का आदिवासी अर्थ उसके लिए ऐसा क्षेत्र का इलाका है जहां सहकार और सामूहिकता के जरिए ही संपत्ति का बोध उसके सामाजिक अधिकार का एहसास बनकर अंतर्भूत होता रहा है। सरकारी हुक्मनामे के कारण आदिवासी अपनी पुश्तैनी समझ से ही बहिष्कृत कर दिया गया। उसे नहीं समझ आया कि जिस भूमि पर वह कभी-कभार यूं ही या अमूमन हर संभावित स्थिति में भी समाज के अंश के रूप में काश्त करता था, अब भूमि का उतना टुकड़ा उसका खुद का अधिकार कहलाएगा। भूमियों के टुकड़े उसी तरह अलग-अलग आदिवासी बंधुओं को सरकारी गोदनामे के अलग-अलग अभिलेख पट्टे की तरह समझा दिए जाएंगे। उसने यह भी समझा कि उसके साथ ऐसा सलूक किया गया है जो उसके परंपरागत पीढ़ी-दर-पीढ़ी के अनुभवों और (तब तक) उसमें विकसित हुई समझ के आयामों के विस्तार के अस्तित्व में ही नहीं था। यह तो भूस्वामी को एक तरह से खुद की भूमि का नया मुख्तारनामा पाना रचित हुआ। उस कथित स्वामित्व का सीधा रिश्ता सरकार नामक अदृश्य लेकिन हर जगह उपस्थित दमनकारी संस्था से हो गया।” (पृष्ठ-27-28)
बस्तर इलाके में यह कहावत प्रचलित है कि ‘अगर जंगल है तो स्वर्ग है और उसमें जंगलात का गार्ड दिखाई देता है, तो वह नरक बन जाता है।’ जंगल और इंसान के सनातन और आत्मीय संबंधों की परख इस पुस्तक में दिखाई देती है। ‘आदिवासी की वन-ग्रामीण सभ्यता के अर्थशास्त्र में वन स्रोतों और वन उत्पादों का मौद्रिक माध्यम के जरिये आकलन करने का रिवाज या अनुभव नहीं था। राज्य ने उसे मुद्रा के आंकड़ों की अंकगणित में फँसाते आदिवासी जीवन के एहसास को ही एक तरह से विस्थापित कर नियंत्रित और संकुचित कर दिया।’ (पृष्ठ 29)
गैरआदिवासियों द्वारा आदिवासी को अक्सर शराब के आदी के रूप में चित्रित किया जाना एक फैशन सा बनता रहा है। ‘आदिवासी के जीवन में स्वैच्छिक मदिरापान का अपना अनोखा सांस्कृतिक इतिहास और एहसास रहा है। उन्होंने उसे कभी भी उद्योग, व्यापार या सामाजिक दुर्गुण नहीं समझा। महुआ या चावल के माड़ वगैरा से कच्ची शराब बनाकर पीना, पिलाना और अपने परिवार तथा समुदाय के साथ धार्मिक और अन्य मनोरंजन के अवसरों पर प्रथागत उपभोग करना उसका जीवनांश रहा है। उसे शराबखोर या शराबव्यसनी नहीं, लेकिन सांस्कृतिक मदिरा प्रेमी की तरह समझा जाता रहा है। पहले ब्रिटिश और बाद में भारतीय शहरी सभ्यता की कुटिल निगाहों से उसकी यह मासूम प्रथा भी विकृत की जाने लगी। नए मनसबदारों को लगा कि उसके इस कुदरती दुर्गुण या आदत को शहरी सभ्यता के घालमेल और आर्थिक शोषण के जरिये उसकी मजबूरी बना दिया जाए। एक आत्मनिर्भर मदिरा उपभोग की पारंपरिकता को सरकार और व्यवस्था पर निर्भर मदिरापान की नयी साजिश में ढाल दिया जाए।’ (पृष्ठ-31)
दुनिया भर के आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रों और खासकर भारत जैसे देश में भूमंडलीकरण की मुहीम के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर तथाकथित विकास का ढाँचा अख्तियार कर लिया गया। इस प्रवृत्ति को तीन दशक से अधिक का समय हो गया है। विकास का यह मॉडल दरअसल राष्ट्र का समग्र उत्थान नहीं होकर केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित है। इसमें बहुराष्ट्रिक निगमों की भूमिका अहम होती जा रही है।
‘औद्योगिक, खनिज, सिंचाई और विद्युत प्रोजेक्ट आदिवासियों की छातियों पर ही अमूमन उगाये गए हैं, लेकिन ‘दिया तले अँधेरा’ जैसी कहावत को चरितार्थ करते उन प्रकल्पों का सीधा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। अंग्रेजों के बनाये बदनाम भू अर्जन अधिनियम 1884 के तहत स्वेच्छया या जबरिया अर्जित भूमि का इतना कम मुआवजा दिया जाने लगा जो प्रभावित आदिवासी को मजबूर करता कि वह अपने प्रभावित परिवेश से विस्थापित होने पर लगभग मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए खुद ही विकल्प ढूंढ़े। वह अपने परिवार, परिवेश और पुश्तैनी संस्कृति की लाक्षणिकताओं से च्युत होकर किसी उपग्रह की तरह आशंकाओं और अनिश्चितताओं के अंतरिक्ष में उछाला जाता रहा। उसका जीवन बुर्जुआ नौकरशाही की समझ और साम्राज्यवादी उद्योगधर्मिता के चारों ओर चकरघिन्नी की तरह घूमते रहने को मानो प्रतिशोधित किया गया।’ लेखक ने इसी क्रम में ‘सेज़ (एसईजेड) के जरिये उद्योगपतियों द्वारा शासित स्वायत्तशासित ‘मिनी भारत’ के मुद्दे को बखूबी उठाया है। (पृष्ठ-43)
भारत के आदिवासी समाज के उत्थान हेतु चिंतन का इतिहास तलाशा जाए तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जयपालसिंह मुंडा का आता है। लेखक ने इस पुस्तक को जिन विभूतियों को समर्पित किया है, उनमें सबसे पहला नाम उन्हीं का है। संविधान निर्मात्री सभा के एकमात्र मुखर सदस्य जयपालसिंह मुंडा ने कहा है कि ‘हम ही भारत के असली मालिक हैं,….हमारे लोग नस्लवाद, हिन्दुओं उन जैसे बाहरी लोगों के नस्लवाद से पिछले छह हजार वर्षों से उत्पीड़ित हैं,…धरती आदिवासी जीवन का आधार है।” उनके हस्तक्षेप को पुस्तक के ‘संविधान में आदिवासी’ अध्याय में लेखक ने अनेक बार रेखांकित किया है। (पृष्ठ 51 से 141तक) कृति के लेखक तिवारी जी की चिंता आदिवासी लोगों के माध्यम से सम्पूर्ण सर्वहारा की चिंता बन जाती है जब वे लिखते हैं कि “सरकारी वजहों से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और यातायात तथा आवास और रहन-सहन के दो संसार बना दिए गए हैं। एक वर्ग विलासिता को अपना मूल अधिकार मानता है और दूसरे के लिए मूल अधिकारों तक को विलासिता समझा जाता है।” (पृष्ठ-142)
नक्सलवाद पर चिंता करते हुए लेखक का निष्कर्ष है कि ‘नक्सलवाद वहाँ नहीं होता है, जहाँ शासकीय योजनाएँ मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संतोषजनक ढंग से लागू की गयी हैं।’ (पृष्ठ 190) मध्यभारत का सर्वाधिक पिछड़ा इलाका छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ है। ‘4 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे 260 गाँवों की 27 हजार की मुख्यत: मरिया आदिवासियों की आबादी का यह इलाका महसूस ही नहीं कर पाया कि कोई सरकार होती भी है।’ (पृष्ठ 194) यही कारण है कि ‘छत्तीसगढ़ सघन नक्सली हिंसा का प्रदेश हो गया है।’ (पृष्ठ 215)
सर्वमत पर आधारित गणतांत्रिक प्रणाली को आदिवासी समाज के गौरवशाली अतीत का स्वर्णिम अध्याय कहा जा सकता है, जो कहीं न कहीं महात्मा गाँधी के ‘ग्राम स्वराज’ की अवधारणा के निकट दिखाई देती है। इस अवधारणा को बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में एक तरह से सिरे से ही खारिज कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ‘यह कथित ग्रामीण गणतंत्र भारत की बरबादी रहे हैं।’ उन्होंने सदस्यों से मुखातिब होकर पूछा कि ‘गाँव क्या है, सिवाय इसके कि स्थानीय झगड़ों के नाबदान और अज्ञान, संकीर्णता तथा संप्रदायवाद की मांद हैं।’ आंबेडकर का सारा जोर समुदाय के स्थान पर व्यक्ति गरिमा पर था। अर्थात नागरिक पहले है और समुदाय बाद में।
कालांतर में राजीव गांधी ने ग्राम गणतंत्र की महत्ता को समझा और पंचायत प्रणाली को कारगर बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि ‘हम एक शक्तिशाली क्रांति की दहलीज पर हैं। यह एक ऐसी क्रांति है जो लोकतंत्र को करोड़ों भारतीयों के दरवाजे पर लाएगी।’ इसी क्रम में सन 1996 में पंचायत उपबंध अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार- पेसा) कानून लाया गया। इस कानून को लेकर लेखक की धारणा है कि ‘पेसा की भाषा आकर्षक, उदार और बहुआयामी है। ग्राम सभा को अकूत अधिकार किताबी भाषा में दिए गए हैं। लेकिन उनका अनुपालन हो नहीं पाता।’ यही कारण है कि अंग्रेजी हुकूमत की तरह से वही काम ‘ताबड़तोड़ गति से कार्पोरेटी अपराधी सरकारी शह से धड़ल्ले से कर रहे हैं। आदिवासी की भाषा, बोली, संस्कृति, कला, पारंपरिक ज्ञान और उसके जीवन पर शहरी सभ्यों द्वारा हमला किया जा रहा है।
अंग्रेजों के खिलाफ धारदार विद्रोह कर चुके आदिवासियों के इंकलाबी तेवर इतिहास का गौरवपूर्ण हिस्सा हैं। अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण के साथ संचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत, खेती, उद्योग और व्यापार का अभाव जैसी चुनौतियों के चलते आदिवासी सदियों से परंपराओं, रूढ़ियों, रुचियों, लोक आदतों और संगीत तथा आध्यात्मिकता में प्रकृति की आत्मा के एहसास में जीते रहे हैं….अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों पर जिनका कब्जा होता है, वे अपने राजनीतिक आकाओं के स्थानीय एजेंट हो जाते हैं।’ (पृष्ठ-277-278) आदिवासी समाज के लिए पंचायत व्यवस्था की जमीनी हकीकत को ‘नक्कारखाने में तूती का सफ़र’ शीर्षक अध्याय में विस्तार के साथ समझा जा सकता है.
537 पृष्ठीय इस पुस्तक में उपसंहार सहित कुल 11 अध्याय और अंत में 9 परिशिष्ट शामिल किये गए हैं। पूर्वोक्त सामग्री के अतिरिक्त कनक तिवारी जी ने भूमि घोटाले, सलवा जुडूम, विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन, आदिवासी धर्म, वनाधिकार कानून और सर्वोच्च न्यायालय के समता निर्णय, कैलाश एवं अन्य और ओड़िशा खनिज निगम जैसे महत्त्वपूर्ण फैसलों का विवरण दिया है। उन्होंने आदिवासी हितैषी के रूप में काम करने वाले ठक्कर बापा, महाश्वेता देवी एवं अरुंधती राय जैसी हस्तियों की भूमिका का विश्लेषण किया है। बीच में लेखक का संक्षिप्त परिचय यही है कि वे जितना प्रभावित महात्मा गांधी से रहे हैं, उसके साथ भगतसिंह के विचारों से भी। वे पेशे से वकील हैं, साथ ही लेखक, विचारक और अच्छे वक्ता भी। उनका लम्बा अनुभव पत्रकारिता का भी रहा है। उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता इस बात में है कि उनके लिए जितने प्रिय लेखक निर्मल वर्मा रहे हैं उससे कम प्रिय मुक्तिबोध भी नहीं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, संविधान, बस्तर सहित अनेक विषयों पर उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं।
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ‘जंगल की शांति को श्मशान की शांति’ में तब्दील करने की सरकारी और निजी निगमों की साजिशों को उजागर किया है। सन 2020 के बिहार चुनावों से पहले जब वहां के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया तो कैमूर मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधौरा प्रखंड कार्यालय के पास 11 सितंबर को पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़प हुई और गोलियां चलीं। गोलीकांड में तीन प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। सोड़ा-सडकी गांव के रहने वाले बजरंगी अगरिया ने तब कहा था कि ‘इस जंगल में पहले भी बाघ रहते थे, हम भी उनके साथ रहते थे। वनवासी बाघ से डरते नहीं हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमें डर सरकार से है जो हमें हमारे वनाधिकारों से वंचित करना चाहती है। टाइगर सफारी के नाम पर हमें बेदखल करने की साजिश रची जा रही है।’ वनाधिकार के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘प्रकट रूप से इंसान और बाघ में कोई द्वंद्व नहीं है, कम से कम आदिवासियों के साथ तो नहीं।’ (पृष्ठ 535) आदिवासी समाज की त्रासदी को लक्षित करते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि ‘आदिवासी को जंगली बाघ से उतना खतरा नहीं है जितना तथाकथित सभ्य और विकसित मनुष्य से।’ कैफ़ी आज़मी का शेर है –
‘शोर यूँ ही परिंदों ने ना मचाया होगा, ज़रूर कोई शहर से जंगल को आया होगा।’
किताब : आदिवासी उपेक्षा की अंतर्कथा (ब्रिटिश हुकूमत से इक्कीसवीं सदी तक)
लेखक : कनक तिवारी
प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली
कीमत : 350 रु. मात्र
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.