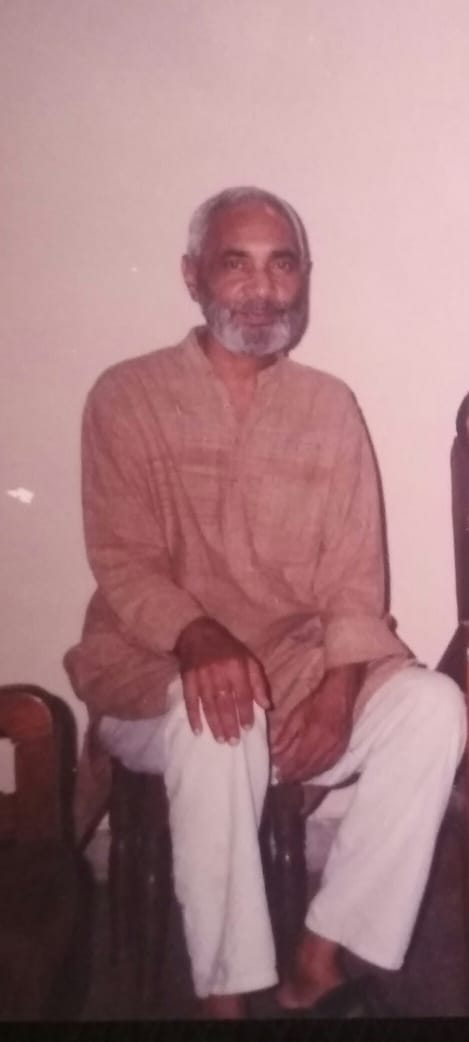— शर्मिला जालान —
प्रेमचंद के नाती (दौहित्र) , अमृतराय के भांजे, साठ के दशक के लेखक प्रबोध कुमार को साल की शुरुआत में याद करना सौभाग्य की बात है। उनके चिंतन, सोच-विचार की दुनिया बहुत बड़ी थी। उन्होंने कई विधाओं में महत्त्वपूर्ण लेखन किया।
कोलकाता (बंगाल) का सफ़र उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। संग-ए मील की हैसियत। समाजवादी और साठ के दशक के लेखक अशोक सेकसरिया से उनकी अभिन्न मित्रता थी। उनके बीच जो संवाद था वह उनके जीवन को विभिन्न स्तरों पर समृद्ध कर रहा था। राजनीति, संस्कृति, साहित्य, नाटक, दर्शन अध्यात्म और खेल-कूद तमाम तरह के विषयों पर उनके पत्र व्यवहार होते थे। अशोक सेकसरिया के निवास स्थल, उनके परिचितों और मित्रो में भी वे गहरी दिलचस्पी रखते थे और वे सभी उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। वहाँ पर लेखक, पत्रकार, प्रकाशक, कवि, चित्रकार, छात्र आदि विविध क्षेत्रों के लोगों से मिलना होता था। ऐसा कहना शायद ग़लत नहीं होगा कि वहीं से एक रास्ता बेबी हालदार द्वारा रचित विश्वविख्यात आत्मकथा ‘आलो आंधारि’ का भी निकला होगा।
प्रबोध कुमार के ऊपर अमृतराय का विशेष प्रभाव था। अमृतराय के मानववाद तथा उनकी तर्कसंगत और सार्वभौम दृष्टि पर उनका विश्वास था। अमृतराय घनघोर कम्युनिस्ट थे। कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट। वह असर जो घर में आ रहा था उसका प्रभाव प्रबोध कुमार पर भी पड़ा। अमृतराय को बांग्ला भाषा से बहुत प्रेम था। वे इतनी अच्छी बांग्ला बोलते थे कि कई लोग उन्हें बांग्लाभाषी समझते थे। उन्होंने बांग्ला सीखी थी। बांग्ला से अनुवाद भी किया था। सत्यजित राय, सुभाष मुखोपाध्याय उनके मित्रों में थे। जो परंपरा अमृतराय के घर में चल रही थी प्रबोध कुमार उससे अछूते नहीं थे। प्रबोध कुमार का भी बांग्ला ज्ञान बहुत अच्छा था। बांग्ला से उन्होंने अनुवाद किया। बेबी हालदार की आत्मकथा- ‘आलो आंधारि’ और ‘ईषत रूपांतरण’, तसलीमा नसरीन की कविताएँ, काजी नज़रुल इस्लाम के भाषणों और कविताओं का बांग्ला से हिन्दी अनुवाद किया। अनुवाद करते समय वे अशोक सेकसरिया से कई शब्दों पर बातें किया करते थे। काजी नज़रुल इस्लाम की भाषा पर मुग्ध हो अशोक सेकसरिया को पत्र लिखा और यह भी बताया कि दिल्ली पुस्तक मेले से कई बांग्ला पुस्तकें और बांग्ला अभिधान (शब्दकोश) ख़रीदा है। अपने पत्रों में रवींद्रनाथ, शरतचंद्र, ताराशंकर बंद्योपाध्याय, विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय, आशापूर्णा देवी का ज़िक्र करते थे। इस तरह उनके बांग्ला प्रेम को हम देख पाते हैं।
अमृतराय की ही तरह प्रबोध कुमार सामाजिक रूप से जागरूक और प्रगतिशील इंसान थे। उनके ढेरों पत्र, पचास से ज़्यादा कहानियाँ, समीक्षा और कई आलेखों का मूल्यांकन किया जाए तो हमें उनकी प्रगतिशील चेतना के बारे में पता चलेगा।
प्रबोध कुमार ने अपनी पत्नी अलित्स्या के देश पोलैंड में कुछ साल गुजारे। ब्रोकला शहर में प्रबोध कुमार का माइकल सोलका-प्रेजिबिलो से परिचय हुआ।
जिनका जन्म 1945 में Lwów, पोलैंड में हुआ था l इनके परिवार को सोवियत संघ द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जातीय संहार के दौरान हटा दिया गया था। उन्होंने ओडेंस विश्वविद्यालय और आरहूस विश्वविद्यालय से 1972-77 में अंग्रेज़ी और तुलनात्मक धर्म में एमए की डिग्री हासिल की। ओडेंस हायर प्रिपरेटरी कोर्स में 1978-2005, सेवानिवृत्त होने तक लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहे। 2008 में नाइट्स क्रॉस ऑफ़ द पीआर ऑर्डर से उन्हें सम्मानित किया गया।

उन दिनों प्रबोध कुमार वहाँ अपना अनुवांशिक अनुसंधान कर रहे थे। माइकल सोलका-प्रेजिबिलो ने ‘लमही’ (प्रबोध कुमार अंक-जनवरी-जून-2022) में प्रकाशित संस्मरणात्मक लेख में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा है।
प्रबोध कुमार को समझने के लिए उनके संस्मरण के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैंl वे ज़िक्र करते हैं कि प्रबोध कुमार के मार्फ़त अशोक सेकसरिया से कोलकाता में मिले और विश्व प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद के पुत्र और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृतराय से भी मिलना हुआ। अशोक सेकसरिया और अमृतराय से उनकी बातचीत भारत के भविष्य को लेकर होती रही। प्रबोध कुमार के प्रगतिशील विचार और अपने देश के भविष्य की चिंता, उनकी सहज नैतिक संवेदना के बारे में अपने संस्मरण में लिखते हैं- ‘प्रबोध से सामाजिक विषयों पर चर्चा होती थी। और मुझे एक वाक्यांश याद आता है जिसमें भारत के मध्य वर्ग के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया था- “जो लोग एक दिन में तीन समय का भोजन पाते हैं वे इस देश में मध्यम वर्ग हैंl” “यह कथन समाजशास्त्रीय पुस्तकों में जो बात कही गई है उससे अधिक कहता है। यह दरअसल, उन दिनों की बात है जब प्रबोध ने पूरी कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में एक आदिवासी जनजाति के, एक गाँव में जाने के लिए आमंत्रित किया था, जो सागर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था।”
“प्रबोध ने अपने भाई प्रमोद की असामयिक मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए परिवार द्वारा स्थापित और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के काम को जारी रखा। इसी ट्रस्ट के निमित्त जिस गाँव का दौरा किया, वह ग्रामीण इलाकों में सबसे पिछड़ा गाँव था। उस गाँव को सुधारने का अभियान शुरू किया। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ थीं जिसके बीच में एक सामूहिक साझा झोपड़ी थी जहाँ ग्रामीणों के उपयोग के लिए किताबों और बर्तनों का संग्रह रख दिया गया था। बीच-बीच में उन्हें निर्देश दिया जाता था कि उनका उपयोग करें पर गाँव वालों की उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रबोध ने यह स्वीकार किया कि यह बहुत दुखद है कि गाँव में कोई उन्नति नहीं हो पाई है। उनकी परिस्थितियाँ इतनी दयनीय थीं फिर भी उनके अंदर आगे बढ़ने की, किसी भी तरह के बदलाव की, विकास और प्रगति की इच्छाशक्ति नहीं थी। गाँव वाले दयालु और मिलनसार थे और अपने उपकारों को पहचानते थे, लेकिन प्रबोध ने स्वीकार किया कि बहुत कम प्रगति हो रही थी। पास के गाँव में जब कोई खेती करता था और लोगों की ज़रूरत होती थी तब ये लोग वहाँ जाते थे और उससे उनका गुजरा चलता था। लेकिन गाँववालों द्वारा कोई भी पहल इस दिशा में नहीं हुई कि, वे बड़े शहर जाएँ या पड़ोस के गाँव में जाकर कोई काम करें। इस ट्रस्ट ने उन्हें ड्रम स्टिक के बीज दिए थे और प्रत्येक झोपड़ी के सामने इसको लगाने की बात कही थी। इससे उनका विकास होता। ड्रमस्टिक पेड़ (सहजन-मोरिंगा) की पत्तियाँ खाने योग्य होती हैं। और उसकी ताज़ा फलियाँ भी स्वादिष्ट होती हैं। उसकी कोपलें, आमतौर पर दांत माँजने के लिए उपयोग में आती हैं, टहनियाँ और ईंधन के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ भी मिलती हैं- ड्रमस्टिक के पेड़ों का रोपण कई समस्याओं का एक जादुई हल था। पर गाँववालों ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रबोध ने उन्हें सोलर-कुकर भी दिखाया जो चावल पकाने का काम करता है, पर गाँव वालों ने उसे भी अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण यह था कि उसमें से धुँआ नहीं निकलता और अगर धुँआ नहीं निकलेगा तो पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा कि उनके यहाँ आज सचमुच भोजन पका है। यह स्थिति काफ़ी हतोत्साहित करने वाली थी और मैं मानता हूँ कि इन सबसे मेरे अंदर क्रोध, आक्रोश और असहायता की भावना ने जन्म लिया था। उनकी उन्नति का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी उपेक्षा किसने की थी? वे किनकी जिम्मेदारी थे? इस बारे में क्या किया जा सकता था, या किया जाना चाहिए था? अब मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभव से कई सामाजिक रूप से जागरूक लोग और कई संस्थाएँ भी गुजरीं होगी और शायद इसी कारण मैंने देखा कि हो सकता है कलकत्ता में श्री अशोक और डॉ अमृत राय भी निराश थे और प्रबोध का उदासीन रवैया भी इसी कारण था। इन लोगों की कौन सहायता करे और कैसे करे! सच्चाई वास्तव में कठिन थी और कौन कैसे मदद कर सकता था? असंख्य वर्जनाओं में जकड़े होने के कारण गाँव वालों के अंदर गतिशीलता और आगे बढ़कर कोई नया क़दम उठाने की क्षमता नहीं थी।”
प्रबोध कुमार स्त्री की स्वतंत्रता और स्वावलंबन की बात करते थे। स्त्री शिक्षा और सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका को लेकर उनके विचार मौलिक और आधुनिक थे। जिस निर्भीकता से उन्होंने बेबी हालदार को आश्रय दिया, प्रेरणा दी और विश्वविख्यात पुस्तक ‘आलो आंधारि’ प्रकाश में आई वह उनके प्रगतिशील विचारों का द्योतक है।
उनका एंथ्रोपोलॉजी पक्ष बहुत प्रबल था। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में उनका काम इस कोटि का था कि एक बार अमृत राय ने बताया कि उनका का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित है। माइकल अपने संस्मरण में भी लिखते हैं-“मुझे प्रबोध के शोध परियोजना के निदेशक के साथ एक रात्रि भोज का निमंत्रण मिला। उनका निदेशक एक स्थानीय व्यक्ति था। उस निमंत्रण के दौरान स्वाभाविक रूप से मैं केवल दो वैज्ञानिकों को उनके अध्ययन के क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हुए सुन रहा था। मुझे यह आभास हुआ कि वे एक महत्त्वपूर्ण स्तर पर-पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातचीत जीव विज्ञान में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार पाने की संभावनाओं को छू रही थी।”
एंथ्रोपोलॉजी से उनकी जो दृष्टि बनी थी उससे वे साहित्य को अपनी तरह से, अलग तरह से गहराई से देखते और परखते थे।
वे जेनेटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल निकालते थे जिसके संपादकीय विभाग में कुछ नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक लोग थे। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक सोसाइटी पंजीकृत करवाई थी। जिसका नाम हिमगिरी था। H I M G I R I. वे शिमला जाते थे। राहुल श्रीवास्तव अपने पिता पर लिखे संस्मरण में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि उनके पिताजी के कई तिब्बती दोस्त थे और वे अपने बच्चों को छुट्टियों में शिमला ले जाते थे।
प्रबोध कुमार जितना अपनी कहानियों, उपन्यास, आलेखों, छोटी-छोटी समीक्षा, एंथ्रोपोलॉजी के शोधपत्र के काम में हैं उतना और उससे ज़्यादा वे अपने पत्रों में हैं। उन्होंने ढेरों पत्र अपने मित्रों, युवा लेखक को लिखें। उनके पत्रों को पढ़ने से उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, साहित्य, राजनीति, खेलकूद, सिनेमा और उनकी विभिन्न अभिरुचियों के बारे में उनके विचार मालूम पड़ते हैं। कहानी को देखने-समझने के नए टूल्स भी उन चिट्ठियों में खोजे जा सकते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान भाषा के क्षेत्र में है।
प्रबोध कुमार की विलक्षण बात यह थी कि वे कई तरह से रचनात्मक जीवन जी रहे थे। उनके बड़े पुत्र राहुल श्रीवास्तव संस्मरण में लिखते हैं कि उनके पिता ने खूबसूरत बिजली के लैंप हाथ से डिजाइन किए जो उनके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अजरा जहांगीर और तसलीमा नासरीन जैसी महिला कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए टी शर्ट डिजाइन किया और उसका उत्पादन किया।
‘लमही’ पत्रिका के संपादक विजय राय ने प्रबोध कुमार पर केंद्रित ‘लमही’ का विशेष अंक पिछले वर्ष निकाला। वहाँ इस बात का उल्लेख है कि प्रबोध कुमार को अपने सेवाकाल में प्रताड़ित और दुखी किया गया। सेवा में उन्हें इतना उत्पीड़ित किया गया कि वह टूट गए। कूट रचना करके उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया गया और पेंशन न दिए जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके शुभचिंतकों के प्रयास से डॉ हरीसिंह ग़ौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में प्रबोध संग्रहालय बनाया गया जिस का सचित्र विवरण ‘लमही’ में दिया गया है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.