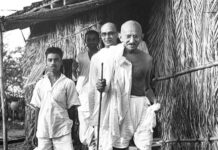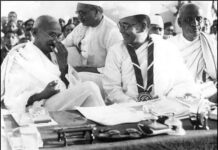(किशन जी चिंतन और कर्म, दोनों स्तरों पर राजनीति में सदाचार, मानवीय मूल्यबोध और आम जन के हित को केंद्र में लाने के लिए सक्रिय रहे। वह मानते थे, जो कि सिर्फ सच का स्वीकार है, कि राजनीति अपरिहार्य है। इसलिए अगर हम वर्तमान राजनीति से त्रस्त हैं तो इससे छुटकारा सिर्फ निंदा करके या राजनीति से दूर जाकर, उससे आँख मूँद कर नहीं मिलेगा, बल्कि हमें इस राजनीति का विकल्प खोजना होगा, गढ़ना होगा। जाहिर है वैकल्पिक राजनीति का दायित्व उठाना होगा, ऐसा दायित्व उठानेवालों की एक समर्पित जमात खड़ी करनी होगी। लेकिन यह पुरुषार्थ तभी व्यावहारिक और टिकाऊ हो पाएगा जब वैकल्पिक राजनीति के वाहकों के जीवन-निर्वाह के बारे में भी समाज सोचे, इस बारे में कोई व्यवस्था बने। दशकों के अपने अनुभव के बाद किशन जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे थे उसे उन्होंने एक लेख में एक प्रस्ताव की तरह पेश किया था। इस पर विचार करना आज और भी जरूरी हो गया है। पेश है उनकी पुण्यतिथि पर उनका वह लेख।)
संविधान के निर्माताओं ने राजनैतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्हें मालूम था कि जिन देशों के संविधानों को आदर्श मानकर वे भारत का संविधान बना रहे थे उन सारे देशों में राजनीति राजनैतिक दलों के द्वारा ही नियंत्रित होती है इसलिए यह बहुत विचित्र और विडंबनापूर्ण लगता है कि राजनैतिक दलों और राजनेताओं के आचरण को मर्यादित करने के तरीकों के बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा है। राजनैतिक दलों को जवाबदेह बनाने की कुछ छिटपुट कोशिश चुनाव आयोग की ओर से हो रही है। लेकिन यह काम चुनाव आयोग के वश का नहीं है।
संविधान में राजनीति और राजनैतिक दलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि हम ‘सफल’ लोकतांत्रिक देशों की नकल कर रहे थे। यूरोप-अमरीका में, जहां लोकतंत्र सफल माना जाता है, वहां कुछ सामाजिक शक्तियों के दबाव से राजनेता मर्यादित रहते हैं। शिक्षा की व्यापकता और जनसाधारण की आर्थिक संपन्नता के चलते वहां जिस प्रकार की सामाजिक शक्तियां हैं उनकी हम नकल नहीं कर सकते। साम्राज्यवादी देशों की एक अन्य विशेषता यह है कि उन्हें अपने देश के बाहर विकासशील देशों में जाकर अंधाधुंध पैसा कमाने तथा अन्य प्रकार के अमर्यादित काम करने का पर्याप्त मौका रहता है। इसलिए उनके अपने देश का नैतिक स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। अगर संविधान बनाते समय इन भिन्नताओं को हम नहीं समझ पाये थे तो बाद के अनुभवों से हमको सावधान हो जाना चाहिए था।
समाजशास्त्र के लिए यह एक शर्म की बात है कि अभी तक राजनीति का अध्ययन करनेवाले समाजशास्त्रियों ने पिछले पचास साल के विकासशील देशों के राजनैतिक अनुभव का कोई गहरा अध्ययन नहीं किया है, जिससे भारत जैसे देशों की राजनैतिक समस्याओं का समाधान हो सके। अध्ययन भी एक प्रकार की निगरानी है। जहां शास्त्र और विश्वविद्यालय अपना काम नहीं करें, वहां राजनीति अधिक स्वेच्छाचारी होती है। तथाकथित सफल लोकतंत्र के देशों में विश्वविद्य़ालय न सिर्फ स्वायत्त हैं, बल्कि स्वाधीन भी हैं। भारत के विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं लेकिन स्वाधीन नहीं हैं। उन पर पराधीनता लादी नहीं गयी है बल्कि वह एक औपनिवेशिक परंपरा है जो बदली नहीं गयी है।
राजनीति पर निगरानी जरूरी है, ‘ब्राह्मणों’ की हो या विश्वविद्यालयों की हो। अखबार या प्रचार माध्यम व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनकी निगरानी सतही और तात्कालिक हो सकती है। व्यवस्था में सुधार का काम बौद्धिक वर्ग का होता है। उनकी निगरानी एक सामाजिक अनिवार्यता होनी चाहिए।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.