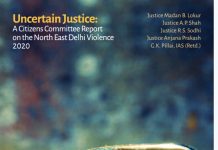— राकेश सिन्हा —
— राकेश सिन्हा —
हमें अपने देश की कृषि को अपनी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से गढ़ना होगा और इसके लिए सबस पहले और सबसे जरूरी है अंग्रेजों के बनाए हुए उस दलदल से निकलना, जिसमें हम अभी तक फँसे हुए हैं। जमीनदारी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में छोटी-छोटी जोतों पर भारी ट्रैक्टर से खेती और वह भी खुद न करके कृषि मजदूरों के दम पर कराना एक तरह की विखंडित कॉरपोरेट खेती है और इस तरह की कृषि व्यवस्था कभी संकट-मुक्त नहीं हो सकती। देश के विकास के साथ सकल उत्पाद में कृषि का हिस्सा और कम होता जाएगा और यह संकट भी बढ़ता जाएगा। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने सत्ता सँभालने के तुरंत बाद कृषि जमीन को जमीनदारों के कब्जे से मुक्त कर, बिना उन्हें कोई मुआवजा दिए, जमीन पर खेती करनेवालों में बाँट दिया था। उस समय शेख का यह शायद अकेला अच्छा प्रगतिवादी कदम था और कश्मीरी समाज को इसका फायदा भी हुआ। लेकिन शेष भारत में यह कदम नहीं उठाया जा सका क्योंकि सत्ता में आया वर्ग कृषि की उस व्यवस्था को नहीं बदलन चाहता था जो देश में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था को मजबूत करती है। लेकिन इस व्यवस्था को और इससे जुड़ी जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना हम भारत में न तो समाज व्यवस्था में और न अपनी आर्थिक स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इन इलाकों में कोई प्रभावी संगठन नहीं बन पाया है और कोई बड़ा किसान आंदोलन भी कभी नहीं हो पाया है। कोरोना काल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ताक पर रख कर केंद्र सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उनके खिलाफ चल रहे किसानों के इतने बड़े आंदोलन में इस क्षेत्र के भूधारी कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं।
पिछले तीन दशकों से सरकार किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन की रही हो, सभी ने ऐसी नीतियां और कानून बनाए हैं जिनसे बेरोजगारी तो लगातार बढ़ी है। आम जनता के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सुविधाओं की उपलब्धता में भी आबादी के हिसाब से वृद्धि नहीं हुई है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवाओं व छात्रों में क्षोभ और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार कॉरपोरेट के बढ़ते दखल के कारण छोटे व्यापारी और दुकानदार परेशान हैं। खेती में घाटे की समस्या तो पूरे देश के किसानों के लिए बनी ही हुई है। लेकिन युवाओं और छात्रों का कोई प्रभावी संगठन नहीं बन पाता और छोटे-छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे किसी तरह के आंदोलन का आधार नहीं बन सकते।
नए कृषि कानूनों को अगर अन्य नीतियों और कानूनों से जोड़कर देखा जाए तो यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि सरकार पूरी आबादी के लिए रोजगार और उसी हिसाब से जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के बजाय कुछ कॉरपोरेट पूंजीपतियों के मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ही काम कर रही है। अब देश की पूरी कृषि व्यवस्था को कॉरपोरेट घरानों के नियंत्रण में देने के लिए बनाए गए काले कानून के विरोध की कमान पंजाब और हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सँभाल ली है और धीरे-धीरे पूरी मजबूती के साथ चल रहे इस आंदोलन के समर्थन में पूरे देश की भावनाएं जुड़ गई हैं। लेकिन हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि जो अर्थव्यवस्था देश में लागू है और जिस दिशा में यह बढ़ रही है उसमें न तो किसानों की समस्या का कोई समाधान है और न युवाओं की बेरोजगारी का। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी इस अर्थव्यवस्था में कोई जगह नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए हम इस सरकार या किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से किसी के पास भी भारत की परिस्थितियों के अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए कोई दृष्टि ही नहीं है।
वर्तमान किसान आंदोलन से बन रही राजनीतिक ऊर्जा ही भारत के भविष्य के लिए आशा की किरण है। इस आंदोलन में छात्रों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को जोड़कर एक अखिल भारतीय स्तर का वृहद आंदोलन ही देश को एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकता है जो देश की पारंपरिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हो।जो संगठन वर्तमान किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें ही इस नए आंदोलन की पहल भी करनी होगी और अगले कुछ वर्षों के लिए इसे सँभालना भी होगा। इस आंदोलन को एक कृषि केंद्रित, ग्राम केंद्रित आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए काम करना होगा। उन्हें ही नई व्यवस्था को मजबूती देने के लिए वर्तमान राजनीतिक दलों के राजनैतिक विकल्प का निर्माण करना होगा और भारत का अपना आधुनिक अर्थशास्त्र भी गढ़ना होगा। नई अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बनाने के पहले हमें कृषि के साथ ही भारत में उद्योगों की स्थिति को भी समझ लेना होगा ताकि पूरी अर्थव्यवस्था के विकल्प पर समग्र रूप से काम किया जा सके।
भारत की आबादी का सत्तर फीसद हिस्सा अब भी गांवों में रहता है और नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में परिवारों में औसतन 4.3 सदस्य हैं। इस प्रकार ग्रामीण आबादी लगभग 95 करोड़ और ग्रामीण परिवारों की संख्या लगभग 22 करोड़ है। इनमें से 10 करोड़ परिवार भूमिहीनों के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की किसान सम्मान योजना के लिए पूरी कोशिश के बाद भी कुल कृषक परिवारों की संख्या 9 करोड़ के करीब ही निकली। क्योंकि इस योजना से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलना था इसलिए इस बात की संभावना कम ही है कि ज्यादा किसान परिवार गिनती से छूट गए होंगे। इसका मतलब एक तरफ तो यह है कि बहुत-से किसान परिवारों का एक से ज्यादा कृषि जोतों पर कब्जा है (कृषि जोतों की कुल संख्या साढ़े चौदह करोड़ है) और दूसरी तरफ यह बात भी आती है कि गांवों में लगभग 3 करोड़ परिवार सीधे खेती से नहीं जुड़े हैं। अगर कुछ जोतों पर लोगों का अवैध कब्जा है तो उनकी पहचान कर हर गांव में अतिरिक्त भूमि का लेखा-जोखा बना लेना चाहिए। भूमिहीन और भूधर किसानों में से खुद खेती करनेवालों की कुल संख्या शायद 15 से 16 करोड़ किसान परिवार की होगी।
भारत में लगभग साढ़े छह लाख गांव हैं और ढाई लाख पंचायतें। कुछ बहुत छोटे गांव हैं जिनकी आबादी पांच सौ से भी कम हो सकती है तो कुछ बहुत बड़े गांव भी हैं जिनकी आबादी दस हजार से ज्यादा है। लेकिन पंचायतों के आकार में ज्यादा एकसमता है और औसतन 3800 की आबादी पर एक पंचायत बनती है। इस तरह एक पंचायत में 850 से 900 परिवार होंगे जिनमें से लगभग 600 परिवार खेती करनेवाले मिल सकते हैं। एक पंचायत में औसतन 600 हेक्टेयर (1500 एकड़ या 2400 बीघा) जमीन होगी। इस प्रकार खेती का काम करनेवाले सब परिवारों के हिस्से में खेती करने के लिए औसतन ढाई एकड़ या चार बीघे जमीन मिल सकती है।
हमें जमीन की एक विशेषता के बारे में ध्यान रखना चाहिए। रिहाइशी जमीन विभाजित होती है लेकिन कृषिभूमि जुड़ती है। कृषिभूमि के सबसे अच्छे और उत्पादक इस्तेमाल के लिए उसकी सिंचाई और जुताई आदि की व्यवस्था एकसाथ होनी चाहिए और इसपर सघन खेती के लिए खेतिहर परिवारों को इसके छोटे-छोटे और लगभग बराबर बराबर हिस्सों पर आपसी सहयोग से मेहनत करनी चाहिए। पंचायत की जमीन पर खेती का काम कराने के लिए सभी परिवारों को एकसाथ जोड़कर एक सहकारी कंपनी बना ली जानी चाहिए जिसका प्रबंधन पंचायत में चुने गए गांव के ही पढ़े-लिखे सुयोग्य व्यक्तियों की समिति की जिम्मेदारी में दे दिया जाना चाहिए लेकिन गांव के लोगों के पास हर साल उनके काम की समीक्षा कर प्रबंधन समिति में बदलाव करने का अधिकार होना चाहिए।
पूरे पंचायत की जमीन के मालिकाना हक का एक रिकार्ड बना लिया जाए और खेती के प्रबंधन के लिए इसे कंपनी के अधीन कर दिया जाए। खेती और गांव के लोगों की जरूरतों के अनुसार कंपनी को गांव की जमीन पर आवश्यकता अनुसार खेत, बगीचे और तालाब आदि बनाने का और गांव के ही लोगों द्वारा खेती कराने का अधिकार होना चाहिए। पंचायत के सारे खेती करनेवाले परिवार मिलकर कितनी जमीन पर किस चीज की फसल उगानी है यह तय कर लें। साल-भर की सभी फसलों के लिए यह बात तय कर ली जानी चाहिए। आपसी सुविधा को देखते हुए पंचायत द्वारा सभी परिवारों को बराबर जमीन खेती के लिए आबंटित कर दी जाए। पंचायत की परिस्थिति के अनुसार अनाज की खेती और सब्जी की खेती के लिए जमीनें अलग-अलग की जा सकती हैं या फिर हर परिवार अपने हिस्से में आई जमीन के एक हिस्से में सब्जी की और बाकी पर अनाज की खेती कर सकता है। फसल के सत्तर प्रतिशत भाग पर खेती करनेवाले का अधिकार होगा और बाकी तीस प्रतिशत को उत्पाद की किस्म के अनुसार अलग-अलग इकट्ठा कर लिया जाएगा और जमीन पर मालिकाना हक रखनेवालों की उनकी जमीन के रकबे के अनुपात में बाँट दिया जाएगा।
जो भूधारी किसान खुद खेती भी करते हैं उन्हें अपनी खेती की जमीन का सत्तर प्रतिशत और मालिकाना हक की जमीन के अनुपात में तीस प्रतिशत का हिस्सा, दोनों मिलेंगे। खेती के खर्चे का बँटवारा भी उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में उपज का हिस्सा मिलता है। यह एक मोटा हिसाब है इसे और व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि कंपनी उत्पादन में हिस्से के स्थान के आधार पर भूस्वामियों को सालाना प्रति एकड़ जमीन पर निर्धारित दर से भुगतान करे और खेती का खर्चा खुद उठाए और खेती के लिए श्रम करनेवालों को मजदूरी दे और फसल पर मूल्य-वर्धन का काम भी कराए। इसपर आगे चर्चा करेंगे।
(बाकी हिस्सा कल )