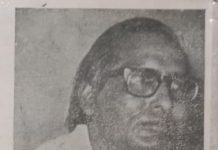— सत्येन्द्र रंजन —
(दूसरी किस्त)
दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीन सरकार ने बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रेरित (या कहें मजबूर) किया है। साथ ही धनी लोगों से ‘साझा समृद्धि’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगदान देने को प्रेरित (या मजबूर) किया है। इस क्रम में अलीबाबा से लेकर टेन्सेंट और ऐसी बहुत सी दूसरी कंपनियों ने अरबों डॉलर की रकम उपलब्ध करायी है।
इसके बावजूद चीन की इस नयी दिशा को लेकर पश्चिमी मीडिया में कयासों का दौर गर्म है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी व्याख्या इस हेडिंग के साथ की है : ‘शी जिनपिंग एम्स टु रेन इन चाइनीज कैपिटलिज्म, ह्यु टु माओज सोशलिस्ट विजन’ (शी जिनपिंग का लक्ष्य माओ की समाजवादी दृष्टि के अनुरूप चीनी पूंजीवाद पर नियंत्रण हासिल करना है)। ‘द इकॉनमिस्ट’ ने कहा- ‘शी जिनपिंग्स असॉल्ट ऑन टेक विल चेंज चाइनाज ट्रैजेक्टरी’ (शी जिनपिंग का टेक्नोलॉजी पर आक्रमण चीन की दिशा बदल देगा)। बीबीसी ने कहा- ‘चेंजिंग चाइना : शी जिनपिंग्स एफर्ट टु रिटर्न टु सोशलिज्म’ (बदलता चीनः शी जिनपिंग की समाजवाद की ओर लौटने की कोशिश)। और ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की हेडिंग रही : ‘द चाइनीज कंट्रोल रिवोल्यूशन : द माओइस्ट इकोज ऑफ शीज पॉवर प्ले’ (चीन में नियंत्रण करने की क्रांति : शी के सत्ता के खेल में माओवादी झलक)।
यह बात पूरे भरोसे से कही जाती है कि जब पश्चिमी मीडिया या बुद्धिजीवी समाजवाद की बात करते हैं, तो वे ऐसा इस विचार की बिना बुनियादी समझ रखते हुए करते हैं। उन्होंने अपने और अपने श्रोता वर्ग के दिमाग में यह धारणा बैठा रखी है कि समाजवाद एक उत्पीड़क व्यवस्था है, जिसमें सबके बीच में गरीबी का बंटवारा किया जाता है। यह बात उनकी समझ के दायरे से बाहर रहती है कि समाजवाद एक आदर्श है और उस आदर्श की दिशा में बढ़ने के कई प्रयोग दुनिया में हुए हैं। उनमें से ही एक प्रयोग अभी चीन में चल रहा है।
न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर झुन शू ने हाल में यह उल्लेखनीय बात कही कि चीन कोई एक ‘फिनिश्ड प्रोडक्ट’ नहीं है। यानी चीन में समाजवाद ठोस रूप ले चुका है, ऐसा नहीं है। ना ही ये सच है कि उसने समाजवाद का रास्ता छोड़ कर पूंजीवाद को अपना लिया है। बीते 70 साल में उसने कई प्रयोग किये हैं। माओ जे दुंग के बाद के काल में जो प्रयोग किया गया, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान मिला। इस कारण अनेक विकृतियां चीनी समाज में आयीं। उनमें सबसे खास अभूतपूर्व गैर-बराबरी और भ्रष्टाचार हैं। लेकिन इस दौर में भी स्कूलों में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ जे दुंग विचार चीन के वैचारिक विमर्श और शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में सर्वोपरि बने रहे हैं। इसलिए वहां स्कूल और कॉलेजों से हर साल लाखों ऐसे छात्र निकलते हैं, जो मार्क्सवाद में दीक्षित होते हैं। उनमें से बहुत-से चीन की दशा-दिशा का मार्क्सवादी नजरिये से विश्लेषण करते रहे हैं। यह वह सामाजिक आधार है, जिसकी अनदेखी चीन की सरकार उस स्थिति में भी नहीं कर सकती, अगर वह दिल से पूंजीवाद और नव-उदारवाद को ग्रहण कर चुकी हो।
यह बात गौरतलब है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे विकासक्रम में माओवाद को कभी अस्वीकार नहीं किया, जिसे चीन के बाहर की दुनिया में समाजवादी या समतावादी दौर समझा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने देंग श्योओ फिंग की मृत्यु के बाद ‘नो टू डिनायल्स’ का सिद्धांत अपनाया था। इसका अर्थ था कि वह न तो माओवादी (यानी समातावादी) दौर को अस्वीकार करती है, और ना देंग की लाइन को, जिसमें गैर-बराबरी और भ्रष्टाचार का जोखिम का उठाते हुए ‘उत्पादक शक्तियों को विकसित होने’ का पूरा अवसर देने की दिशा अपनायी गयी थी।
देंग की दिशा में चीन लगभग ढाई दशक तक दौड़ता रहा। हालांकि इस बीच कई बार ‘कोर्स करेक्शन’ (यानी दिशा में सुधार) किया गया, लेकिन वह बहुत स्पष्ट नहीं था। अलबत्ता 2020 से चीन ने जो कोर्स करेक्शन शुरू किया है, वह सबको दिख रहा है। उसकी ही दुनिया में आज चर्चा है। इसको लेकर पश्चिमी कॉरपोरेट मीडिया ने चीन को चेतावनी दी है कि उसकी नयी दिशा उसे उच्च आर्थिक वृद्धि दर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आविष्कार भावना से वंचित कर देगी। चूंकि कॉरपोरेट मानस यह नहीं समझ पाता है कि जीडीपी की वृद्धि दर और अधिक से अधिक मुनाफा दिलानेवाली तकनीक से अलग और ज्यादा महत्त्वपूर्ण भी जीवन में कुछ हो सकता है, इसलिए उसे यह लगना स्वाभाविक ही है कि चीन ने आत्मविनाश का रास्ता चुन लिया है।
बहरहाल, लोग यह समझते हैं कि समाजवाद एक निरंतर प्रयोग है, जिसकी मूल बात यह होती है कि उसकी नीतियों और अपनाये जानेवाले सामाजिक ढांचों के केंद्र में आम लोग रहते हैं। आर्थिक विकास लोगों के लिए होता है, लोगों की कीमत पर नहीं। चीन ने एक समय धन निर्मित करने की दिशा चुनी, ताकि वह लोगों की गरीबी दूर कर सके और एक समृद्ध समाज बन कर समाजवाद का नया और ऐसा मॉडल पेश कर सके, जो सबको खुली आंखों से भी पूंजीवाद से अधिक आकर्षक दिखे। जैसा कि झुआन शु ने कहा है कि चीन एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए अभी यह कहना ठीक नहीं होगा कि चीन का मॉडल सचमुच सबको अधिक आकर्षक दिखता है। वहां अभिव्यक्ति की आजादी पर नियंत्रण और अपने विचार के अनुरूप संगठित होने की स्वतंत्रता का अभाव ऐसी बातें हैं, जो चीन की व्यवस्था को लगातार कठघरे में खड़ा किये रखती हैं।
लेकिन इस बिंदु पर दो और बातों पर गौर किया जाना चाहिए। चीन ने हाल में डेटा संरक्षण का ऐसा कानून लागू किया है, जिसमें लोगों के निजी डेटा के दुरुपयोग को रोकने की कारगर व्यवस्था की गयी है। जिस दौर में डेटा सबसे अहम पहलू बन कर उभरा है, उसमें लोगों की निजता सुरक्षित करना एक ऐसे अधिकार का संरक्षण है, जिसकी जरूरत आज दुनिया भर में महसूस की जा रही है। लेकिन दुनिया में ऐसे देश अभी कम हैं, जिन्होंने इस दिशा में सार्थक कदम उठाये हों। जबकि चीन ने इस ओर ठोस पहल की है।
दूसरी बात चीन का यह लक्ष्य है कि 2035 तक वह अपने यहां कानून का राज (रूल ऑफ लॉ) स्थापित कर लेगा। सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा के तहत कानून को सबसे ऊपर मानने और उसे सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका का चलन नहीं रहा है। मगर ये समझ मौजूद रही है कि यह ऐसा लक्ष्य है, जिसके बिना समग्र न्याय की व्यवस्था समाज में नहीं हो सकती।
यह बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ऐसे तमाम प्रयोग जोखिम भरे होते हैं। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त (खुलेपन) और पेरेस्त्रोइका (पुनर्रचना) के जो प्रयोग किये, वे आत्मघाती साबित हुए। चीन ऐसे जोखिमों से मुक्त है, यह दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रयोग में सफलता और विफलता की गुंजाइश हमेशा रहती है। कई बार प्रयोग हाथ से निकल जाए, तो वह खतरनाक भी होता है। मगर खास बात यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 72 साल के अपने इतिहास में ऐसे प्रयोगों से कभी गुरेज नहीं किया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सर्वहारा की सांस्कृतिक क्रांति, नियंत्रित आर्थिक सुधार, विकसित उत्पादक शक्तियों को पार्टी में स्थान देने और अब साझा समृद्धि को सुनिश्चित करने की कोशिश ऐसे प्रयोगों की ही मिसाल हैं। समाजवादी आदर्श के साथ कानून का राज कायम करना भी वैसा ही प्रयोग होगा, जैसा अभी तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
इन तमाम प्रयोगों में चीन के कॉलैप्स हो जाने का खतरा है। लेकिन एवरग्रैंड कंपनी के साथ जो हो रहा है, उससे उसका कॉलैप्स होगा, इसकी तनिक भी आशंका नहीं है। हां, जिनकी दबी इच्छा है कि ऐसा हो, वे ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे। आखिर पश्चिमी व्यवस्था में, जहां विमर्श को वित्तीय पूंजीवाद नियंत्रित करता है, ऐसी चर्चाओं की न सिर्फ पूरी आजादी रहती है, बल्कि ऐसी चर्चा करने में ही मीडिया और बुद्धिजीवियों का स्वार्थ भी निहित रहता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.