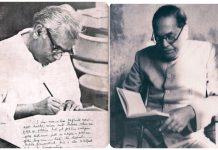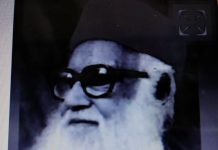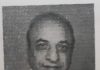— सच्चिदानंद सिन्हा —
जेपी के चरित्र की यह विशेषता थी कि वह अपनी पुरानी मान्यताओं से चिपके नहीं रहते थे। उन्हें यह लगने लगा कि राजनैतिक दलों और यहां तक कि उनके ‘नये चहेते’ सर्वोदय आंदोलन की संभावनाएं चुक गयी हैं और वे समाज–परिवर्तन की दिशा में कुछ कर पाने में अक्षम हैं। ऐसी मनःस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि छात्र-युवा शक्ति समाज-परिवर्तन का एक स्रोत बन सकती है; सो वह उसकी तरफ मुखातिब हुए।
मुखातिब होने का यह अवसर 1974 में आया। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही थी और इसकी भयावहता के प्रति शासकों में चिंता का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह वक्त खाद्य पदार्थों और जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं के विकट अभाव का भी वक्त था। ऊपर से प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार अपनी सारी सीमाएँ लाँघ चुका था और इसके चलते पीड़ित जनता को राहत पहुँचाने का कोई भी प्रयत्न निष्फल हो जाता था। 1973 के अंत में गुजरात के छात्रों में प्रशासन के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के खिलाफ ऐसा क्षोभ पैदा हुआ कि उन्होंने चिमन भाई पटेल मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ दिया। 1974 के फरवरी-मार्च में बिहार के छात्र जीवनयापन के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं के भयावह अभाव के खिलाफ सड़कों पर निकल आए।
जेपी को छात्रों के आक्रोश के एक आंदोलन में परिवर्तित होने की संभावना दिखाई पड़ी। गुजरात का उदाहरण उनके सामने था। उन्होंने कहा भी “गुजरात के छात्रों को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने ऐसी माँगों के लिए संघर्ष छेड़ा जो उनके तात्कालिक हितों के परे जाती थीं और जो सारे देश और सारी जनता की माँगें थीं। गुजरात ने इस तथ्य को एकदम उजागर कर दिया कि वहाँ का मंत्रिमंडल चरम रूप से भ्रष्ट था, उसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था– अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस मंत्रिमंडल को हटाना ही होगा। महँगाई, शिक्षित-अशिक्षित, बेरोजगारी और अभाव को समाप्त करना ही होगा। ये तीनों समस्याएँ सिर्फ गुजरात या उसके छात्रों की नहीं हैं। ये ऐसी बुराइयाँ हैं जो सारे राष्ट्र को सता रही हैं। लेकिन यह पहला अवसर था, जब गुजरात के छात्रों ने इन समस्याओं को उठाया। कुछ देर बाद बिहार के छात्रों ने उनका अनुसरण किया।”
बिहार के छात्र नेताओं के अनुरोध पर जेपी ने उनके आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। राजनैतिक रणनीति के एक उस्ताद के रूप में उन्होंने राजनैतिक भ्रष्टाचार और जनता की समस्याओं के प्रति सरकार और विधायकों की उदासीनता को दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली से जोड़कर देखा। इसलिए मंत्रिमंडल के इस्तीफे की माँग के साथ चुनाव प्रणाली में सुधार और सुधारी गयी प्रणाली के तहत नये चुनावों की माँग की गयी।
चुनाव प्रणाली में सुधार की माँग में ‘प्रतिनिधि वापसी का अधिकार’ एक मुख्य मुद्दा था। जेपी का तर्क यह था कि प्रतिनिधि वापसी का अधिकार यदि मतदाताओं को मिल जाता है तो उससे जनता की समस्याओं के प्रति विधायकों और सरकार की उदासीनता को दूर किया जा सकेगा।
जेपी के साहस और उनकी संगठन-क्षमता ने सारे राज्य में खलबली पैदा कर दी। सारा छात्र समुदाय– स्कूलों और कॉलेजों के छात्र– आंदोलन में किसी न किसी रूप में शामिल हो गया; सड़कों पर उतर आया। विधायकों को इस्तीफा देने को बाध्य करने के लिए उनके घरों पर धरने दिये गये। सरकारी वाहनों और अन्य सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किये। अगस्त के महीने में जब बिहार के बहुत से इलाके बाढ़ की चपेट में थे, तब छात्रों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाने का भी काम किया। ऐसा लगता था कि बिहार में विभिन्न रूप में स्वतःस्फूर्त ढंग से जोश और उत्साह का कोई सोता फूट पड़ा है। बहुत से विधायकों ने इस्तीफा दिया। सरकार दमन पर उतर आयी। पटना में सरकारी प्रतिबंध की अवज्ञा कर एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोग न जा सकें, इसके लिए सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी– गंगा पर पुलिस और अर्धसैनिक टुकड़ियाँ दिन-रात गश्त लगाती रहीं कि लोग नावों से पटना न आ पाएं। इतने सारे भारी बंदोबस्त के बावजूद 4 नवंबर, 1974 को जगह-जगह से हजारों छात्र बिहार की राजधानी में उमड़ पड़े। स्वयं जेपी ने इस प्रदर्शन (मार्च) का नेतृत्व किया। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया जिसमें जेपी को भी चोटें आयीं।
छात्रों और युवों को ऐक्यबद्ध रखने के लिए जेपी ने सारे छात्र और युवा संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के छात्र संगठनों को छोड़ कर अन्य सारे बड़े युवा और छात्र संगठन आंदोलन में शामिल हो गये। जेपी ने आंदोलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष की निरंतरता बनाये रखने के उद्देश्य से छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी के नाम से अपना खुद का भी एक संगठन बनाया। उन्होंने आंदोलन के लक्ष्य को ‘संपूर्ण क्रांति’ के रूप में निरूपित किया। चूंकि संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य को विशद रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, समाज के सभी वर्गों ने उसमें अपनी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित होता महसूस किया। आंदोलन में उन्हें स्वाधीनता और अच्छे भौतिक जीवन की अपनी चाह अभिव्यक्त होती मालूम पड़ी। ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा मोहक था और देखते-देखते वह सारे देश में सुनाई पड़ने लगा– लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करने लगे।
आंदोलन के दौरान जेपी ने समानांतर जन प्रशासन (जनता सरकार) स्थापित करने का भी कार्यक्रम रखा। इसके बारे में ध्यान देने की बात यह है कि 1971 में लेनिन ने रूस में सारी सत्ता सोवियतों को हस्तांतरित किये जाने की माँग की थी। जेपी के समानांतर जन प्रशासन के कार्यक्रम में लेनिन की माँग की अनुगूंज महसूस होती है। लेकिन एक बड़ा फरक यह था कि लेनिन का आंदोलन हिंसक था जबकि जेपी का अहिंसक।
जेपी के समानांतर जन प्रशासन के कार्यक्रम में भी (सोवियतों की तरह) खुद जनता द्वारा गठित कमेटियों को गांव स्तर से विधानसभा स्तर तक अपने हाथों में सत्ता लेने की बात कही गयी थी। लेकिन एक ऐसे समाज में, जिसमें बहुसंख्यक आबादी एक बेडौल भीड़ सरीखी थी, जेपी का समानांतर जन प्रशासन का विचार सिर्फ आंदोलन की सघनता और अवधारणा की अभिव्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि संगठित सामाजिक जीवन की सारी परंपराएं ही समाप्त हो चुकी थीं; परंपराओं को खो डालनेवाले लोगों में कमेटियां बनाने और उनके माध्यम से सत्ता हाथ में लेने की कूवत नहीं रह गयी थी। बहरहाल, इससे प्रशासकीय मशीनरी दमन का औचार बनकर पूरी तरह ठप पड़ गयी।
आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में फैलना शुरू हो गया था लेकिन उसके अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर पाने के पहले ही कुछ ऐसी राजनैतिक घटनाएं हो गयीं, जिन्होंने जेपी के एजेंडे को पूरी तरह बदल डाला। 1975 के जून महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने चुनाव में अनियमितताएं बरतने के अभियोग में दोषी पाकर लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद उन्हें हटाये जाने की माँग जोर पकड़ने लगी। सत्ता से हटाये जाने की संभावना से घबराकर 25 जून की मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। जेपी को मध्य रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया और चंडीगढ़ में तनहा कैद में रखा गया। कैद में उनके दोनों गुर्दे बेकार हो गये और जब सरकार को लगा कि वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच गये हैं तो उन्हें रिहा किया गया।
राजनैतिक सत्ता की वास्तविकता से जेपी का एक बार फिर आमना-सामना हुआ। इंदिरा गांधी को हराने का एकमात्र उपाय यही बच गया था कि लोकसभा के चुनाव में उन्हें पराजित किया जाए। जेपी ने अपने निर्दलीयता के सिद्धांत का परित्याग कर चुनाव में इंदिरा गांधी को चुनौती देने का निश्चय किया। उन्होंने प्रायः उन सारी राजनैतिक पार्टियों को, जो इंदिरा गांधी का विरोध कर रही थीं, अपना अस्तित्व विलीन कर एक नयी पार्टी– जनता पार्टी– बनाने को प्रेरित किया। यह उनके व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नान्डीज, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे किसिम-किसिम के व्यक्तियों को वह एक पार्टी के भीतर ला पाये।
1977 के प्रारंभ में इमरजेंसी को लागू रखते हुए आम चुनाव का ऐलान किया गया तो जनता पार्टी के रूप में एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गयी थी, जो इंदिरा गांधी को पराजित कर सके। जेपी का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ चुका था, पर वह इंदिरा गांधी की तानाशाही को समाप्त कर देश में फिर से लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध थे। एक प्रकार से उन्होंने अपनी मृत्युशैया से राष्ट्र का आह्वान किया कि वह तानाशाही को उखाड़ फेंके। इंदिरा गांधी को पराजित करने और इमरजेंसी को हटाने में उनकी भूमिका अतुलनीय थी।
जेपी एक अथक योद्धा और आदर्शवादी थे। एक बेहतर दुनिया बनाने के उत्साह में उन्होंने कई आंदोलनों में महत भूमिका निभायी। इन आंदोलनों में से अलबत्ता बहुत से या अधिकतर बीच ही में समाप्त हो गये और अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाये। जेपी के प्रयत्न भले ही पूरी तरह सफल न रहे हों लेकिन यह कहना होगा कि उनके प्रयत्नों ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने और देश के लोगों में नागरिक अधिकारों का अहसास पैदा करने की दिशा में बहुत कुछ किया है।
अगर सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने गठन नहीं किया होता तो भारतीय वामपंथ भी अन्य देशों के वामपंथ की तरह सर्वसत्तावादी मार्ग अपना लेता। देशभक्ति के उन्माद के बीच भी नगालैंड और कश्मीर की समस्याओं के बारे में जेपी ने हमेशा उदार और संयत रुख अपनाया। देश में उन्होंने नागरिक अधिकारों के आंदोलन को जन्म दिया; अक्तूबर 1976 में जब देश में नागरिक अधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा था और सरकार दमन पर उतारू थी तब उन्होंने पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज– नागरिक अधिकार रक्षा संघ) की स्थापना की। जेपी ने अपनी असफलताओं से जितना हासिल किया उतना हासिल करने का दावा सफल कहलानेवाले व्यक्ति भी नहीं कर सकते।
(यह लेख पहली बार सामयिक वार्ता के अक्टूबर 2001 के अंक में प्रकाशित हुआ था)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.