- गांधीजी सनातनी हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन डॉ. आंबेडकर के सारे विचार उन्हें मान्य नहीं थे। मसलन उनका कहना था कि विद्वेष के जरिये नहीं, प्रेम और सहानुभूति की भावनाओं और इंसान की अच्छाइयों का आह्वान करके ही इस तरह के सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। 1944 तक गांधीजी के सामाजिक मामलों संबंधी विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। जो गांधीजी शुरू में अंतर्जातीय विवाहों को युक्तिसंगत नहीं मानते थे, उन्होंने अब घोषणा कर दी थी कि मैं केवल उन्हीं विवाहों में वर-वधुओं को आशीर्वाद देने जाऊंगा जहाँ दोनों में से एक हरिजन और दूसरा सवर्ण होगा। यानी अब वे न केवल अंतर्जातीय, बल्कि अंतरधर्मी विवाहों के पक्ष में हो गए थे बशर्ते कि दोनों एक-दूसरे के धर्म के मामले में सहिष्णुता दिखाएं, पत्नी अपने धर्म का पालन करे और पति अपने धर्म का।
भारत की संविधान निर्मात्री परिषद में जब नए संविधान पर चर्चा हुई तो कांग्रेस द्वारा दिए आश्वासनों को मौलिक अधिकारों की सूची में समाविष्ट किया गया। अस्पृश्यता को संविधान की एक धारा द्वारा समाप्त कर दिया गया और कानून के सामने समानता को स्वीकार किया गया। इतना ही नहीं, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर और संरक्षण प्रदान करने के विचार को भी संविधान में मान्यता दी गई। पिछड़े और दलित वर्ग के लिए सार्वजनिक सेवाओं तथा विधानमंडलों में जहां आरक्षण के सिद्धांत को संविधान में स्वीकार किया गया, उसके साथ ही शिक्षण के क्षेत्र में भी इनको प्रश्रय देना तय किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (हरिजन-आदिवासी) की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन-कार्यान्वयन करने के लिए स्थायी अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन की स्थापना की गई। अन्य पिछड़े वर्गों के प्रश्नों पर विचार करने तथा उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने संबंधी सिफारिश करने के लिए भी एक प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया है। काका कालेलकर और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन इसी प्रावधान के तहत गठित हुए थे।
अतः अंत में हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छेड़ी गई थी, वह आज भी जारी है। निःसंदेह आज हरिजन-आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में एक नई चेतना जगी है। उनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन भी आया है। लेकिन गांधीजी और डॉ. आंबेडकर जिस विषमता रहित समाज की कल्पना करने थे, वह अभी तक साकार नहीं हुआ है। इतना ही कि गांधीजी के कारण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ राजनैतिक न रहकर आर्थिक और सामाजिक आंदोलन भी बन गया था। उस समय तिलक पक्ष यदि ‘सामाजिक आंदोलन की बात स्वराज्य प्राप्ति के बाद’ की बात नहीं कहता, बल्कि उसी समय दोनों आंदोलन साथ-साथ चलते और उसी तरह यदि जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगी समाजवादी सिर्फ आर्थिक शोषण की चर्चा में लीन न रहकर सामाजिक विषमता दूर करने के लिए भी संघर्ष करते तो मेरा विचार है कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की गति भी आरंभ से ही तेज रहती। उसके उपरांत भी यह संतोष की बात है कि महात्मा फुले, गांधीजी, डॉ. आंबेडकर, डॉ. लोहिया आदि के प्रयासों से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की कमियां अंशतः ही सही दूर हुईं। डॉ. लोहिया की सप्तक्रांति ऐसे ही विचारों का निचोड़ है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



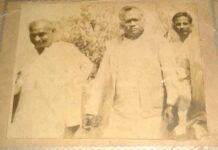








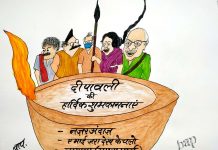


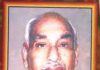

Shaandaar 👍👌👏👏👏