
— कुमार विजय —
मैं मरूंगा तो मुझ पर लिखोगे न !’ समता मार्ग पर सत्यजित राय की जन्मशताब्दी पर लिखे मेरे लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने अचानक पूछा, तो पल भर को सकते में आ गया था।लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, हॉं सर क्यों नहीं, मेरे पास कोई मंच होगा, तो जरूर लिखूंगा। उनका अगला वाक्य था, ‘वैसे भी मैं तो देख नहीं पाऊंगा।’ तकरीबन पंद्रह महीने पहले कुंवरजी अग्रवाल ने जब यह सवाल किया था, तब बात हास-परिहास में कहीं पीछे छूट गयी थी। तब भला किसे पता था कि, यह इतना निकट आसन्न था? बीते मंगलवार को नब्बे की उम्र में उनके निधन के साथ निश्चय ही बनारस के रंगमच का एक युग भी समाप्त हो गया।
आजादी के पहले ही रंगमंच के प्रति उनमें एक रुचि पैदा हो गयी थी। उनका जन्म पटना में तीस के दशक के किसी शुरुआती साल में हुआ था, 31अक्टूबर को वह अपना जन्मदिन मानते-मनाते थे। बचपन उनका बनारस के पुराने मुहल्ले ‘भुतही इमली’ में ननिहाल में बीता था। माध्यमिक शिक्षा हरिश्चंद्र इन्टर कालेज में और उच्च शिक्षा बीएचयू में सम्पन्न हुई थी।
उनके वयस्क जीवन का एक लम्बा समय ‘भारतेन्दु भवन’ के बिलकुल निकट सुड़िया में बीता, जहॉं रहते हुए उन्होंने एक सक्रिय रंग-जीवन जीया था। उन्होंने अपने सात दशक से भी ज्यादा के रंग-जीवन में हिन्दी तथा कन्नड़, मराठी, बांग्ला के ज्यादातर महत्त्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन किया। गिरीश कर्नाड का ‘हयवदन’, विजय तेन्दुलकर का ‘अमीर’, खानोलकर का ‘कालाय तस्मै नमः’, बलवन्त गार्गी का ‘धूनी की आग’, रमेश उपाध्याय का ‘पेपरवेट’, शंकर शेष का ‘अरे मायावी सरोवर’, ‘पोस्टर’, गिरीशचन्द्र घोष के बांग्ला नाटक का बादल सरकार द्वारा रूपांतरित (हिन्दी रूपांतरण : प्रतिभा अग्रवाल) ‘अबू हसन’, ‘जुलूस’, मणि मधुकर का ‘दुलारीबाई’, मौलियर कृत ‘कंजूस’, आदि कुछ ऐसे ही नाटक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतेन्दु के ‘प्रेमजोगिनी’ और एक अपूर्ण नाटक ‘ऐबी-गैबी के साथ अनेक प्रयोग किये।
हालांकि समकालीन हिन्दी रंगजगत के परिदृश्य को लेकर बराबर जिज्ञासु और उससे अवगत भी थे। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें बराबर लगता था कि सही मायनों में आधुनिक हिन्दी रंगमंच का विकास अभी होना शेष है, और इसे लेकर कभी लोक रंगमच तो कभी रामलीला और दूसरे लोक रूपों से उम्मीद बांधते थे। हबीब तनवीर के नया थियेटर और अपने मित्र कारन्त (रा ना वि के पूर्व निदेशक) की प्रस्तुतियों के बाद, वे मणिपुरी के रतन थियम और वामन केंद्रे की प्रस्तुतियों की सराहना करते थे।
कुंवरजी के साथ यह एक संयोग भले रहा हो कि उन्हें ‘भारतेन्दु भवन’ के बिलकुल निकट लम्बे समय तक रहने का अवसर मिला था, बल्कि रंगमंच को लेकर उनकी दृष्टि पर भारतेन्दु और उनके नाटकों का बहुत गहरा प्रभाव था। यह अनायास नहीं था कि हिन्दी के पहले आधुनिक नाटक ‘जानकी मंगल’ (पण्डित शीतला प्रसाद त्रिपाठी लिखित) के बनारस के छावनी क्षेत्र में 3 अप्रैल, 1868 को मंचित होने की जानकारी मिली तभी से कुंवर जी उस स्थल की खोजबीन करने में जुट गये थे और अंततः बंगला नं.25 ‘नाचघर’ (असेंबली रूम्स एंड थियेटर) की खोज कर ली। इस नाटक की दूसरी खासियत थी कि इसमें युवा भारतेन्दु को आकस्मिक रूप से लक्ष्मण की भूमिका करनी पड़ी थी। उल्लेखनीय है कि इसी तिथि और स्थल को आधार बनाकर हिन्दी रंगमंच की जन्मशती 1968 में मनायी गयी। तब से लेकर अभी हाल के वर्षों तक उनका ‘नाचघर’ आना जाना लगातार बना ही रहा। वह बराबर वहां गोष्ठियों और नाट्य प्रयोगों का आयोजन करते रहे थे, जिनमें अलग-अलग दौर में अनेक पीढ़ियों की भागीदारी होती रही थी। इस तरह का संभवत: आखिरी आयोजन 2012 में हुआ था, जिसमें उनपर केन्द्रित रंग सामग्री आधारित पुस्तक ‘काशी के रंग कुंवरजी के संग’ का विमोचन उनके समकालीन, मित्र और कथाकार काशीनाथ सिंह ने किया। पुस्तक का सम्पादन-संयोजन उनकी भतीजी अर्चना अग्रवाल ने किया है।
कुंवरजी एक प्रयोगधर्मी रंग निर्देशक और अभिनेता के साथ-साथ एक बहुश्रुत लेखक और नाट्य चिन्तक भी थे। उन्होंने नाटक और सिनेमा के सौंदर्य शास्त्र पर ढेरों लेख लिखे, जो ‘नटरंग’ और दूसरी महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित हुए और सराहे गए। ‘रंगमंच : एक माध्यम’ रंगमंच को एक माध्यम के रूप में परिभाषित करने वाली उनकी एक महत्त्वपूर्ण किताब है। इसके आलावा ‘नाट्य युग’, ‘आधुनिक नाटक का अन्वेषण’, ‘काशी का रंग-परिवेश’, ‘आधुनिक नाट्य’ आदि पुस्तकें भी हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कई पुस्तकों की सामग्री थी, जिसे स्वास्थ्य की दिक्कतों के चलते अंतिम रूप नहीं दे पाए। सम्भव है कि अर्चना, जो खुद एक लेखिका और हिन्दी की अध्यापिका हैं और उनकी प्रस्तावनाओं से परिचित भी हैं, ऐसी अप्रकाशित सामग्रियों को सम्पादित-प्रकाशित करें।
कुंवरजी एक जिज्ञासु अध्येता के साथ ही एक सजग अध्यापक भी थे। 1994 से कीर्ति जैन के रा.ना.वि.के और बाद में देवेन्द्रराज अंकुर के निर्देशकीय कार्यकाल के दौरान लगभग सात-आठ सालों तक द्वितीय वर्ष के छात्रों को ‘रंगमंच का सौन्दर्यशास्त्र’ पढ़ाने हर वर्ष रा.ना.वि.दिल्ली जाते रहे थे। इसके बहुत पहले वर्षों उन्होंने बीएचयू के ‘दृश्य कला संकाय’ में छात्रों को ‘कला का इतिहास’ भी पढ़ाया था। बाद में उनके पढ़ाये छात्रों में से अनेक यहीं प्रोफेसर और डीन हुए। युवावस्था में उन्होंने हरिश्चंद्र इन्टर कालेज में भी अस्थायी शिक्षक के तौर पर पढ़ाया था।
कुंवरजी की शख्सियत सही मायनों में बहुमुखी है। उनकी रुचियां और उनका विस्तार विस्मित करने वाला था। उनसे किसी भी विषय पर बात की जा सकती थी। बात चाहे साहित्य की हो, दर्शन की हो, मनोविज्ञान की, अध्यात्म की अथवा सिनेमा और संस्कृति की, या फिर पेंटिंग हो या शिल्प, आर्किटेक्चर हो प्रकृति। दरअसल, उन्होंने विविध किस्म का साहित्य विपुलता में पढ़ा था और उनकी स्मृति भी बहुत तीव्र थी।
78-79 में जब पहली बार, कृष्णमोहन मिश्र के बताये हुए मुताबिक उनका घर खोजते हुए, उनके यहॉं पहुंचा था, तब से लेकर बराबर उनका सान्निध्य लाभ मिला। लगभग 43-44 वर्षों के लम्बे दौर में कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई बाहरी हूॅं। कुॅंवर जी सगे तो नहीं थे लेकिन किसी सगे जैसे ही थे। इसलिए उनके बारे में यह आधा-अधूरा लिखना भी कठिन लगता है। मेरे लिए उनकी उपस्थिति फ्रेंड, फिलासफर और गाइड जैसी थी। इस तरह उनकी अनुपस्थिति एक व्यक्तिगत क्षति जैसी भी लगती है। यदि ऐसे और भी लोग हों, तो आश्चर्य नहीं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


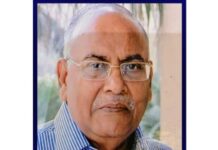












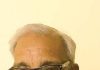

मर्मस्पर्शी स्मृति लेख।आभार,कुमार विजय।कुंवरजी काशी के जिम्मेदार बुद्धिजीवी थे इसलिए सामाजिक तथा राजनैतिक सरोकारों को उन्होंने बखूबी निभाया,रहनुमाई की।
रचना और अभिव्यक्ति की बातें तुलसीघाट पर बैठ कर याद आ सकती हैं उन्हें धता बता कर ‘संस्कृति-रक्षा’ के नाम पर मुष्टिमेय लोगों द्वारा दीपा मेहता की फिल्म ‘वॉटर’ के सेट को तोड़ा-फोड़ा गया, उसी घाट पर । तत्कालीन राज्य सरकार की मदद से दीपा मेहता की टीम को काशी से विदा भी कर दिया गया । इस घटना के तुरन्त बाद बनारस के स्त्री सरोकारों के साझा मंच ‘समन्वय’ की पहल पर कवि,लेखक ,रंगकर्मी तुलसीघाट पर जुटे । नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान कुँवरजी अग्रवाल और कवि ज्ञानेन्द्रपति की इस पहल में भागीदारी उल्लेखनीय थी। ज्ञानेन्द्रपति ने काशी के भजनाश्रमों पर अपनी कविता ‘टेर’ का प्रथम पाठ किया। सती-प्रथा पर रोक के बाद विधवाओं को काशी और वृन्दावन में ऐसे भजनाश्रमों में छोड़ दिया जाता था ।