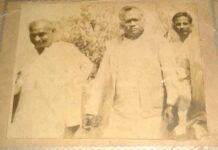— अरुण कुमार त्रिपाठी —
दरअसल डा आंबेडकर कांग्रेस, अंग्रेज सरकार, हिंदूवादी संगठनों और मुस्लिम लीग के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अस्पृश्य वर्ग के लिए सत्ता प्राप्त करने की सौदेबाजी कर रहे थे। उन्हें हिंदू संप्रदाय में सामाजिक परिवर्तन से ज्यादा उम्मीद राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के माध्यम से होने वाले सबलीकरण में थी। लेकिन विडंबना यही थी कि वे सबसे ज्यादा टकराव महात्मा गांधी से ही कर रहे थे और इसीलिए लगता है कि जहाँ गांधी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वहीं बाबासाहेब, गांधी से टकरा रहे थे। शायद इसकी वजह यह भी थी कि गांधी पूरे भारतीय समाज पर अपने नेतृत्व का दावा करते थे और आंबेडकर उस दावे को चुनौती दे रहे थे। सौदेबाजी के इसी प्रयास में आंबेडकर ने गांधी को पत्र लिखा, “अगर भारतीय राजनीतिक ध्येय प्राप्त करना है तो हिंदू-मुस्लिम समस्या के निर्णय के साथ-साथ स्पृश्य-अस्पृश्य का निर्णय करना भी आवश्यक है। जिन मुद्दों का निर्णय करना है उसे प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं।’’ लेकिन तब तक महात्मा गांधी डा आंबेडकर से सतर्क हो चुके थे या वे जितने प्रकार की चुनौतियों से घिरे थे उसमें वे एक और चुनौती नहीं उठाना चाहते थे। क्योंकि उनके सामने जिन्ना की चुनौती, ब्रिटिश साम्राज्य की चुनौती और हिंदूवादी संगठनों की चुनौती मुँह बाए खड़ी थी। छह अगस्त 1944 को गांधी ने आंबेडकर को जवाब दिया, “दलित वर्ग की समस्या धार्मिक और सामाजिक है। मुझे आपके कर्तव्य की पूरी जानकारी है। आप जैसा व्यक्ति अगर मेरा सहयोगी बने तो मुझे प्रसन्नता होगी। तथापि इस महत्त्व की समस्या के बारे में आपके मतभेद हैं, यह एक बार बड़ी कीमत देने की वजह से मुझे मालूम हुआ है।’’(डा बाबासाहेब आंबेडकर : जीवन चरित— धनंजय कीर)
यह एक तरीका था जिसके चलते गांधी, आंबेडकर से किसी तरह का टकराव लेने से बचना चाहते थे। आजादी के बारे में दोनों नेताओं की अलग अलग राय थी और वह आंबेडकर के कलकत्ता में दिए बयान से जाहिर होती है। डा आंबेडकर ने कहा, “नए संविधान के अनुसार हिंदुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा। विश्वयुद्ध खत्म होगा और सफलता दिखाई पड़ रही है। फिर भी आप सब संगठित रहें। वायसराय ने एक अच्छी बात की है कि उन्होंने गांधीजी से यह कहा है कि भारत में सत्ता हस्तांतरण होने से पहले हिंदुओं, मुसलमानों और अस्पृश्यों तीनों में समझौता होना चाहिए। अगर हिंदू महासभा ने हमारी माँगें स्वीकार कीं तो हम हिंदू महासभा से मिल जाएंगे और कांग्रेस ने स्वीकार कीं तो कांग्रेस से।’’
डा आंबेडकर की इस सौदेबाजी से हिंदू महासभा विशेष रूप से उत्साहित थी। वह चाहती थी कि डा आंबेडकर कांग्रेस की बजाय उसके साथ आ जाएँ। इसीलिए डा मुंजे ने आंबेडकर को पत्र लिखकर उनकी माँगों के बारे में पूछा लेकिन आंबेडकर ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। इस बीच डा आंबेडकर पर देशहित के साथ दगा करने का आरोप भी लग रहा था। इसके जवाब में उन्होंने कहा, “अस्पृश्य वर्ग समाज का एक अलग अंग है। भारत की स्वतंत्रता पर उसकी भक्ति अन्यों से तनिक कम नहीं है। लेकिन उसे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के साथ अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए।’’ एक जगह उन्होंने श्रीनिवास शास्त्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “मेरे सार्वजनिक जीवन के इतिहास में मेरे हाथों कोई कलंकित काम नहीं हुआ है।…..भारत को अगर किसी ने दगा दिया हो तो वह अस्पृश्य वर्ग से नहीं बल्कि गांधी, शास्त्री आदि लोगों ने।’’
डा आंबेडकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। वही पूर्ण स्वतंत्रता जिसकी प्राप्ति की घोषणा कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर तिरंगा फहराते हुए की थी। डा आंबेडकर डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे। यह माँग कांग्रेस ने 1908 में की थी जिसे देने के लिए अंग्रेजी राज तैयार नहीं हुआ था। आंबेडकर ने 20 मई 1945 को बंबई में एक भाषण में कहा, “हिंदुस्तान स्वतंत्रता की अपेक्षा औपनिवेशिक स्वराज्य(डोमिनियन स्टेटस) स्वीकार करे। भारतीय लोगों से स्वतंत्रता की रक्षा करना संभव शायद नहीं है इसलिए वे औपनिवेशिक स्वराज पसंद करें। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता ही है।’’ औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब कनाडा जैसे देशों की उस स्थिति से था जिसमें आंतरिक मामलों की देखभाल देशी लोगों को करना था और बाहरी मामलों का नियंत्रण साम्राज्य के हाथ में रहना था। उनके इसी विचार को कांग्रेस के लोग नापसंद करते थे।
इसी मतभेद के चलते डा आंबेडकर ने गांधीजी और कांग्रेस पर जून 1945 में धमाकेदार प्रहार किया। उनकी एक मशहूर किताब है `व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स’(कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के साथ क्या किया)। ध्यान देने की बात है कि इस किताब में गांधी के नाम के साथ जी बाद में जोड़ा गया है पहले गांधी ही था। उस किताब का संक्षिप्त वर्णन करते हुए धनंजय कीर लिखते हैं, “यह ग्रंथ वाद विवाद के त्वेष से भरा हुआ है। शैली जोशीली और प्रभावशाली है। जानकारी और मुद्दे आँकड़ों और विश्वास पैदा करनेवाली बातों से परिपूर्ण हैं।……..इस ग्रंथ का प्रमुख मुद्दा यह था कि कांग्रेस ने 1917 से अस्पृश्यों के उद्धार का काम शुरू किया। यह कांग्रेस कार्यसमिति के कार्यों में से एक था। कांग्रेस का प्रयोजन अस्पृश्यों की दुर्बलता प्रत्यक्षतः नष्ट करने की बजाय यह करना था कि वे राष्ट्रीय जीवन से अलग घटक न दिखाई दें। इस ग्रंथ में आंबेडकर ने गांधी के हरिजन कार्य की आलोचना की है तो स्वामी श्रद्धानंद का गौरवपरक उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि श्रद्धानंद अस्पृश्यों के महान हिमायती थे।….आंबेडकर ने यह भी इशारा किया है कि अस्पृश्य वर्ग गांधीजी और गांधीवाद से सचेत रहे।’’ इस ग्रंथ में आंबेडकर ने अछूतोद्धार के लिए जुटाए गए चंदे में भ्रष्टाचार और हरिजन सेवक संघ के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगाया।
आंबेडकर के मतानुसार गांधीवाद और कुछ नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन का पुनरुज्जीवन, निसर्ग की ओर वापस लौटने, जानवरों जैसा जीवन बिताने और आधुनिक यंत्रयुगीन मानव के लिए एक अभिशाप है। कांग्रेस और गांधी के प्रति आंबेडकर की आलोचना का तेवर कमजोर पड़ने की बजाय तेज ही होता जा रहा था। लेकिन गांधी अब उनसे सीधे टकराने से कतराते थे। शायद उन्हें लग रहा था कि जातिव्यवस्था ने आंबेडकर को कटु बना दिया है और कांग्रेस का संगठन और नेतृत्व अस्पृश्यता और जाति को मिटाने की बजाय उसे ढकने को कोशिश कर रहा है। साथ ही कांग्रेस अस्पृश्यों को दबाने की राजनीति भी कर रही है। वे आंबेडकर की तीखी आलोचनाओं से विपक्ष पर पड़ते प्रभाव को भी देख रहे थे। इसलिए उन्होंने आंबेडकर की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और के संथानम को लगाया। धनंजय कीर के अनुसार राजगोपालाचारी का जवाब तो कमजोर था लेकिन संथानम ने काफी मेहनत और कल्पनाशीलता के साथ जवाब देने की कोशिश की।
गांधी इस बढ़ती कटुता और इसके राजनीतिक खतरे को समझ रहे थे। इसीलिए आजादी मिलने के बाद उन्होंने नेहरू और पटेल को यह सलाह दी कि वे डा आंबेडकर को देश के पहले मंत्रिमंडल में शामिल करें। जब उन लोगों ने डा आंबेडकर के विरोध को देखते हुए आपत्तियाँ दर्ज कराईं तो गांधीजी ने कहा कि सत्ता भारत को मिल रही है न कि कांग्रेस को। (कास्ट एंड आउटकास्ट : द गुड बोटमैन—राजमोहन गांधी)। बातचीत के दौरान मौजूद रहे जी. रामचंद्रन ने राजमोहन गांधी को बताया कि, “नेहरू और सरदार दोनों इस पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि यह व्यक्ति लगातार कांग्रेस पर हमले करता रहा है और उसे बदनाम करता रहा है।’’ “रामचंद्रन के अनुसार गांधी मानते थे कि आंबेडकर को कैबिनेट में शामिल करके भारत उस पाप का प्रायश्चित कर सकेगा जो अस्पृश्यों के साथ उसने किया है।’’
गांधी आंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित थे। 26 जुलाई को जब यह तय हो रहा था कि देश की पहली कैबिनेट में किन प्रतिभाओं को स्थान दिया जाए तो गांधी ने कहा, “हमें हर किसी की सेवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरकार वे सब हमारे देशवासी हैं। क्या नहीं हैं? अंग्रेज सरकार की सेवा करने से वे हमारे दुश्मन नहीं हो गए। गिरिजाशंकर वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने किस तरह हमें 1942 में गाली दी थी। अगर वे हमारी मदद करना चाहें तो क्या हम उन्हें दरकिनार कर दें? इससे हमारा नुकसान होगा। अगर हम ऐसे व्यक्तियों की सलाह लेंगे तो वे अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेंगे।’’ (कास्ट एंड आउटकास्ट : द गुड बोटमैन—राजमोहन गांधी)।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.