
— राजेन्द्र भट्ट —
क्या हमारा देश-समाज एक अभूतपूर्व बुनियादी गुणात्मक परिवर्तन (क्वालिटेटिव चेंज) से गुजर रहा है?
बात शुरू करें आजीवकों/चार्वाक-पंथियों से–भारत का सबसे पुराना, धार्मिक आस्थाओं पर बेहद कड़वा प्रहार करने वाला नास्तिक या ‘निहिलिस्ट’ समुदाय। इतिहासविद बेहतर बता सकते हैं पर मेरे सामान्य अध्ययन के अनुसार, इनका अपना मूल साहित्य उपलब्ध नहीं है। जो है, वह इनके बारे में, या इनका खंडन करते हुए, इनकी आलोचना में धार्मिक आस्थावानों का रचा हुआ है। फिर भी, चार्वाक-दर्शन को छह दर्शनों में स्थान दिया गया और इनके कथित प्रणेता आचार्य बृहस्पति को ठीक-ठाक सम्मान भी दिया गया।
लेकिन कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं पढ़ा कि आस्था को निर्भयता से, कटु शब्दों से चुनौती देने वाले इन नास्तिकों से आमलोगों की भावनाएँ इतनी आहत हो गई हों कि उन्होंने इन्हें खदेड़ कर मारा हो, डराया हो, हत्याएँ की हों।
फिर बौद्ध और जैन परंपरा पर आते हैं। ये भी स्थापित वैदिक/ब्राह्मण परंपरा की विरोधी थीं। लेकिन बुद्ध और महावीर को अपने विचार फैलाने में रोकने के कोई हिंसक, डरावने प्रयास हुए हों, ऐसे प्रसंग नहीं सुने। दोनों ही श्रमण महापुरुषों और उनके प्रमुख शिष्यों के बिना किसी सुरक्षा के ताम-झाम के उत्तर भारत के बड़े इलाके में घूमने के विवरण हैं, छवियाँ हैं। ये माना जाता है कि बुद्ध के समय के कोई साढ़े तीन सौ साल बाद, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग शासकों ने बौद्धों पर हिंसक अत्याचार किए, उनकी इमारतें-प्रतिमाएँ गिराईं। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने की बात यह है कि यह हिंसा भी शासकों और उनके कारिंदों द्वारा की गई है। शासकों द्वारा की जाने वाली हिंसा और उसके जरिए उन्माद पैदा करने के प्रायः राजनीतिक कारण अधिक प्रबल होते हैं ताकि पराजित शासक, उसके सहयोगी और विचारधाराएँ आतंकित रहें और लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपनी सत्ता के औचित्य को साबित किया जा सके, अपने पक्षधर ‘विद्वान’, धर्मगुरु खड़े कर अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन ऐसे प्रयासों के बावजूद, ऐसे शायद कोई प्रसंग सामूहिक स्मृति में नहीं आते कि ‘करतल भिक्षा, तरुतल वास’ करने वाले किसी अरक्षित भिक्षु को गाँव-नगरों के आमलोगों ने इसलिए खदेड़ा या मारा हो कि उसके विचारों से उनकी भावनाओं और आस्थाओं को ठेस लगी हो अथवा उनका धर्म खतरे में आने की आशंका हो गई हो। उलटे अपने देश में तो कड़वा बोलने वाले बाबाओं को भी भिक्षा ज़रूर दी जाती थी।
चौदहवीं सदी के बाद से भारत में भक्ति की विविधतापूर्ण धारा में अनेक भाव-छवियाँ हैं। निर्गुण हैं, राम-भक्त हैं, कृष्ण-भक्त हैं, सूफी हैं। लेकिन सभी का मूल स्वभाव राज्याश्रय से दूर रह कर अपने प्रभु के साथ सीधा तादात्म्य बनाने का रहा है। रहीम जैसे दरबार में रह रहे कवियों की भी भाव-धारा चाटुकारिता की नहीं, अपने प्रभु से लौ लगाने और नैतिक जीवन तथा आस्तिकता में लीन रहने की है। इन संतों, कवियों में बड़ी संख्या कथित सवर्ण, कर्मकांडी परंपरा से बाहर के संतों की हैं जो धर्मों-संप्रदायों की कुरीतियों, पाखंड और वर्णानुक्रम (हाइरार्की) को निर्भीक, कड़वे शब्दों में चुनौती देते हैं।
अगर कबीर को हम इस परंपरा का प्रतिनिधि मानें और पाखंड, कुरीतियों और प्रभु-वर्गों के खिलाफ उनके शब्दों को देखें तो लगता है कि इनके निशाने पर आ रही कोई भी सत्ता और व्यक्ति निश्चय ही तिलमिला जाते होंगे। लेकिन यहाँ भी ऐसा कोई प्रसंग, छवि या स्मृति नहीं है कि काशी के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें अपनी बात कहने से रोका हो, डराया-धमकाया हो या मारपीट की हो।
कबीर जैसे कथित ‘नीची जातियों’ के लोगों के ‘कलियुग’ में इस तरह बेखौफ मुॅंह खोलने को लेकर उनके परवर्ती ‘गो-द्विज हितकारी’ प्रभु के कर्मकांडी भक्त तुलसीदास जी को काफी खुन्नस रही होगी। कलियुग-वर्णन प्रसंग में उन्होंने ‘जानिय ब्रह्म सो विप्रवर’ कहने वाले द्विजों से लड़ने वाले ‘शूद्रों’ और सगुण राम की बजाय किसी और ‘राम’ की बात करने वाले (कबीर जैसों) को ‘अधम, पाखंडी’ वगैरह कह कर खूब भड़ास निकाली है। लेकिन, ऐसे गुस्से के बावजूद, किसी कबीर को बोलने से रोकने, उनकी ‘साखी, सबद, रमैनी’ को नष्ट करने के लोक-जीवन में कोई प्रयास नहीं मिलते।
यों तुलसी बाबा जैसे सनातनी और मर्यादा से एक इंच भी न विमुख होने वाले कवि भी थोड़ा मौज में आ जाते हैं तो वर्षा ऋतु के वर्णन में मेढकों के टर्राने से ‘बटु-समुदाय’ के वेदपाठ की तुलना कर देते हैं। लेकिन, किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी पढ़ी-लिखी या अनपढ़ सेना की भावनाएँ आहत नहीं हुईं। दूसरी ओर, संस्कृत भाषा में लिखी धार्मिक और साहित्यिक रचनाओं (कालिदास ले लें या पुराण ले लें ) में, देव-चरित्रों के उद्दाम काम-वर्णन, छेड़-छाड़ और चुहल से भी उस जमाने में किसी को तकलीफ नहीं हुई। (गनीमत है कि आज के ‘गर्व करने वालों’ ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं पढ़ा तो इन किताबों को भी नहीं पढ़ा।)
कबीर यूरोप के कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो से करीब सौ साल पुराने थे। इन वैज्ञानिकों की चर्च-विरुद्ध मान्यताओं के लिए उन्हें जलाया गया या माफी मांगने पर मजबूर किया गया या प्रतिबंधित कर दिया गया। पर अपने देश-समाज में, कबीर और उनके जैसे संतों को पाखंडों पर फटकार लगाने से वे आमलोग भी हिंसक गुस्से में नहीं आए जो पूर्ण सनातनी-वर्णाश्रमी थे।
ऐसा ही एक उदाहरण पाँचवीं शताब्दी के गणितज्ञ आर्यभट्ट का है। उन्होंने तो कोपरनिकस, गैलीलियो आदि से हज़ार साल पहले पृथ्वी के घूमने की बात कह दी थी जो धार्मिक साहित्य की मान्यताओं से मेल नहीं खाती थी।
आर्यभट्ट की पुस्तकें उन्नीसवीं सदी तक लुप्त हो गईं और आजकल गर्व की जाने वाली दूसरी किताबों की तरह, एक हालैंड-वासी विद्वान ने ‘आर्यभटीय’ को पहली बार छापा। भारत में वराहमिहिर का फलित ज्योतिष छाया रहा जिसमें सूर्य-चंद्रमा-ग्रह और काल्पनिक राहु-केतु मानवीय जीवन को प्रभावित करते रहे। आर्यभट्ट के पहले बड़े टीकाकार भास्कर प्रथम ने उनकी मान्यताओं में, धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बनाने के लिए तोड़-मरोड़ भी की। लेकिन आर्यभट्ट को भी, अपने समाज ने गैलीलियो, ब्रूनो की तरह डराया और प्रताड़ित नहीं किया।
कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम-विरोधी विचारों के लिए सूफी फकीर सरमद को फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ भी गौर करने की बात है कि सरमद तब 60 साल से ज्यादा उम्र का था और खासा लोकप्रिय भी था। यहाँ तक कि शहज़ादा दारा शिकोह उसे मुगल दरबार में भी लाया था। मतलब, आमलोगों को उसकी बातों से आमतौर पर कोई तकलीफ नहीं थी। जैसा शुंग राजाओं द्वारा बौद्धों के दमन का प्रसंग है, यहाँ भी एक बादशाह (औरंगजेब) सियासी तंदूर को गरम रखने के लिए सरमद को मरवाकर ‘धर्म-रक्षक’ की इमेज बना रहा था (खासतौर पर अपने विरोधी दारा शिकोह के दोस्त को मरवाकर।) लेकिन आमलोगों ने उसी सरमद को बरसों आराम से बर्दाश्त किया था और इज्जत भी दी थी। ऊपर से तब, जब कि मुगल राज में सरमद का प्रिय शिष्य – अभयचंद एक हिन्दू था।
क्या इन सारे प्रसंगों से नहीं लगता कि अपने देश में सहिष्णुता की लंबी परंपरा रही है–खासतौर पर हमारे अवाम में!
हम विरोधी विचारों पर चिढ़ सकते थे, उन्हें बुरा-भला भी कहते थे, कभी-कभी तोड़-मरोड़ भी करते थे, उन्हें उपेक्षा से लगभग लुप्त भी कर देते थे–लेकिन विरोधी और परंपरा-असम्मत विचारों के लिए आमलोग उग्र हिंसा और उन्माद का रास्ता नहीं अपनाते थे। (भले ही, राजे-रजवाड़े अपने तात्कालिक फायदे के लिए कभी-कभी ऐसा करते हों और सत्ता स्थिर हो जाने के बाद, वे भी आमतौर पर ऐसी हरकतें छोड़ देते थे।) मतलब, किसी के विचारों से दूसरों को सामूहिक तौर पर चोट नहीं पहुंचती थी। हम अपने देव-चरित्रों का जिक्र करते समय, उनका पूरा सम्मान करते हुए हॅंस भी सकते थे और उनका शृंगार -वर्णन भी कर सकते थे।
तब क्या पिछले कुछ वर्षों से, अपने समाज में यह बुनियादी, आमूल गुणात्मक परिवर्तन आ गया है? क्या हम बात-बात में षड्यंत्र की आशंका से जबड़े कसने लग गए हैं? क्या हजारों वर्षों से ‘जिसकी हस्ती नहीं मिट सकी’, ऐसे समाज के वंशज इस अमृत काल में असुरक्षित होने का माहौल बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? क्या उन्मादी भीड़ के साथ मत-भिन्नता और व्यंग्य-परिहास अब हिंसा की आशंका से डरावना हो रहा है?
क्या चार हजार साल से अपनी संस्कृति-समाज-धर्म के टिके रहने का सुकूनदेह एहसास, पिछले कुछ सालों में कमजोर हो गया है और हमारे अवाम को काल्पनिक भयों से, कुछ ‘लुंपेन’ तत्त्व विचलित कर सकते हैं कि वे आलोचना, मत-भिन्नता, परिहास या व्यंग्य को सहजता से लेने वाला अपना सदियों का आत्म-विश्वास और बड़प्पन खोने लगे हों और चिड़चिड़े, गुस्सैल, क्षुद्रबुद्धि और संकीर्ण होने लगे हों?
क्या, अपने देश-समाज में, पहली बार जनता को जनता से सफलतापूर्वक लड़ा दिया गया है, जनता के हिस्से ही आपस में शक और घृणा करने लगे हैं, आपस में ही हिंसक हो गए हैं? यह जॉर्ज ऑरवेल के ‘1984’ उपन्यास जैसा संसार बन रहा है, जहां हर इंसान दूसरे इंसान पर शक करता है, उससे घृणा करता है, डरता है। अगर ऐसा है तो निश्चय ही यह एक बहुत बुरा आमूल गुणात्मक परिवर्तन होगा।
मुझे तो, अंत में एक मासूम सी चिंता दुखी कर रही है–क्या मैं अपनी परंपरा के किशन-कन्हैया की शैतानियों से अपने आप को सौम्य और प्रफुल्लित रख सकूँगा? क्या मैं उन्हें, बिना किसी कसे जबड़े वाले आस्तिक की आहत भावनाओं के आतंक के, ‘माखनचोर’ कह सकूँगा?
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.











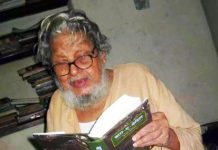





शानदार लिखा राजेन्द्र जी हम समेकित हैं इसी लिये जीवंत हैं
बहुत धन्यवाद।
नमस्कार सर,
आपका लेख पढ़ा, इसमें शायद आप एक विषय जोड़ना भूल गए कि भारतीय संस्कृति में कभी भी अपने धर्म या सम्प्रदाय को किसी दुसरे पर जबरदस्ती थोपने का चलन नहीं रहा मगर अब यही हो रहा है 🌹🙏
जी, मुझे तो लगता है कि यही तो इस लेख का विषय है कि भारतीय अवाम हर तरीके के विचार के साथ जी लेने का स्वभाव रखता है। वह इतना ओछाऔर डरपोक कभी नहीं रहा कि उसे अपने मन माफिक विचार या सम्प्रदाय न होने से इतना डर लगे कि वह हिंसा या नफरत फैलाने लगे। और यह बात मैं अवाम के लिए कह रहा हूँ, हुक्मरानों, फिरकों के नेताओं या उनके ज़रखरीद प्यादों के लिए नहीं।
राजेंद्र भट्ट की चिंता बिल्कुल सही है।
आज जो माहौल बिगड़ रहा है उस पर समाज को सोचने की , चिंता करने की आवश्यकता है।
समाज वैज्ञानिकों का दायित्व बढ़ गया है।
राजनीतिज्ञ तो सभी एक जैसे हैं।
धन्यवाद, राधेश्याम जी
कलम का सिपाही।
धन्यवाद।
मेरे लेख के सुंदर तरीके से प्रकाशन के लिए आभार। एक निवेदन है। इस लेख में भारतीय गणितज्ञ-खगोलविद ‘आर्यभट’ का नाम गलती से ‘आर्यभट्ट’ चला गया है। उनका सही नाम ‘आर्यभट’ है और उनके ग्रंथ का नाम ‘आर्यभटीय’ है।