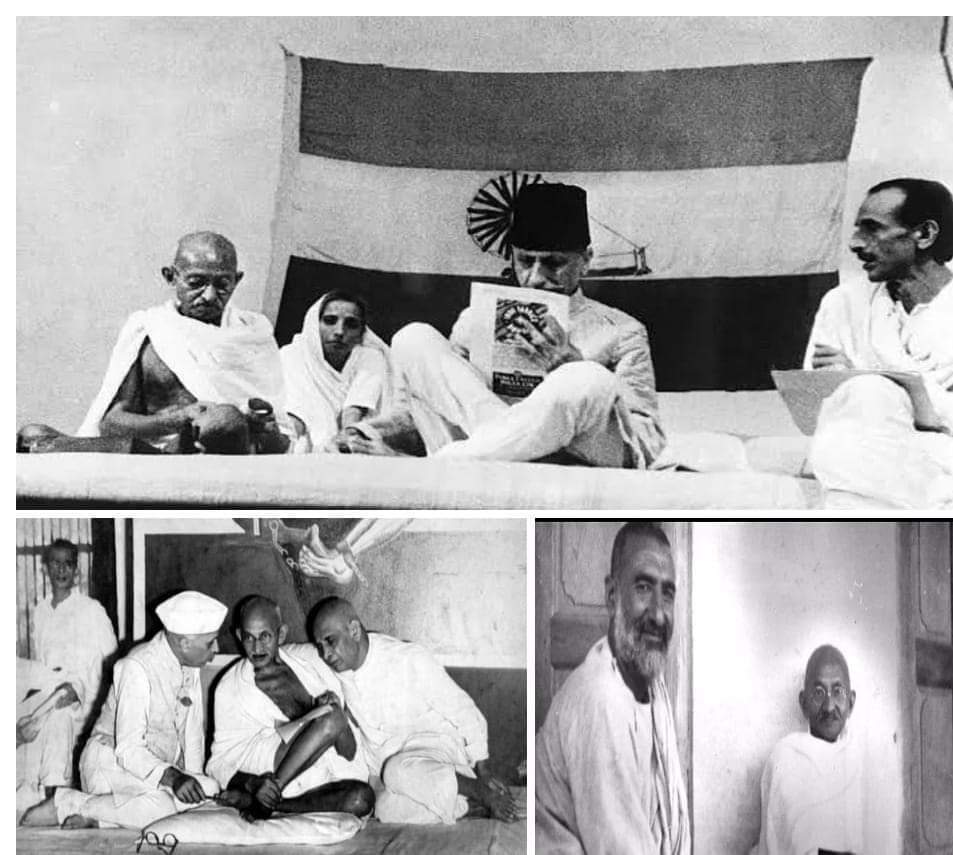— जनेश्वर मिश्र —
अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे मन में डॉ० लोहिया की कौन-सी सबसे उल्लेखनीय स्मृति है तो ऐसी किसी एक बात का जिक्र संभव नहीं है; क्योंकि उनकी स्मृतियों की कोई सीमा नहीं है। मैंने उन्हें बी० ए० में पढ़ते हुए दूर से सुना। फिर छात्र-नेता बनकर निकट से देखा। जेल में साथ रहा। उनके सांसद बनने पर सहायक की तरह उनकी दिनचर्या से जुड़ा। राजनीतिक दौरों में साथ घूमा। उनके जीवन समापन की दुःखद घड़ियों का साक्षी भी बना।
मैंने उनको पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1953 में सुना था। वैसे अपने बचपन में हम समाजवाद वगैरह नहीं जानते थे; लेकिन सन् 1952 के चुनाव में अपने गाँव में हमने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उसने ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसे सन् 42 के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में गोली लगी थी और देश की आजादी के लिए जेल गया था। उस आन्दोलन में मेरे गाँव के निकट बैरिया पुलिस थाना पर छब्बीस लोगों ने शहादत दी थी। यह संभवतः पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी संख्या थी। मैंने भी सन् 52 के चुनाव में बरगद निशानवाली समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, क्योंकि स्वतंत्रतासेनानी का आकर्षण था। उस चुनाव में पण्डित नेहरू मेरे स्कूल के मैदान में एक सभा में बोलने आये थे और एक लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ हुई।
समाजवादियों में तब ऐसा जोश था कि लगता था कांग्रेस का विकल्प बन जाएँगे। पण्डित नेहरू ने अपने भाषण में सोशलिस्टों का जिक्र करते हुए कहा था कि समाजवादी सबको बराबर करने की बात करते हैं; फिर तमक कर अपनी हथेली खोलकर कहा कि देखो कुदरत ने भी हमारी अँगुलियाँ बराबर नहीं बनाई हैं। नेहरूजी की बात से मुझे भी लगा कि बात तो ठीक ही है। हथेली में उँगलियाँ कहाँ बराबर हैं। उनके दो-तीन दिन बाद जयप्रकाशजी आए। मैं उनको भी सुनने गया था। उन्होंने अपने भाषण में पण्डित नेहरू के तर्क का जिक्र किया। मुझे लगा कि अब बहस रास्ते पर आ रही है। जे० पी० ने कहा कि पाँचों उँगलियों का बराबर न होना सही है, लेकिन इन उँगलियों में ऐसा अंतर नहीं है कि एक उँगली एक हाथ की हो और दूसरी एक इंच की हो। ऐसा होने पर मुट्ठी नहीं बन पाएगी; इसलिए हम समाजवादी ऐसा ही अंतर चाहते हैं कि समाज में एकजुटता बनी रहे। जब डॉ० लोहिया को मैंने इलाहाबाद में पहली बार सुना तो वह समता पर बोल रहे थे। उन्होंने संपूर्ण और संभव समता के बारे में बताया- सम्पूर्ण समता हमारा आदर्श है और संभव समता हमारा प्रयास है। यह बात मेरे मन में बैठ गई। फिर उनका अंदाज भी खूब पसंद आया। बड़े प्रोफेसरों से लेकर नये विद्यार्थियों तक सबसे सहज भाव से जुड़ जाते थे। उनकी हँसी तो बहुत ही सहज थी।
फिर 1953 में ही इलाहाबाद में समाजवादियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। आचार्य नरेन्द्रदेवजी अध्यक्ष और डॉ० लोहिया महामंत्री थे। मैं एक स्वयंसेवक था। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब सम्मेलन में बहुत कम बैठते थे। अक्सर किसी चाय की दुकान पर कुछ कार्यकर्ताओं से बोलते-बतियाते रहते थे। ऐसा लगता था कि चौबीसों
घंटा गप में ही लगाते हैं। हम लोग भी उनको खोजते रहते थे कि उनकी बातें सुन सकें। सम्मेलन के दौरान अखबार में जे० पी० की एक फोटो छपी। जे० पी० प्रभाजी के साथ रिक्शे पर बैठकर स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ी लकड़ी बेचनेवाले का एक ठेला पड़ा। जे० पी० ने रिक्शे से उतर कर ठेलेवाले की मदद की। ठेले को हाथ लगाया जिससे कि उस गरीब की सहायता हो जाए। इसी घटना की तस्वीर छपी और चर्चा भी हुई। इसको लेकर डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया मुझे आज भी याद है। यह खबर पढ़ने के बाद जब डॉक्टर साहब को प्रभाजी दिखाई पड़ीं तो उन्होंने रोककर चाय के लिए पूछा। प्रभाजी रुक गईं तो डॉक्टर साहब ने उनसे बड़ी नरमी से कहा, “अपने आदमी को समझाओ कि गरीब की हमदर्दी का नाटक न करें। ठेलेवाले के लिए तो हमदर्दी और रिक्शेवाले के लिए कोई सोच नहीं।”
1953 के बाद तो मैं उनकी ओर खिंचता ही चला गया। 1958 में इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चल गई थी। मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मार पड़ गयी। शायद सौ से ज्यादा लाठियाँ लगीं थीं। लोहियाजी ने मेरे बारे में पुछवाया। किसी ने कह दिया कॉफ़ी हाउस में बैठकर सिगरेट पी रहा होगा। इस पर डॉक्टर साहब बहुत बिगड़े। मुझे खबर हुई कि डॉक्टर साहब खोज रहे हैं। मैं पहुँच गया, फिर घर के बुजुर्ग की तरह, जैसे बड़े भाई या पिता हों; शरीर की तकलीफों का सारा विवरण पूछा। माथे की चोट का असर विस्तार से जाना। एक-एक घाव को जानना और मेरे सिर की चोट की गंभीरता को महसूस करना मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर मर्मस्पर्शी सिद्ध हुआ। मेरा तो इलाहाबाद में कोई नहीं था। मुझे लगा कि आज से मेरा भी कोई है जो वक्त पड़ने पर मेरी चिन्ता करेगा।
1955-56 में प्रजा समाजवादी पार्टी से अलगाव की बात आई। चंद्रशेखरजी मेरे पास आए, कमरे में भीड़ थी। मुझसे कहा कुछ अलग से बात करनी है, कंपनी बाग चलें। चंद्रशेखरजी ने कई व्यक्तिगत सवाल एक साथ दाग दिए। क्या मुझमें कोई व्यक्तिगत कमी है? मैंने कहा नहीं। फिर पूछा कि प्रसोपा पर आरोप है कि कांग्रेस की बी टीम हो गई है। फिर बात लोहियाजी की व्यक्तिगत चर्चा पर चली आई। तब मैंने पूछा कि अगर प्रसोपा कांग्रेस में चली गई तो क्या आप डॉ० लोहिया के साथ आ जाएँगे ? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जब डॉ० लोहिया इलाहाबाद स्टेशन पर उतरते हैं तो काशीनाथ या धर्मवीर गोस्वामी के कंधे पर हाथ रख देते हैं। मेरे कंधे पर तो कभी नहीं रखा। मैंने जब यह बात डॉक्टर साहब को बताई वह खूब हँसे। उन्होंने कहा कि उसे यह समझाना कि मैं उनके कंधों पर हाथ इसलिए रखता हूँ कि वे छोटे हैं। चंद्रशेखर के कंधे पर हाथ रखा तो लटक जाऊँगा। अब मैं यह बात कैसे बताता !
डॉक्टर साहब के राजनीतिक कार्यों को लेकर अक्सर नासमझी दिखाई जाती है। उनके द्वारा चलाये गए सभी अभियान और आंदोलन एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। वह निर्गुण सिद्धांतों को सगुण कार्यक्रमों का जामा पहनाने का आग्रह करते थे। जैसे-जब तक समान अवसर का सिद्धांत चलता रहेगा और कमजोर वर्ग यानी महिला-पिछड़े-दलित-अल्पसंख्यकों के कमजोर हिस्से को विशेष अवसर नहीं दिया जाता तो समानता का सिद्धांत बेमतलब हो जाता है। समानता का अर्थ दौलत की बराबरी रहा है। लेकिन यह एकांगी था। जब तक सिर्फ पैसे और जन्म की समानता को हासिल करने के लिए लड़ा जाएगा और दिमाग की पूर्ण समानता के लिए नहीं, जिसका संबंध भाषा से होता है, तब तक हम धन और जन्म की समानताएँ भी हासिल नहीं कर सकते।
हमने केवल विदेशी भाषा को ही विषमता का आधार नहीं माना बल्कि उनके कपड़े लत्ते, खेल और साहित्य को भी ज्यादा रुतबा दिया। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। लोहियाजी ने यह स्पष्ट किया कि यह संभव है कि समाज में धन एक बार बराबरी की धारा के साथ प्रभावित हो जाए और जन-जीवन में भी जाति-आधारित छोटे-बड़े की धारा को तोड़कर समानता की धारा बहे, लेकिन भाषा की मानसिक गुलामी से मुक्त हुए बिना एक मजबूत देश की कल्पना संभव नहीं है। हिन्दी, तमिल, मराठी या बांग्ला आदि भाषाएँ अंग्रेजी की गुलाम जैसी रहें और हमारे सभी खेल फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि क्रिकेट के चलते दबे रहें तो हमारी स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी।
डॉ० लोहिया इस पूरे जंजाल के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए हम उनके किसी एक पक्ष को लेकर पूरी बात नहीं समझ सकते। उनके समाजवादी चिंतन और कार्यक्रम में सभी एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी एक मोर्चे पर लड़ाई जीतने से पूरी व्यवस्था के बदलाव को सम्पन्न नहीं माना जा सकता। इन सबको जीतने के साथ ही देश को मजबूत बनाने के लिए वह ‘हिमालय बचाओ’ जैसी लड़ाई को आगे बढ़ाना जरूरी मानते थे। एक मजबूत समाज और राष्ट्र की पूर्ण कल्पना की बजाय उनके विचारों को हल्का सिद्ध करने के लिए किसी एक की ओर इशारा करना उनके आलोचकों की कमजोरी रही है।
लोहिया-विरोधी लोग लोहिया-धारा के सारांश के रूप में नेहरू-विरोध, कांग्रेस-विरोध या मार्क्सवाद-विरोध को याद रखते हैं और मानते हैं कि उनकी राजनीति की परिणति गैर-कांग्रेसवाद की सफल रणनीति के रूप में हुई जबकि लोहियाजी के लिए यह तीनों सिर्फ प्रतीक थे और तीनों का एक ही परिणाम रहा है। जैसे-अंग्रेजी भाषा एक प्रतीक है और पण्डित नेहरू उसका नाम था। जब तक गांधीजी की गर्मी का असर था और पटेल, प्रसाद, पंत आदि जिंदा थे, तब तक जवाहरलाल नेहरू थोड़ा शांत थे और कांग्रेसी थे। लेकिन जैसे ही ये बड़े लोग गए और दूसरी पीढ़ी आगे आई, नेहरूजी में दुनिया की निगाह में प्रगतिशील दिखने का शौक उभरा। वह अपने शुरूआती दौर में गांधीजी से डरकर या प्रभावित होकर दूर नहीं गये थे। पर वही नेहरू बाद में अशोक मेहता जैसे सोशलिस्टों और डांगे-जोशी जैसे कम्युनिस्टों से प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट लेने लगे।
खुश्चेव-बुल्गानिन से तो प्रगतिशील होने का तमगा ही ले लिया। चीन के चाओ से रिश्ता सुधार कर प्रगतिशीलता प्रमाण लेना चाहते थे। हालाँकि इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। वस्तुतः कुछ लोगों में यह एक मानसिक रोग होता है कि वे होते कुछ हैं और दिखना कुछ और चाहते हैं। ऐसे ही कम्युनिज्म का भी मामला रहा है। गोपालन-रणदिवे-ज्योति बसुवाली धारा को छोड़कर बाकी के बारे में यह मानना होगा कि प्रायः सभी कम्युनिस्ट नेहरू विरुदावली से जुड़े रहते थे। ऐसा ही रुझान आधे से ज्यादा सोशलिस्टों में भी था। डॉक्टर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी में गए लोगों के प्रति मित्रभाव रखते थे; लेकिन उनकी दृष्टि में केरल का कम्युनिस्ट बंगाल के कम्युनिस्ट की तुलना में ज्यादा आदर्शवादी था। जैसे ज्योति बसु कमजोर नहीं थे, लेकिन व्यावहारिकता के ज्यादा नजदीक चले जाते थे। जब राजनीति व्यावहारिकता की ओर बढ़ती है तो सैद्धांतिकता से फिसल जाती है। इसे हम सोशलिस्टों ने बहुत भोगा है। बैतुल में ‘पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरियाँ’ और आवाडी में ‘सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी’ जैसे नारों से हमारे कई लोग व्यावहारिकता की ओर आकर्षित हो गये थे।
कांग्रेस के बारे में डॉक्टर साहब के मोहभंग का कारण कांग्रेस के नेतृत्त्व का निरंकुश होना था। जब कोई नेतृत्त्व निरंकुश हो जाता है तो उसका पहला काम विपक्ष को तिकड़म और ताकत से नष्ट-भ्रष्ट करना होता है; दूसरे, लोहियाजी जिस मिट्टी के बने थे वह गांधी की तैयार की हुई थी। गांधी की मिट्टी में यह खूबी थी कि उन्होंने अमरीका को कभी पसंद नहीं किया। कभी वहाँ नहीं गए। जब बुलाया तो कहा कि अभी अमेरिका हमारे लायक नहीं बना है। कोई-कोई मिट्टी एकबारगी बड़ी कड़ी हो जाती है। ऐसी ही मिट्टी से लोहिया तैयार किये गये थे। तब तक समाजवादी आन्दोलन के नेता लोग उमर की आखिरी सीढ़ी के नजदीक जा रहे थे। संकल्प- शक्ति के हाथ-पैर भी थोड़ा-बहुत कमजोर हो रहे थे। ऐसे में आदमी छड़ी लेकर चलता है। 1952 का आम चुनाव हारने के बाद जैसी भगदड़ मची थी, उसके बाद जो बचे-खुचे थे, वे फिसलने के डर से किसान-मजदूर प्रजा पार्टी की छड़ी लेकर चलने लगे। मुझे लगता है कि हमारे आन्दोलन के इस पक्ष को भी कभी समझदारी से जाँचना चाहिए।
वैसे तो शुरूआत पहले ही हो चुकी थी जब आचार्य नरेन्द्रदेव और लोहियाजी महासचिव पद पर थे। प्रयोग के तौर पर केरल में हमारी सरकार बन गई। यह अल्पमत की सरकार थी और एक व्यावहारिक समझौते का नतीजा थी। सरकार कांग्रेस के समर्थन पर निर्भर थी। उस सरकार ने एक निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी। कुछ लोग मारे गए। लोहियाजी एक सत्याग्रह में नैनी जेल में बंद थे। वहाँ से उन्होंने समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री पटट्मथानु पिल्लई को तार दिया कि मजिस्ट्रेट जाँच कराओ या इस्तीफा दो। यह बात 1953-54 की है।
आजादी के कुल पाँच साल ही हुए थे। अगर तब सरकारी हिंसा और राजनीतिक हिंसा के सवाल पर निर्णायक बहस हो गयी होती, तो आज समाज में सरकारी और गैरसरकारी हिंसा और नक्सलपंथ से लेकर आतंकवाद की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनका सिलसिला ही बंद हो गया होता। लेकिन एक बड़े सवाल पर लोहिया की पहल के बावजूद हम सभी चूक गए। यह बहस गांधी के सिद्धांतों के आधार पर थी कि जनता की निहत्थी भीड़ और सरकारी पुलिस की बंदूक का रिश्ता क्या होना चाहिए। यह संबंध आज भी तय होना बाकी है। नागपुर में लोहिया हार गए और सरकारी हिंसा की जीत हुई। तबसे आज तक हमारा समाज जहाँ तक फिसला है, उसमें नागपुर सम्मेलन के फैसले का बहुत बड़ा योगदान है।
इसी तरह सरकारी दल या विरोधी दल के रिश्तों का सवाल भी उसी दौर में उलझा था। बम्बई की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकारी पार्टी से समझौता कर लिया। इस पर एक नेता ने बयान दिया तो उसे निकाल दिया गया। तब लोहिया ने दो शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक आचरण का एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया
था- वाणी-स्वतंत्रता और कर्म-नियंत्रण। अपनी बात कहने का अधिकार रहेगा, लेकिन सामूहिक निर्णय के खिलाफ काम का अधिकार नहीं होगा। यही मंत्र लेकर उत्तर प्रदेश में श्री दलसिंगार दूबे ने समाजवादियों का सम्मेलन बुला लिया। मधु लिमये को उद्घाटन के लिए बुलाया। इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वाणी- स्वतंत्रता और कर्म-अनुशासन पर जोर देने के लिए लोहिया को निकाल दिया। पूरी समाजवादी पार्टी टूट गई।
मैं इन घटनाओं का जिक्र करके यह याद दिलाना चाहता हूँ कि किन मूल्यों के लिए और कितने बुनियादी सवालों के लिए लोहिया को दुःख उठाना पड़ा। पार्टी के टूट जाने के बाद जिन मुफलिसी बियाबानों से लोहिया और समाजवादियों को गुजरना पड़ा, इसे हम कम जानते हैं। हम लोगों को लोहियाजी को अमीनाबाद से लखनऊ से कॉफी हाउस तक ताँगे में लाने में शर्म लगती थी। लेकिन कॉफी हाउस से निकलने के बाद जब डॉ० लोहिया श्री के० सी० मिश्रा से यह कहते थे, “कैलाश ! एक ‘हार्स पावर’ की गाड़ी मँगाओ।” तो पढ़े-लिखे आदमी होने के बावजूद समझ नहीं पाते थे कि एक हार्स पावर की गाड़ी कैसी होती है। तब हँसकर कहते थे कि “ताँगा मँगाओ”। ‘वन हार्स पावर’ शब्द का इस्तेमाल करके डॉ० लोहिया मुफलिसी में भी शान से जीना सिखाते थे। वह बराबर कहते थे कि कभी मन को छोटा मत करना, खुश रहना। किसी तरह से 57 का जमाना आया। हम लोग थोड़ा-बहुत सँभले। उन दिनों समाजवादियों ने ‘एकला चलो’ की लकीर को खींच दिया था।
लेकिन 1962 आते-आते नेहरू-व्यवस्था के दिन ‘गुड ईवनिंग’ के रूप में बदलने लगे। उनका ‘गुड नाईट’ आता तब तक डॉ० लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का आह्वान किया-सब लोग मिलकर देश को लड़खड़ाहट से बचाएँ। वह एक मजबूत नेता की रणनीति थी जिसे मालूम हो गया था कि हम अकेले राजनीतिक बदलाव की चुनौती को नहीं सँभाल पाएँगे। यह सच है कि गैर-कांग्रेसवाद में गैर-समाजवादी तत्त्व भी आये, लेकिन तब तक हमारी धारणा बन गई कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे-छोटे लोगों की मदद ली जा सकती है। हमारी यह रणनीति प्रयोगों के कई दौर से गुजरते हुए 1977 तक देश की राजनीति में चलती रही। इसमें हमने उत्तर प्रदेश में सरकार अगर झारखण्ड राज्य के बगल में बैठकर चलाई, तो रामप्रकाश गुप्ता के बगल में भी बैठे। अलग-अलग जमातों के रामस्वरूप वर्मा, प्रभुनारायण और मंगलदेव ‘विशारद’ हमारी ओर से मंत्री बने।
जब डॉ० लोहिया इस रास्ते पर आगे बढ़े तो कम्युनिस्ट बोलते थे कि साम्प्रदायिक शक्तियों से सहयोग ले रहे हैं जबकि जनसंघ कहती थी कि राष्ट्रद्रोही शक्तियों से जुड़ रहे हैं। ऐसा लगता था कि दोनों भड़के हुए थे। एक देशीपन के और दूसरा विदेशीपन के अतिरोग से पीड़ित था। आखिर में लोहिया ने यही कहा कि पहले मिल-बैठकर तय करो कि हमारा देश बिगड़ने से बच जाए। तब यह तय करेंगे कि सिर्फ देशी चले या विदेशी चले या कोई और रास्ता निकले, 77 आते-आते मामला बहुत बिगड़ा जब अलीगढ़ में मुसलमानों को काटा गया। तब राजनारायण और मधु लिमये ने नाम लेकर बताया कि कौन अगुआई कर रहा था। इस पर दोहरी सदस्यता का सवाल जनता पार्टी में उठा।
मुसलमान तादाद में कमजोर था। उसकी हिफाजत हमारा फर्ज था। इसमें हमारी जनता पार्टी टूट गई और हमारी सरकार भी बिखर गयी। लोहियाजी की विचारधारा और कर्मधारा दोनों के समन्वय से ही उनके व्यक्तित्त्व में आकर्षण पैदा होता था। वह सच कहने का साहस रखते थे और झूठ और पाखण्ड के खिलाफ अपनी समूची लोकप्रियता को बार-बार दाँव पर लगाते रहे, इसीलिए बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों को उनसे विशेष अनुराग था। हमें यह भी याद रखना होगा कि लोहिया स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। किसी भी विद्वान से जानकारी और समझदारी में बराबरी रखते थे। वह अपनी अतिव्यस्तता के बावजूद कुछ समय बुद्धिजीवियों के लिए जरूर निकालते थे। कॉफी और चाय पर लम्बी बहस और चर्चाएँ करते थे। ऐसी बहसों से लोहिया को कुछ मिलता था और लोहिया से बुद्धिजीवियों को भी जरूर कुछ मिला करता था। लोकसभा का सदस्य बनने के बाद वह कभी दिनकरजी, कभी दुर्गादास और कभी निखिल चक्रवर्ती जैसे किसी बुद्धिजीवी को स्वयं बुलाकर बातें करते थे।
लोहिया की सोच में समग्रता का होना बुद्धिजीवियों और जनसाधारण दोनों को आकर्षित करता था। वैसे वर्ण-व्यवस्था और जाति के खिलाफ डॉ० अम्बेडकर का आन्दोलन पहले से ही था। ऐसे ही श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जैसे नेता थे जो हिन्दी के लिए बहुत लड़ते थे। इसी तरह महिलाओं को परदे से बाहर लाने और समाज में सम्मानजनक स्थान के लिए कई तरह के कार्यों का सिलसिला था। लेकिन लोहियाजी ने समाज और राष्ट्र दोनों को मजबूत बनाने के लिए भाषा से लेकर जाति तक होते हुए नर-नारी समता और आर्थिक समानता के प्रश्नों को समाजवादी आन्दोलन का मूलाधार बनाकर एकजुटता दी। इसी प्रकार राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए ‘हिमाचल बचाओ’ प्रश्न उठाया। लोहिया की जातिनीति, भाषानीति, दामनीति और हिमालय-नीति के आधे-अधूरे कार्यान्वयन के लिए हम दोषी हैं। लोहिया-विचार के मूल में कोई कमी नहीं थी।
दूसरी दूर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिन्दुस्तान में आज तक कोई क्रांति नहीं हो पाई है। बहुत रूढ़िग्रस्त देश रहा है। जब कोई बड़ी क्रांति होती है तो उसमें से कुछ शब्द अपने-आप निकल आते हैं। कोई विचारक उन्हें नहीं गढ़ता। वह क्रांति से ही पैदा होते हैं। फिर वह सारी दुनिया के लिए शाश्वत बन जाते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, जो फ्रांस से लेकर अमरीका तक फैल गया। फिर समानता, जिसने रूस से लेकर चीन तक असर पैदा किया और बंधुत्त्व-यह भारत समेत समूची गुलाम दुनिया में बहुत महत्त्वपूर्ण बना। भारत से भी अहिंसा-करुणा-वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे शब्द आए हैं। क्रांति का प्रकाश गांधीजी ने भी दिया। अपनी राजनीतिक यात्रा के अंत तक आते-आते गांधीजी ने भी ‘भारत छोड़ो’ का नारा दिया। यह एक नकारात्मक नारा था। ऐसे नारे से पैदा क्रांति के पेट से बाद में भी नकारात्मक नारे ही -निकलते रहेंगे, जैसे अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो वगैरह। लोहिया के मूल्यांकन में यह मानना गलत होगा कि उनका रास्ता नकारात्मक था। उन्होंने बहुत बड़े सपने देखे और हमें दिखाए। लेकिन हम उनके नाकाबिल सहयोगी थे। इसलिए कई समकालीन लोगों ने जलन में उनकी
राजनीति को छोटा करके दिखाने की कोशिश की। इसमें देश को दोष देना गलत होगा। दोष सहयोगियों और अनुयायियों का है। वैसे यह भी याद दिलाना जरूरी होगा कि इस देश में नेता अनेक हुए हैं; लेकिन सिर्फ दो ही नेताओं के लोग हुए-गांधी के लोग और फिर लोहिया के लोग।
…..
परिचय…
‘छोटे लोहिया’ के नाम से प्रसिद्ध । छात्र जीवन से ही लोहिया के अनुयायी। 1954 से जीवन-पर्यन्त लोहिया धारा के सक्रिय नेता। अनेक बार लम्बी जेलयात्राएँ एवं 5 बार संसद की सदस्यता एवं केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य। निधन 22 जनवरी 2010
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.