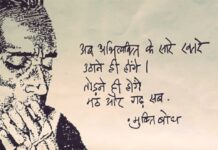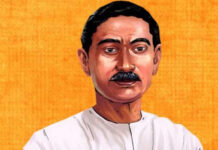— परिचय दास —
धनुर्धर तो थे अर्जुन, लेकिन केवल तीर चलाने वाले नहीं थे। वे उन दुर्लभ योद्धाओं में से एक थे जो अपने चित्त की गति को शस्त्र की नोक से भी अधिक सूक्ष्म बना सके थे। वे चलते थे, लेकिन उनके पाँव में युद्ध की गर्जना नहीं, नितांत मौन का प्रणाद होता था। हस्तिनापुर की असंख्य गलियों से जब वे गुज़रे होंगे, तो कितनी स्त्रियाँ थीं जो उनके रथ की छाया में अपने भीतर का युद्ध महसूस करती थीं—और कितने वृद्ध थे जिनकी आँखों में उस नवयुवक की छवि किसी भूले हुए धर्म की पुनरावृत्ति बन जाती थी। अर्जुन, केवल कुरुक्षेत्र के नायक नहीं, आत्मा के एकांत में विचरने वाले वे रथी थे जिनके लिये युद्ध केवल बाह्य स्थितियों का तर्क नहीं था, वह एक आंतरिक तर्जनी थी जो मन के गांधार तक पहुँचना चाहती थी।
कृष्ण उनके सारथी थे—लेकिन यह दृश्य केवल महाभारत का नहीं था। यह उस सनातन सम्बन्ध का प्रमाण था जहाँ ईश्वर स्वयं मनुष्य के भीतर के द्वन्द्वों को खींचने का भार उठाता है। अर्जुन का धनुष उनके बाहुबल का प्रतीक था, पर गाण्डीव से अधिक वज्रभूत तो वह क्षण था जब उन्होंने युद्धभूमि में रथ का अग्रभाग छोड़कर अपने ही हृदय में उतर जाने का साहस किया। यह कौन करता है? वह जो अपने भीतर की ग्लानि से डरता नहीं—और अर्जुन ने डर को युद्ध की पहली विभूति मानकर शिथिलता को अंगीकार किया। यह कमजोरी नहीं थी, यह वह शक्ति थी जो आत्मा को युद्ध से भी अधिक पारदर्शी बनाती है।
वे पाँचों पांडवों में सबसे अधिक सौंदर्यवान, सबसे अधिक प्रशिक्षित, और सबसे अधिक प्रिय थे—लेकिन क्या सबसे अधिक अकेले नहीं थे? युधिष्ठिर न्याय की मूर्ति बने रहे, भीम बल का प्रमाण, नकुल और सहदेव अपनी शुद्धता के प्रतीक—पर अर्जुन? वे तो उस स्पंदन का नाम हैं जो पवित्रता और युद्ध, प्रेम और अनुशासन, गुरु और शिष्य, नारी और वीर, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक पथ का निर्माण करता है। जब वे द्रौपदी के लिये स्वयंवर में धनुष उठाते हैं, तो वह केवल लक्ष्य भेदन नहीं होता—वह स्त्री को सम्मान देने का सबसे शांत और सबसे सौन्दर्यपूर्ण विद्रोह होता है।
द्रौपदी उन्हें प्रेम करती थीं—किंतु वह प्रेम तड़प से कहीं अधिक उच्चतर था। वह उस अग्नि का नाम था जिसमें अर्जुन की सभी अस्थियाँ गल कर एक वंशी की तरह वज्र हो गई थीं। कृष्ण उन्हें मित्र कहते हैं—लेकिन उस मित्रता में सृष्टि के प्रथम संवादों की स्मृति होती है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में अपने ही रक्त को शत्रु के रंग में देखकर कंपित हो जाते हैं, तब कृष्ण उन्हें गीत देते हैं। गीता कोई पुस्तक नहीं, वह उस क्षण की उच्चतम कविता है जिसमें मनुष्य का युद्ध मनुष्य से नहीं, स्वयं से होता है। और अर्जुन, उस कविता के पहले श्रोता हैं।
उनका रथ युद्ध के बीच में रुका था, लेकिन वह रथ धरती पर नहीं, अंतरात्मा की कगार पर खड़ा था। ‘न हन्यते हन्यमाने शरीरे’—इस वाक्य को कहने वाला कृष्ण था, लेकिन उसे समझने वाला अर्जुन था। एक योद्धा जिसने अपने ही प्रियजनों को देखकर तीर छोड़ना बंद किया—क्या वह दुर्बल था? या वह इतना प्रखर था कि उसे पता था कि हर विजय, हर पराजय से पहले एक मौन होता है, जिसे सुनना अनिवार्य होता है।
जब अर्जुन ने कर्ण को मारा, तब युद्ध केवल बाहरी नहीं रहा। कर्ण के रथ का चक्का धँस चुका था, और उसने शस्त्र-विहीन करुणा में शरण ली थी। अर्जुन ने मार दिया—कृष्ण की सलाह पर। क्या अर्जुन रोये होंगे? क्या उन्होंने युद्ध के बाद एकांत में कर्ण की परछाईं को छुआ होगा? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत नहीं देता, लेकिन हमारी आत्मा देती है—हाँ, अर्जुन ने उस दिन तीर से नहीं, एक क्षमा से कर्ण को छुआ होगा।
गांधारी ने उन्हें शाप दिया—कि वे मृत्यु के समय स्मृति खो देंगे। कितना अद्भुत है यह शाप! अर्जुन, जिसने गीता सुनी थी, जिसने रथ चलवाया था स्वयं कृष्ण से, जो संसार का सबसे बड़ा योद्धा था—वह मृत्यु के समय कुछ न याद रख पाए। यह विस्मृति कोई दंड नहीं थी, वह मोक्ष थी। जिस अर्जुन ने जीवन भर युद्ध की ज्वाला में अपने चित्त को तपाया, वह अंततः मृत्यु में निष्पलक रहा—जैसे कोई शांत झील।
अर्जुन का जीवन एक रेखा है जो प्रेम, करुणा, युद्ध, त्याग और अंततः विषाद तक जाती है। उन्होंने अभिमन्यु को खोया—और उस शोक में भी वे शांत रहे। यह शोक पिता का था, योद्धा का नहीं। और शायद अर्जुन का सबसे गहन युद्ध अभिमन्यु की मृत्यु के बाद आरम्भ होता है—जहाँ वे अपने भीतर के शून्य से संघर्ष करते हैं।
जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और अर्जुन उसका प्रत्युत्तर देने को तैयार होते हैं, तो वे जानते हैं कि यह शक्ति अब विध्वंस से नहीं, क्षमा से जीती जा सकती है। महाभारत का यह क्षण अर्जुन की चरम भूमिका है—जहाँ वे क्षमा को युद्ध की अंतिम परिणति मानते हैं। और कृष्ण वहाँ भी उनके साथ हैं—न केवल सलाह देने के लिये, बल्कि उन्हें साक्षी रूप में स्वीकारने के लिये।
अर्जुन, केवल योद्धा नहीं, एक काव्य हैं—जिसे युद्ध के शिलाखंडों पर नहीं, आत्मा के तरल प्रदेशों में लिखा गया है। वे उस लौ की तरह हैं जो किसी दीपक से नहीं, किसी मौन से जली थी। उनका गांडीव, उनका रथ, उनका कृष्ण—ये सब प्रतीक हैं उस चित्त की परिपक्वता के, जिसे हम “धर्म” कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में करुणा है।
उन्होंने द्रौपदी को बाँटने का निर्णय नहीं लिया—पर उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि मातृवाक्य उनके लिये धर्म से अधिक अनुलंघ्य था। वे उस पारंपरिकता के भी प्रतीक हैं जो अनिवार्य नहीं थी, किंतु समय की गति को सहन करने के लिये आवश्यक थी। अर्जुन का धर्म कहीं भी जड़ नहीं हुआ, वह चलता रहा—कभी कृष्ण के पीछे, कभी द्रौपदी की आँखों में, कभी अभिमन्यु की राख में, कभी अश्वत्थामा के रथ के धुएँ में।
और अंत में जब वे हिमालय की ओर जाते हैं—सशरीर स्वर्गारोहण की ओर—तो वे गिरते हैं। कृष्ण जा चुके थे, युद्ध समाप्त हो चुका था, द्रौपदी पंचतत्व में लीन हो चुकी थीं, और अर्जुन? वे भी गिरते हैं—क्योंकि मोह शेष था। शायद उन्हें कृष्ण की अनुपस्थिति में संसार फिर से अर्थहीन लगने लगा था। और वह गिरना—कोई पराजय नहीं, एक अत्यंत मानवीय निवेदन था कि ईश्वर जब चला जाता है, तो युद्ध जीते हुए भी मनुष्य अधूरा रह जाता है।
अर्जुन को स्मरण करना, आत्मा के भीतर के सबसे नाजुक तंतु को छूना है। वे एक महानायक नहीं, एक मनुष्य थे जो महानता के क्षणों में भी मनुष्यता को नहीं भूले। और यही कारण है कि कृष्ण ने उन्हें गीता दी—क्योंकि अर्जुन उसे समझ सकते थे। वे हारे हुए नहीं थे, लेकिन विजेता भी नहीं थे—वे तो उस यात्रा के यात्री थे, जो जीत और हार दोनों से परे थी।
किसी क्षण अर्जुन एक विराट धनुर्धारी हैं—और किसी क्षण वे उस वृद्ध पिता की तरह मौन, जो पुत्र के वध के बाद आँसुओं को भी संस्कार समझता है। अर्जुन के भीतर का यह द्वैध—युद्ध और क्षमा, वेग और मौन, प्रभुता और शरणागतता—महाभारत की कथा को केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं रहने देता, वह उसे मानवीय चेतना का दस्तावेज़ बना देता है।
वे वनवास में भी अर्जुन थे, और राजसूय यज्ञ के समय भी। इन्द्रलोक में जाकर जब उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किए, तो वह अर्जुन का बाह्य विस्तार नहीं था, वह आत्मा का एक मौन पुनराविष्कार था। अर्जुन जान चुके थे कि युद्ध केवल भुजबल से नहीं जीता जाता—बल्कि उसे सहने की तैयारी, उसे न टालने की क्षमता, और अंतिम क्षण में उसे छोड़ सकने की शक्ति चाहिए। यह अर्जुन की आन्तरिक तैयारी थी, जो उन्हें द्रौपदी के अपमान के क्षण में मौन तो रखती है—पर उस मौन में ही कोई प्रतिज्ञा जन्म लेती है, कोई असहाय करुणा तलवार में बदल जाती है।
उन्हें देखकर भीष्म शांत हो जाते थे। एक बार नहीं, कई बार भीष्म ने अर्जुन को देखा होगा—और सोचा होगा: यह वही बालक है जो द्रोण से युद्ध की पहली शपथ लेकर आया था, अब धर्म के द्वार तक पहुँच चुका है। अर्जुन की उपस्थिति स्वयं भीष्म के संकल्पों को कँपाती थी। जब अर्जुन ने शिखण्डी के आड़ से पितामह को बाणों से विदीर्ण किया, तब वह कोई त्रिकालदर्शी युद्धनीति नहीं थी, वह एक संचित पीड़ा का विसर्जन था। क्या अर्जुन ने उस क्षण अपराध बोध महसूस किया होगा? शायद नहीं। या शायद हाँ—क्योंकि अर्जुन अपने प्रत्येक तीर के पीछे एक प्रश्न रखते थे—कि क्या यह धर्म है?
जब वे यक्षप्रश्न में उत्तर देने वाले युधिष्ठिर के साथ खड़े रहते हैं, तब वे केवल अनुज नहीं होते। वे एक प्रश्नचिन्ह की तरह युधिष्ठिर की सत्य-प्रवृत्ति के सामने उपस्थित होते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे अपने समय के सबसे बड़े उत्तरदाता कृष्ण के साथ होते हुए भी प्रश्न करना नहीं छोड़ते। वे शंका करते हैं, संवाद करते हैं, असहमत होते हैं। गीता का जन्म अर्जुन की इसी असहमति से होता है। और यही उन्हें विशिष्ट बनाता है—कि वे युद्ध में खड़े होकर भी विवेक का अवसर छोड़ते नहीं।
कितनी स्त्रियाँ अर्जुन के जीवन में आईं, और कितनी बार वे स्वयं स्त्रियों की पीड़ा के समीप आए। द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा—अर्जुन ने प्रेम किया, लेकिन उसमें संग्रह नहीं था। प्रत्येक नारी उनकी जीवन कथा में आई, और उन्हें अर्जुन के भीतर के किसी नए द्वार तक ले गई। सुभद्रा उन्हें कृष्ण के परिजनों में बाँधती है, उलूपी उन्हें नागलोक तक ले जाती है, चित्रांगदा उन्हें युद्ध और प्रेम के बीच का बिन्दु दिखाती है। और द्रौपदी? वह तो उनके हृदय का वह कोना है जहाँ आत्मग्लानि, सामूहिकता और स्वत्व का सबसे गहरा युद्ध हुआ।
द्रौपदी जब चीरहरण के समय कृष्ण को पुकारती हैं, तब अर्जुन की मौनता एक प्रतीक है। वे बोलते नहीं, लेकिन उनके भीतर कोई अग्नि अवश्य भभकती है। उसी अग्नि में पिघल कर एक प्रतिज्ञा जन्म लेती है, जो भीम की प्रतिज्ञा से अलग है। अर्जुन की प्रतिज्ञा न्याय की होती है, प्रतिशोध की नहीं। और यही न्याय उन्हें उस युद्ध तक ले जाता है जहाँ कौरवों के रक्त की धारों में उनका अपना रक्त बहता है।
अर्जुन की गाथा में समय स्थिर नहीं रहता। वे चलते हैं—और हर गति में एक ठहराव होता है। उनका रथ जितना तेजी से बढ़ता है, उतनी ही गहराई से वे अपने भीतर उतरते जाते हैं। यह एक दुर्लभ समानांतरता है—बाह्य वेग और आन्तरिक धैर्य का।
वे गुरु के शिष्य थे, पर जब गुरु ने एकलव्य का अंगूठा माँगा, तब अर्जुन मौन थे। यह मौन एक नैतिक थकान का संकेत था। क्या अर्जुन ने उस क्षण कुछ सोचा? क्या उन्होंने स्वयं को उस न्याय की छाया में खड़ा पाया जिसमें उन्हें श्रेष्ठता मिली पर किसी और का बलिदान हुआ? महाभारत यह नहीं कहता लेकिन अर्जुन की आँखों में वह क्षण कहीं संचित रहता है—और शायद इसी लिये वे बाद के जीवन में इतने अनिश्चित हो जाते हैं।
अश्वमेध यज्ञ के समय उनका रथ फिर से निकलता है लेकिन कृष्ण नहीं होते। यह अकेले अर्जुन का युद्ध होता है। उन्होंने सुना था कि राजा को यज्ञ में अश्व छोड़ना चाहिए—पर उन्हें तो अपने भीतर का अश्व भी बन्धन में लगता है। यज्ञ समाप्त होता है, लेकिन अर्जुन की आत्मा मुक्त नहीं होती।
जब कृष्ण देह छोड़ते हैं, तो अर्जुन टूटा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने जिस परम मित्र को युद्ध में सारथी बनाया था, वह अब समय की रेखा से पार चला गया है। अर्जुन की वह विवशता—जिसे उन्होंने समुद्र के तट पर वृद्धों और स्त्रियों की रक्षा न कर पाने के क्षण में जिया—वह उनके सम्पूर्ण तेज का अवसान नहीं थी, बल्कि उस तेज की अंतिम आलोचना थी।
अर्जुन के लिये जीवन कभी केवल जीवन नहीं रहा। वह एक प्रश्नावली थी। हर निर्णय में एक गहरी साँस, हर विजय में एक चुप्पी। और हर पराजय में एक मौन आकाश। अर्जुन का जीवन उन लोगों के लिये साक्ष्य है जो मानते हैं कि आत्मा का युद्ध बाहरी युद्धों से कहीं अधिक कठिन होता है।
वे अंतिम पलों में हिमालय की ओर बढ़ते हैं—पांडव एक-एक करके गिरते हैं, और अर्जुन भी। लेकिन यह गिरना पतन नहीं था—यह एक यात्रा थी पृथ्वी से आकाश की ओर, भीतर से शून्य की ओर।
वे युद्ध में वीर थे, लेकिन आत्मा में वे कवि थे। और यह काव्य कोई कविता नहीं, एक जीवन था—जिसमें शौर्य, करुणा, मोह, क्षमा और ज्ञान सभी ने अपने स्वरों को अर्जुन की बाँसुरी में ढाल दिया था।
अर्जुन का हृदय कोई युद्धभूमि नहीं, एक रंगभूमि थी। जहाँ प्रतिदिन कोई न कोई प्रश्न उठता और उत्तर देने से पूर्व अर्जुन उसमें उतरते थे। अर्जुन के भीतर जो घटित हुआ, वही महाभारत के बाहर घटित हुआ। वह युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, उससे पहले एक युद्ध अर्जुन ने अपनी चेतना में लड़ा था। उस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं था—सिर्फ दृष्टियाँ थीं, स्मृतियाँ थीं, और एक ऐसी करुणा जो बार-बार तर्कों को पिघलाती रही।
वे कोई देवता नहीं थे, इसलिए कृष्ण उनके सारथी बने। देवता को देवता की आवश्यकता नहीं होती। पर अर्जुन में जो मनुष्यत्व था, वही उन्हें कृष्ण के योग्य बनाता है। और कृष्ण? वे अर्जुन को अकेले छोड़ते नहीं, बल्कि उस स्थान तक ले जाते हैं जहाँ आत्मा स्वयं को पहचान सके। अर्जुन का समस्त जीवन इस पहचान की यात्रा था। वे खोज रहे थे अपने भीतर उस ‘स्व’ को जो न युद्ध से हारता है, न प्रेम से बहकता है।
कभी-कभी यह लगता है कि अर्जुन का अस्तित्व ही एक प्रश्न है। युधिष्ठिर की तरह स्थिर नहीं, भीम की तरह एकरेखीय नहीं, नकुल-सहदेव की तरह मौन नहीं—बल्कि अर्जुन की हर गति में एक घुमाव है, एक संशय, एक प्रतीक्षा। वे निर्णय लेते हैं, पर निर्णय से पूर्व ठहरते हैं। वे तीर चलाते हैं, लेकिन पहले अपने हृदय को सुनते हैं। यह विलम्ब ही उन्हें ‘अर्जुन’ बनाता है—एक ऐसा योद्धा जो युद्ध से अधिक उस क्षण को पहचानता है जब युद्ध से बाहर निकलना चाहिए।
वे सिर्फ तपस्वी नहीं थे, वे स्वयं के ऊपर शासन करने वाले एक मौन शासक थे। अर्जुन का जीवन जितना युद्धों में बसा है, उतना ही युद्ध से इंकार करने में भी। यही कारण है कि कृष्ण ने उन्हें ‘क्लैब्यं मा स्म गमः’ कहकर झकझोरा—क्योंकि अर्जुन हर भाव को पहले अनुभव करते हैं, फिर उसके उत्तर में उतरते हैं।
वे अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाते देखते हैं। और फिर लौटते हुए नहीं देखते। यह दृश्य ही अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मौन है। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध सिखाया, पर पूरा नहीं। यह अधूरापन अर्जुन की सबसे बड़ी थकान है। वे जीवन भर उस रिक्तता को भरने के लिये तीर चलाते रहे, लेकिन शायद अन्ततः समझ लिया कि पुत्र को सम्पूर्ण सिखाया नहीं जा सकता—और हर पिता को अंत में मौन ही होना पड़ता है।
वे बार-बार कृष्ण के पास लौटते हैं—कभी प्रश्न लेकर, कभी उत्तर पाने के बाद भी अंधकार के भय से। क्योंकि कृष्ण उनके लिए सिर्फ ईश्वर नहीं थे, वे आत्मा के निर्भीक स्वर थे। जब कृष्ण मुस्कराते हैं और अर्जुन काँपते हैं, तो वह केवल संवाद नहीं, एक परंपरा का जन्म है—जिसे हमने ‘गीता’ कहकर पुकारा।
महाभारत के पश्चात अर्जुन कोई उत्सव नहीं मनाते। वे विजेता हैं, पर विजय उनका आलंकार नहीं बनती। वे शान्त हो जाते हैं—एक ऐसी शान्ति जो सब कुछ जीत लेने के बाद आती है और फिर प्रश्न पूछती है: अब क्या? यही ‘अब क्या?’ अर्जुन की आत्मा की वह गहराई है जिसे समझना गीता के बाद ही सम्भव होता है।
हिमालय की ओर जाते हुए वे चुपचाप चलते हैं। न कोई जयघोष, न कोई अंतिम तीर। वह अर्जुन जो युद्धभूमि में कृष्ण के साथ था, अब शून्य में कृष्ण की अनुपस्थिति को समझ रहा है। और यही अनुपस्थिति सबसे बड़ा पाठ है। अर्जुन ने युद्ध जीता था, लेकिन ईश्वर को खोकर। और यह हानि इतनी नाजुक थी कि शब्द उसे सह नहीं सकते थे।
यदि अर्जुन की आत्मा में उतरना हो, तो महाभारत को नहीं, उसके बीच के मौन को पढ़ना होगा। जहाँ वे अकेले बैठकर अपने प्रियजनों के मुख देखते हैं, जहाँ वे अपने ही तीरों से घायल होते हैं, जहाँ वे जान जाते हैं कि धर्म कोई दिशा नहीं, एक अन्तःगति है।
वे जो शिष्य थे, वही गुरुओं से आगे निकल गये। वे जो योद्धा थे, उन्होंने युद्ध से उपर उठकर युद्ध का ही समाधान खोजा। वे जो पति थे, द्रौपदी के समानान्तर कभी दिखाई नहीं दिये, पर उनकी आँखों में जो मौन था, वह कहीं द्रौपदी की अग्नि को नमी देता रहा।
अर्जुन को किसी ने समझा नहीं—क्योंकि वे किसी परिभाषा में नहीं समाते। वे नायक भी हैं, और उन नायकों के मध्य भी हैं जिन्हें इतिहास याद नहीं रखता। वे न होने पर भी उपस्थित हैं—और यह उपस्थिति वही है जिसे कृष्ण ने महसूस किया और गीता दी।
जब वे रथ से उतरते हैं, और कृष्ण उसे मैदान से बाहर ले जाते हैं, तो रथ जल जाता है। यह दृश्य गहरा है। यह दिखाता है कि अर्जुन जो भी कर सके, वह कृष्ण की उपस्थिति के कारण था। उनके जाने के बाद रथ का मूल्य भी राख हो गया।
यह अर्जुन की सबसे गहन सीख है—कि शक्ति का स्रोत स्वयं नहीं, वह अनुपस्थित भी हो सकता है, और तब हम जान पाते हैं कि हम क्या नहीं हैं।
अर्जुन को केवल तीर चलाते हुए देखना, उन्हें अधूरा देखना है। वे तीर से कहीं ज़्यादा अपने हाथों की झिझक में, अपनी दृष्टि की भटकन में, और अपने मौन के कंपन में विद्यमान हैं। महाभारत उन्हें ‘किरात’ भी कहता है, ‘क्लांत’ भी। वे उस गाथा के नायक हैं जो अपने ही युद्ध को कई बार टाल देना चाहते थे। यह टालना किसी कायरता का नहीं, अपितु आत्मा की वह विवेकशीलता थी जो जानती है कि हर युद्ध की एक सही घड़ी होती है। अर्जुन ने अपने समय को पकड़ा, लेकिन अपने समय से कभी पूरी तरह सहमत नहीं हो सके।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्वयं को बार-बार प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करते हैं। वे अपने संदेहों से डरते नहीं। यही उन्हें महान बनाता है। वे कृष्ण को रोकते हैं, टोकते हैं, उलझते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ रहने वाले पहले ऐसे मनुष्य हैं जो ईश्वर को गुरु तो मानते हैं, पर आँख मूँदकर नहीं। वे उसकी आलोचना करते हैं, आग्रह करते हैं, विरोध करते हैं—और अन्ततः आत्मसमर्पण करते हैं। यह समर्पण अर्जुन की यात्रा का चरम बिन्दु है। न वह अंधभक्ति है, न विवशता—बल्कि आत्मा के सम्यक् बोध की परिणति।
युद्ध के अंतिम क्षणों में, जब सारे शस्त्र बिखर चुके थे, जब भीष्म शरशैय्या पर लेटे थे, जब द्रौपदी की आँखें प्रश्न बन चुकी थीं, और जब स्वयं कृष्ण भी अब मौन हो चुके थे—तब अर्जुन अकेले बचे थे। उस अकेलेपन में उनकी गाथा पुनः आरम्भ होती है। उन्होंने सब खो दिया—भाई, पुत्र, पत्नी, गुरु, रथ, तीर, और सबसे अंत में—कृष्ण। लेकिन वे रोते नहीं। वे कुछ भी नहीं कहते। बस धीरे-धीरे पृथ्वी से ऊपर की ओर चढ़ते हैं—हिमालय की ठंडी चुप्पी में, जहाँ कोई युद्ध नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई गीता नहीं—सिर्फ एक उत्तरहीन यात्रा है।
कृष्ण ने उन्हें गीता दी, लेकिन अर्जुन की मौनता वह भूमि थी जहाँ गीता का बीज अंकुरित हुआ। यदि अर्जुन न होते, तो गीता एक व्याख्यान होती—पर अर्जुन के कारण वह एक जीवित संवाद बनी। गीता की साक्षी में जो अर्जुन खड़ा है, वह केवल रथी नहीं है, वह भारतीय आत्मा का प्रतिनिधि है—जो युद्ध करता है, लेकिन युद्ध से डरता है; जो धर्म के लिये खड़ा होता है, पर धर्म को अंधत्व नहीं मानता; जो ईश्वर के साथ है, लेकिन अपने मानवत्व से बाहर नहीं जाता।
वे जितने संपूर्ण योद्धा थे, उतने ही अधूरे भी। और यह अधूरापन ही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य है। वे अपने भीतर एक रिक्तता के साथ जीते रहे—जिसे कभी अभिमन्यु की मृत्यु ने भरा, कभी द्रौपदी की पीड़ा ने, कभी अपने ही तीरों की गूंज ने। अर्जुन का जीवन एक ऐसी वीरता है जो कांपती हुई आती है, एक ऐसा निर्णय जो प्रश्नों से उपजा है, और एक ऐसी यात्रा जो अंततः मौन में समाप्त होती है।
अर्जुन को याद करना आत्मा के गहरे तल पर उतरना है। उनके चेहरे पर कोई दैवी प्रभा नहीं, कोई आलंकारिक तेज नहीं, बल्कि एक थका हुआ, सोचता हुआ, और लगातार पूछता हुआ मनुष्य है—जो कभी गांडीव उठाता है, कभी उसे त्याग देना चाहता है। अर्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वे किसी एक स्वरूप में स्थिर नहीं रहते। वे बहते हैं—और इसी प्रवाह में हम उन्हें पहचानते हैं।
कविता का वह क्षण जब शब्द चुप हो जाते हैं और अर्थ अपनी सबसे कोमल पीड़ा में प्रकट होता है—अर्जुन उस क्षण के नायक हैं। वे एक गीत हैं जिसे कृष्ण ने गाया, लेकिन जिसकी गूँज आज भी हमारे भीतर बजती है।
( पुस्तक : व्यास- उत्सव / परिचय दास )
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.