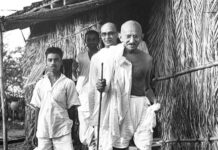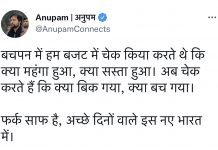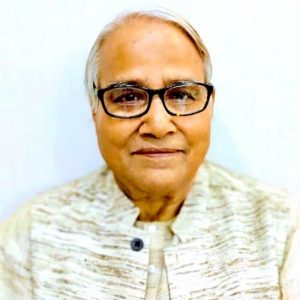
— सुज्ञान मोदी —
धर्मसाधना की प्रारंभिक प्रेरणा
गांधीजी को धर्म की प्राथमिक शिक्षा तो अपनी माता पुतलीबाई से ही मिली। कबा गांधी का परिवार तो वैष्णव वैश्यों का परिवार था, लेकिन माता पुतलीबाई का मायका परनामी या प्रणामी संप्रदाय को मानता था जो राम और रहीम में भेद नहीं करते थे। जो गीता और कुरान में भी भेद नहीं करते थे। फिर भी विवाह के बाद पुतलीबाई अपनी धार्मिक जिज्ञासाओं और दुविधाओं के समाधान के लिए जैन मुनियों की शरण में ही जाती थीं। बालक मोहनदास भी साथ जाते ही होंगे। तो शुरू में ही बालक मोहन पर धर्म के सार्वजनीन स्वरूप का प्रभाव पड़ा होगा।
रामचरितमानस की कथाओं से भी उनका परिचय बचपन में ही हो चुका था। राजा हरिश्चंद्र और श्रवणकुमार की कथाओं पर आधारित नाटकों का उनके बालमन पर बहुत प्रभाव हुआ था। 18 वर्ष के मोहनदास जब जातिगत-बंधनों से संघर्ष कर उच्च शिक्षा के लिए लंदन जा रहे थे, तो माता ने उनसे मांसाहार, मद्यपान और परस्त्रीगमन न करने का वचन लिया था। ऐसा माना जाता है कि जैन मुनि बेचरदास जी की सलाह पर माता ने उनसे ये वचन लिये थे। बाद में ऐसे अवसर आए जब युवा मोहनदास के लिए पापों में पड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन माता पुतलीबाई को दिए वचन ने उनके धर्म की रक्षा कर ली।
लंदन में जब वे शाकाहार का प्रचार करने वाली संस्था ‘वेजिटेरियन सोसायटी’ से जुड़े और उनकी पत्रिका के लिए भारत-विषयक लेख लिखना शुरू किया, तब उन्होंने भारत की धर्म-संस्कृति और तीज-त्यौहारों आदि के विषय में व्यवस्थित चिंतन और अध्ययन शुरू किया। मोहनदास गांधी वेजिटेरियन सोसायटी के सचिव थे और ब्रिटेन के मशहूर लेखक एडविन अर्नोल्ड इस संस्था के उप-सभापति थे। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन में अर्नोल्ड की गहरी रुचि थी और गौतम बुद्ध के जीवन पर उनकी लिखी पुस्तक ‘दी लाइट ऑफ एशिया’ तब तक दुनियाभर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अर्नोल्ड ने भगवद् गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसका नाम दिया था- ‘द सॉन्ग सेलेस्टियल’। तो भारतीय सनातन धारा के इन दो महान धर्मचिंतन से युवा मोहनदास का आरंभिक परिचय अर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद के जरिए ही हुआ। लेकिन अर्नोल्ड द्वारा वर्णित बुद्ध से ज्यादा भगवद्-गीता का उनपर विशेष प्रभाव पड़ा। गीता को मूल संस्कृत में पढ़ने में उनकी रुचि उत्पन्न हुई। उसी दौरान थियोसोफिस्टों से भी उनका लंदन में परिचय हुआ। इससे भारत की आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा के प्रति भी उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
लेकिन मोहनदास में किशोरावस्था से ही एक विशेष प्रवृत्ति देखी जा सकती थी और वह थी जीवन और जगत के सत्य को एक तटस्थ जिज्ञासु की तरह जानने और समझने की प्रवृत्ति। यही बात धर्म और अध्यात्म विषयक उनकी जिज्ञासाओं पर भी लागू होती है। इसलिए जब इंग्लैंड के सदाचारी ईसाइयों की संगति में वे आए तो ईसा के प्रेम, त्याग, बलिदान और क्षमा आदि के जीवन-संदेशों ने भी उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। इसके बाद तो कई मिशनरियों ने उनका धर्म-परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाने का भी असफल प्रयास जीवनभर किया। लेकिन जिन दो धर्मपुरुषों के अध्यात्म चिंतन ने उन्हें ईसाई संप्रदायार्थक रिलीजन और भारत की मुक्त धर्म परंपरा को ठीक से समझने में मदद की, वे थे ऋषितुल्य लियो टॉल्स्टॉय और तपस्वी श्रावक एवं सिद्ध श्रीमद् राजचंद्र।
लियो टॉल्स्टॉय और श्रीमद् राजचंद्र जैसे महान धर्मपुरुषों का प्रभाव
अपनी आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ में गांधीजी ने लिखा है –
“यद्यपि उस समय मैं अपनी दिशा स्पष्ट नहीं कर पाया था; यह भी नहीं कह सकता कि साधारणतः मुझे धर्म चर्चा में ही रस था; फिर भी रायचंद्र भाई की धर्म चर्चा रुचिपूर्वक सुनता था। उसके बाद मैं अनेक धर्माचार्यों के संपर्क में आया हूं। मैंने हरेक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है। पर मुझपर जो छाप रायचंद्र भाई ने डाली, वैसी दूसरा कोई न डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उसकी प्रामाणिकता के लिए मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि वे मुझे जान-बूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे और उनके मन में जो होगा वही कहेंगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था।”
इस अध्याय में आगे गांधीजी लिखते हैं- “यहां तो इतना ही कहना काफी होगा कि मेरे जीवन पर प्रभाव डालने वाले आधुनिक पुरुष तीन हैं : रायचंद्र भाई (श्रीमद् राजचंद्र) ने अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने ‘बैकुण्ठ तेरे हृदय में है’ (दी किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू) नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन (जॉन रस्किन) ने ‘अनटू दिस लास्ट’ नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया।”
तो आखिर इन धर्मपुरुषों का वह कौन सा धर्म-विचार था जिसने गांधीजी के धर्मचिंतन को इतना प्रभावित किया? टॉल्सटॉय ने ईसाइयत को संप्रदायमुक्त होकर शुद्ध धर्म के स्तर पर समझने की कोशिश की थी। उनपर बुद्ध और उपनिषदों के धर्मचिंतन का भी प्रभाव था। इसलिए उन्होंने ईसा की सिखावन को चर्च और बाइबिल के अंधविश्वासी शिकंजे से मुक्त करने की कोशिश की। उन्होंने वैराग्य धारण कर सीधे सत्यस्वरूप ईश्वर को समझने और आत्मसात करने की कोशिश की। इसलिए चर्च ने टॉल्स्टॉय को अलग-थलग करने की कोशिश की। उनकी इसी सत्यशोधी धर्मसाधना ने गांधीजी को प्रभावित किया। उनकी श्रमनिष्ठा और उनके वैराग्य ने गांधीजी के सामने इस युग के कर्मयोगी धर्मसाधक का नया ही स्वरूप सामने रखा।
श्रीमद् राजचंद्र जैन परंपरा के साधक थे, लेकिन उन्होंने सत्य धर्म के संप्रदायमुक्त स्वरूप को समझ लिया था। इसलिए गांधीजी भी मजहबों के बाड़े से मुक्त धर्ममात्र की साधना की ओर बढ़ चले। इस संबंध में गांधीजी ने लिखा है- “पुस्तकें पढ़ने और सार ग्रहण करने की शक्ति उनमें अपार थी…उन्होंने अनुवाद के द्वारा ‘कुरान’ और ‘जेंद अवेस्ता’ आदि का पठन भी कर लिया था।…रायचंद भाई के मन में अन्य धर्मों के प्रति अनादर का भाव नहीं था। वेदान्त के प्रति तो उनमें विशेष अनुराग भी था। वेदान्ती को कवि (श्रीमद्) वेदान्ती ही जान पड़ते थे। मेरे साथ चर्चा करते हुए उन्होंने मुझे कभी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए अमुक धर्म का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने मुझे मेरे आचार पर ही विचार करने के लिए कहा। मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने मेरी रुचि और मेरे बचपन के संस्कार को ध्यान में रखकर ‘गीता’ का अध्ययन करने के लिए कहा और प्रोत्साहित किया तथा दूसरी पुस्तकों में ‘पंचीकरण’, ‘मणिरत्नमाला’, ‘योगवाशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण’, ‘काव्य दोहन’ पहला भाग और ‘मोक्षमाला’ पढ़ने का सुझाव दिया।”
गांधीजी ने आगे लिखा है- “रायचंदभाई अकसर कहा करते थे कि धर्म तो बाड़ों की तरह हैं जिनमें मनुष्य कैद है। जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ माना है, उन्हें अपने भाल पर किसी धर्म का तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ‘…तुम चाहे जैसे भी रहो। जैसे-तैसे हरि को लहो।’ यह सूत्र जिस तरह अखाभगत का था, उसी तरह रायचंदभाई का भी था। धर्म के झगड़ों से उनका भी जी ऊब उठता था, वे उसमें शायद ही पड़ते थे। उन्होंने सब धर्मों के गुणों को अच्छी तरह देख लिया था और जो जिस धर्म का होता, वे उसके सामने उसी धर्म की खूबियां रखते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए मैंने उनके साथ जो पत्र-व्यवहार किया था उसमें से भी मैंने उनसे यही बात सीखी थी।”
सनातन धर्म रूपी भारत के उदात्त धार्मिक परंपरा के प्रवाह का हिस्सा ही हिंदू धर्म भी है ऐसा गांधीजी मानते थे। इस बारे में गांधीजी के विचार हमें 21 नवंबर 1947 के उनके प्रार्थना प्रवचन में मिलते हैं जहां वे कहते हैं –
ये सब इस वक्त के लिए योग्य सवाल हैं। मैं इतिहास का कोई बड़ा जानकार नहीं हूं। मैं विद्वान होने का दावा भी नहीं करता। मगर हिन्दुत्व पर लिखी हुई किसी प्रामाणिक किताब में मैंने पढ़ा है कि हिंदू शब्द वेदों में नहीं है। जब सिकन्दर महान ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की, तब सिंधु नदी के पूर्व के देश में रहने वाले लोग, जिसे अंग्रेजी दां हिंदुस्तानी ‘इंडस’ कहते हैं, हिंदू के नाम से पुकारे गए। सिंधु का ‘स’ ग्रीक भाषा में ‘ह’ हो गया। इस देश के रहने वालों का धर्म हिंदु धर्म कहलाया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है। इसने उन ईसाइयों को आसरा दिया जो विधर्मियों से सताये जाकर भागे थे। इसके सिवा इसने उन यहूदियों को जो बेनिइजराइल कहे जाते हैं, और पारसियों को भी आसरा दिया। मैं इस हिंदू धर्म का सदस्य होने में अभिमान महसूस करता हूं जिसमें सभी धर्म शामिल हैं और जो बड़ा सहनशील है। आर्य विद्वान वैदिक धर्म को मानते थे और हिंदुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था। वह फिर से आर्यावर्त कहलाये ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। (मेरी कल्पना का हिंदू-धर्म मेरे लिए अपने आप में पूर्ण है। बेशक उसमें वेद शामिल हैं, मगर उसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। यह कहने में मुझे कोई नामुनासिब बात नहीं मालूम होती कि हिंदू-धर्म की महत्ता को किसी भी तरह कम किये बगैर मैं मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी-धर्म में जो महत्ता है उसके प्रति हिंदू-धर्म के बराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं। ऐसा हिंदू-धर्म तब तक जिंदा रहेगा जब तक आकाश में सूरज चमकता है। इस बात को तुलसीदास ने एक दोहे में रख दिया है –
“दया धरम को मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िये, जब लगि घट में प्रान।।”
तो आखिर में तो यही समझ में आता है कि मत-संप्रदाय के रूप में हम धर्म का कुछ भी नाम रखें, असल धर्म तो गांधीजी की दृष्टि में और सभी संतों की दृष्टि में दया, क्षमा, सत्य, प्रेम और करुणा को जीवन व्यवहार में आत्मसात करना ही है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.